Manjit Thakur's Blog, page 9
March 23, 2020
कोराना ही नहीं, पहले भी तबाह किया है इंसानों को महामारियों ने
कोरोना यानी कोविड-19 से सारी दुनिया भयभीत है. इंसानी नस्ल की सबसे बड़ी दुश्मनों में संक्रामक बीमारियां रही हैं. भले ही, हम अभी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो पाए हैं कि कोविड-19 असल में, जैसा कि आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी दबे-छिपे जारी है, चीन या अमेरिका की किसी प्रयोगशाला में विकसित वायरस है या कुदरती आपदा, पर अब यह इंसानों को वैसे ही संक्रमित करके काल के गाल में समाने पर मजबूर कर रही है जैसे कभी काली मौत ने किया था.
पुराने जमाने में भी शोरगुल भरे बड़े व्यापारिक शहर रोगाणुओं का घर हुआ करते थे. ऐसे में एथेंस हो या कुस्तुनतुनिया (कॉन्सटेंटिनोपल) लोग इस अहसास के साथ ही जीते थे कि वे बीमार पड़कर अगरे हफ्ते मर सकते हैं. या उनको यह डर तो हमेशा बना रहता होगा कि कोई महामारी फैलेगी और उनका पूरा परिवार झटके में खत्म हो जाएगा.
 काली मौत से फैला मृत्यु का साम्राज्य फोटो सौजन्यः जेनेटिक लिटरेसी प्रोजेक्ट
काली मौत से फैला मृत्यु का साम्राज्य फोटो सौजन्यः जेनेटिक लिटरेसी प्रोजेक्ट
ऐसी महामारियों में सबसे मशहूर है काली मौत या ब्लैक डेथ. इसकी शुरुआत पूर्वी या मध्य एशिया में किसी जगह पर 1330 के दशक में हुई थी. तब, चूहों के शरीर पर रहने वाले पिस्सुओं में मौजूद यर्सीनिया पेस्टिस नाम के जीवाणु ने पिस्सुओं के काटे हुए लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया था. मध्य या पूर्वी एशिया से यह जीवाणु रेशम मार्ग से होता हुआ 1343 में यूरोप के क्रीमिया पहुंच गया था.
एशिया से चूहों और पिस्सुओं के जरिए यह महामारी पूरे एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में फैल गई थी. बीस साल से कम समय में यह अटलांटिक महासागर के तटों तक पहुंच गई. हालांकि, एशिया में यह प्लेग या काली मौत का दूसरा मामला था, पर यूरोप में यह पहली बार पहुंचा था और वहां इसने भयानक तबाही मचा दी.
इस काली मौत से 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे जो यूरेशिया की कुल आबादी का 25 फीसद से अधिक था. इंग्लैंड में हर दस में से चार लोग मारे गए थे और आबादी महामारी से पहले की 37 लाख से घटकर 22 लाख रह गई थी. युवाल नोरा हरारी की किताब होमो डेयस में इस मौत का आंकड़ा दिया गया है जिसके मुताबिक, "फ्लोरेंस शहर में एक लाख की आबादी में से 50 हजार लोग मारे गए."
एस्टिन अक्लोन की किताब ए पेस्ट इन द लैंडः न्यू वर्ल्ड एपिडेमिक्स इन अ ग्लोबल पर्सपैक्टिव में लिखा है, "यूरोप के कई देशों में 60 फीसद तक आबादी साफ हो गई थी." विश्व जनगणना का अनुमान लगाने वाली हिस्टोरिकल एस्टीमेट्स ऑफ वल्र्ड पॉप्युलेशन के मुताबिक, "चौदहवीं सदी में प्लेग की वजह से दुनिया की आबादी में काफी कमी आई थी. यह 47.5 करोड़ से घटकर 35 से 37.5 करोड़ के बीच रह गई थी. आबादी के लिहाज से अपने महामारी पूर्व की स्थिति में आने में यूरोप को 200 साल लग गए. फ्लोरेंस जैसे शहर तो 19वीं सदी में आकर उस पुरानी स्थिति में लौट पाए."
लेकिन काली मौत न तो अकेली ऐसी घटना थी और न ही वह इतिहास की सबसे ख़राब महामारी थी, सबसे ज़्यादा विनाशकारी महामारियों ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के टापुओं पर यूरोपीय लोगों के हमलों के बाद तांडव मचाया.
हरारी अपनी किताब में लिखते हैं, "5 मार्च, 1520 को जहाज़ों का एक छोटा बेड़ा क्यूबा के द्वीप से मैक्सिको के लिए रवाना हुआ. इनमें घोड़ों के साथ 900 स्पेनी सैनिक, तोपें और कुछ अफ्रीकी गुलाम भी थे. इनमें से एक गुलाम फ्रासिस्को दि एगिया अपनी देह पर कहीं अधिक घातक माल लादे था....चेचक का विषाणु."
फांसिस्को के मैक्सिको में उतने के बाद इस विषाणु ने उसके शरीर में तेजी से बढ़ना शुरू किया और उसके शरीर पर भयावह फुंसियां फूट पड़ी. बुखार में तपते फ्रांसिस्को को मैक्सिको में केम्पोआलान के एक अमेरिकी परिवार के घर पर रखा गया. नतीजतन, दस दिन में पूरा केम्पोआलान कब्रगाह में बदल गया.
उस समय वहां की माया सभ्यता के लोग वहां के तीन दुष्ट देवताओं की कारस्तानी मानते रहे. पुरोहितों से वैद्यों से परामर्श किया गया, प्रार्थना, शीतल स्नान, शरीर पर तारकोल चुपड़ने से लेकर तमाम उपाय अपनाए गए, पर फायदा नहीं हुआ. हजारों की संख्या में लाशें सड़कों पर सड़ती रहीं. शवों को दफनाने की हिम्मत किसी में नहीं थी. ऐसे में अधिकारियों ने आदेश दिया कि मकानों को शवों पर गिरा दिया जाए.
सन 1520 के सितंबर में महामारी मैक्सिको की घाटी में पहुंच गई और अक्तूबर में अज्टैक राजधानी तेनोचतित्लान में घुस गई जो ढाई लाख की आबादा वाला भव्य शहर था. दो महीनों के भीतर वहां के सम्राट समेत 35 फीसद आबादी खत्म हो गई. जहाजी बेड़े के मैक्सिको पहुंचने के छह महीने के भीतर सवा दो करोड़ आबादी वाले मैक्सिको में डेढ़ करोड़ से भी कम लोग जिंदा बचे. वजह था, चेचक. अगले कई दशकों तक चेचक का प्रकोप जारी रहा और उसके साथ फ्लू, खसरा और दूसरी संक्रामक महामारियों की वजह से 1580 तक मैक्सिको की आबादी महज 20 लाख रह गई.
इस घटना के दो सौ साल बाद, 19 जनवरी, 1778 को ब्रिटिश खोजी जेम्स कुक हवाई द्वीप पहुंचा. वहां की आबादी उस वक्त 5 लाख थी. उस समय तक वे लोग यूरोप और अमेरिका के संपर्क में नहीं आए थे. कुक के बेड़े की वजह से हवाई द्वीप पर फ्लू, टीबी, और सिफलिस जैसे रोग फैले. बाद में आए यूरोपियनों ने मोतीझरा और चेचक भी जोड़ दिए. और 1853 तक हवाई द्वीप की आबादी सिर्फ 70 हजार ही रह गई.
आज से सौ साल पहले 1918 में उत्तरी फ्रांस में जनवरी के महीने में खंदकों से एक खास तरह की बीमारी फैली जो सैनिकों में फैल रही थी और जिसका नाम स्पेनिश फ्लू रखा गया. पहले विश्वयुद्ध के दौरान वह मोर्चा एक नेटवर्क से जुड़ा था. ब्रिटेन अमेरिका भारत और ऑस्ट्रेलिया से लगातार आदमियों और रसद की आपूर्ति वहां की जा रही थी. पश्चिमी एशिया से तेल, अर्जेंटीना से अनाज और बीफ, मलाया से रबर, और कांगो से तांबा भेजा जा रहा था. बदले में उन सबको स्पेनिश फ्लू मिला. कुछ ही महीनों में आधा अरब लोग यानी दुनिया की उस समय की आबादी का करीबन 35 फीसद हिस्सा इस बिषाणु की चपेट में आ गए.
हरारी लिखते हैं, “भारत में तो स्पेनिश फ्लू से 5 प्रतिशत आबादी यानी डेढ़ करोड़ लोग मारे गए. ताहित द्वीप पर 14 फीसद लोग, सामोआ में 20 फीसद लोग मरे. कांगो की खदानों में हर पांच में से एक मजदूर मर गया. कुल मिलाकर एक साल के भीतर करीबन 10 करोड़ लोग मारे गए."
वैसे ध्यान रखने वाली बात है कि पहले विश्वयुद्ध के दौरान 1914 से 1918 के बीच 4 करोड़ लोग अलग से मरे.
पिछले कुछ सालों में भी हमने नए किस्म की महामारियां देखी हैं. 2002-03 में सार्स, 2005 में फ्लू, 2009-10 में स्वाइन फ्लू और 2014 में इबोला.
लेकिन सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 1000 से कम लोग मरे. पश्चिम अफ्रीका में शुरू हुआ इबोला शुरुआत में नियंत्रण से बाहर जाता लगा था और कुल 11000 लोग मारे गए.
वैसे एक महामारी ऐड्स भी रही, जिसकी वजह से 1980 के दशक से लेकर आजतक 3 करोड़ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. पर इन सबको हमने काबू कर लिया है.
आज कोरोना एक बड़े खतरे के रूप में पूरी मानवता के सामने आ उपस्थित हुआ है. अभी इसके इलाज के लिए दवाएं नहीं है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं. अभी इससे बचने के लिए कुछ बुनियादी स्वच्छता के उपाय ही एकमात्र तरीके हैं. सामाजिक दूरी और आइसोलेशन ही उपाय है.
उम्मीद है, कोरोना को हम रोक लेंगे.
***
पुराने जमाने में भी शोरगुल भरे बड़े व्यापारिक शहर रोगाणुओं का घर हुआ करते थे. ऐसे में एथेंस हो या कुस्तुनतुनिया (कॉन्सटेंटिनोपल) लोग इस अहसास के साथ ही जीते थे कि वे बीमार पड़कर अगरे हफ्ते मर सकते हैं. या उनको यह डर तो हमेशा बना रहता होगा कि कोई महामारी फैलेगी और उनका पूरा परिवार झटके में खत्म हो जाएगा.
 काली मौत से फैला मृत्यु का साम्राज्य फोटो सौजन्यः जेनेटिक लिटरेसी प्रोजेक्ट
काली मौत से फैला मृत्यु का साम्राज्य फोटो सौजन्यः जेनेटिक लिटरेसी प्रोजेक्टऐसी महामारियों में सबसे मशहूर है काली मौत या ब्लैक डेथ. इसकी शुरुआत पूर्वी या मध्य एशिया में किसी जगह पर 1330 के दशक में हुई थी. तब, चूहों के शरीर पर रहने वाले पिस्सुओं में मौजूद यर्सीनिया पेस्टिस नाम के जीवाणु ने पिस्सुओं के काटे हुए लोगों को संक्रमित करना शुरू कर दिया था. मध्य या पूर्वी एशिया से यह जीवाणु रेशम मार्ग से होता हुआ 1343 में यूरोप के क्रीमिया पहुंच गया था.
एशिया से चूहों और पिस्सुओं के जरिए यह महामारी पूरे एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में फैल गई थी. बीस साल से कम समय में यह अटलांटिक महासागर के तटों तक पहुंच गई. हालांकि, एशिया में यह प्लेग या काली मौत का दूसरा मामला था, पर यूरोप में यह पहली बार पहुंचा था और वहां इसने भयानक तबाही मचा दी.
इस काली मौत से 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे जो यूरेशिया की कुल आबादी का 25 फीसद से अधिक था. इंग्लैंड में हर दस में से चार लोग मारे गए थे और आबादी महामारी से पहले की 37 लाख से घटकर 22 लाख रह गई थी. युवाल नोरा हरारी की किताब होमो डेयस में इस मौत का आंकड़ा दिया गया है जिसके मुताबिक, "फ्लोरेंस शहर में एक लाख की आबादी में से 50 हजार लोग मारे गए."
एस्टिन अक्लोन की किताब ए पेस्ट इन द लैंडः न्यू वर्ल्ड एपिडेमिक्स इन अ ग्लोबल पर्सपैक्टिव में लिखा है, "यूरोप के कई देशों में 60 फीसद तक आबादी साफ हो गई थी." विश्व जनगणना का अनुमान लगाने वाली हिस्टोरिकल एस्टीमेट्स ऑफ वल्र्ड पॉप्युलेशन के मुताबिक, "चौदहवीं सदी में प्लेग की वजह से दुनिया की आबादी में काफी कमी आई थी. यह 47.5 करोड़ से घटकर 35 से 37.5 करोड़ के बीच रह गई थी. आबादी के लिहाज से अपने महामारी पूर्व की स्थिति में आने में यूरोप को 200 साल लग गए. फ्लोरेंस जैसे शहर तो 19वीं सदी में आकर उस पुरानी स्थिति में लौट पाए."
लेकिन काली मौत न तो अकेली ऐसी घटना थी और न ही वह इतिहास की सबसे ख़राब महामारी थी, सबसे ज़्यादा विनाशकारी महामारियों ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के टापुओं पर यूरोपीय लोगों के हमलों के बाद तांडव मचाया.
हरारी अपनी किताब में लिखते हैं, "5 मार्च, 1520 को जहाज़ों का एक छोटा बेड़ा क्यूबा के द्वीप से मैक्सिको के लिए रवाना हुआ. इनमें घोड़ों के साथ 900 स्पेनी सैनिक, तोपें और कुछ अफ्रीकी गुलाम भी थे. इनमें से एक गुलाम फ्रासिस्को दि एगिया अपनी देह पर कहीं अधिक घातक माल लादे था....चेचक का विषाणु."
फांसिस्को के मैक्सिको में उतने के बाद इस विषाणु ने उसके शरीर में तेजी से बढ़ना शुरू किया और उसके शरीर पर भयावह फुंसियां फूट पड़ी. बुखार में तपते फ्रांसिस्को को मैक्सिको में केम्पोआलान के एक अमेरिकी परिवार के घर पर रखा गया. नतीजतन, दस दिन में पूरा केम्पोआलान कब्रगाह में बदल गया.
उस समय वहां की माया सभ्यता के लोग वहां के तीन दुष्ट देवताओं की कारस्तानी मानते रहे. पुरोहितों से वैद्यों से परामर्श किया गया, प्रार्थना, शीतल स्नान, शरीर पर तारकोल चुपड़ने से लेकर तमाम उपाय अपनाए गए, पर फायदा नहीं हुआ. हजारों की संख्या में लाशें सड़कों पर सड़ती रहीं. शवों को दफनाने की हिम्मत किसी में नहीं थी. ऐसे में अधिकारियों ने आदेश दिया कि मकानों को शवों पर गिरा दिया जाए.
सन 1520 के सितंबर में महामारी मैक्सिको की घाटी में पहुंच गई और अक्तूबर में अज्टैक राजधानी तेनोचतित्लान में घुस गई जो ढाई लाख की आबादा वाला भव्य शहर था. दो महीनों के भीतर वहां के सम्राट समेत 35 फीसद आबादी खत्म हो गई. जहाजी बेड़े के मैक्सिको पहुंचने के छह महीने के भीतर सवा दो करोड़ आबादी वाले मैक्सिको में डेढ़ करोड़ से भी कम लोग जिंदा बचे. वजह था, चेचक. अगले कई दशकों तक चेचक का प्रकोप जारी रहा और उसके साथ फ्लू, खसरा और दूसरी संक्रामक महामारियों की वजह से 1580 तक मैक्सिको की आबादी महज 20 लाख रह गई.
इस घटना के दो सौ साल बाद, 19 जनवरी, 1778 को ब्रिटिश खोजी जेम्स कुक हवाई द्वीप पहुंचा. वहां की आबादी उस वक्त 5 लाख थी. उस समय तक वे लोग यूरोप और अमेरिका के संपर्क में नहीं आए थे. कुक के बेड़े की वजह से हवाई द्वीप पर फ्लू, टीबी, और सिफलिस जैसे रोग फैले. बाद में आए यूरोपियनों ने मोतीझरा और चेचक भी जोड़ दिए. और 1853 तक हवाई द्वीप की आबादी सिर्फ 70 हजार ही रह गई.
आज से सौ साल पहले 1918 में उत्तरी फ्रांस में जनवरी के महीने में खंदकों से एक खास तरह की बीमारी फैली जो सैनिकों में फैल रही थी और जिसका नाम स्पेनिश फ्लू रखा गया. पहले विश्वयुद्ध के दौरान वह मोर्चा एक नेटवर्क से जुड़ा था. ब्रिटेन अमेरिका भारत और ऑस्ट्रेलिया से लगातार आदमियों और रसद की आपूर्ति वहां की जा रही थी. पश्चिमी एशिया से तेल, अर्जेंटीना से अनाज और बीफ, मलाया से रबर, और कांगो से तांबा भेजा जा रहा था. बदले में उन सबको स्पेनिश फ्लू मिला. कुछ ही महीनों में आधा अरब लोग यानी दुनिया की उस समय की आबादी का करीबन 35 फीसद हिस्सा इस बिषाणु की चपेट में आ गए.
हरारी लिखते हैं, “भारत में तो स्पेनिश फ्लू से 5 प्रतिशत आबादी यानी डेढ़ करोड़ लोग मारे गए. ताहित द्वीप पर 14 फीसद लोग, सामोआ में 20 फीसद लोग मरे. कांगो की खदानों में हर पांच में से एक मजदूर मर गया. कुल मिलाकर एक साल के भीतर करीबन 10 करोड़ लोग मारे गए."
वैसे ध्यान रखने वाली बात है कि पहले विश्वयुद्ध के दौरान 1914 से 1918 के बीच 4 करोड़ लोग अलग से मरे.
पिछले कुछ सालों में भी हमने नए किस्म की महामारियां देखी हैं. 2002-03 में सार्स, 2005 में फ्लू, 2009-10 में स्वाइन फ्लू और 2014 में इबोला.
लेकिन सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 1000 से कम लोग मरे. पश्चिम अफ्रीका में शुरू हुआ इबोला शुरुआत में नियंत्रण से बाहर जाता लगा था और कुल 11000 लोग मारे गए.
वैसे एक महामारी ऐड्स भी रही, जिसकी वजह से 1980 के दशक से लेकर आजतक 3 करोड़ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. पर इन सबको हमने काबू कर लिया है.
आज कोरोना एक बड़े खतरे के रूप में पूरी मानवता के सामने आ उपस्थित हुआ है. अभी इसके इलाज के लिए दवाएं नहीं है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं. अभी इससे बचने के लिए कुछ बुनियादी स्वच्छता के उपाय ही एकमात्र तरीके हैं. सामाजिक दूरी और आइसोलेशन ही उपाय है.
उम्मीद है, कोरोना को हम रोक लेंगे.
***

Published on March 23, 2020 04:06
February 27, 2020
हवा को बांधने वाले उत्साही लड़के की कहानी द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड
द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड मलावी के एक ऐसे गांव को बचाने वाले लड़के की कहानी है जहां भुखमरी है और भयानक सूखा है. उम्दा अभिनय, शानदार पटकथा और बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी इस फिल्म में दर्शक को अंत तक बांधे रखती है. यह फिल्म एक राजनीतिक टिप्पणी भी है
कुछ फिल्मों को सिर्फ इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि उनमें एक ऐसा संदेश होता है, जो मुश्किल वक्त में भी इंसान को जिंदा रहने की वजहें देती हैं. लेकिन अगर किसी फिल्म में एक मजबूत और प्रेरणास्पद कथाक्रम के साथ ही, शानदार सिनेमैटोग्राफी और बेजोड़ संपादन और उम्दा अभिनय भी हो तो बात ही क्या!
किसी को पता नहीं था कि लेखक-निर्देशक चिवेटेल ज्योफोर अपने पहले ही शाहकार में ऐसा कमाल कर गुजरेंगे. ऐसी कहानी, जिसमें राजनीतिक टिप्पणी है, पर वह लाउड नहीं है, ऐसी कहानी जिसमें त्रासदी है, भूख है, पर वह इंसान को बेचारा साबित नहीं करती. बल्कि तमाम बाधाओं के बीच प्रतिभा के विस्फोट और संसाधन जुटाने की चतुराई के साथ एक पिता और पुत्र के पीड़ाओं के बीच एकदूसरे के साथ खड़े होने की कथा कहती है.
फिल्म में कमाल की किस्सागोई है जिसमें संवेदनशीलता और सहानुभूति दोनों भावनाएं गजब तरीके से पिरोई गई हैं. कहानी में प्रवाह है.
 फिल्म द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड का वीडियो ग्रैब
फिल्म द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड का वीडियो ग्रैब
असल में, ज्योफोर ने मलावी नाम के देश के एक इंजीनियर विलियम कंक्वाम्बा की असली कहानी को रूपहले परदे के लिए ढाला है और इस कहानी में परत दर परत आप गरीबी, सूखा, गृहयुद्ध और भुखमरी को उघड़ता देखते हैं. मलावी में कथित तौर पर लोकतंत्र आने के बाद राजनैतिक नेतृत्व का रवैया भी उधेड़ा गया है.
फिल्म की शुरुआत एक ऐसे लॉन्ग शॉट से होती है जहां हरी फसल के फोरग्राउंड में मलावी के आदिवासी कबीलों के पारंपरिक वेषभूषा में आते दिखते हैं. इनकी मेहमानवाजी कबीले के सरदार के जिम्मे है. अगले शॉट में मक्के की पकी फसल है जिसकी कटाई के दौरान ही नायक विलियम के दादाजी की मौत हो जाती है. गरीबी से जूझ रहे गांव में हर तरफ सूखा और गरीबी है और निर्देशक आहिस्ते से अपनी बात को शॉट्स के बेहतर संयोजन से बता जाते हैं. विलियम अपने गांव में रेडियो के लिए छोटे विंड टरबाइन के जरिए बिजली का इंतजाम करते हैं. यहां निर्देशक ज्योफोर थोड़ी रचनात्मक छूट लेते हैं, पर ज्योफोर की रचनात्मकता इस सृजनात्मक छूट का औचित्य साबित भी करती है, जो कहानी को दृश्यात्मक बनाने के लिहाज से जरूरी भी थी कि सूखे ग्रस्त गांव में कुआं सूखा नहीं था और उसका पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए बड़े पवनचक्की की जरूरत होती है.
हालांकि बड़ी पवनचक्की बनाने के वास्ते विलियम को अपने पिता की एकमात्र पूंजी साइकिल की जरूरत है. और यहीं नायक के साथ पिता के रिश्तों में तनाव आता है. पिता इस नए प्रयोग के लिए न जाने क्यों अपनी साइकिल देने से मना करता है और यह जाने क्यों पुत्र के साथ उसकी प्रतिस्पर्धी भावना है.
इस फिल्म में निर्देशक-लेखक ज्योफोर ने खुद ट्राइवेल (विलियम के पिता) का किरदार निभाया है. यह ऐसा चरित्र है जो एक किसान और पिता के तौर पर दहशत के साए में जीता है. उनके अभिनय में गजब की गहराई है. उनकी आंखों में उनका किरदार दिखता है. उनके पुत्र विलियम के किरदार में मैक्सवेल सिंबा हैं और वह इस फिल्म की जान हैं.
फ्रेम दर फ्रेम आप बगैर किसी संवाद से जबरिया सुझाए बिना जानते जाते हैं कि विलियम का यह गांव गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है. यहां भी जमीन के मालिकान जमीनों के सौदे करने की कोशिश करते हैं. सियासी लोग हमेशा की तरह सनकी, हिंसक और भ्रष्ट दिखाए गए हैं जो एक हद तक सही भी है.
इन सबके बीच विलियम के भीतर तकनीक को लेकर कुदरती रुझान है और स्कूली शिक्षा को सरकार की मदद के अभाव में स्कूल दर स्कूल बंद होते हैं और वहां विलियम स्कूल की लाइब्रेरी की मदद लेता है. वहीं एक किताब से उसे लगता है कि बिजली की मदद से वह गांव को बचा ले जाएगा.
सिंबा अपने अभिनय में परिपक्वता से उभरे हैं और वह बतौर अभिनेता कहीं भी ज्योफोर से उन्नीस नहीं बैठते. फिल्म में हर फ्रेम की लाइटिंग चटख है और आपको बांधे रखती है. सिनेमैटोग्राफर डिक पोप ने रंगों का खास खयाल रखा है.
यह फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर भारतीय दर्शकों के लिए उपलब्ध है. और पूरी फिल्म की कहानी में उतार-चढ़ाव के बीच, हालांकि आपको लगता है कि विलियम आखिर में कामयाब होंगे ही, पर साइकिल के पहिए की मदद से बनी पवनचक्की जब हवा के साथ तेज घूमती है तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और कुछेक सेकेंड के सिनेमैटिक साइलेंस के बाद जब कुएं पर लगा और विलियम के बनाए मोटर की पाइप से पानी आने लगता है तो फिल्म के किरदारों के साथ आपका मन में रोमांच में कूदने लग जाने का करने लगेगा.
इस फिल्म की यही कामयाबी है.
हिंसा, भूख, त्रासदियों के दौर में अ बॉय हू हार्नेस्ड द विंड सपने देखने और उन्हें साकार करने की गाथा है.
फिल्मः द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड
निर्देशकः चिवेटल ज्योफोर
कहानीः विलियम कम्कवम्बा
पटकथाः चिवेटल ज्योफोर
अभिनेताः मैक्सवेल सिंबा, चिवेटल ज्योफोर
***
कुछ फिल्मों को सिर्फ इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि उनमें एक ऐसा संदेश होता है, जो मुश्किल वक्त में भी इंसान को जिंदा रहने की वजहें देती हैं. लेकिन अगर किसी फिल्म में एक मजबूत और प्रेरणास्पद कथाक्रम के साथ ही, शानदार सिनेमैटोग्राफी और बेजोड़ संपादन और उम्दा अभिनय भी हो तो बात ही क्या!
किसी को पता नहीं था कि लेखक-निर्देशक चिवेटेल ज्योफोर अपने पहले ही शाहकार में ऐसा कमाल कर गुजरेंगे. ऐसी कहानी, जिसमें राजनीतिक टिप्पणी है, पर वह लाउड नहीं है, ऐसी कहानी जिसमें त्रासदी है, भूख है, पर वह इंसान को बेचारा साबित नहीं करती. बल्कि तमाम बाधाओं के बीच प्रतिभा के विस्फोट और संसाधन जुटाने की चतुराई के साथ एक पिता और पुत्र के पीड़ाओं के बीच एकदूसरे के साथ खड़े होने की कथा कहती है.
फिल्म में कमाल की किस्सागोई है जिसमें संवेदनशीलता और सहानुभूति दोनों भावनाएं गजब तरीके से पिरोई गई हैं. कहानी में प्रवाह है.
 फिल्म द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड का वीडियो ग्रैब
फिल्म द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड का वीडियो ग्रैबअसल में, ज्योफोर ने मलावी नाम के देश के एक इंजीनियर विलियम कंक्वाम्बा की असली कहानी को रूपहले परदे के लिए ढाला है और इस कहानी में परत दर परत आप गरीबी, सूखा, गृहयुद्ध और भुखमरी को उघड़ता देखते हैं. मलावी में कथित तौर पर लोकतंत्र आने के बाद राजनैतिक नेतृत्व का रवैया भी उधेड़ा गया है.
फिल्म की शुरुआत एक ऐसे लॉन्ग शॉट से होती है जहां हरी फसल के फोरग्राउंड में मलावी के आदिवासी कबीलों के पारंपरिक वेषभूषा में आते दिखते हैं. इनकी मेहमानवाजी कबीले के सरदार के जिम्मे है. अगले शॉट में मक्के की पकी फसल है जिसकी कटाई के दौरान ही नायक विलियम के दादाजी की मौत हो जाती है. गरीबी से जूझ रहे गांव में हर तरफ सूखा और गरीबी है और निर्देशक आहिस्ते से अपनी बात को शॉट्स के बेहतर संयोजन से बता जाते हैं. विलियम अपने गांव में रेडियो के लिए छोटे विंड टरबाइन के जरिए बिजली का इंतजाम करते हैं. यहां निर्देशक ज्योफोर थोड़ी रचनात्मक छूट लेते हैं, पर ज्योफोर की रचनात्मकता इस सृजनात्मक छूट का औचित्य साबित भी करती है, जो कहानी को दृश्यात्मक बनाने के लिहाज से जरूरी भी थी कि सूखे ग्रस्त गांव में कुआं सूखा नहीं था और उसका पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए बड़े पवनचक्की की जरूरत होती है.
हालांकि बड़ी पवनचक्की बनाने के वास्ते विलियम को अपने पिता की एकमात्र पूंजी साइकिल की जरूरत है. और यहीं नायक के साथ पिता के रिश्तों में तनाव आता है. पिता इस नए प्रयोग के लिए न जाने क्यों अपनी साइकिल देने से मना करता है और यह जाने क्यों पुत्र के साथ उसकी प्रतिस्पर्धी भावना है.
इस फिल्म में निर्देशक-लेखक ज्योफोर ने खुद ट्राइवेल (विलियम के पिता) का किरदार निभाया है. यह ऐसा चरित्र है जो एक किसान और पिता के तौर पर दहशत के साए में जीता है. उनके अभिनय में गजब की गहराई है. उनकी आंखों में उनका किरदार दिखता है. उनके पुत्र विलियम के किरदार में मैक्सवेल सिंबा हैं और वह इस फिल्म की जान हैं.
फ्रेम दर फ्रेम आप बगैर किसी संवाद से जबरिया सुझाए बिना जानते जाते हैं कि विलियम का यह गांव गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है. यहां भी जमीन के मालिकान जमीनों के सौदे करने की कोशिश करते हैं. सियासी लोग हमेशा की तरह सनकी, हिंसक और भ्रष्ट दिखाए गए हैं जो एक हद तक सही भी है.
इन सबके बीच विलियम के भीतर तकनीक को लेकर कुदरती रुझान है और स्कूली शिक्षा को सरकार की मदद के अभाव में स्कूल दर स्कूल बंद होते हैं और वहां विलियम स्कूल की लाइब्रेरी की मदद लेता है. वहीं एक किताब से उसे लगता है कि बिजली की मदद से वह गांव को बचा ले जाएगा.
सिंबा अपने अभिनय में परिपक्वता से उभरे हैं और वह बतौर अभिनेता कहीं भी ज्योफोर से उन्नीस नहीं बैठते. फिल्म में हर फ्रेम की लाइटिंग चटख है और आपको बांधे रखती है. सिनेमैटोग्राफर डिक पोप ने रंगों का खास खयाल रखा है.
यह फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर भारतीय दर्शकों के लिए उपलब्ध है. और पूरी फिल्म की कहानी में उतार-चढ़ाव के बीच, हालांकि आपको लगता है कि विलियम आखिर में कामयाब होंगे ही, पर साइकिल के पहिए की मदद से बनी पवनचक्की जब हवा के साथ तेज घूमती है तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और कुछेक सेकेंड के सिनेमैटिक साइलेंस के बाद जब कुएं पर लगा और विलियम के बनाए मोटर की पाइप से पानी आने लगता है तो फिल्म के किरदारों के साथ आपका मन में रोमांच में कूदने लग जाने का करने लगेगा.
इस फिल्म की यही कामयाबी है.
हिंसा, भूख, त्रासदियों के दौर में अ बॉय हू हार्नेस्ड द विंड सपने देखने और उन्हें साकार करने की गाथा है.
फिल्मः द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड
निर्देशकः चिवेटल ज्योफोर
कहानीः विलियम कम्कवम्बा
पटकथाः चिवेटल ज्योफोर
अभिनेताः मैक्सवेल सिंबा, चिवेटल ज्योफोर
***

Published on February 27, 2020 06:15
February 19, 2020
वनवास के बाद बाबूलाल मरांडी की घर वापसी से पांचों उंगली घी में
झारखंड में भाजपा को बाबूलाल मरांडी की और मरांडी को भाजपा की जरूरत थी. दोनों एकदूसरे के पूरक बनेंगे तो प्रदेश भाजपा को एक साफ-सुथरी छवि का आदिवासी नेता मिलेगा और मरांडी को अपने लिए मजबूत संगठन. 2009 से 2019 के लोकसभा तक, एक के बाद एक चार चुनाव हार चुके बाबूलाल मरांडी के लिए भाजपा में शामिल होना उनके सियासी करियर के लिहाज से संजीवनी की तरह है.
आखिरकार झारखंड (Jharkhand) के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का 14 साल का वनवास खत्म हो ही गया. मरांडी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में 'घर वापसी' हो गई. बाबूलाल खुद तो भाजपा में आए ही, अपने साथ-साथ वह पूरी पार्टी भी लेकर आए और उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) का भाजपा में विलय भी कर दिया. केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी को माला पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया. अब उम्मीद यह है कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश भाजपा में बड़ा पद दिया जा सकता है.
बाबूलाल मरांडी को भाजपा की जरूरत समझ में आती है पर सवाल यह है कि आखिर भाजपा को मरांडी की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? असल में, इन सवालों के उत्तर मार्च में संभावित राज्यसभा चुनावों में भी मिल सकते हैं. झाविमो के भाजपा में विलय से झारखंड की 2 सीटों में से भाजपा के लिए एक सीट जीतने की राह आसान हो गई है. बाबूलाल मरांडी के भाजपा में आने से यह संभावनाएं बनी हैं. 2014 में निर्विरोध जीते राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रेमचंद गुप्ता और निर्दलीय परिमल नथवाणी भले ही इस बार झारखंड से राज्यसभा में न जाएं, पर इस बार भी यह चुनाव निर्विरोध ही होने की उम्मीद है. जहां भाजपा की एक सीट तय मानी जाने लगी है. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की एक सीट पहले से पक्की है.
झामुमो सूत्र संकेत दे रहे हैं कि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को सीबीआई अदालत से राहत दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व सांसद संजीव कुमार को झामुमो फिर से राज्यसभा भेज सकता है.
असल में, प्रदेश भाजपा में इसे लेकर थोड़ी पेशोपेश की स्थिति है. नेतृत्व अभी यह तय नहीं कर पा रहा है कि दांव स्थानीय नेताओं पर लगाया जाए या किसी बाहरी को टिकट दिया जाए.
9 अप्रैल को राज्यसभा में झारखंड से दो सीटें खाली हो रही हैं. चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 28 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी. झामुमो के पास 30 विधायक हैं. बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने के बाद इस पार्टी की सदस्य संख्या 26 हो जाएगी. आजसू के दो विधायकों को मिला लें तो भाजपा समर्थक विधायकों की संख्या 28 हो जाती है. वैसे भाजपा का दावा है कि दो निर्दलीय विधायक भी उनके संपर्क में हैं. इन्हें मिला लें तो भाजपा 30 तक पहुंच जाती है. इस प्रकार झामुमो-भाजपा अपने-अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकते हैं.
अब बात, बाबूलाल मरांडी के भाजपा में आऩे की. असल में, मरांडी को अपने सियासी करियर का अस्तितिव बचाए रखने के लिए आज न कल यह कदम तो उठाना ही था.
झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तो पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी. तब भाजपा के वे झारखंड के कद्दावर नेता माने जाते थे. पर 28 महीनों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद गुटबाजी की वजह से उन्हें कुरसी छोड़नी पड़ी थी और उनकी जगह अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया था. तब से यह टीस उनके मन में पैठी हुई थी. 2006 में उन्होंने गुटबाजी का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी और तभी से उनके सियासी करियर पर ग्रहण लगना शुरू हो गया. लगातार दस साल तक, यानी 2009 के बाद 2019 तक बाबूलाल मरांडी कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे. उनकी किस्मत ने उनका साथ एक दशक बाद 2019 के विधानसभा चुनावों में दिया, जब वह धनवार से जीते.
2009 से 2019 लोकसभा चुनाव तक, मरांडी लगातार चार चुनाव हार चुके थे. 2009 में वे कोडरमा से सांसद चुने गये थे. कोडरमा से 2004 और 2006 के उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंचे थे. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे दुमका चले गये जहां शिबू सोरेन ने उन्हें हरा दिया था.
2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने धनवार और गिरिडीह से परचा दाखिल किया था पर दोनों ही जगह से उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था. 2014 के बाद उनकी पार्टी के छह विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो गए थे. इससे उनकी पार्टी और छवि दोनों को गहरा धक्का लगा था. लगातार चुनाव हारने से भी मरांडी की छवि कमजोर नेता के तौर पर बनती जा रही थी और यह साफ दिखने लगा था कि अब बाबूलाल मरांडी वह नेता नहीं रहे जो झारखंड स्थापना के वक्त थे.
2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोडरमा से फिर से किस्मत आजमाई पर भाजपा की अन्नपूर्णा देवी ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी. और इस बार यानी 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भी उनके लिए मुकाबला कोई बहुत आसान नहीं रहा, पर आखिरकार वह जीत गए.
अब, 2014 में मिले सबक को याद रखकर, जब उनके 8 जीते विधायकों में से 6 भाजपा में मिल गए थे, मरांडी ने हर कदम फूंक-फूंककर रखा. उनकी पार्टी के टिकट पर जीते 3 विधायकों में से पहले उन्होंने बंधु तिर्की को पार्टी से बाहर किया और फिर प्रदीप यादव को. तिर्की तो कांग्रेस में शामिल हो गए पर प्रदीप यादव को लेकर खुद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है. प्रदेश कांग्रेस के एक कार्यकारी अध्य़क्ष डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है. वह यादव को पार्टी में नहीं आऩे देने को लेकर कमर कसे हुए हैं.
बहरहाल, अपने दोनों विधायकों से छुट्टी पाने के बाद मरांडी भाजपा में आए हैं, क्योंकि अब विलय के बाद उन पर दल-बदल कानून प्रभावी नहीं रहेगा. और यह भी तय है कि मरांडी को पार्टी कोई प्रतिष्ठित पद देगी. इसकी एक वजह यह भी रही कि खुद अमित शाह बाबूलाल मरांडी को पसंद करते हैं और मरांडी की पृष्ठभूमि भी संघ के प्रचारक की रही है. मरांडी भाजपा में आने को कितने आतुर थे इसकी झलक उनके इस बयान से भी मिलती है कि वह भाजपा दफ्तर में झाड़ू लगाने को भी तैयार हैं.
सीधे-सादे राजनीतिज्ञ के रूप में छवि बनाए मरांडी को भाजपा में वाकई पद भी मिलेगी और प्रतिष्ठा भी, पर उनकी पार्टी में यह असमंजस है कि उनके पार्टी पदाधिकारियों के हिस्से में क्या आएगा?

आखिरकार झारखंड (Jharkhand) के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का 14 साल का वनवास खत्म हो ही गया. मरांडी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में 'घर वापसी' हो गई. बाबूलाल खुद तो भाजपा में आए ही, अपने साथ-साथ वह पूरी पार्टी भी लेकर आए और उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) का भाजपा में विलय भी कर दिया. केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी को माला पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया. अब उम्मीद यह है कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश भाजपा में बड़ा पद दिया जा सकता है.
बाबूलाल मरांडी को भाजपा की जरूरत समझ में आती है पर सवाल यह है कि आखिर भाजपा को मरांडी की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? असल में, इन सवालों के उत्तर मार्च में संभावित राज्यसभा चुनावों में भी मिल सकते हैं. झाविमो के भाजपा में विलय से झारखंड की 2 सीटों में से भाजपा के लिए एक सीट जीतने की राह आसान हो गई है. बाबूलाल मरांडी के भाजपा में आने से यह संभावनाएं बनी हैं. 2014 में निर्विरोध जीते राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रेमचंद गुप्ता और निर्दलीय परिमल नथवाणी भले ही इस बार झारखंड से राज्यसभा में न जाएं, पर इस बार भी यह चुनाव निर्विरोध ही होने की उम्मीद है. जहां भाजपा की एक सीट तय मानी जाने लगी है. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की एक सीट पहले से पक्की है.
झामुमो सूत्र संकेत दे रहे हैं कि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को सीबीआई अदालत से राहत दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व सांसद संजीव कुमार को झामुमो फिर से राज्यसभा भेज सकता है.
असल में, प्रदेश भाजपा में इसे लेकर थोड़ी पेशोपेश की स्थिति है. नेतृत्व अभी यह तय नहीं कर पा रहा है कि दांव स्थानीय नेताओं पर लगाया जाए या किसी बाहरी को टिकट दिया जाए.
9 अप्रैल को राज्यसभा में झारखंड से दो सीटें खाली हो रही हैं. चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 28 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी. झामुमो के पास 30 विधायक हैं. बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने के बाद इस पार्टी की सदस्य संख्या 26 हो जाएगी. आजसू के दो विधायकों को मिला लें तो भाजपा समर्थक विधायकों की संख्या 28 हो जाती है. वैसे भाजपा का दावा है कि दो निर्दलीय विधायक भी उनके संपर्क में हैं. इन्हें मिला लें तो भाजपा 30 तक पहुंच जाती है. इस प्रकार झामुमो-भाजपा अपने-अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज सकते हैं.
अब बात, बाबूलाल मरांडी के भाजपा में आऩे की. असल में, मरांडी को अपने सियासी करियर का अस्तितिव बचाए रखने के लिए आज न कल यह कदम तो उठाना ही था.
झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तो पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी. तब भाजपा के वे झारखंड के कद्दावर नेता माने जाते थे. पर 28 महीनों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद गुटबाजी की वजह से उन्हें कुरसी छोड़नी पड़ी थी और उनकी जगह अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया था. तब से यह टीस उनके मन में पैठी हुई थी. 2006 में उन्होंने गुटबाजी का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी और तभी से उनके सियासी करियर पर ग्रहण लगना शुरू हो गया. लगातार दस साल तक, यानी 2009 के बाद 2019 तक बाबूलाल मरांडी कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे. उनकी किस्मत ने उनका साथ एक दशक बाद 2019 के विधानसभा चुनावों में दिया, जब वह धनवार से जीते.
2009 से 2019 लोकसभा चुनाव तक, मरांडी लगातार चार चुनाव हार चुके थे. 2009 में वे कोडरमा से सांसद चुने गये थे. कोडरमा से 2004 और 2006 के उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंचे थे. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे दुमका चले गये जहां शिबू सोरेन ने उन्हें हरा दिया था.
2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने धनवार और गिरिडीह से परचा दाखिल किया था पर दोनों ही जगह से उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था. 2014 के बाद उनकी पार्टी के छह विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो गए थे. इससे उनकी पार्टी और छवि दोनों को गहरा धक्का लगा था. लगातार चुनाव हारने से भी मरांडी की छवि कमजोर नेता के तौर पर बनती जा रही थी और यह साफ दिखने लगा था कि अब बाबूलाल मरांडी वह नेता नहीं रहे जो झारखंड स्थापना के वक्त थे.
2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोडरमा से फिर से किस्मत आजमाई पर भाजपा की अन्नपूर्णा देवी ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी. और इस बार यानी 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भी उनके लिए मुकाबला कोई बहुत आसान नहीं रहा, पर आखिरकार वह जीत गए.
अब, 2014 में मिले सबक को याद रखकर, जब उनके 8 जीते विधायकों में से 6 भाजपा में मिल गए थे, मरांडी ने हर कदम फूंक-फूंककर रखा. उनकी पार्टी के टिकट पर जीते 3 विधायकों में से पहले उन्होंने बंधु तिर्की को पार्टी से बाहर किया और फिर प्रदीप यादव को. तिर्की तो कांग्रेस में शामिल हो गए पर प्रदीप यादव को लेकर खुद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है. प्रदेश कांग्रेस के एक कार्यकारी अध्य़क्ष डॉ. इरफान अंसारी ने इस प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है. वह यादव को पार्टी में नहीं आऩे देने को लेकर कमर कसे हुए हैं.
बहरहाल, अपने दोनों विधायकों से छुट्टी पाने के बाद मरांडी भाजपा में आए हैं, क्योंकि अब विलय के बाद उन पर दल-बदल कानून प्रभावी नहीं रहेगा. और यह भी तय है कि मरांडी को पार्टी कोई प्रतिष्ठित पद देगी. इसकी एक वजह यह भी रही कि खुद अमित शाह बाबूलाल मरांडी को पसंद करते हैं और मरांडी की पृष्ठभूमि भी संघ के प्रचारक की रही है. मरांडी भाजपा में आने को कितने आतुर थे इसकी झलक उनके इस बयान से भी मिलती है कि वह भाजपा दफ्तर में झाड़ू लगाने को भी तैयार हैं.
सीधे-सादे राजनीतिज्ञ के रूप में छवि बनाए मरांडी को भाजपा में वाकई पद भी मिलेगी और प्रतिष्ठा भी, पर उनकी पार्टी में यह असमंजस है कि उनके पार्टी पदाधिकारियों के हिस्से में क्या आएगा?

Published on February 19, 2020 00:55
February 16, 2020
देश का मिजाज सर्वेक्षण पर आजतक रेडियो पर मेरा साप्ताहिक शोः एपिसोड एक
देश का मिजाज सर्वेक्षण
आजतक रेडियो पर मेरा साप्ताहिक शोः एपिसोड एक
नरेंद्र मोदी के लिए उनके नेतृत्व पर धारणाएं कभी इस कदर बंटी नहीं रहीं, जितनी आज हैं. सात महीने पहले ही तो प्रधानमंत्री को बेजोड़ बताया गया और ऐसा माना गया था कि वे कोई चूक नहीं कर सकते. उन्होंने मई 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ऐसी जीत दिलाई कि विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया और वे इंदिरा गांधी के बाद, लोकसभा में लगातार दो बार अपनी पार्टी को बहुमत दिलाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने. इंदिरा गांधी ने 1967 और 1971 के चुनावों में बहुमत हासिल किया था. अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मोदी ने 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को दुगुना करके उसे पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का काफी ऊंचा लक्ष्य रखा. अगस्त में, उन्होंने अनुच्छेद 370 को बेमानी बनाकर जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निर्णायक तौर पर खत्म कर दिया.
आजतक रेडियो पर सुनिए मेरा खास कार्यक्रम देश का मिजाज सर्वेक्षण मेंः कार्यक्रम सुनने के लिए नीचे के लिंक पर चटका लगाएं
देश का मूड किस नेता के साथ
आजतक रेडियो पर मेरा साप्ताहिक शोः एपिसोड एक
नरेंद्र मोदी के लिए उनके नेतृत्व पर धारणाएं कभी इस कदर बंटी नहीं रहीं, जितनी आज हैं. सात महीने पहले ही तो प्रधानमंत्री को बेजोड़ बताया गया और ऐसा माना गया था कि वे कोई चूक नहीं कर सकते. उन्होंने मई 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ऐसी जीत दिलाई कि विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया और वे इंदिरा गांधी के बाद, लोकसभा में लगातार दो बार अपनी पार्टी को बहुमत दिलाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने. इंदिरा गांधी ने 1967 और 1971 के चुनावों में बहुमत हासिल किया था. अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मोदी ने 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को दुगुना करके उसे पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का काफी ऊंचा लक्ष्य रखा. अगस्त में, उन्होंने अनुच्छेद 370 को बेमानी बनाकर जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निर्णायक तौर पर खत्म कर दिया.
आजतक रेडियो पर सुनिए मेरा खास कार्यक्रम देश का मिजाज सर्वेक्षण मेंः कार्यक्रम सुनने के लिए नीचे के लिंक पर चटका लगाएं
देश का मूड किस नेता के साथ

Published on February 16, 2020 23:32
पुस्तक समीक्षाः बुढ़ापे में जीवन प्रबंधन की उम्दा गाइड
अगले एक दशक में भारत में बुजुर्गों की संख्या आज से कहीं अधिक होने लगेगी. न्यक्लियर परिवारों की वजह से समाज में बुुजर्गों का दखल कम हुआ है ऐसे में बीमारियों और तमाम दुश्वारियों के प्रबंधन सुझाने के लिहाज से एम्स के डॉ. प्रसून चटर्जी की किताब उम्दा गाइड सरीखी है
बुढ़ापे के बारे में कहा गया कि जीवन संध्या में आकर इंसान खुद बच्चा हो जाता है और उसे बच्चों जैसी ही देखभाल की जरूरत होती है. और अमूमन बुजुर्गों को भारतीय समाज में धर्म-कर्म-ईमान की तरफ मोड़ दिया जाता है. ऐसे में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के गेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग (ऐसी दवाइयां जो बुढापे से जुड़ी हों) के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने एक उम्दा किताब लिखी है, जिसका नाम है हेल्थ ऐंड वेल बीइंग इन लेट लाइफः पर्सपैक्टिव्स ऐंड नैरेटिव्स फ्रॉम इंडिया.
सबकी बड़ी बात कि यह किताब ओपन एक्सेस है. किताब पर मूल्य अंकित नहीं है और यही बात इस किताब के प्रकाशन को अमूल्य बनाती है. डॉ. प्रसून चटर्जी की किताब का कवर. फोटोः मंजीत ठाकुर
डॉ. प्रसून चटर्जी की किताब का कवर. फोटोः मंजीत ठाकुर
वैसे सचाई यही है कि बढ़ती उम्र को आगे बढ़ते जाने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे खूबसूरत और स्वस्थ जरूर बनाया जा सकता है. एम्स, दिल्ली के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने अपनी पुस्तक में बताया है कि कैसे आप वृद्धावस्था में प्रसन्न रह सकते हैं. इस किताब में कई कहानियां हैं जो कि प्रेरणा से भरपूर है.
डॉ. चटर्जी की किताब हेल्थ ऐंड वेल बीइंग इन लेटलाइफः पर्सेपेक्टिव्स ऐंड नैरेटिव्स फ्रॉम इंडिया में इस बात का उल्लेख किया है कि कैसे आप अपने जीवन को सक्रियता से भर सकते हैं. इस किताब में ऐसे किस्से हैं जिन्हें पढ़कर आप खुद को उससे जोड़ पाएंगे. इन कहानियों के किरदार ऐसे हैं जो अपनी शारीरिक एवं सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं. इस किताब में कुल दस अध्याय हैं.
किताब के ये दस अध्यायों में पहला फ्रैलिटी पर है. यानी बढ़ती उम्र के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से आ रहे ढलान पर. डॉ. चटर्जी विस्तार से बताते हैं कि इससे निबटा कैसे जाए. इसके साथ ही, भूलने की आदत और यादद्धाश्त का कम होते जाने जैसे बुढ़ापे के सामान्य मर्ज पर एक पूरा अध्याय है.
अगर आपको बुढ़ापे में कब्ज पर बने पीकू जैसी फिल्म की याद है तो एक पूरा अध्याय कब्ज की समस्या पर है. इसके साथ ही, कैंसर और स्ट्रोक जैसे वृद्धावस्था के तमाम पहलुओं पर बात की गई है. लेखक ने कई तरह की भ्रांतियों को भी दूर करने की कोशिश की है जैसे वृद्धावस्था का दूसरा नाम संन्यास नहीं है. साथ ही किताब में यह भी बताया गया है कि बढ़ती उम्र में उन्हें कब और किन चीज़ों का इलाज कराना चाहिए, और कब नहीं.
किताब का आठवां अध्याय यौन स्वास्थ्य पर आधारित है. यह एक ऐसी समस्या है जिसमें पूरे उप-महाद्वीप में बातचीत से बचा जाता है. ऐसे में यह किताब एक जरूरी किताब बन जाती है.
वैसे डॉ. चटर्जी की यह किताब उनकी कई पहलों का एक पहलू भर है. वह समाज को बेहतर बनाने की जिद के चलते नित नए-नए प्रयोग करते रहते हैं. उनकी ही प्रेरणा से नोएडा के सेक्टर-12 के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंटर जनरेशनल लर्निंग सेंटर (आइजीएलसी) इस मुहिम को साकार रूप देने में लगा है. उनके इस संकल्प को आगे बढ़ाने में सरकारी सेवा से रिटायर हुए कुछ लोग भी शामिल हैं.
जाहिर है, भारत में जहां जीवन-संध्या में आकर लोग हिम्मत हारने लगते हैं वहां यह किताब एक रोशनी की तरह काम करेगी. खासकर यह और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगले एक दशक में हम अपने डिमोग्राफिक डिविडेंड में से बुढाते हुए लोगों की बढ़ती संख्या देखेंगे. समाज में जिस तरह से न्यूक्लियर परिवारों का चलन बढ़ा है और परिवार नाम की संस्था में बुजुर्गों का दखल कम हुआ है, ऐसे में यह किताब मौजूदा बुजुर्गों और भावी बुजुर्गों के लिए बेहतरीन साबित होगी. फिलहाल, यह किताब अंग्रेजी में है और इसका हिंदी संस्करण अधिक लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचा सकेगा.किताबः हेल्थ ऐंड वेल बीइंग इन लेट लाइफः पर्सपेक्टिव्स ऐंड नैरेटिव्स फ्रॉम इंडिया
लेखकः डॉ. प्रसून चटर्जी
कीमतः ओपन एक्सेस (कीमत का उल्लेख नहीं)
प्रकाशकः स्प्रींगर ओपन
***
बुढ़ापे के बारे में कहा गया कि जीवन संध्या में आकर इंसान खुद बच्चा हो जाता है और उसे बच्चों जैसी ही देखभाल की जरूरत होती है. और अमूमन बुजुर्गों को भारतीय समाज में धर्म-कर्म-ईमान की तरफ मोड़ दिया जाता है. ऐसे में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के गेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग (ऐसी दवाइयां जो बुढापे से जुड़ी हों) के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने एक उम्दा किताब लिखी है, जिसका नाम है हेल्थ ऐंड वेल बीइंग इन लेट लाइफः पर्सपैक्टिव्स ऐंड नैरेटिव्स फ्रॉम इंडिया.
सबकी बड़ी बात कि यह किताब ओपन एक्सेस है. किताब पर मूल्य अंकित नहीं है और यही बात इस किताब के प्रकाशन को अमूल्य बनाती है.
 डॉ. प्रसून चटर्जी की किताब का कवर. फोटोः मंजीत ठाकुर
डॉ. प्रसून चटर्जी की किताब का कवर. फोटोः मंजीत ठाकुरवैसे सचाई यही है कि बढ़ती उम्र को आगे बढ़ते जाने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे खूबसूरत और स्वस्थ जरूर बनाया जा सकता है. एम्स, दिल्ली के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने अपनी पुस्तक में बताया है कि कैसे आप वृद्धावस्था में प्रसन्न रह सकते हैं. इस किताब में कई कहानियां हैं जो कि प्रेरणा से भरपूर है.
डॉ. चटर्जी की किताब हेल्थ ऐंड वेल बीइंग इन लेटलाइफः पर्सेपेक्टिव्स ऐंड नैरेटिव्स फ्रॉम इंडिया में इस बात का उल्लेख किया है कि कैसे आप अपने जीवन को सक्रियता से भर सकते हैं. इस किताब में ऐसे किस्से हैं जिन्हें पढ़कर आप खुद को उससे जोड़ पाएंगे. इन कहानियों के किरदार ऐसे हैं जो अपनी शारीरिक एवं सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं. इस किताब में कुल दस अध्याय हैं.
किताब के ये दस अध्यायों में पहला फ्रैलिटी पर है. यानी बढ़ती उम्र के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से आ रहे ढलान पर. डॉ. चटर्जी विस्तार से बताते हैं कि इससे निबटा कैसे जाए. इसके साथ ही, भूलने की आदत और यादद्धाश्त का कम होते जाने जैसे बुढ़ापे के सामान्य मर्ज पर एक पूरा अध्याय है.
अगर आपको बुढ़ापे में कब्ज पर बने पीकू जैसी फिल्म की याद है तो एक पूरा अध्याय कब्ज की समस्या पर है. इसके साथ ही, कैंसर और स्ट्रोक जैसे वृद्धावस्था के तमाम पहलुओं पर बात की गई है. लेखक ने कई तरह की भ्रांतियों को भी दूर करने की कोशिश की है जैसे वृद्धावस्था का दूसरा नाम संन्यास नहीं है. साथ ही किताब में यह भी बताया गया है कि बढ़ती उम्र में उन्हें कब और किन चीज़ों का इलाज कराना चाहिए, और कब नहीं.
किताब का आठवां अध्याय यौन स्वास्थ्य पर आधारित है. यह एक ऐसी समस्या है जिसमें पूरे उप-महाद्वीप में बातचीत से बचा जाता है. ऐसे में यह किताब एक जरूरी किताब बन जाती है.
वैसे डॉ. चटर्जी की यह किताब उनकी कई पहलों का एक पहलू भर है. वह समाज को बेहतर बनाने की जिद के चलते नित नए-नए प्रयोग करते रहते हैं. उनकी ही प्रेरणा से नोएडा के सेक्टर-12 के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंटर जनरेशनल लर्निंग सेंटर (आइजीएलसी) इस मुहिम को साकार रूप देने में लगा है. उनके इस संकल्प को आगे बढ़ाने में सरकारी सेवा से रिटायर हुए कुछ लोग भी शामिल हैं.
जाहिर है, भारत में जहां जीवन-संध्या में आकर लोग हिम्मत हारने लगते हैं वहां यह किताब एक रोशनी की तरह काम करेगी. खासकर यह और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगले एक दशक में हम अपने डिमोग्राफिक डिविडेंड में से बुढाते हुए लोगों की बढ़ती संख्या देखेंगे. समाज में जिस तरह से न्यूक्लियर परिवारों का चलन बढ़ा है और परिवार नाम की संस्था में बुजुर्गों का दखल कम हुआ है, ऐसे में यह किताब मौजूदा बुजुर्गों और भावी बुजुर्गों के लिए बेहतरीन साबित होगी. फिलहाल, यह किताब अंग्रेजी में है और इसका हिंदी संस्करण अधिक लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचा सकेगा.किताबः हेल्थ ऐंड वेल बीइंग इन लेट लाइफः पर्सपेक्टिव्स ऐंड नैरेटिव्स फ्रॉम इंडिया
लेखकः डॉ. प्रसून चटर्जी
कीमतः ओपन एक्सेस (कीमत का उल्लेख नहीं)
प्रकाशकः स्प्रींगर ओपन
***

Published on February 16, 2020 23:26
February 14, 2020
नदीसूत्रः मुंबई की मीठी नदी का कड़वा वर्तमान और जहरीला भविष्य
मायानगरी मुंबई कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर आरे के जंगल बचाने जाग गई थी. पर शहर के लोगों ने एक मरती हुई नदी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया. मुंबई ने एक नदी को मौत की नींद सोने पर मजबूर कर दिया है. नाम है मीठी, पर इसका भविष्य और वर्तमान दोनों कड़वा-कसैला है.
मायानगरी मुंबई कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर आरे के जंगल बचाने जाग गई थी. पर शहर के लोगों ने एक मरती हुई नदी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया. मुंबई ने एक नदी को मौत की नींद सोने पर मजबूर कर दिया है. नाम है मीठी, पर इसका भविष्य और वर्तमान दोनों कड़वा-कसैला है. खुद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने माना है कि मीठी नदी में अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा तयशुदा मानकों से 16 गुना अधिक है.
करीब 17.8 किमी लंबी मीठी नदी मुंबई के दिल से गुजरती है और माहीम क्रीक में जाकर मिल जाती है और बोर्ड के मुताबिक इसमें प्रदूषण उच्चतम स्तर का है.
झटके खाने वाली बात यह है कि आरे के जंगलों पर आरा चलने की खबर से एक्टिव मोड में आ गए मुंबईकर मीठी नदी की दुर्दशा पर अमूमन चुप हैं. और सरकार ने इस नदी के पुनरोद्धार पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं पर समस्या का निराकरण कहीं दिखता तक नहीं है. इस नदी में अभी फीकल कॉलीफॉर्म, एक बैक्टिरिया जो इंसानों और जानवरों के मल में मौजूद होता है, की उच्चतम मात्रा मौजूद है. 2018 के जनवरी-मार्च महीनों में मीठी नदी में यह बैक्टिरिया 1,600 प्रति 100 मिली था, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक यह तयशुदा मात्रा 100 प्रति 100 मिली ही होनी चाहिए.
हालांकि, 2005 में मुंबई में आई बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने मीठी रिवर डिवेलपमेंट ऐंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी (एमआरडीपीए) का गठन किया था और इसने ताजा जानकारी मिलने तक (2018 तक), इसके मद में 1,156 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं.
करीबन डेढ़ दशक के पुनरोत्थान कार्य के बाद भी नदी की सांस घुट रही है. असल में, इंडिया टुडे में 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा गया कि इस रकम का अधिकतर हिस्सा नदी को गहरा और चौड़ा करने में खर्च हो गया. साथ में नदी के साथ की दीवारों की भी मरम्मत की गई. महाराष्ट्र सरकार के ताजा आंकड़े के मुताबिक, मीठी नदी को पुनर्जीवित करने का पूरा मद करीबन 2136.89 करोड़ रुपए है. इनमें से करीबन 1156.75 करोड़ रु. को 12 पुल बनाने. नदी को चौड़ा करने, दीवारें खड़ी करने, अतिक्रमण हटाने, सर्विस रोड बनाने और गाद हटाने में खर्च किया जा चुका है.
पर यह तो अगली बाढ़ से बचाव का रास्ता हुआ. यह तो महानगर का स्वार्थ है. नदी के लिए क्या काम हुआ? इस रिपोर्ट में लिखा गया कि उस वक्त मद में बचे 600 करोड़ को नदी पर मौजूद पांच पुलो, माहीम कॉजवे, तान्सा, तुलसी, धारावी और माहीम रेलवे ब्रिज को चौड़ा करने में खर्च किया जाना है. इससे नदी का संकरा रास्ता चौड़ा हो जाएगा.
पर नदी की सेहत की बात करें तो मीठी नदी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) सुरक्षित स्तर से पांच गुना अधिक है. बीओडी पानी में जलीय जीवन के जीवित रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा होती है. हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित 2019 की एक रिपोर्ट में आइआइटी बॉम्बे और एनईईआरआइ को उद्धृत करते हुए कहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस कचरे ने मीठी नदी को एक खुले नाले में बदल दिया है.
वैसे इस नदी को साफ करना कोई खेल नहीं है. इसके दोनों किनारों पर करीब 15 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं.
द हिंदू में प्रकाशित जून, 2019 एक लेख में महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम को उद्धृत किया गया है जिन्होंने 2015 में कहा था कि मीठी नदी में 93 फीसद अपशिष्ट घरेलू है जबकि बाकी का 7 फीसद ही औद्योगिक कचरा है. पर सचाई यह है कि इस नदी के किनारे करीबन 1500 औद्योगिक इकाईयां है और उनमें से अधिकतर अपना अपशिष्ट सीधे इसी नदी में बहाते हैं.
असल में इस नदी के किनारे की झुग्गियों में कचरा निस्तारण व्यवस्ता ठीक नहीं है. ऐसे में लोगों को सारा अपशिष्ट नदी में ही डालने पर मजबूर होना होता है.
2004 में मीठी नदी के प्रदूषण पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक रिपोर्ट दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि यह नदी अपने उद्गम पर ही प्रदूषित हो जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, "नदी घनी आबादी से होकर बहती है और इस आबादी का सीवेज इस नदी को मुंबई के सबसे बड़े नाले में बदल देता है."
 मीठी नदी, मुंबई सरकार ने उस वक्त इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और जब 26 जुलाई, 2005 को शहर को एक ही दिन में 944 मिमी की बरसात झेलनी पड़ी और जिसमें करीबन 1000 लोग मारे गए तो लोगों की आंख खुली. इस सैलाब के पीछे बरसात के साथ साथ नदी का बदला भी था. एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने पाया कि मीठी की कम चौड़ाई ही इस सैलाब की बड़ी वजहों में से क थी. बाढ़ के बाद सरकार ने प्रस्ताव पास किया और जैसा कि ऊपर मैंने बताया, एमआरडीपीए की गठन किया गया. इस अथॉरिटी की भूमिका विकास योजनाएं बनाना और इसके किनारे रह रहे लोगों का पुनर्वास वगैरह था.
मीठी नदी, मुंबई सरकार ने उस वक्त इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और जब 26 जुलाई, 2005 को शहर को एक ही दिन में 944 मिमी की बरसात झेलनी पड़ी और जिसमें करीबन 1000 लोग मारे गए तो लोगों की आंख खुली. इस सैलाब के पीछे बरसात के साथ साथ नदी का बदला भी था. एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने पाया कि मीठी की कम चौड़ाई ही इस सैलाब की बड़ी वजहों में से क थी. बाढ़ के बाद सरकार ने प्रस्ताव पास किया और जैसा कि ऊपर मैंने बताया, एमआरडीपीए की गठन किया गया. इस अथॉरिटी की भूमिका विकास योजनाएं बनाना और इसके किनारे रह रहे लोगों का पुनर्वास वगैरह था.
पर डेढ़ दशक के बाद और हजार करोड़ रुपए बहाने के बाद आज भी मीठी नदी की हालत जस की तस ही है. वैसे महाराष्ट्र में पिछली फड़णवीस सरकार ने मीठी को बचाने के लिए एक रिवर एंदेम बनाया था. पर, नदी को बचाने के लिए घाट, सड़क-पुल-दीवार बनाना झुंझला देने वाली बात है.
हमारी नदियों को आरती और चुनर चढ़ाए जाने की ज़रूरत नहीं है. उनमें सीवर का मल नहीं, साफ पानी बहे, तब उनकी जान बचेगी. मीठी नदी मर गई तो मुंबई के लिए सबक कड़वा होगा.
***
मायानगरी मुंबई कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर आरे के जंगल बचाने जाग गई थी. पर शहर के लोगों ने एक मरती हुई नदी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया. मुंबई ने एक नदी को मौत की नींद सोने पर मजबूर कर दिया है. नाम है मीठी, पर इसका भविष्य और वर्तमान दोनों कड़वा-कसैला है. खुद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने माना है कि मीठी नदी में अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा तयशुदा मानकों से 16 गुना अधिक है.
करीब 17.8 किमी लंबी मीठी नदी मुंबई के दिल से गुजरती है और माहीम क्रीक में जाकर मिल जाती है और बोर्ड के मुताबिक इसमें प्रदूषण उच्चतम स्तर का है.
झटके खाने वाली बात यह है कि आरे के जंगलों पर आरा चलने की खबर से एक्टिव मोड में आ गए मुंबईकर मीठी नदी की दुर्दशा पर अमूमन चुप हैं. और सरकार ने इस नदी के पुनरोद्धार पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं पर समस्या का निराकरण कहीं दिखता तक नहीं है. इस नदी में अभी फीकल कॉलीफॉर्म, एक बैक्टिरिया जो इंसानों और जानवरों के मल में मौजूद होता है, की उच्चतम मात्रा मौजूद है. 2018 के जनवरी-मार्च महीनों में मीठी नदी में यह बैक्टिरिया 1,600 प्रति 100 मिली था, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक यह तयशुदा मात्रा 100 प्रति 100 मिली ही होनी चाहिए.
हालांकि, 2005 में मुंबई में आई बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने मीठी रिवर डिवेलपमेंट ऐंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी (एमआरडीपीए) का गठन किया था और इसने ताजा जानकारी मिलने तक (2018 तक), इसके मद में 1,156 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं.
करीबन डेढ़ दशक के पुनरोत्थान कार्य के बाद भी नदी की सांस घुट रही है. असल में, इंडिया टुडे में 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा गया कि इस रकम का अधिकतर हिस्सा नदी को गहरा और चौड़ा करने में खर्च हो गया. साथ में नदी के साथ की दीवारों की भी मरम्मत की गई. महाराष्ट्र सरकार के ताजा आंकड़े के मुताबिक, मीठी नदी को पुनर्जीवित करने का पूरा मद करीबन 2136.89 करोड़ रुपए है. इनमें से करीबन 1156.75 करोड़ रु. को 12 पुल बनाने. नदी को चौड़ा करने, दीवारें खड़ी करने, अतिक्रमण हटाने, सर्विस रोड बनाने और गाद हटाने में खर्च किया जा चुका है.
पर यह तो अगली बाढ़ से बचाव का रास्ता हुआ. यह तो महानगर का स्वार्थ है. नदी के लिए क्या काम हुआ? इस रिपोर्ट में लिखा गया कि उस वक्त मद में बचे 600 करोड़ को नदी पर मौजूद पांच पुलो, माहीम कॉजवे, तान्सा, तुलसी, धारावी और माहीम रेलवे ब्रिज को चौड़ा करने में खर्च किया जाना है. इससे नदी का संकरा रास्ता चौड़ा हो जाएगा.
पर नदी की सेहत की बात करें तो मीठी नदी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) सुरक्षित स्तर से पांच गुना अधिक है. बीओडी पानी में जलीय जीवन के जीवित रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा होती है. हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित 2019 की एक रिपोर्ट में आइआइटी बॉम्बे और एनईईआरआइ को उद्धृत करते हुए कहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस कचरे ने मीठी नदी को एक खुले नाले में बदल दिया है.
वैसे इस नदी को साफ करना कोई खेल नहीं है. इसके दोनों किनारों पर करीब 15 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं.
द हिंदू में प्रकाशित जून, 2019 एक लेख में महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम को उद्धृत किया गया है जिन्होंने 2015 में कहा था कि मीठी नदी में 93 फीसद अपशिष्ट घरेलू है जबकि बाकी का 7 फीसद ही औद्योगिक कचरा है. पर सचाई यह है कि इस नदी के किनारे करीबन 1500 औद्योगिक इकाईयां है और उनमें से अधिकतर अपना अपशिष्ट सीधे इसी नदी में बहाते हैं.
असल में इस नदी के किनारे की झुग्गियों में कचरा निस्तारण व्यवस्ता ठीक नहीं है. ऐसे में लोगों को सारा अपशिष्ट नदी में ही डालने पर मजबूर होना होता है.
2004 में मीठी नदी के प्रदूषण पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक रिपोर्ट दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि यह नदी अपने उद्गम पर ही प्रदूषित हो जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, "नदी घनी आबादी से होकर बहती है और इस आबादी का सीवेज इस नदी को मुंबई के सबसे बड़े नाले में बदल देता है."
 मीठी नदी, मुंबई सरकार ने उस वक्त इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और जब 26 जुलाई, 2005 को शहर को एक ही दिन में 944 मिमी की बरसात झेलनी पड़ी और जिसमें करीबन 1000 लोग मारे गए तो लोगों की आंख खुली. इस सैलाब के पीछे बरसात के साथ साथ नदी का बदला भी था. एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने पाया कि मीठी की कम चौड़ाई ही इस सैलाब की बड़ी वजहों में से क थी. बाढ़ के बाद सरकार ने प्रस्ताव पास किया और जैसा कि ऊपर मैंने बताया, एमआरडीपीए की गठन किया गया. इस अथॉरिटी की भूमिका विकास योजनाएं बनाना और इसके किनारे रह रहे लोगों का पुनर्वास वगैरह था.
मीठी नदी, मुंबई सरकार ने उस वक्त इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और जब 26 जुलाई, 2005 को शहर को एक ही दिन में 944 मिमी की बरसात झेलनी पड़ी और जिसमें करीबन 1000 लोग मारे गए तो लोगों की आंख खुली. इस सैलाब के पीछे बरसात के साथ साथ नदी का बदला भी था. एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने पाया कि मीठी की कम चौड़ाई ही इस सैलाब की बड़ी वजहों में से क थी. बाढ़ के बाद सरकार ने प्रस्ताव पास किया और जैसा कि ऊपर मैंने बताया, एमआरडीपीए की गठन किया गया. इस अथॉरिटी की भूमिका विकास योजनाएं बनाना और इसके किनारे रह रहे लोगों का पुनर्वास वगैरह था.पर डेढ़ दशक के बाद और हजार करोड़ रुपए बहाने के बाद आज भी मीठी नदी की हालत जस की तस ही है. वैसे महाराष्ट्र में पिछली फड़णवीस सरकार ने मीठी को बचाने के लिए एक रिवर एंदेम बनाया था. पर, नदी को बचाने के लिए घाट, सड़क-पुल-दीवार बनाना झुंझला देने वाली बात है.
हमारी नदियों को आरती और चुनर चढ़ाए जाने की ज़रूरत नहीं है. उनमें सीवर का मल नहीं, साफ पानी बहे, तब उनकी जान बचेगी. मीठी नदी मर गई तो मुंबई के लिए सबक कड़वा होगा.
***

Published on February 14, 2020 00:22
February 6, 2020
नदीसूत्रः स्वर्ग ले जानी वाली नदी वैतरणी आखिर है किधर
हिंदुओं के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाली वैतरणी नदी ओडिशा में भी है और महाराष्ट्र में भी. रावी, व्यास और सतलज हांगकांग में भी हैं और कर्नाटक की अधिकांश नदियों के नाम वैदिक संस्कृत में हैं. जाहिर है, नदियों के नाम इतिहास के सूत्र छोड़ते हैं. भाषा विज्ञानियों को इस दिशा में काम करना चाहिए.
नदियों के नामों को लेकर पिछली एक पोस्ट पर बहुत दिलचस्प जानकारियां मुझे मिली थीं और आपके साथ साझा भी किया था. इसको आगे बढ़ाने का मन है.
हिंदुओं के लिए गरुण पुराण बेहद महत्वपूर्ण है. मुमुक्षुओं के लिए इसकी महत्ता काफी अधिक है और आखिरी सांसें गिन रहे लोगों को यह पुराण पढ़कर सुनाया जाता है. गुरुड़ पुराण के मुताबिक, मरने के बाद वैतरणी नाम की नदी पार करनी होती है. बहरहाल, ओडिशा में एक नदी है जिसका नाम वैतरणी है. इसके बेसिन को ब्राह्मणी-वैतरणी बेसिन कहा जाता है. लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी एक वैतरणी नदी है, जो नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिरती है. अब इसमें से किस नदी को पार करने पर स्वर्ग मिलेगा यह स्पष्ट नहीं है.
वैतरणी से थोड़ी ही दूरी पर मशहूर गोदावरी का भी उद्गम स्थल है, और नासिक के पास से निकलकर यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बन जाती है. इसको दक्षिण की गंगा भी कहते ही हैं. लेकिन, एक अदद गोदावरी नेपाल में भी है. वैसे, बुंदेलखंड के चित्रकूट में एक गुप्त गोदावरी भी निकलती है और जो एक पहाड़ी गुफा के भीतर से पतली धारा के रूप में बहती है. गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, जो छत्तीसगढ़ में बहती है पर एक इंद्रावती नेपाल में भी मौजूद है.
उत्तर प्रदेश की प्रदूषित नदियों में शर्मनाक रूप से टॉप पर रहने वाली गोमती नदी की बात करें तो एक गोमती त्रिपुरा में भी है जो वहां से आगे बांग्लादेश में घुस जाती है. इसी नदी पर त्रिपुरा में का सबसे बड़ा और बदनाम बांध बना हुआ है. गंगा का नाम तो नदी शब्द का करीबन पर्यायवाची ही बन गया है. आदिगंगा से लेकर गोरीगंगा और काली गंगा से लेकर वनगंगा और बाल गंगा तक नाम की नदियां अस्तित्व में हैं.
पंजाब की रावी का एक नाम इरावती भी है. लेकिन, एक और इरावती है. पर यह इरावती नमाइ और माली नदियों के मिलने से बनती है और म्यांमार में बहती है. यह हिमालयी हिमनदों से शुरू होती है. पंजाब वाली रावी पाकिस्तान होती हुई सिंधु में मिल जाती है और म्यांमार वाली इरावदी अंडमान सागर में.
परिणीता दांडेकर लिखती हैं कि कावेरी नाम की भी दो नदियां हैं. एक तो वह मशहूर कावेरी नदी, जिसके पानी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक में रार मचा रहता है. जबकि दूसरी कावेरी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा की सहायक नदी है और दांडेकर के मुताबिक, ओंकारेश्वर नर्मदा और कावेरी के संगम पर ही बसा है.
दांडेकर अपने लेख में चर्चा करती हैं कि हांगकांग में सतलज, झेलम और व्यास नदियां मौजूद हैं. संभवतया, यह 1860 के आसपास हुआ जब हांगकांग में तैनात पंजाब के सिख सैनिकों ने वहां की नदियों के नाम अपने पसंद के रख दिए. हांगकांग की सबसे बड़ी ताजे पानी की नम भूमि लॉन्ग वैली को दोआब नाम दिया गया और यह वहां की सतलज और व्यास के बीच की भूमि है. शायद, इन छोटे मैदानों को देखकर सिख फौजियों को अपने वतन की याद आती होगी.
दांडेकर अपने लेख में धीमान दासगुप्ता को उद्धृत करती हैं जो कहते है कि लोग अपने साथ कुछ नाम भी लिए चलते हैं. मसलन, "प्राचीन वैदिक लोग अपने साथ नाम लेकर चले थे. असली सरस्वती और सरयू नदियां (जिनका जिक्र रामायण में है, अफगानिस्तान और ईरान में थीं. असली यमुना फारस की मुख्य देवी थीं." जाहिर है, इतिहास के इस नए नजरिए के साथ भी देखना चाहिए.
नदियों के नामों में वैदिक संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट रूप से कर्नाटक में दिखता है जहां शाल्मला, नेत्रावती, कुमारधारा, पयस्विनी, शौपर्णिका, स्वर्णा, अर्कावती, अग्नाशिनी, कबिनी, वेदवती, कुमुदावती, शर्वती, वृषभावती, गात्रप्रभा, मालप्रभा जैसी नदियों के नाम मौजूद हैं.
गुजरात की नदियों साबरमती और रुक्मावती का नाम याद करिए. कितने सुंदर और शास्त्रीय नाम हैं! लेकिन एक नदी वहां ऐसी भी है जिसका नाम है भूखी. एक अन्य नदी है उतावली. राजस्थान अलवर जिले में एक नदी का नाम जहाजवाली भी है.
कुछ नदियों के नाम भी वक्त के साथ बदले हैं जैसे, गोदावरी आंध्र प्रदेश में गोदारी कही जाने लगती है और पद्मा बांग्लादेश में पोद्दा. चर्मावती चंबल हो जाती है और वेत्रावती, बेतवा.
दांडेकर लिखती हैं, कुछ नदियों के नाम में इलाकाई और भाषायी असर भी आता है. मसलन, तमिल और मलयालम में आर और पुझा (यानी नदी) कई नदियों के नाम में जुड़ा हुआ है. गौर कीजिए, चालाकुडी पूझा, पेरियार, पेंडियार वगैरह. इसी तरह भूटान, सिक्कम और तवांग इलाके में छू का मतलब नदी ही होता है. अब वहां की नदियों हैं, न्यामजांगछू या राथोंग छू. तो अब इसके आगे नदी शब्द मत लगाइए. क्योंकि पहले ही छू कहकर नदी कह चुके हैं. असम में भी नदियों के नाम के आगे कुछ खास शब्द लगाए जाते हैं, और वो हैं दि. दिहांग, दिबांग, दिखोऊ, दिक्रोंग आदि. बोडो में दि शब्द का मतलब होता है पानी और याद रखिए ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे पहले बसने का दावा भी बोडी ही करते हैं.
जाहिर है, नदियों के नाम इतिहास के सूत्र छोड़ते हैं. भाषा विज्ञानियों को इस दिशा में काम करना चाहिए.
***
नदियों के नामों को लेकर पिछली एक पोस्ट पर बहुत दिलचस्प जानकारियां मुझे मिली थीं और आपके साथ साझा भी किया था. इसको आगे बढ़ाने का मन है.
हिंदुओं के लिए गरुण पुराण बेहद महत्वपूर्ण है. मुमुक्षुओं के लिए इसकी महत्ता काफी अधिक है और आखिरी सांसें गिन रहे लोगों को यह पुराण पढ़कर सुनाया जाता है. गुरुड़ पुराण के मुताबिक, मरने के बाद वैतरणी नाम की नदी पार करनी होती है. बहरहाल, ओडिशा में एक नदी है जिसका नाम वैतरणी है. इसके बेसिन को ब्राह्मणी-वैतरणी बेसिन कहा जाता है. लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी एक वैतरणी नदी है, जो नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिरती है. अब इसमें से किस नदी को पार करने पर स्वर्ग मिलेगा यह स्पष्ट नहीं है.
वैतरणी से थोड़ी ही दूरी पर मशहूर गोदावरी का भी उद्गम स्थल है, और नासिक के पास से निकलकर यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बन जाती है. इसको दक्षिण की गंगा भी कहते ही हैं. लेकिन, एक अदद गोदावरी नेपाल में भी है. वैसे, बुंदेलखंड के चित्रकूट में एक गुप्त गोदावरी भी निकलती है और जो एक पहाड़ी गुफा के भीतर से पतली धारा के रूप में बहती है. गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, जो छत्तीसगढ़ में बहती है पर एक इंद्रावती नेपाल में भी मौजूद है.
उत्तर प्रदेश की प्रदूषित नदियों में शर्मनाक रूप से टॉप पर रहने वाली गोमती नदी की बात करें तो एक गोमती त्रिपुरा में भी है जो वहां से आगे बांग्लादेश में घुस जाती है. इसी नदी पर त्रिपुरा में का सबसे बड़ा और बदनाम बांध बना हुआ है. गंगा का नाम तो नदी शब्द का करीबन पर्यायवाची ही बन गया है. आदिगंगा से लेकर गोरीगंगा और काली गंगा से लेकर वनगंगा और बाल गंगा तक नाम की नदियां अस्तित्व में हैं.
पंजाब की रावी का एक नाम इरावती भी है. लेकिन, एक और इरावती है. पर यह इरावती नमाइ और माली नदियों के मिलने से बनती है और म्यांमार में बहती है. यह हिमालयी हिमनदों से शुरू होती है. पंजाब वाली रावी पाकिस्तान होती हुई सिंधु में मिल जाती है और म्यांमार वाली इरावदी अंडमान सागर में.
परिणीता दांडेकर लिखती हैं कि कावेरी नाम की भी दो नदियां हैं. एक तो वह मशहूर कावेरी नदी, जिसके पानी के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक में रार मचा रहता है. जबकि दूसरी कावेरी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा की सहायक नदी है और दांडेकर के मुताबिक, ओंकारेश्वर नर्मदा और कावेरी के संगम पर ही बसा है.
दांडेकर अपने लेख में चर्चा करती हैं कि हांगकांग में सतलज, झेलम और व्यास नदियां मौजूद हैं. संभवतया, यह 1860 के आसपास हुआ जब हांगकांग में तैनात पंजाब के सिख सैनिकों ने वहां की नदियों के नाम अपने पसंद के रख दिए. हांगकांग की सबसे बड़ी ताजे पानी की नम भूमि लॉन्ग वैली को दोआब नाम दिया गया और यह वहां की सतलज और व्यास के बीच की भूमि है. शायद, इन छोटे मैदानों को देखकर सिख फौजियों को अपने वतन की याद आती होगी.
दांडेकर अपने लेख में धीमान दासगुप्ता को उद्धृत करती हैं जो कहते है कि लोग अपने साथ कुछ नाम भी लिए चलते हैं. मसलन, "प्राचीन वैदिक लोग अपने साथ नाम लेकर चले थे. असली सरस्वती और सरयू नदियां (जिनका जिक्र रामायण में है, अफगानिस्तान और ईरान में थीं. असली यमुना फारस की मुख्य देवी थीं." जाहिर है, इतिहास के इस नए नजरिए के साथ भी देखना चाहिए.
नदियों के नामों में वैदिक संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट रूप से कर्नाटक में दिखता है जहां शाल्मला, नेत्रावती, कुमारधारा, पयस्विनी, शौपर्णिका, स्वर्णा, अर्कावती, अग्नाशिनी, कबिनी, वेदवती, कुमुदावती, शर्वती, वृषभावती, गात्रप्रभा, मालप्रभा जैसी नदियों के नाम मौजूद हैं.
गुजरात की नदियों साबरमती और रुक्मावती का नाम याद करिए. कितने सुंदर और शास्त्रीय नाम हैं! लेकिन एक नदी वहां ऐसी भी है जिसका नाम है भूखी. एक अन्य नदी है उतावली. राजस्थान अलवर जिले में एक नदी का नाम जहाजवाली भी है.
कुछ नदियों के नाम भी वक्त के साथ बदले हैं जैसे, गोदावरी आंध्र प्रदेश में गोदारी कही जाने लगती है और पद्मा बांग्लादेश में पोद्दा. चर्मावती चंबल हो जाती है और वेत्रावती, बेतवा.
दांडेकर लिखती हैं, कुछ नदियों के नाम में इलाकाई और भाषायी असर भी आता है. मसलन, तमिल और मलयालम में आर और पुझा (यानी नदी) कई नदियों के नाम में जुड़ा हुआ है. गौर कीजिए, चालाकुडी पूझा, पेरियार, पेंडियार वगैरह. इसी तरह भूटान, सिक्कम और तवांग इलाके में छू का मतलब नदी ही होता है. अब वहां की नदियों हैं, न्यामजांगछू या राथोंग छू. तो अब इसके आगे नदी शब्द मत लगाइए. क्योंकि पहले ही छू कहकर नदी कह चुके हैं. असम में भी नदियों के नाम के आगे कुछ खास शब्द लगाए जाते हैं, और वो हैं दि. दिहांग, दिबांग, दिखोऊ, दिक्रोंग आदि. बोडो में दि शब्द का मतलब होता है पानी और याद रखिए ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे पहले बसने का दावा भी बोडी ही करते हैं.
जाहिर है, नदियों के नाम इतिहास के सूत्र छोड़ते हैं. भाषा विज्ञानियों को इस दिशा में काम करना चाहिए.
***

Published on February 06, 2020 23:16
February 4, 2020
पिछले साल रहा मौसम बेहाल, अब खेती में राहत की उम्मीद
2019 का साल अति प्राकृतिक घटनाओं का साल रहा. अतिवृष्टि, लू के थपेड़े और चक्रवातों के बाद बारी हिमपात और शीतलहर. पर अब सर्दियों में हुई ठीक-ठाक बारिश से इस बार रबी की फसल बढ़िया होने की उम्मीद जगी है. सरकार की कोशिश अब इसके जरिए मंदी से निपटने की होनी चाहिए
मंदी और कृषि क्षेत्र में तमाम आशंकाओं के बाद एक खुशखबरी मिल रही है. 2020 की पहली फसल कटाई में रबी की पैदावार बेहतर हो सकती है और जाहिर है इससे किसानों को राहत मिलेगी. मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी एजेंसी स्काइमेट ने रबी रिपोर्ट, 2020 जारी करते हुए अच्छी पैदावार की उम्मीद जाहिर की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मॉनसून और मॉनसून के बाद के सीजन में अच्छी बारिश हुई है. रबी उत्पादक प्रमुख राज्यों में भी जनवरी के पहले पखवाड़े में पर्याप्त बरसात हुई है इससे फसल की सेहत को काफी फायदा मिला है.
लेकिन 2019 में मौसम से जुड़े मामले कुछ ठीक नहीं रहे थे.
2019 का साल अति प्राकृतिक घटनाओं का साल रहा. देश को लू के थपेड़ों के बाद अतिवृष्टि, और चक्रवातों के बाद बारी हिमपात और शीतलहर का सामना करना पड़ा था. पर अब सर्दियों में हुई ठीक-ठाक बारिश से इस बार रबी की फसल बढ़िया होने की उम्मीद जगी है. सरकार की कोशिश अब इसके जरिए मंदी से निपटने की होनी चाहिए
पिछले 25 साल के मुकाबले हालांकि, मॉनसून अधिक रहा था और मानक बरसात से 110 फीसद अधिक बारिश हुई थी. गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को बाढ़ का सामना करना पड़ा था. इसके साथ ही कुल मिलाकर 9 चक्रवातीय तूफान भी आए थे. यही नहीं, करेला नीम पर तब चढ़ा जब दिसंबर महीने में उत्तर भारत में शीतलहर की सबसे लंबी अवधि भी रिकॉर्ड की गई. हिमालयी राज्य़ों में अक्तूबर से लेकर दिसंबर तक भारी हिमपात भी दर्ज किया गया. पिछले साल अप्रैल से जून के महीने में मॉनसून से पहले भारी लू भी चली थी. जबकि, मॉनसून के बाद अक्तूबर से दिसंबर तक की अवधि में अतिवृष्टि भी हुई.
हालांकि इस बढ़िया बरसात ने देश के जलाशयों का पेट भर दिया है. इसका असर रबी की अच्छी बुआई पर पड़ा था. मिट्टी में नमी की मौजूदगी ने फसल उत्पादकता पर भी असर डाला है. और इस बार इस असर को सकारात्मक मानना चाहिए. हालांकि, रबी की पैदावार पर सर्दियों का तापमान भी प्रभावित करता है और अच्छा जाड़ा पड़ने से वह भी सकारात्मक ही रहा है.
स्काइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक, गेहूं की पैदावार में इस सीजन में करीबन 10.6 फीसद की बढ़ोतरी होगी और पिछले सीजन के 10.21 करोड़ टन के मुकाबले इस बार उपज 11.30 टन के आसपास रहने की उम्मीद है.
मौसम के मद्देनजर चने और धान की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी. तिलहन की फसल भी अच्छी होने की उम्मीद है जिससे खाद्य तेलों की मौजूदा महंगाई को थामा जा सकेगा. जाहिर है, किसानों की परेशानी के दौर में यह एक बढ़िया खबर तो है पर आगे की भूमिका सरकार को निभानी होगी जो किसानों की उपज को सही तरीके से खरीदे. किसानों के पास क्रयशक्ति बढ़ेगी तो बाजार में छाई मंदी से भी निपटा जा सकेगा.

मंदी और कृषि क्षेत्र में तमाम आशंकाओं के बाद एक खुशखबरी मिल रही है. 2020 की पहली फसल कटाई में रबी की पैदावार बेहतर हो सकती है और जाहिर है इससे किसानों को राहत मिलेगी. मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी एजेंसी स्काइमेट ने रबी रिपोर्ट, 2020 जारी करते हुए अच्छी पैदावार की उम्मीद जाहिर की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मॉनसून और मॉनसून के बाद के सीजन में अच्छी बारिश हुई है. रबी उत्पादक प्रमुख राज्यों में भी जनवरी के पहले पखवाड़े में पर्याप्त बरसात हुई है इससे फसल की सेहत को काफी फायदा मिला है.
लेकिन 2019 में मौसम से जुड़े मामले कुछ ठीक नहीं रहे थे.
2019 का साल अति प्राकृतिक घटनाओं का साल रहा. देश को लू के थपेड़ों के बाद अतिवृष्टि, और चक्रवातों के बाद बारी हिमपात और शीतलहर का सामना करना पड़ा था. पर अब सर्दियों में हुई ठीक-ठाक बारिश से इस बार रबी की फसल बढ़िया होने की उम्मीद जगी है. सरकार की कोशिश अब इसके जरिए मंदी से निपटने की होनी चाहिए
पिछले 25 साल के मुकाबले हालांकि, मॉनसून अधिक रहा था और मानक बरसात से 110 फीसद अधिक बारिश हुई थी. गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को बाढ़ का सामना करना पड़ा था. इसके साथ ही कुल मिलाकर 9 चक्रवातीय तूफान भी आए थे. यही नहीं, करेला नीम पर तब चढ़ा जब दिसंबर महीने में उत्तर भारत में शीतलहर की सबसे लंबी अवधि भी रिकॉर्ड की गई. हिमालयी राज्य़ों में अक्तूबर से लेकर दिसंबर तक भारी हिमपात भी दर्ज किया गया. पिछले साल अप्रैल से जून के महीने में मॉनसून से पहले भारी लू भी चली थी. जबकि, मॉनसून के बाद अक्तूबर से दिसंबर तक की अवधि में अतिवृष्टि भी हुई.
हालांकि इस बढ़िया बरसात ने देश के जलाशयों का पेट भर दिया है. इसका असर रबी की अच्छी बुआई पर पड़ा था. मिट्टी में नमी की मौजूदगी ने फसल उत्पादकता पर भी असर डाला है. और इस बार इस असर को सकारात्मक मानना चाहिए. हालांकि, रबी की पैदावार पर सर्दियों का तापमान भी प्रभावित करता है और अच्छा जाड़ा पड़ने से वह भी सकारात्मक ही रहा है.
स्काइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक, गेहूं की पैदावार में इस सीजन में करीबन 10.6 फीसद की बढ़ोतरी होगी और पिछले सीजन के 10.21 करोड़ टन के मुकाबले इस बार उपज 11.30 टन के आसपास रहने की उम्मीद है.
मौसम के मद्देनजर चने और धान की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी. तिलहन की फसल भी अच्छी होने की उम्मीद है जिससे खाद्य तेलों की मौजूदा महंगाई को थामा जा सकेगा. जाहिर है, किसानों की परेशानी के दौर में यह एक बढ़िया खबर तो है पर आगे की भूमिका सरकार को निभानी होगी जो किसानों की उपज को सही तरीके से खरीदे. किसानों के पास क्रयशक्ति बढ़ेगी तो बाजार में छाई मंदी से भी निपटा जा सकेगा.

Published on February 04, 2020 00:01
January 29, 2020
नदीसूत्रः ...और जी उठी पौराणिक महत्व की नदी छोटी सरयू
अब तक हमने नदीसूत्र में नदियों की व्यथा कथा ही लिखी थी. पर कुछ लोग वाकई अपनी तरफ से योगदान देकर विरासत बचा रहे हैं. सरयू की पूर्व धारा रही छोटी सरयू भी काल के गाल में समाने वाली थी, पर पवन सिंह जैसे कुछ लोगों ने अथक मेहनत से उसे बचा लिया. लिहाजा, नदी जी गई है.
हाल में खबर आई कि उत्तर प्रदेश शासन ने घाघरा नदी, जिसको अयोध्या के आसपास के टुकड़े को सरयू कहा जाता था, का नाम बदलकर सरयू कर दिया. नाम बदलने में कोई बुराई नहीं. पर आराध्य राम से जुड़ी सरयू नदी पर सरकार की इतनी कृपा है तो थोड़ी कृपादृष्टि तो छोटी सरयू पर भी बनती थी. आजमगढ़ की नदियों पर काम कर रहे और गैर-सरकारी संस्था लोक दायित्व के संयोजक पवन कुमार सिंह ने 2018 में छोटी सरयू को मूल सरयू का नाम देकर इसको बचाने के लिए अभियान प्रारम्भ किया. उनका कहना है कि छोटी सरयू ही मूल सरयू है.
बहरहाल, 2018 तक स्थिति यह थी कि आकार में काफी हद तक सिकुड़ चुकी छोटी सरयू नदी का क्षेत्रफल लगातार सिमटता जा रहा था. (अभी यह बहुत संकरे बरसाती नाले की रूप में है) साफ-सफाई न होने से नदी का प्रवाह थम-सा गया था. आजमगढ़ के लाटघाट से शुरू हुआ 59 किलोमीटर का सफर तय करते-करते नगर की तलहटी में प्रवाहित तमसा तक आते-आते नदी का पानी काला पड़ जाता था. नदी का अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच गया था पर प्रशासन मौन ही रहा.
आंबेडकर नगर जिले से निकली छोटी सरयू नदी आजमगढ के विभिन्न इलाकों से होते हुए बड़गांव ब्लाक क्षेत्र से होते हुए कोपागंज ब्लाक के सहरोज गांव के पास टौंस नदी में मिल जाती है. एक जमाना था कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के सिंचाई का एकमात्र साधन छोटी सरयू नदी थी. सैकड़ों गांवों के लोग पेयजल के लिए भी इसी पर निर्भर थे.
[image error]
लेकिन प्रदूषण की मार से कहीं-कहीं नदी का पानी इतना जहरीला हो गया है कि पशु भी इसका पानी पीने से कतराते हैं. इस नदी में पानी की कमी थी और गर्मियों में हालात और भी खराब थे.
आजमगढ़ जिले के महुआ गढ़वल रेगुलेटर से समय-समय पर पानी छोड़ा जाता, तो नदी में थोड़ी जिंदगी लौट आती थी. अतिक्रमण सुरसा की तरह अलग मुंह फाड़े नदी को निगल रही थी (यह संकट अब भी है) लोकदायित्व संस्था के पवन सिंह कहते हैं, "सिकुड़ती नदियां और उनका प्रदूषण आज राष्ट्रीय चिंता का विषय है. गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि बड़ी नदियों पर सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इन बड़ी नदियों को पोषित करने वाली छोटी नदियों की दुर्दशा पर भी लोगों को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए."
बहरहाल, लोकदायित्व और पवन सिंह ने दायित्व उठाया कि छोटी सरयू को दोबारा जिलाया जाए.
असल में, आजमगढ़ जिले में छोटी-बड़ी मिलाकर लगभग डेढ़ दर्जन नदियां हैं जिनके बेसिन में पानी का ऐसा संकट है कि वहां डार्क जोन बन रहा है. पवन सिंह कहते हैं कि आजमगढ़ जिले के उत्तरी इलाके के तमाम गांव में जलस्तर काफी नीचे चला गया है और पानी प्रदूषित हो चुका है. जबकि इस क्षेत्र में सरयू नदी का एक बड़ा तंत्र रहा है, जिसके अवशेष आज भी दिखते हैं. ऐसी ही एक नदी है- छोटी सरयू.
लोकदायित्व ने 2018 में छोटी सरयू को मूल सरयू का नाम देकर इसको बचाने के लिए अभियान प्रारम्भ किया.असल में, मूल सरयू नदी, जिसे सरकारी अभिलेखों में छोटी सरयू के नाम से दर्ज किया गया है, पहले सरयू की मुख्य धारा हुआ करती थी. समय के साथ अपने कटाव और धारा बदलती हुई यह नदी पिछले कुछ सदियों में 15 से 70 किमी तक उत्तर दिशा की ओर बढ़ गयी. इसके छाड़न के रूप में नदी का मार्ग रह गया, जिसे बाद में छोटी सरयू कहा जाने लगा.
छोटी सरयू कम्हरिया घाट से करीब तीन किमी पूर्व की तरफ कम्हरिया मांझा से निकलती है. यहां से कुछ आगे गढ़वल बाजार के पूरब से आती स्थानीय नदी पिकिया इसमें मिलती है. इस संगम पर मोहरे बाबा का स्थान है. आंबेडकर नगर जिले के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल भैरव बाबा पर अतरौलिया बाजार की तरफ से एक नदी (जिसे सरकारी अभिलेख में छोटी सरयू भाग-1 कहा गया है) आकर मिलती है. बहवलघाट होते हुए यह नदी प्रसिद्ध सलोना ताल के बाद मऊ जिले में प्रवेश करती है.
छोटी सरयू की पौराणिकता की तरफ इशारा करते हुए श्रीराम सांस्कृतिक शोध संस्थान दिल्ली के डॉ. रामअवतार शर्मा ने कहा है कि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण इसी के दाहिने किनारे से आगे गए थे. स्थानीय किंवदन्ती है कि 23वें त्रेतायुग में प्रजापति दक्ष ने यहीं पर यज्ञ किया था और यहीं पर यज्ञकुंड में माता सती ने अपने प्राण दिए थे.
छोटी सरयू की व्यथा का आरंभ होता है 1955 में आई बाढ़ से. जब बाढ़ के समाधान के तौर पर इलाके में महुला गढ़वल बांध बनाया गया. इस बांध ने छोटी सरयू को बड़ी सरयू से अलग कर दिया, जिसके कारण छोटी सरयू में प्रवाहित जल से रिश्ता टूट गया, और वह बरसात के जल पर निर्भर हो गयी. जब तक बारिश ठीक होती रही नदी अपने जीवन को किसी तरह बचाती रही. धीरे धीरे जलस्तर गिरता गया नदी सिकुड़ती गयी और नदी का चरित्र बदलता गया. नदी में गिरनेवाले नालों की संख्या बढ़ती गयी जिससे उसमें जलकुंभियां और अन्य वनस्पतियां घर बनाने लगीं.
पवन सिंह कहते हैं, "नदी वेगेन शुद्धयति. नदी को शुद्ध रखना है तो उसकी अविरलता को बचाना होगा. प्रवाह में आने वाली बाधाओं को रोकना होगा. पानी में नालों के माध्यम से गिरने वाले खनिजयुक्त व उर्वर पदार्थों को रोकना होगा. महुला गढ़वल बांध पर रेगुलेटर लगाकर बाढ़ के समय नियंत्रित जल मूल सरयू में छोड़ना होगा. अवैध कब्जों को हटाना होगा. यह सभी कार्य न ही अकेले सरकार कर सकती है और न ही कोई एजेंसी. इसलिए जनजागरूकता फैलाकर लोगों को प्रशिक्षित कर इस अभियान से जोड़ना होगा."
[image error]
इस नदी की हालत देखकर 25 स्वयंसेवकों की टोली के साथ लोक दायित्व और पवन सिंह ने काम करना शुरू किया. उस समय नदी में जलकुंभी और कचरे की भीषण समस्या थी. लगातार छह महीने की मेहनत से भैरव स्थल पर नदी की सूरत बदल गई है. नदी साफ लगने लगी और लोग उसमें कूड़ा फेंकना भी बंद कर चुके हैं.
इस साफ-सफाई में अच्छी बात यह हुई कि नदी तल में तीन पातालतोड़ कुएं भी निकल आए, जिससे नदी को नवजीवन मिल रहा है.
छोटी सरयू का जी जाना यह यकीन दिलाता है कि जो समाज अपने विरासतों को संभालकर रखना चाहता है, जिसके लिए नदी की पूजा कर्मकांड नहीं है, असल में वही समाज जीवित है.
(इस ब्लॉग के लिए तस्वीरें लोकदायित्व संस्था ने मुहैया कराई हैं)
हाल में खबर आई कि उत्तर प्रदेश शासन ने घाघरा नदी, जिसको अयोध्या के आसपास के टुकड़े को सरयू कहा जाता था, का नाम बदलकर सरयू कर दिया. नाम बदलने में कोई बुराई नहीं. पर आराध्य राम से जुड़ी सरयू नदी पर सरकार की इतनी कृपा है तो थोड़ी कृपादृष्टि तो छोटी सरयू पर भी बनती थी. आजमगढ़ की नदियों पर काम कर रहे और गैर-सरकारी संस्था लोक दायित्व के संयोजक पवन कुमार सिंह ने 2018 में छोटी सरयू को मूल सरयू का नाम देकर इसको बचाने के लिए अभियान प्रारम्भ किया. उनका कहना है कि छोटी सरयू ही मूल सरयू है.
बहरहाल, 2018 तक स्थिति यह थी कि आकार में काफी हद तक सिकुड़ चुकी छोटी सरयू नदी का क्षेत्रफल लगातार सिमटता जा रहा था. (अभी यह बहुत संकरे बरसाती नाले की रूप में है) साफ-सफाई न होने से नदी का प्रवाह थम-सा गया था. आजमगढ़ के लाटघाट से शुरू हुआ 59 किलोमीटर का सफर तय करते-करते नगर की तलहटी में प्रवाहित तमसा तक आते-आते नदी का पानी काला पड़ जाता था. नदी का अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच गया था पर प्रशासन मौन ही रहा.
आंबेडकर नगर जिले से निकली छोटी सरयू नदी आजमगढ के विभिन्न इलाकों से होते हुए बड़गांव ब्लाक क्षेत्र से होते हुए कोपागंज ब्लाक के सहरोज गांव के पास टौंस नदी में मिल जाती है. एक जमाना था कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के सिंचाई का एकमात्र साधन छोटी सरयू नदी थी. सैकड़ों गांवों के लोग पेयजल के लिए भी इसी पर निर्भर थे.
[image error]
लेकिन प्रदूषण की मार से कहीं-कहीं नदी का पानी इतना जहरीला हो गया है कि पशु भी इसका पानी पीने से कतराते हैं. इस नदी में पानी की कमी थी और गर्मियों में हालात और भी खराब थे.
आजमगढ़ जिले के महुआ गढ़वल रेगुलेटर से समय-समय पर पानी छोड़ा जाता, तो नदी में थोड़ी जिंदगी लौट आती थी. अतिक्रमण सुरसा की तरह अलग मुंह फाड़े नदी को निगल रही थी (यह संकट अब भी है) लोकदायित्व संस्था के पवन सिंह कहते हैं, "सिकुड़ती नदियां और उनका प्रदूषण आज राष्ट्रीय चिंता का विषय है. गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि बड़ी नदियों पर सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इन बड़ी नदियों को पोषित करने वाली छोटी नदियों की दुर्दशा पर भी लोगों को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए."
बहरहाल, लोकदायित्व और पवन सिंह ने दायित्व उठाया कि छोटी सरयू को दोबारा जिलाया जाए.
असल में, आजमगढ़ जिले में छोटी-बड़ी मिलाकर लगभग डेढ़ दर्जन नदियां हैं जिनके बेसिन में पानी का ऐसा संकट है कि वहां डार्क जोन बन रहा है. पवन सिंह कहते हैं कि आजमगढ़ जिले के उत्तरी इलाके के तमाम गांव में जलस्तर काफी नीचे चला गया है और पानी प्रदूषित हो चुका है. जबकि इस क्षेत्र में सरयू नदी का एक बड़ा तंत्र रहा है, जिसके अवशेष आज भी दिखते हैं. ऐसी ही एक नदी है- छोटी सरयू.
लोकदायित्व ने 2018 में छोटी सरयू को मूल सरयू का नाम देकर इसको बचाने के लिए अभियान प्रारम्भ किया.असल में, मूल सरयू नदी, जिसे सरकारी अभिलेखों में छोटी सरयू के नाम से दर्ज किया गया है, पहले सरयू की मुख्य धारा हुआ करती थी. समय के साथ अपने कटाव और धारा बदलती हुई यह नदी पिछले कुछ सदियों में 15 से 70 किमी तक उत्तर दिशा की ओर बढ़ गयी. इसके छाड़न के रूप में नदी का मार्ग रह गया, जिसे बाद में छोटी सरयू कहा जाने लगा.
छोटी सरयू कम्हरिया घाट से करीब तीन किमी पूर्व की तरफ कम्हरिया मांझा से निकलती है. यहां से कुछ आगे गढ़वल बाजार के पूरब से आती स्थानीय नदी पिकिया इसमें मिलती है. इस संगम पर मोहरे बाबा का स्थान है. आंबेडकर नगर जिले के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल भैरव बाबा पर अतरौलिया बाजार की तरफ से एक नदी (जिसे सरकारी अभिलेख में छोटी सरयू भाग-1 कहा गया है) आकर मिलती है. बहवलघाट होते हुए यह नदी प्रसिद्ध सलोना ताल के बाद मऊ जिले में प्रवेश करती है.
छोटी सरयू की पौराणिकता की तरफ इशारा करते हुए श्रीराम सांस्कृतिक शोध संस्थान दिल्ली के डॉ. रामअवतार शर्मा ने कहा है कि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण इसी के दाहिने किनारे से आगे गए थे. स्थानीय किंवदन्ती है कि 23वें त्रेतायुग में प्रजापति दक्ष ने यहीं पर यज्ञ किया था और यहीं पर यज्ञकुंड में माता सती ने अपने प्राण दिए थे.
छोटी सरयू की व्यथा का आरंभ होता है 1955 में आई बाढ़ से. जब बाढ़ के समाधान के तौर पर इलाके में महुला गढ़वल बांध बनाया गया. इस बांध ने छोटी सरयू को बड़ी सरयू से अलग कर दिया, जिसके कारण छोटी सरयू में प्रवाहित जल से रिश्ता टूट गया, और वह बरसात के जल पर निर्भर हो गयी. जब तक बारिश ठीक होती रही नदी अपने जीवन को किसी तरह बचाती रही. धीरे धीरे जलस्तर गिरता गया नदी सिकुड़ती गयी और नदी का चरित्र बदलता गया. नदी में गिरनेवाले नालों की संख्या बढ़ती गयी जिससे उसमें जलकुंभियां और अन्य वनस्पतियां घर बनाने लगीं.
पवन सिंह कहते हैं, "नदी वेगेन शुद्धयति. नदी को शुद्ध रखना है तो उसकी अविरलता को बचाना होगा. प्रवाह में आने वाली बाधाओं को रोकना होगा. पानी में नालों के माध्यम से गिरने वाले खनिजयुक्त व उर्वर पदार्थों को रोकना होगा. महुला गढ़वल बांध पर रेगुलेटर लगाकर बाढ़ के समय नियंत्रित जल मूल सरयू में छोड़ना होगा. अवैध कब्जों को हटाना होगा. यह सभी कार्य न ही अकेले सरकार कर सकती है और न ही कोई एजेंसी. इसलिए जनजागरूकता फैलाकर लोगों को प्रशिक्षित कर इस अभियान से जोड़ना होगा."
[image error]
इस नदी की हालत देखकर 25 स्वयंसेवकों की टोली के साथ लोक दायित्व और पवन सिंह ने काम करना शुरू किया. उस समय नदी में जलकुंभी और कचरे की भीषण समस्या थी. लगातार छह महीने की मेहनत से भैरव स्थल पर नदी की सूरत बदल गई है. नदी साफ लगने लगी और लोग उसमें कूड़ा फेंकना भी बंद कर चुके हैं.
इस साफ-सफाई में अच्छी बात यह हुई कि नदी तल में तीन पातालतोड़ कुएं भी निकल आए, जिससे नदी को नवजीवन मिल रहा है.
छोटी सरयू का जी जाना यह यकीन दिलाता है कि जो समाज अपने विरासतों को संभालकर रखना चाहता है, जिसके लिए नदी की पूजा कर्मकांड नहीं है, असल में वही समाज जीवित है.
(इस ब्लॉग के लिए तस्वीरें लोकदायित्व संस्था ने मुहैया कराई हैं)

Published on January 29, 2020 07:27
January 22, 2020
पुस्तक समीक्षाः एक थे फूफा में उपन्यास होने की संभावना है
एक थे फूफा, एक फूफा का रसदार ब्यौरा है जो एकदम भदेस किरदार हैं, और अस्पष्ट से ब्यौरों के बीच उनके बचपन से लेकर उनके हैं से थे होने का सफर पूरा होता है. 32 पृष्ठों की इस किताब में उपन्यास होने की संभावना है
पुरातत्व विशेषज्ञ और संस्कृतिकर्मी कई दफा समाज की नब्ज पकड़ने वाला हो तो इसका असर उसकी भाषा पर पड़ना लाजिम सा लगता है. ऐसे ही हैं छत्तीसगढ़ के पुरातत्व विशेषज्ञ और संस्कृतिकर्मी राहुल कुमार सिंह. उनकी पतली सी कितबिया है एक थे फूफा, जो लंबी कहानी या रेखाचित्र सरीखी है और उसमें एक बढ़िया उपन्यास का शानदार कथ्य और शैली तो है ही, संभावना भी है.
बहुत मुमकिन है कि राहुल कुमार सिंह अपने पाठकों की नब्ज टटोल रहे हों.
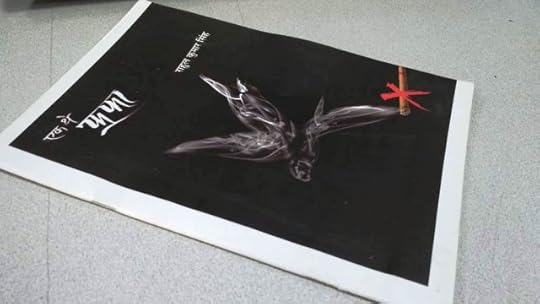 राहुल कुमार सिंह की किताब एक थे फूफा का कवरमहज 32 पृष्ठों और 50 रुपए कीमत वाली यह किताब आप एक ही बैठक में खत्म कर देंगे. वजह इसका आकार नहीं है, वजह है फूफा का रसदार ब्यौरा. फूफा एकदम भदेस किरदार हैं, और अस्पष्ट से ब्यौरों के बीच उनके बचपन से लेकर उनके हैं से थे होने का सफर पूरा होता है. असल में किताब की पहली पंक्ति है, एक थे फूफा (और यही शीर्षक भी है) और साथ ही में यही किताब की आखिरी पंक्ति भी है.
राहुल कुमार सिंह की किताब एक थे फूफा का कवरमहज 32 पृष्ठों और 50 रुपए कीमत वाली यह किताब आप एक ही बैठक में खत्म कर देंगे. वजह इसका आकार नहीं है, वजह है फूफा का रसदार ब्यौरा. फूफा एकदम भदेस किरदार हैं, और अस्पष्ट से ब्यौरों के बीच उनके बचपन से लेकर उनके हैं से थे होने का सफर पूरा होता है. असल में किताब की पहली पंक्ति है, एक थे फूफा (और यही शीर्षक भी है) और साथ ही में यही किताब की आखिरी पंक्ति भी है.
गांवों-कस्बों से ताल्लुक रखने वाले पाठक फूफा जैसे किरदारों से मिले जरूर होंगे और जाहिर है, फूफा से उनका जुड़ाव भी पन्ना-दर-पन्ना बढ़ता जाएगा.
फूफा समझिए गांव के रसिक व्यक्ति हैं जो पंचायत में पंच की कुरसी पर बैठते हैं, आस-पड़ोस की खबर रखते हैं. बचपन से कुशाग्र रहे हैं और दादाजी के बाद जायदाद की साज-संभाल में सत्ता हस्तांतरण पिता को शामिल किए बिना खुद कूद कर ताज हथिया लेते हैं. उनके जगत फूफा होने में कहीं कोई संदेह नहीं.
उनके पास जिंदगी का खासा तजुर्बा है और वह इस कदर है कि बैठे-ठाले जीवंत किस्से गढ़कर 'सच की लय' में सुना दें.
पर फूफा का 'फू-फा' और 'फूं-फा' और इसी तरह के अन्य शाब्दिक खिलवाड़ रोचक है, जिस तरह फूफा का अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना 'जागते रहो' फिल्मप देखकर और पारिवारिक मिल्कियत हाथ में लेना 'लैंडलार्ड' धोती पहनते हुए.
भाषा में रवानगी तो गजब है पर छत्तीसगढ़ी भाषा की वजह से आंचलिकता का यह पुट कुछ अधिक होने पर अखरता भी है. पर, छत्तीसगढ़ के पाठकों को इसमें रस मिलेगा, अपनत्व भी.
एक थे फूफा में बीड़ी (किताब में बिड़ी) का सविस्तार और सप्रसंग विवरण है और इतना बारीक है कि ऐसी मिसाल सिर्फ एक जगह और मिलती है, वह है ज्ञान चतुर्वेदी की बारामासी. पर वहां बुंदेलखंड का ब्यौरा है, यहां छत्तीसगढ़िया तहजीब का. पर, एक थे फूफा में बीड़ी को सजाने और इसको पीने की परंपरा का अगली पीढ़ी तक जाने का ब्यौरा वाकई कमाल है.
कहानी अमूमन एकरेखीय नहीं है. यह कई पाठकों को भटका सकता है पर रसरंजन के शौकीनों के लिए अलग किस्म का शिल्प का मजा साबित हो सकता है. कुल मिलाकरः गागर में सागर, जिसमें एक उपन्यास होने की पूरी संभावना है.
किताबः एक थे फूफा
लेखकः राहुल कुमार सिंह
कीमतः 50 रुपए
प्रकाशकः वैभव प्रकाशन
***
पुरातत्व विशेषज्ञ और संस्कृतिकर्मी कई दफा समाज की नब्ज पकड़ने वाला हो तो इसका असर उसकी भाषा पर पड़ना लाजिम सा लगता है. ऐसे ही हैं छत्तीसगढ़ के पुरातत्व विशेषज्ञ और संस्कृतिकर्मी राहुल कुमार सिंह. उनकी पतली सी कितबिया है एक थे फूफा, जो लंबी कहानी या रेखाचित्र सरीखी है और उसमें एक बढ़िया उपन्यास का शानदार कथ्य और शैली तो है ही, संभावना भी है.
बहुत मुमकिन है कि राहुल कुमार सिंह अपने पाठकों की नब्ज टटोल रहे हों.
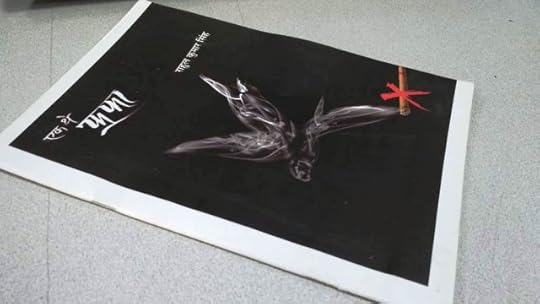 राहुल कुमार सिंह की किताब एक थे फूफा का कवरमहज 32 पृष्ठों और 50 रुपए कीमत वाली यह किताब आप एक ही बैठक में खत्म कर देंगे. वजह इसका आकार नहीं है, वजह है फूफा का रसदार ब्यौरा. फूफा एकदम भदेस किरदार हैं, और अस्पष्ट से ब्यौरों के बीच उनके बचपन से लेकर उनके हैं से थे होने का सफर पूरा होता है. असल में किताब की पहली पंक्ति है, एक थे फूफा (और यही शीर्षक भी है) और साथ ही में यही किताब की आखिरी पंक्ति भी है.
राहुल कुमार सिंह की किताब एक थे फूफा का कवरमहज 32 पृष्ठों और 50 रुपए कीमत वाली यह किताब आप एक ही बैठक में खत्म कर देंगे. वजह इसका आकार नहीं है, वजह है फूफा का रसदार ब्यौरा. फूफा एकदम भदेस किरदार हैं, और अस्पष्ट से ब्यौरों के बीच उनके बचपन से लेकर उनके हैं से थे होने का सफर पूरा होता है. असल में किताब की पहली पंक्ति है, एक थे फूफा (और यही शीर्षक भी है) और साथ ही में यही किताब की आखिरी पंक्ति भी है. गांवों-कस्बों से ताल्लुक रखने वाले पाठक फूफा जैसे किरदारों से मिले जरूर होंगे और जाहिर है, फूफा से उनका जुड़ाव भी पन्ना-दर-पन्ना बढ़ता जाएगा.
फूफा समझिए गांव के रसिक व्यक्ति हैं जो पंचायत में पंच की कुरसी पर बैठते हैं, आस-पड़ोस की खबर रखते हैं. बचपन से कुशाग्र रहे हैं और दादाजी के बाद जायदाद की साज-संभाल में सत्ता हस्तांतरण पिता को शामिल किए बिना खुद कूद कर ताज हथिया लेते हैं. उनके जगत फूफा होने में कहीं कोई संदेह नहीं.
उनके पास जिंदगी का खासा तजुर्बा है और वह इस कदर है कि बैठे-ठाले जीवंत किस्से गढ़कर 'सच की लय' में सुना दें.
पर फूफा का 'फू-फा' और 'फूं-फा' और इसी तरह के अन्य शाब्दिक खिलवाड़ रोचक है, जिस तरह फूफा का अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना 'जागते रहो' फिल्मप देखकर और पारिवारिक मिल्कियत हाथ में लेना 'लैंडलार्ड' धोती पहनते हुए.
भाषा में रवानगी तो गजब है पर छत्तीसगढ़ी भाषा की वजह से आंचलिकता का यह पुट कुछ अधिक होने पर अखरता भी है. पर, छत्तीसगढ़ के पाठकों को इसमें रस मिलेगा, अपनत्व भी.
एक थे फूफा में बीड़ी (किताब में बिड़ी) का सविस्तार और सप्रसंग विवरण है और इतना बारीक है कि ऐसी मिसाल सिर्फ एक जगह और मिलती है, वह है ज्ञान चतुर्वेदी की बारामासी. पर वहां बुंदेलखंड का ब्यौरा है, यहां छत्तीसगढ़िया तहजीब का. पर, एक थे फूफा में बीड़ी को सजाने और इसको पीने की परंपरा का अगली पीढ़ी तक जाने का ब्यौरा वाकई कमाल है.
कहानी अमूमन एकरेखीय नहीं है. यह कई पाठकों को भटका सकता है पर रसरंजन के शौकीनों के लिए अलग किस्म का शिल्प का मजा साबित हो सकता है. कुल मिलाकरः गागर में सागर, जिसमें एक उपन्यास होने की पूरी संभावना है.
किताबः एक थे फूफा
लेखकः राहुल कुमार सिंह
कीमतः 50 रुपए
प्रकाशकः वैभव प्रकाशन
***

Published on January 22, 2020 06:04



