Manjit Thakur's Blog, page 13
September 10, 2019
जीएम फसलों पर दुविधा में फंसी सरकार और किसान
संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि इस बात का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि ये फसलें मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं हैं. हालांकि इससे जीएम फसलों पर पूरी पाबंदी का मामला फिट नहीं बैठता, लेकिन पर्यावरण को लेकर चिंतित लोग और कुछ किसानों के समूह भी, कहते हैं कि सरकार इस मसले पर ऐसे अध्ययनों को नजरअंदाज कर रही है जो जीएम फसलों की पैदावार को सेहत के नुक्सान से जोड़कर देखते हैं
महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के किसान आनुवंशिक इंजीनियरिंग से दुरुस्त किए गए फसलों (जीएम) को उगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनका तर्क है कि इन्हें उगाने में कम लागत आती है, उपज अधिक होती है और इनपर कीटों और खरपतवारों का हमला भी कम होता है. सरकार ने जीएम कॉटन (कपास) की एक प्रजाति को छोड़कर बाकी जीएम फसलों पर पाबंदी लगा रखी है.
लेकिन 19 जुलाई को संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि इस बात का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि ये फसलें मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं हैं. हालांकि इससे जीएम फसलों पर पूरी पाबंदी का मामला फिट नहीं बैठता, लेकिन पर्यावरण को लेकर चिंतित लोग और कुछ किसानों के समूह भी, कहते हैं कि सरकार इस मसले पर ऐसे अध्ययनों को नजरअंदाज कर रही है जो जीएम फसलों की पैदावार को सेहत के नुक्सान से जोड़कर देखते हैं. पर्यावरणविदों का कहना है कि जीएम फूड के इस्तेमाल से कैंसर भी हो सकता है.
अब सवाल यह भी है कि क्या आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार फसलें सेहत की लिए ठीक है या नहीं, इस पर निगाह कौन रखेगा. या खेती में अधिक पैदावार हासिल करने की इच्छा से हम पर्यावरण और सेहत की चिंता को ताक पर रख दें. इसके बरअक्स एक सवाल यह पैदा होता है कि जीएम फसलें बदलते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के दौर में मुफीद साबित हो सकती हैं और इससे बढ़ती आबादी का पेट भी भरा जा सकता है.
असल में, बीटी कॉटन को मंजूरी मिले 17 साल बीत गए हैं. यह एकमात्र जीएम फसल है जिसे भारत में उगाने की कानूनी मंजूरी मिली हुई है. हालांकि बीटी ब्रिंजल (बैंगन) और जीएम सरसों को भी 2017 में सरकारी मंजूरी दी जा चुकी है.
पिछली जुलाई में महाराष्ट्र में 12 किसानों को सरकारी बंदिश का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया था. ये किसान बिना मंजूरी वाले जीएम कपास के बीजों का इस्तेमाल कर रहे थे. इस बाबत, 60 एफआइआर दर्ज किए गए और 1100 किलोग्राम गैरकानूनी बीज भी जब्त किया गया था.
गौरतलब है कि गैरकानूनी जीएम फसलें उगाने पर पांच साल की कैद और 1 लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है.
यहां ध्यान देने वाली बात है कि देश में साल 2017-18 में 62 लाख मीट्रिक टन कपास की पैदावार हुई थी. चीन के बनिस्बत यह उपज काफी अधिक थी. चीन में 60 लाख मीट्रिक टन, अमेरिका में 46 लाख मीट्रिक टन, ब्राजील में 19 लाख मीट्रिक टन और पाकिस्तान में 18 लाख मीट्रिक टन कपास उगाया गया. भारत से 2017-18 में 11.3 लाख मीट्रिक टन कपास का निर्यात किया गया था. निर्यात के मामले में भारत अमेरिका से काफी पीछे है. अमेरिका में 34.5 लाख मीट्रिक टन कपास उस साल निर्यात किया गया था. भारत कपास का आयात करने में पूरी दुनिया में सातवें पायदान पर है जहां 3,70,000 मीट्रिक टन कपास का आयात किया गया.
देश में कपास की खेती का रकबा करीबन 1.17 करोड़ हेक्टेयर है. यानी दुनिया भर में जितनी जमीन में कपास उगाया जाता है उसका 37.5 फीसदी खेत भारत में है. देश के 10 राज्यों के 65 लाख कपास किसान और करीबन 6 करोड़ लोग कपास से जुड़े कामकाज से अपनी रोटी कमाते हैं.
देश के कपास पैदा करने वाले इलाकों में से 15 फीसदी इलाके महाराष्ट, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं जहां गैर-कानूनी जीएम कपास (2017-18 में) उगाई गई थी. इसमें हर हेक्टेयर में करीबन 2800 से 5000 रुपए तक का फायदा हुआ था.
कॉटन एसोशिएसन ऑफ इंडिया के मुताबिक, साल 2010 से 2015 के बीच प्रति हेक्टेयर 73,200 रुपये की औसत आमदनी कपास उगाने वाले किसानों को हुई थी. जबकि इसी अवधि में कपास उगाने का प्रति हेक्टेयर औसत खर्च 63,941 रुपये था.
***
महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के किसान आनुवंशिक इंजीनियरिंग से दुरुस्त किए गए फसलों (जीएम) को उगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनका तर्क है कि इन्हें उगाने में कम लागत आती है, उपज अधिक होती है और इनपर कीटों और खरपतवारों का हमला भी कम होता है. सरकार ने जीएम कॉटन (कपास) की एक प्रजाति को छोड़कर बाकी जीएम फसलों पर पाबंदी लगा रखी है.
लेकिन 19 जुलाई को संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि इस बात का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि ये फसलें मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं हैं. हालांकि इससे जीएम फसलों पर पूरी पाबंदी का मामला फिट नहीं बैठता, लेकिन पर्यावरण को लेकर चिंतित लोग और कुछ किसानों के समूह भी, कहते हैं कि सरकार इस मसले पर ऐसे अध्ययनों को नजरअंदाज कर रही है जो जीएम फसलों की पैदावार को सेहत के नुक्सान से जोड़कर देखते हैं. पर्यावरणविदों का कहना है कि जीएम फूड के इस्तेमाल से कैंसर भी हो सकता है.
अब सवाल यह भी है कि क्या आनुवंशिक इंजीनियरिंग से तैयार फसलें सेहत की लिए ठीक है या नहीं, इस पर निगाह कौन रखेगा. या खेती में अधिक पैदावार हासिल करने की इच्छा से हम पर्यावरण और सेहत की चिंता को ताक पर रख दें. इसके बरअक्स एक सवाल यह पैदा होता है कि जीएम फसलें बदलते पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के दौर में मुफीद साबित हो सकती हैं और इससे बढ़ती आबादी का पेट भी भरा जा सकता है.
असल में, बीटी कॉटन को मंजूरी मिले 17 साल बीत गए हैं. यह एकमात्र जीएम फसल है जिसे भारत में उगाने की कानूनी मंजूरी मिली हुई है. हालांकि बीटी ब्रिंजल (बैंगन) और जीएम सरसों को भी 2017 में सरकारी मंजूरी दी जा चुकी है.
पिछली जुलाई में महाराष्ट्र में 12 किसानों को सरकारी बंदिश का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया था. ये किसान बिना मंजूरी वाले जीएम कपास के बीजों का इस्तेमाल कर रहे थे. इस बाबत, 60 एफआइआर दर्ज किए गए और 1100 किलोग्राम गैरकानूनी बीज भी जब्त किया गया था.
गौरतलब है कि गैरकानूनी जीएम फसलें उगाने पर पांच साल की कैद और 1 लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है.
यहां ध्यान देने वाली बात है कि देश में साल 2017-18 में 62 लाख मीट्रिक टन कपास की पैदावार हुई थी. चीन के बनिस्बत यह उपज काफी अधिक थी. चीन में 60 लाख मीट्रिक टन, अमेरिका में 46 लाख मीट्रिक टन, ब्राजील में 19 लाख मीट्रिक टन और पाकिस्तान में 18 लाख मीट्रिक टन कपास उगाया गया. भारत से 2017-18 में 11.3 लाख मीट्रिक टन कपास का निर्यात किया गया था. निर्यात के मामले में भारत अमेरिका से काफी पीछे है. अमेरिका में 34.5 लाख मीट्रिक टन कपास उस साल निर्यात किया गया था. भारत कपास का आयात करने में पूरी दुनिया में सातवें पायदान पर है जहां 3,70,000 मीट्रिक टन कपास का आयात किया गया.
देश में कपास की खेती का रकबा करीबन 1.17 करोड़ हेक्टेयर है. यानी दुनिया भर में जितनी जमीन में कपास उगाया जाता है उसका 37.5 फीसदी खेत भारत में है. देश के 10 राज्यों के 65 लाख कपास किसान और करीबन 6 करोड़ लोग कपास से जुड़े कामकाज से अपनी रोटी कमाते हैं.
देश के कपास पैदा करने वाले इलाकों में से 15 फीसदी इलाके महाराष्ट, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं जहां गैर-कानूनी जीएम कपास (2017-18 में) उगाई गई थी. इसमें हर हेक्टेयर में करीबन 2800 से 5000 रुपए तक का फायदा हुआ था.
कॉटन एसोशिएसन ऑफ इंडिया के मुताबिक, साल 2010 से 2015 के बीच प्रति हेक्टेयर 73,200 रुपये की औसत आमदनी कपास उगाने वाले किसानों को हुई थी. जबकि इसी अवधि में कपास उगाने का प्रति हेक्टेयर औसत खर्च 63,941 रुपये था.
***

Published on September 10, 2019 04:33
September 9, 2019
पुस्तक समीक्षाः सूखे पत्तों का राग मर्मस्पर्शी गिरहों को आहिस्ते से खोलता है.
गुरमीत बेदी का कथा संग्रह 'सूखे पत्तों का राग' में 14 कहानियां हैं. इस किताब कि कहानियां वर्तमान दौर में लिखी जा रही अधिकांश कहानियों से कुछ अलग एवं उम्दा हैं. कुछेक कहानियों को छोड़ दें तो, सभी कहानियों में लेखक ने पहाड़ों और पर्वतीय राज्य और शहरों का परिवेश बनाये रखा है. पहली कहानी पुल से लेकर आखिरी कहानी चिड़िया तक यह साफ झलकता है.
ज्वारभाटा कहानी में एक विधवा स्त्री के अपने मृत पति के लिए प्रेम का खूबसूरती से वर्णन किया गया है, वहीं पांचवी कहानी खिला रहेगा इंद्रधनुष में एक युवा जोड़े की मर्मस्पर्शी प्रेम कहानी है, जो किसी को भी भावुक कर सकती है.
नींद से बाहर में आज के समाज में सोशल मीडिया से मनुष्य के पारिवारिक जीवन में पड़ते प्रभाव का उल्लेख प्रभावी रुप से किया गया है. एक रात कहानी में एक पुत्र का मां के प्रति लगाव के बारे में तो, हवा में ठिठकी इबारत के माध्यम से समाज में होती बेमेल शादियों के बारे में जिक्र किया गया है.
सूखे पत्तों का राग कहानी में हेम सिंह का भोलापन हंसाता और गुदगुदाता तो है ही इसके साथ-साथ गरीबी में भी हार नहीं मानने की उसकी आदत पाठक के मानस पटल पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं. आखिरी कहानी चिड़िया एक अकेली लड़की की कहानी है जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है. अकेली लड़की के बारे में समाज क्या सोचता है इस बारे में कहानी अपने तरीके से बात कहती है.
इस कहानी के माध्यम से जो सच सामने आता है वह दिल दहला देने के लिए काफी है.
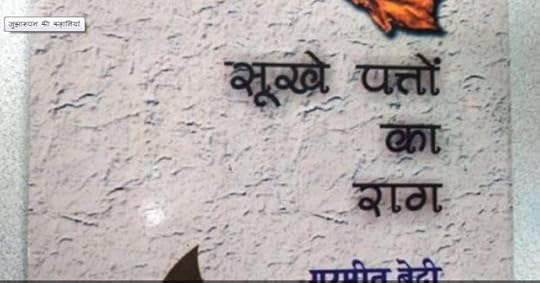
सूखे पत्तों का राग किताब की कुछ कहानियों को छोड़ दें तो ज्यादातर कहानियां मर्मस्पर्शी हैं, जो भावुक करने के साथ-साथ मानस पटल पर एक गहरा असर डालती हैं. कहीं-कहीं इस किताब में मुद्रण की गलतियां भी हैं. कहानी पढ़ने में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी किताब है. चूंकि गुरमीत बेदी की यह दूसरी ही किताब है फिर भी इस संग्रह की प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी.
लेखक गुरमीत बेदी ने अपनी इस किताब में आसान भाषा का चयन किया है, जिससे किसी भी कहानी को समझने में किसी प्रकार कि मुश्किल नहीं होती है. यह हिंदी के पाठकों से इतर दूसरे भाषा-भाषियों तक पहुंच बना पाएगी.
किताबः सूखे पत्तों का राग
लेखकः गुरमीत बेदी
प्रकाशनः भावना प्रकाशन
मूल्यः 250 रुपए
***
ज्वारभाटा कहानी में एक विधवा स्त्री के अपने मृत पति के लिए प्रेम का खूबसूरती से वर्णन किया गया है, वहीं पांचवी कहानी खिला रहेगा इंद्रधनुष में एक युवा जोड़े की मर्मस्पर्शी प्रेम कहानी है, जो किसी को भी भावुक कर सकती है.
नींद से बाहर में आज के समाज में सोशल मीडिया से मनुष्य के पारिवारिक जीवन में पड़ते प्रभाव का उल्लेख प्रभावी रुप से किया गया है. एक रात कहानी में एक पुत्र का मां के प्रति लगाव के बारे में तो, हवा में ठिठकी इबारत के माध्यम से समाज में होती बेमेल शादियों के बारे में जिक्र किया गया है.
सूखे पत्तों का राग कहानी में हेम सिंह का भोलापन हंसाता और गुदगुदाता तो है ही इसके साथ-साथ गरीबी में भी हार नहीं मानने की उसकी आदत पाठक के मानस पटल पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं. आखिरी कहानी चिड़िया एक अकेली लड़की की कहानी है जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है. अकेली लड़की के बारे में समाज क्या सोचता है इस बारे में कहानी अपने तरीके से बात कहती है.
इस कहानी के माध्यम से जो सच सामने आता है वह दिल दहला देने के लिए काफी है.
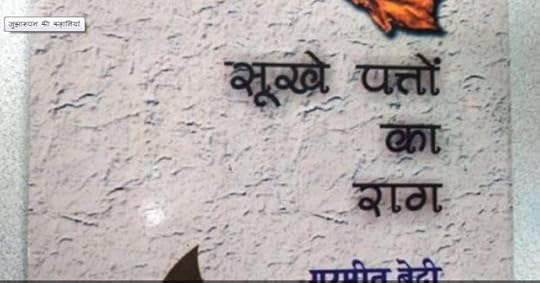
सूखे पत्तों का राग किताब की कुछ कहानियों को छोड़ दें तो ज्यादातर कहानियां मर्मस्पर्शी हैं, जो भावुक करने के साथ-साथ मानस पटल पर एक गहरा असर डालती हैं. कहीं-कहीं इस किताब में मुद्रण की गलतियां भी हैं. कहानी पढ़ने में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी किताब है. चूंकि गुरमीत बेदी की यह दूसरी ही किताब है फिर भी इस संग्रह की प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी.
लेखक गुरमीत बेदी ने अपनी इस किताब में आसान भाषा का चयन किया है, जिससे किसी भी कहानी को समझने में किसी प्रकार कि मुश्किल नहीं होती है. यह हिंदी के पाठकों से इतर दूसरे भाषा-भाषियों तक पहुंच बना पाएगी.
किताबः सूखे पत्तों का राग
लेखकः गुरमीत बेदी
प्रकाशनः भावना प्रकाशन
मूल्यः 250 रुपए
***

Published on September 09, 2019 01:56
September 4, 2019
नदीसूत्रः बेतवा नदी का राख से घुटता दम
बेतवा देश की 38 सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है. इसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 250 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से भी अधिक है. यह पानी में प्रदूषण का वह स्तर है जिसे सीवेज ट्रीटमेंट में भेजे जाने की जरूरत है. बेतवा अकाल मौत की तरफ बढ़ रही है
बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है. खेती-बाड़ी, पीने से लेकर उद्योग-धंधे सब बेतवा के भरोसे चलता है यहां. बेतवा नहीं तो कुछ नहीं. इसकी अहमियत कुछ ऐसे समझी जा सकती है कि बुंदेलखंड को सूखे से निजात दिलाने के लिए नदी जोड़ने की परियोजना में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है. या कम से कम यह मान लेना चाहिए कि सरकार की सदिच्छा दोनों नदियों को जोड़ने की है.
पर, अगर कभी आप उत्तर प्रदेश के झांसी जिला मुख्यालय से कानपुर हाइवे पर 25 किलोमीटर चलें और परीछा थर्मल पॉवर प्लांट और बेतवा नदी के बीच स्थित रिछौरा और परीछा गांव जाएं तब जाकर आपको पता चलेगा कि विकास की कितनी कीमत खुद नदी और उसके किनारे रहने वाले लोग अदा कर रहे हैं. इन गांवों में आपको एक भी मवेशी दिखाई नहीं पड़ेगा. रिछौरा गांव के 30 वर्षीय अमर सिंह अहिरवार पांच वर्ष पहले दो गाय खरीदकर लाए थे. पर कुछ ही दिन बाद उनकी गायें बीमार रहने लगीं. डॉक्टरों से पता चला कि बेतवा नदी का प्रदूषित पानी पीने से गायों के पेट में राख जमा हो रही है.
कुछ ही दिनों में अमर की दोनों गायें चल बसीं. बुंदेलखंड पैकेज के तहत अमर सिंह को जो तीन बकरियां मिली थीं, उनमें से आखिरी ने पिछले हफ्ते दम तोड़ दिया. बेतवा नदी के किनारे फैली राख को दिखाते हुए अमर सिंह बताते हैं कि पॉवर प्लांट लगने से गांव में बिजली तो मिली लेकिन प्लांट की राख ने बेतवा नदी की सांसें छीन ली हैं.
झांसी-कानपुर हाइवे पर जैसे-जैसे परीछा पॉवर प्लांट के नजदीक पहुंचते हैं, तापघर की ओर जाने वाली सड़कें राख से पटी नजर आती हैं. मकानों की छतों पर राख का साम्राज्य है. हाल में हुई बारिश ने कुछ राहत दी है. छतों पर जमी कोयले की राख को बारिश का पानी बहा तो ले गया पर इसने गांव के किनारे बह रही बेतवा को और "विषैला'' करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
इस राख ने बिजलीघरों के इर्द-गिर्द बसे इलाकों में लोगों का जीवन नारकीय बना दिया है.
परीछा थर्मल पॉवर प्लांट के ठीक पीछे स्थित रिछौरा और परीछा गांवों में पसरा सन्नाटा अलग किस्सा बताता है. 30 वर्ष पहले दस हजार से अधिक आबादी वाले इन गांवों से आधे से ज्यादा लोग पलायन कर गए हैं.
पानी के लिए तरस रहे बुंदेलखंड में नदी का पानी ही जहरीला हो जाए तो इनके किनारे बसे गांवों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. वर्ष 1984 में काम शुरू करने वाले परीछा थर्मल पॉवर प्लांट में अब छह इकाइयां हैं जहां रोजाना 16,000 मीट्रिक टन कोयले की खपत होती है और रोजाना 14,000 मीट्रिक टन गीली राख निकलती है जिसे डैम में भेजा जाता है.
परीछा थर्मल पॉवर प्लांट के एक अधिकारी बताते हैं, "210 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयों से निकलने वाली राख के लिए बने दोनों डैम भर चुके हैं जबकि 110 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयों के लिए बने डैम का एक कंपार्टमेंट भर चुका है. अब राख दूसरे कंपार्टमेंट में डाली जा रही है. इसमें भी छह महीने तक ही राख रखने की व्यवस्था है.''
बेतवा में मिलाई जा रही राख से जहरीले हुए पानी ने पिछले दो साल में परीछा और रिछौरा गांवों में 50 से ज्यादा पालतू पशुओं की जान ले ली है. परीछा गांव के जगदीश परिहार बताते हैं, "बेतवा में केमिकल वाली राख मिलने का असर गांव के हैंडपंपों पर भी पड़ा है.
अब इन हैंडपंपों से भी प्रदूषित पानी ही मिलता है.'' रिछौरा गांव के प्रधान कुलदीप सिंह बताते हैं, "बेतवा नदी की तलहटी में 20 से 25 फुट तक राख जमा हो जाने से नदी छिछली हो गई है. जरा-सा पानी बढऩे पर यह गांव में पहुंच जाता है.''
नदी पर बना परीछा बांध भी छिछला हो गया है. झांसी में सिंचाई विभाग में तैनात इंजीनियर श्रीशचंद बताते हैं, "बांध की तलहटी में राख जमने से इसकी भंडारण क्षमता काफी कम हो गई है जिससे आने वाले दिनों में सिंचाई पर संकट हो सकता है.'' परीछा बिजलीघर की राख को ठिकाने लगाने के लिए एक नया ऐश डैम बनाने की भी योजना है. इसके लिए प्लांट से सटे गांव महेबा, गुलारा और मुराटा की 572 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जानी थी. किसानों को जमीन का मुआवजा देने के लिए "सेंट्रल पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन'' से 195 करोड़ रुपए का ऋण भी परीछा थर्मल पॉवर प्लांट को मिल गया.
लेकिन प्रशासन को पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं मिल पाया क्योंकि नियमानुसार डैम की जमीन को नेशनल हाइवे और नदी से 500 मीटर दूर होना चाहिए. लेकिन बेतवा नदी और हाइवे के बीच की दूरी ही 500 मीटर से कम है और इसी के बीच में अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले नवंबर में बेतवा नदी की पानी की जांच की और पाया कि बेतवा के पानी में टोटल डिजॉल्वड सॉलिड (टीडीएस) की मात्रा 700 से 900 पॉइंट प्रति लीटर और टोटल हार्डनेस (टीएच) 150 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गया है.
वैसे इससे पहले मार्च, 2018 में पर्यावरण मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि बेतवा देश की 38 सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है. इसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 250 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से भी अधिक है.मंत्रालय ने माना है कि यह पानी में प्रदूषण का वह स्तर है जिसे सीवेज ट्रीटमेंट में भेजे जाने की जरूरत है.
फिलहाल, आप हर घर नल योजना के बारे में सोच-सोचकर पुलकित होइए कि गरीब से गरीब आदमी के किचन में सीधे झर्र से नल का पानी आएगा. पर, इस शोशेबाजी से थोड़ी मोहलत मिले तो सोचिएगा कि झर्र से आने के लिए पानी होना बहुत जरूरी होगा. और पानी का स्रोत रही नदियां तो अकाल मौत का शिकार हो रही हैं.
***
बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है. खेती-बाड़ी, पीने से लेकर उद्योग-धंधे सब बेतवा के भरोसे चलता है यहां. बेतवा नहीं तो कुछ नहीं. इसकी अहमियत कुछ ऐसे समझी जा सकती है कि बुंदेलखंड को सूखे से निजात दिलाने के लिए नदी जोड़ने की परियोजना में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है. या कम से कम यह मान लेना चाहिए कि सरकार की सदिच्छा दोनों नदियों को जोड़ने की है.
पर, अगर कभी आप उत्तर प्रदेश के झांसी जिला मुख्यालय से कानपुर हाइवे पर 25 किलोमीटर चलें और परीछा थर्मल पॉवर प्लांट और बेतवा नदी के बीच स्थित रिछौरा और परीछा गांव जाएं तब जाकर आपको पता चलेगा कि विकास की कितनी कीमत खुद नदी और उसके किनारे रहने वाले लोग अदा कर रहे हैं. इन गांवों में आपको एक भी मवेशी दिखाई नहीं पड़ेगा. रिछौरा गांव के 30 वर्षीय अमर सिंह अहिरवार पांच वर्ष पहले दो गाय खरीदकर लाए थे. पर कुछ ही दिन बाद उनकी गायें बीमार रहने लगीं. डॉक्टरों से पता चला कि बेतवा नदी का प्रदूषित पानी पीने से गायों के पेट में राख जमा हो रही है.
कुछ ही दिनों में अमर की दोनों गायें चल बसीं. बुंदेलखंड पैकेज के तहत अमर सिंह को जो तीन बकरियां मिली थीं, उनमें से आखिरी ने पिछले हफ्ते दम तोड़ दिया. बेतवा नदी के किनारे फैली राख को दिखाते हुए अमर सिंह बताते हैं कि पॉवर प्लांट लगने से गांव में बिजली तो मिली लेकिन प्लांट की राख ने बेतवा नदी की सांसें छीन ली हैं.
झांसी-कानपुर हाइवे पर जैसे-जैसे परीछा पॉवर प्लांट के नजदीक पहुंचते हैं, तापघर की ओर जाने वाली सड़कें राख से पटी नजर आती हैं. मकानों की छतों पर राख का साम्राज्य है. हाल में हुई बारिश ने कुछ राहत दी है. छतों पर जमी कोयले की राख को बारिश का पानी बहा तो ले गया पर इसने गांव के किनारे बह रही बेतवा को और "विषैला'' करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
इस राख ने बिजलीघरों के इर्द-गिर्द बसे इलाकों में लोगों का जीवन नारकीय बना दिया है.
परीछा थर्मल पॉवर प्लांट के ठीक पीछे स्थित रिछौरा और परीछा गांवों में पसरा सन्नाटा अलग किस्सा बताता है. 30 वर्ष पहले दस हजार से अधिक आबादी वाले इन गांवों से आधे से ज्यादा लोग पलायन कर गए हैं.
पानी के लिए तरस रहे बुंदेलखंड में नदी का पानी ही जहरीला हो जाए तो इनके किनारे बसे गांवों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है. वर्ष 1984 में काम शुरू करने वाले परीछा थर्मल पॉवर प्लांट में अब छह इकाइयां हैं जहां रोजाना 16,000 मीट्रिक टन कोयले की खपत होती है और रोजाना 14,000 मीट्रिक टन गीली राख निकलती है जिसे डैम में भेजा जाता है.
परीछा थर्मल पॉवर प्लांट के एक अधिकारी बताते हैं, "210 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयों से निकलने वाली राख के लिए बने दोनों डैम भर चुके हैं जबकि 110 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयों के लिए बने डैम का एक कंपार्टमेंट भर चुका है. अब राख दूसरे कंपार्टमेंट में डाली जा रही है. इसमें भी छह महीने तक ही राख रखने की व्यवस्था है.''
बेतवा में मिलाई जा रही राख से जहरीले हुए पानी ने पिछले दो साल में परीछा और रिछौरा गांवों में 50 से ज्यादा पालतू पशुओं की जान ले ली है. परीछा गांव के जगदीश परिहार बताते हैं, "बेतवा में केमिकल वाली राख मिलने का असर गांव के हैंडपंपों पर भी पड़ा है.
अब इन हैंडपंपों से भी प्रदूषित पानी ही मिलता है.'' रिछौरा गांव के प्रधान कुलदीप सिंह बताते हैं, "बेतवा नदी की तलहटी में 20 से 25 फुट तक राख जमा हो जाने से नदी छिछली हो गई है. जरा-सा पानी बढऩे पर यह गांव में पहुंच जाता है.''
नदी पर बना परीछा बांध भी छिछला हो गया है. झांसी में सिंचाई विभाग में तैनात इंजीनियर श्रीशचंद बताते हैं, "बांध की तलहटी में राख जमने से इसकी भंडारण क्षमता काफी कम हो गई है जिससे आने वाले दिनों में सिंचाई पर संकट हो सकता है.'' परीछा बिजलीघर की राख को ठिकाने लगाने के लिए एक नया ऐश डैम बनाने की भी योजना है. इसके लिए प्लांट से सटे गांव महेबा, गुलारा और मुराटा की 572 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जानी थी. किसानों को जमीन का मुआवजा देने के लिए "सेंट्रल पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन'' से 195 करोड़ रुपए का ऋण भी परीछा थर्मल पॉवर प्लांट को मिल गया.
लेकिन प्रशासन को पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं मिल पाया क्योंकि नियमानुसार डैम की जमीन को नेशनल हाइवे और नदी से 500 मीटर दूर होना चाहिए. लेकिन बेतवा नदी और हाइवे के बीच की दूरी ही 500 मीटर से कम है और इसी के बीच में अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले नवंबर में बेतवा नदी की पानी की जांच की और पाया कि बेतवा के पानी में टोटल डिजॉल्वड सॉलिड (टीडीएस) की मात्रा 700 से 900 पॉइंट प्रति लीटर और टोटल हार्डनेस (टीएच) 150 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गया है.
वैसे इससे पहले मार्च, 2018 में पर्यावरण मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि बेतवा देश की 38 सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है. इसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 250 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से भी अधिक है.मंत्रालय ने माना है कि यह पानी में प्रदूषण का वह स्तर है जिसे सीवेज ट्रीटमेंट में भेजे जाने की जरूरत है.
फिलहाल, आप हर घर नल योजना के बारे में सोच-सोचकर पुलकित होइए कि गरीब से गरीब आदमी के किचन में सीधे झर्र से नल का पानी आएगा. पर, इस शोशेबाजी से थोड़ी मोहलत मिले तो सोचिएगा कि झर्र से आने के लिए पानी होना बहुत जरूरी होगा. और पानी का स्रोत रही नदियां तो अकाल मौत का शिकार हो रही हैं.
***

Published on September 04, 2019 06:58
September 3, 2019
बूम बूम बूमराह
भारत ने वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में हरा दिया. पहला टेस्ट मैच 318 रनों के अंतर से हराना बड़ी बात है. पर बड़ी बात यह भी है कि भारत ने दूसरा टेस्ट मैच भी 257 रनों से जीत लिया. पर यह ऐसी खबर है जिसे आपने सुबह से पढ़-सुन लिया होगा.
पर असली खबर हैं भारत के यॉर्करमैन जसप्रीत बूमराह. एंटीगा टेस्ट में बूमराह ने महज 7 रन खर्च करके 5 विकेट उड़ा लिए. पहली पारी में भले ही इशांत शर्मा जलवाफरोश हुए हों पर दूसरी पारी में भारत का हाथ ऊंचा किया बूमराह ने ही. दूसरे जमैका टेस्ट में बूमराह ने पहली पारी में हैटट्रिक समेत 6 और दूसरी पारी में एक विकेट लिया.
बुमराह टेस्ट में हैटट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने, जबकि कैरेबियाई धरती पर यह कारनामा करने वाले वह पहले भारतीय गेंदबाज हैं. दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैटट्रिक सहित 6 विकेट झटके, वह भी सिर्फ 16 रन देकर. बुमराह ने यह कारनामा पारी के 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर डारेन ब्रावो (4), तीसरी गेंद पर शाहमार ब्रूक्स (0) और चौथी गेंद पर रोस्टन चेज (0) को आउट कर किया.
इस तरह जसप्रीत बुमराह टेस्ट में हैटट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने, जबकि वेस्ट इंडीज में हैटट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने.
बुमराह से पहले भारत के लिए हरभजन सिंह (रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न) ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में हैटट्रिक ली थी. वह टेस्ट में हैटट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने थे. उनके बाद यह कारनामा तेज गेंदबाज इरफान पठान (सलमान बट्ट, यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ) ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ किया था. यह मैच कराची में खेला गया था. ओवरऑल यह टेस्ट क्रिकेट की 44वीं हैटट्रिक है.
कम रन देकर ज्यादा से ज्यादा विकेट लेना किसी भी गेंदबाज का सपना होता है. एंटीगा में कारनामा करना जसप्रीत बूमराह के लिए कोई पहली बार का मसला नहीं था. बुमराह सबसे कम रन देकर टेस्ट की एक पारी में 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए. बुमराह से पहले यह रिकॉर्ड वेंकटपति राजू के नाम था, जिन्होंने 1990 में श्रीलंका के खिलाफ चंडीगढ़ में 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे.
टेस्ट मैच की एक पारी में जसप्रीत बूमराह ने ऐसा कारनामा चौथी बार किया है जब उन्होंने पांच या इससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं. उनको यह उपलब्धि चार अलग-अलग दौरों में हासिल हुई है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अब वेस्टइंडीज दौरे पर यह उपलब्धि हासिल की. बुमराह भारत ही नहीं, एशिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जो इन चार देशों के हर दौरे में पांच विकेट लिए हैं.
जरा बूमराह की गेंदबाजी देखिए, बगूले की तरह उड़ान भरते और रन अप लेते समय उनकी देहभाषा देखिए. किसी भी तेज़ गेंदबाज की बनिस्बत उनका रन अप छोटा है पर तेजी कम नहीं. और जितनी तेजी है उससे भी अधिक सटीक गेंदे डालते हैं. खासकर यॉर्कर.
अभी भारत की गेंदबाजी में धार आई है. मोहम्मद शमी भले ही पारंपारकि अंदाज में गेंदबाजी करते हैं लेकिन वह एक छोर पर बल्लेबाजों की नकेल डाले रहते हैं. जाहिर है, उसके बाद बूमराह अपनी नेज़े जैसी तीखी गेंदों से बल्लेबाज को पवेलियन भेजने पर उतारू रहते हैं. इशांत की स्विंग और जाडेजा की स्पिन अपने तरीके से रन रोके रहते हैं.
एक दफा पांच विकेट ले लेना शायद उतनी बड़ी बात नहीं, पर कप्तान अगर मुश्किल घड़ी में बारंबार बूमराह को ही गेंद पकड़ाए तो मैदान में उनकी भूमिका की अहमियत साफ हो जाती है.
बूमराह पर विश्वास इसलिए भी है कि वह सिर्फ रफ्तार की सौदागरी नहीं करते. गेंदें सटीक भी डालते हैं और हवा में उसे घुमाते भी हैं. अमूमन उनकी गेंद टप्पा खाने के बाद कांटा भी बदलती है. विकेट भारतीय परिस्थितियों का हो या फिर विदेशी सरजमीं पर भारी मौसम वाला, बूमराह ने लाल और सफेद दोनों गेंदों को अपने मन मुताबिक स्पीड और घुमाव दिया है.
पर बूमराह ने क्रिकेट के तीनों फॉरमेट में अपनी गेंदबाजी से चमत्कृत किया है. आऩे वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट उन पर अपनी निगाह बनाए रखेगा बल्कि आंख मूंदकर भरोसा भी करता रहेगा.
***
पर असली खबर हैं भारत के यॉर्करमैन जसप्रीत बूमराह. एंटीगा टेस्ट में बूमराह ने महज 7 रन खर्च करके 5 विकेट उड़ा लिए. पहली पारी में भले ही इशांत शर्मा जलवाफरोश हुए हों पर दूसरी पारी में भारत का हाथ ऊंचा किया बूमराह ने ही. दूसरे जमैका टेस्ट में बूमराह ने पहली पारी में हैटट्रिक समेत 6 और दूसरी पारी में एक विकेट लिया.
बुमराह टेस्ट में हैटट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने, जबकि कैरेबियाई धरती पर यह कारनामा करने वाले वह पहले भारतीय गेंदबाज हैं. दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैटट्रिक सहित 6 विकेट झटके, वह भी सिर्फ 16 रन देकर. बुमराह ने यह कारनामा पारी के 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर डारेन ब्रावो (4), तीसरी गेंद पर शाहमार ब्रूक्स (0) और चौथी गेंद पर रोस्टन चेज (0) को आउट कर किया.
इस तरह जसप्रीत बुमराह टेस्ट में हैटट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने, जबकि वेस्ट इंडीज में हैटट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने.
बुमराह से पहले भारत के लिए हरभजन सिंह (रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न) ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में हैटट्रिक ली थी. वह टेस्ट में हैटट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बने थे. उनके बाद यह कारनामा तेज गेंदबाज इरफान पठान (सलमान बट्ट, यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ) ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ किया था. यह मैच कराची में खेला गया था. ओवरऑल यह टेस्ट क्रिकेट की 44वीं हैटट्रिक है.
कम रन देकर ज्यादा से ज्यादा विकेट लेना किसी भी गेंदबाज का सपना होता है. एंटीगा में कारनामा करना जसप्रीत बूमराह के लिए कोई पहली बार का मसला नहीं था. बुमराह सबसे कम रन देकर टेस्ट की एक पारी में 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए. बुमराह से पहले यह रिकॉर्ड वेंकटपति राजू के नाम था, जिन्होंने 1990 में श्रीलंका के खिलाफ चंडीगढ़ में 12 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे.
टेस्ट मैच की एक पारी में जसप्रीत बूमराह ने ऐसा कारनामा चौथी बार किया है जब उन्होंने पांच या इससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं. उनको यह उपलब्धि चार अलग-अलग दौरों में हासिल हुई है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अब वेस्टइंडीज दौरे पर यह उपलब्धि हासिल की. बुमराह भारत ही नहीं, एशिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जो इन चार देशों के हर दौरे में पांच विकेट लिए हैं.
जरा बूमराह की गेंदबाजी देखिए, बगूले की तरह उड़ान भरते और रन अप लेते समय उनकी देहभाषा देखिए. किसी भी तेज़ गेंदबाज की बनिस्बत उनका रन अप छोटा है पर तेजी कम नहीं. और जितनी तेजी है उससे भी अधिक सटीक गेंदे डालते हैं. खासकर यॉर्कर.
अभी भारत की गेंदबाजी में धार आई है. मोहम्मद शमी भले ही पारंपारकि अंदाज में गेंदबाजी करते हैं लेकिन वह एक छोर पर बल्लेबाजों की नकेल डाले रहते हैं. जाहिर है, उसके बाद बूमराह अपनी नेज़े जैसी तीखी गेंदों से बल्लेबाज को पवेलियन भेजने पर उतारू रहते हैं. इशांत की स्विंग और जाडेजा की स्पिन अपने तरीके से रन रोके रहते हैं.
एक दफा पांच विकेट ले लेना शायद उतनी बड़ी बात नहीं, पर कप्तान अगर मुश्किल घड़ी में बारंबार बूमराह को ही गेंद पकड़ाए तो मैदान में उनकी भूमिका की अहमियत साफ हो जाती है.
बूमराह पर विश्वास इसलिए भी है कि वह सिर्फ रफ्तार की सौदागरी नहीं करते. गेंदें सटीक भी डालते हैं और हवा में उसे घुमाते भी हैं. अमूमन उनकी गेंद टप्पा खाने के बाद कांटा भी बदलती है. विकेट भारतीय परिस्थितियों का हो या फिर विदेशी सरजमीं पर भारी मौसम वाला, बूमराह ने लाल और सफेद दोनों गेंदों को अपने मन मुताबिक स्पीड और घुमाव दिया है.
पर बूमराह ने क्रिकेट के तीनों फॉरमेट में अपनी गेंदबाजी से चमत्कृत किया है. आऩे वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट उन पर अपनी निगाह बनाए रखेगा बल्कि आंख मूंदकर भरोसा भी करता रहेगा.
***

Published on September 03, 2019 07:44
September 2, 2019
हिंदू होने का अर्थ: आस्था, नई दुनिया और उम्दा किताब
हिंदोल सेनगुप्ता की बेहद सामयिक और प्रासंगिक किताब, हिंदू होने का अर्थ हिंदूपन की बात करती है हिंदुत्व की नहीं. मौजूदा वक्त में जब धर्म पर बात करना, धर्म को लेकर अपनी बात रखना मुश्किल हो गया है, तब, खासकर हिंदू धर्म की बात करते ही मामला संजीदा होने लग जाता है. यह किताब निजी तजुर्बों की किताब है.
नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता के लिए चुने जाने के ठीक एक दिन बाद जब एक किताब देर से सही आपके हाथ आए, जिसका शीर्षक 'हिंदू होने का अर्थ' हो, तो उस ओर ध्यान जाना लाजिमी है. देश भर में जिस लहर के साथ मोदी जीतकर आए हैं, वैसे में कई लोग हिंदुत्व के और अधिक आक्रामक होने की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं. पर असल में हिंदोल सेनगुप्ता की यह किताब हिंदुत्व को नए नजरिए से देखने का कोण मुहैया कराती है.
एक भाव यह है कि हिंदुत्व सार्वभौमिकता का संदेश देता है. दूसरा भाव यह भी है कि हिंदुत्व एक प्रकार के उन्माद का नाम है जो मुसलमानों को निशाना बनाता है. ऐसा विरोधाभास अकारण नहीं है. फिर भी, मैं हिंदुत्व का अर्थ गुणात्मक पद के रूप में लगाता हूं. इसका मतलब ''हिंदुपन" है, हिंदू धर्म नहीं. हालांकि हिंदू धर्म उसमें शामिल है.
 हिंदोल सेनगुप्ता की किताब हिंदू होने का अर्थ हिंदूपन को हिंदुत्व से अलग करती है
हिंदोल सेनगुप्ता की किताब हिंदू होने का अर्थ हिंदूपन को हिंदुत्व से अलग करती है
ऐसे में सेनगुप्ता की यह किताब बेहद प्रासंगिक किताब है, क्योंकि मौजूदा वक्त में धर्म पर बात करना, धर्म को लेकर अपनी बात रखना मुश्किल हो गया है. खासकर हिंदू धर्म की बात करते ही मामला संजीदा होने लग जाता है. किताब में कई सारे अध्याय हैं और सेनगुप्ता स्थापित करते हैं कि ईश्वरत्व सजीव और निर्जीव सबमें और सब ओर व्याप्त है, यह प्रज्ञा और आस्था का संगम है. मनुष्य प्रकृति का ही हिस्सा है, उसका विजेता नहीं क्योंकि संसार मानव के उपभोग के लिए ही नहीं रचा गया है (इसका अर्थ है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों और वनस्पतियों यहां तक कि भूमि, जलस्रोतों और वायुमंडल के भी अपने अधिकार हैं.)
हिंदोल का लेखन हिंदूपन के नए परिभाषाओं से रूबरू कराती है. किताब के कवर पर ही लिखा है 'प्राचीन आस्था, नई दुनिया और आप'. जाहिर है कि लेखक इतिहास की भूलभुलैया की बजाए मौजूदा वक्त में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के वास्तविक मर्म को सहज-सरल तरीकों से बताने और जताने की कोशिश कर रहा है.
इस किताब में सेनगुप्ता के निजी तजुर्बे हैं और नए जमाने की सोच भी है. किताब बनारस के मंदिरों से लेकर जटिल विषयों तक सहजता से बताती है. किताब का पहला अध्याय है हिंदुओं के बारे में कैसे लिखा जाए? यह सवाल बेहद मौजूं है और ऐसा लगता है कि इस प्रश्न ने खुद सेनगुप्ता को काफी परेशान किया होगा. दूसरा अध्याय पूछता है हिंदू कौन है और तीसरा, क्या चीज है जो आपको हिंदू बनाती है. ये ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो घोर आक्रामक और बेचैन हिंदुत्व के झंडाबरदारों और आंख मूंदकर हिंदू शब्द से ही घृणा करने वालों के लिए ही हैं और उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए.
पर इस किताब का सातवां अध्याय वाकई थोड़े कम रिसर्च के आधार पर लिखा गया है पर जो मेरा पसंदीदा विषय है, जिसका शीर्षक है क्या हिंदू होने का अर्थ आपका शाकाहारी होना है? जो लोग इस आधार पर हिंदूपन को पारिभाषित करते हैं वो सिरे से गलत हैं. पर इस अध्याय में सेनगुप्ता पूरी तरह चूक गए हैं. वह मांसाहार के बाद सीधे गोवध पर आते हैं और उन्हें लगता है कि मांसाहार का अर्थ महज गोमांस भक्षण ही है. मछली खाना भी मांसाहार है और हिंदू जीवन शैली का हिस्सा है यह शायद सेनगुप्ता भूल गए हैं. दूसरी तरफ, बंगाल, असम बिहार जैसे इलाके हैं जहां मांसाहार, खासकर मछली खाने का रिवाज है. तो अगर सेनगुप्ता इनकी तरफ थोड़ा इशारा कर पाते तो किताब गहरी बन जाती.
फिर भी, हिंदू धर्म पर व्यापक और अलग नजरिए वाले इस काम के लिए सेनगुप्ता वाकई बधाई के हकदार हैं. वो भी बिना किसी अनावश्यक टीका-टिप्पणी के वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अपनी बात कह जाते हैं. मदन सोनी ने किताब में ऊंचे दरजे का अनुवाद किया है.
किताबः हिंदू होने का अर्थः प्राचीन आस्था, नई दुनिया और आप
पृष्ठ संख्याः 182
कीमतः 250 रुपए
प्रकाशकः मंजुल पब्लिशिंग हाउस
***
नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता के लिए चुने जाने के ठीक एक दिन बाद जब एक किताब देर से सही आपके हाथ आए, जिसका शीर्षक 'हिंदू होने का अर्थ' हो, तो उस ओर ध्यान जाना लाजिमी है. देश भर में जिस लहर के साथ मोदी जीतकर आए हैं, वैसे में कई लोग हिंदुत्व के और अधिक आक्रामक होने की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं. पर असल में हिंदोल सेनगुप्ता की यह किताब हिंदुत्व को नए नजरिए से देखने का कोण मुहैया कराती है.
एक भाव यह है कि हिंदुत्व सार्वभौमिकता का संदेश देता है. दूसरा भाव यह भी है कि हिंदुत्व एक प्रकार के उन्माद का नाम है जो मुसलमानों को निशाना बनाता है. ऐसा विरोधाभास अकारण नहीं है. फिर भी, मैं हिंदुत्व का अर्थ गुणात्मक पद के रूप में लगाता हूं. इसका मतलब ''हिंदुपन" है, हिंदू धर्म नहीं. हालांकि हिंदू धर्म उसमें शामिल है.
 हिंदोल सेनगुप्ता की किताब हिंदू होने का अर्थ हिंदूपन को हिंदुत्व से अलग करती है
हिंदोल सेनगुप्ता की किताब हिंदू होने का अर्थ हिंदूपन को हिंदुत्व से अलग करती हैऐसे में सेनगुप्ता की यह किताब बेहद प्रासंगिक किताब है, क्योंकि मौजूदा वक्त में धर्म पर बात करना, धर्म को लेकर अपनी बात रखना मुश्किल हो गया है. खासकर हिंदू धर्म की बात करते ही मामला संजीदा होने लग जाता है. किताब में कई सारे अध्याय हैं और सेनगुप्ता स्थापित करते हैं कि ईश्वरत्व सजीव और निर्जीव सबमें और सब ओर व्याप्त है, यह प्रज्ञा और आस्था का संगम है. मनुष्य प्रकृति का ही हिस्सा है, उसका विजेता नहीं क्योंकि संसार मानव के उपभोग के लिए ही नहीं रचा गया है (इसका अर्थ है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों और वनस्पतियों यहां तक कि भूमि, जलस्रोतों और वायुमंडल के भी अपने अधिकार हैं.)
हिंदोल का लेखन हिंदूपन के नए परिभाषाओं से रूबरू कराती है. किताब के कवर पर ही लिखा है 'प्राचीन आस्था, नई दुनिया और आप'. जाहिर है कि लेखक इतिहास की भूलभुलैया की बजाए मौजूदा वक्त में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के वास्तविक मर्म को सहज-सरल तरीकों से बताने और जताने की कोशिश कर रहा है.
इस किताब में सेनगुप्ता के निजी तजुर्बे हैं और नए जमाने की सोच भी है. किताब बनारस के मंदिरों से लेकर जटिल विषयों तक सहजता से बताती है. किताब का पहला अध्याय है हिंदुओं के बारे में कैसे लिखा जाए? यह सवाल बेहद मौजूं है और ऐसा लगता है कि इस प्रश्न ने खुद सेनगुप्ता को काफी परेशान किया होगा. दूसरा अध्याय पूछता है हिंदू कौन है और तीसरा, क्या चीज है जो आपको हिंदू बनाती है. ये ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो घोर आक्रामक और बेचैन हिंदुत्व के झंडाबरदारों और आंख मूंदकर हिंदू शब्द से ही घृणा करने वालों के लिए ही हैं और उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए.
पर इस किताब का सातवां अध्याय वाकई थोड़े कम रिसर्च के आधार पर लिखा गया है पर जो मेरा पसंदीदा विषय है, जिसका शीर्षक है क्या हिंदू होने का अर्थ आपका शाकाहारी होना है? जो लोग इस आधार पर हिंदूपन को पारिभाषित करते हैं वो सिरे से गलत हैं. पर इस अध्याय में सेनगुप्ता पूरी तरह चूक गए हैं. वह मांसाहार के बाद सीधे गोवध पर आते हैं और उन्हें लगता है कि मांसाहार का अर्थ महज गोमांस भक्षण ही है. मछली खाना भी मांसाहार है और हिंदू जीवन शैली का हिस्सा है यह शायद सेनगुप्ता भूल गए हैं. दूसरी तरफ, बंगाल, असम बिहार जैसे इलाके हैं जहां मांसाहार, खासकर मछली खाने का रिवाज है. तो अगर सेनगुप्ता इनकी तरफ थोड़ा इशारा कर पाते तो किताब गहरी बन जाती.
फिर भी, हिंदू धर्म पर व्यापक और अलग नजरिए वाले इस काम के लिए सेनगुप्ता वाकई बधाई के हकदार हैं. वो भी बिना किसी अनावश्यक टीका-टिप्पणी के वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अपनी बात कह जाते हैं. मदन सोनी ने किताब में ऊंचे दरजे का अनुवाद किया है.
किताबः हिंदू होने का अर्थः प्राचीन आस्था, नई दुनिया और आप
पृष्ठ संख्याः 182
कीमतः 250 रुपए
प्रकाशकः मंजुल पब्लिशिंग हाउस
***

Published on September 02, 2019 06:18
August 30, 2019
नदीसूत्रः मौत के मुहाने पर खड़ी दामोदर नदी
जब प्रदूषण से कराहती दामोदर नदी ही मर जाएगी तो इसके नाम पर चलने वाले बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य आखिरकार सध जाएगा या फिर वह निरुद्देश्य रह जाएगा?
नदीसूत्र / मंजीत ठाकुर
यह नदी कभी बंगाल का शोक कही जाती थी. अथाह जलराशि, और उससे भी अधिक रौद्र रूप. बरसात में यह नदी अपने कूल-किनारे तोड़कर बंगाल के मैदानों में फैलकर तबाही ले आती थी. जी, यह दामोदर नदी है. पर दामोदर का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, उसकी बाढ़ पर अंकुश लगाने के लिए आजादी के बाद दामोदर घाटी परियोजना (डीवीसी) शुरू हुई. बाढ़ पर तो खैर अंकुश लगा, पर असली नजर थी इसके बेसिन में मौजूद लोहे और कोयले पर. अनगिनत उद्योग लगे और आज की तारीख में दंतकथाओं में मौजूद दामोदर नदी देश की अधिक प्रदूषित नदियों की फेहरिस्त में शामिल है.
दामोदर नदी के किनारे 10 ताप बिजलीघर हैं जो सालाना कोई 24 लाख मीट्रिक टन राख पैदा करते हैं. इन बिजलीघरों में 65.7 लाख मीट्रिक टन कोयले की सालाना खपत होती है और इससे 8,768 मेगवॉट बिजली पैदा होती है.
दामोदर नदी को प्रदूषित करने का खेल रांची जिले के कोल बेल्ट खेलारी में शुरू होता है. फिर रामगढ़ जिले में घुसते ही पतरातू थर्मल पावर स्टेशन और सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की कोल वाशरी इस नदी को और भी प्रदूषित करते हैं. कोल वॉशरी से निकले मलबे की मात्रा 30 लाख टन सालाना होती है. बोकारो जिले में घुसते ही ये तीन बिजलीघर दामोदर में कोयले की राख सीधे बहा दिया करते थे.
धनबाद में इस नदी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उद्योग जगत के तमाम दवाबों के बावजूद पर्यावरण मंत्रालय ने धनबाद में नए उद्योगों को मंजूरी देने से मना कर दिया था.
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) की वेबसाइट में दामोदर में अपशिष्ट गिराने वाले 94 उद्योगों के नाम दर्ज हैं जिनमें अधिकतर तापबिजली घर और कोल वॉशरी ही हैं.
सन् 2004 में दामोदर बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले नेता और झारखंड सरकार में मंत्री सरयू राय का मानना है कि यह हालत तो तब है जब दामोदर के प्रदूषण स्तर में काफी सुधार हुआ है. लेकिन राज्य सरकार की एक इकाई तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट आज भी चोरी-छुपे कोयले की राख को सीधे नदी के किनारे डाल देता है क्योंकि इसका ऐश पॉन्ड अब किसी काम का नहीं. पिछले साल दिसंबर (2017) में सीपीसीबी ने तेनुघाट संयंत्र को बंद करने का निर्देश दिया था क्योंकि यह दामोदर नदी को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा था.
फिर भी स्थिति यह हो गई है कि बोकारो के आसपास के लोग दामोदर में छठ भी नहीं मनाने जाते. दामोदर का पत्थरों से अठखेलियां करता पानी काले और गंदले सड़न भरे बहाव में तब्दील हो गया है.
हालांकि जेएसपीसीबी के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी का दावा है कि पहले के मुकाबले प्रदूषण नियंत्रण के कानूनों को काफी कड़ाई के साथ लागू करवाया जाता है और इन उत्पादक इकाइयों की सतत मॉनीटरिंग चलती रहती है. पर इसका असर नदी की सेहत पर पड़ता दिखा नहीं है.
सन् 2011 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दामोदर नदी की सूरतेहाल पर एक सर्वे करवाया था जिसमें ताप बिजलीघरों की वजह से इस नदी के खराब हालात का ब्योरा मौजूद है. दामोदर घाटी के बिजलीघरों से हवा में गैस के रूप में जा रही गंधक बारिश के साथ तेजाब बन जाती है और नदी में मिल जाती है. सीएसएमई की करीब दो दशक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, इस गंधक की मात्रा करीब 65,000 टन सालाना से ज्यादा होती है.
दामोदर नदी घाटी के दायरे में आने वाले झारखण्ड के नौ जिले हैं और इसके किनारे कई शहर बसे हुए हैं. कई पर्यावरणविद तो दामोदर को जैविक रेगिस्तान और काला रेगिस्तान भी कहते हैं. कभी भारत सरकार ने बहुद्देश्यीय दामोदर परियोजना के ऐलान के साथ लोगों को विकास का सब्जबाग दिखाया था. फिलहाल स्थिति यह है कि दामोदर का पानी पीने लायक नहीं बचा है. पानी छोड़िए, यह इतना अधिक प्रदूषित है कि लोग नहाने से भी कतराते हैं.
हजारीबाग, बोकारो एवं धनबाद जिलों में इस नदी के दोनों किनारों पर बड़े कोल वाशरी हैं, जो रोजाना हजारों घनलीटर कोयले का धोवन नदी में बहाते हैं. इन कोलवाशरियों में गिद्दी, टंडवा, स्वांग, कथारा, दुगदा, बरोरा, मुनिडीह, लोदना, जामाडोबा, पाथरडीह, सुदामडीह और चासनाला शामिल हैं. इसके साथ ही इस इलाके में कोयला पकाने वाले बड़े-बड़े कोलभट्ठी हैं जो नदी को लगातार प्रदूषित करते रहते हैं.
चंद्रपुरा ताप बिजलीघर में रोजाना 12 हजार मीट्रिक टन कोयले की खपत होती है और उससे हर रोज निकलने वाला राख दामोदर में बहाया जाता है. नतीजतन, दामोदर नदी के पानी में ठोस पदार्थों का मान औसत से काफी अधिक है.
दामोदर नदी के पानी में भारी धातु, लोहा, मैगनीज, तांबा, लेड, निकल वगैरह मौजूद हैं, पहले यहां के लोगों में मान्यता थी कि दामोदर नदी में नहाने से त्वचा रोग दूर हो जाते हैं. पर आज स्थिति यह है कि आपने हिम्मत करके दामोदर में डुबकी लगाई तो त्वचा रोग होना तय है.
दामोदर नदी में प्रदूषण का असर यहां के लोगों की आजीविका पर भी पड़ा है. कुछ दशक पहले तक इस नदी में बहुत सारी नस्लों की मछलियां होती थीं. पर अब जहरीले पानी में मछली छोड़िए किसी भी किस्म का जलीय जीवन नामुमकिन है. दामोदर नदी के किनारे से सटे खेतों की मिट्टी जहरीली हो गई है और जानकार बताते हैं कि इस इलाके में खेतों में उपज पचास फीसदी कम हो गई है.
दामोदर नदी के दम पर इस नदीघाटी में मौजूद ताप बिजलीघर ही नहीं, कई सारे स्टील प्लांट भी चलते हैं. कई उद्योगों के इस्तेमाल का और शहरों के पीने का पानी दामोदर से मिलता है. जब दामोदर नदी ही मर जाएगी तो क्या इसके नाम पर चलने वाले बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य आखिरकार सध जाएगा या फिर वह निरुद्देश्य रह जाएगा?
सवाल दुश्वार जरूर है पर जवाब जानना भी उतना ही जरूरी है. आखिर भविष्य से जो जुड़ा है.
नदीसूत्र / मंजीत ठाकुर
यह नदी कभी बंगाल का शोक कही जाती थी. अथाह जलराशि, और उससे भी अधिक रौद्र रूप. बरसात में यह नदी अपने कूल-किनारे तोड़कर बंगाल के मैदानों में फैलकर तबाही ले आती थी. जी, यह दामोदर नदी है. पर दामोदर का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, उसकी बाढ़ पर अंकुश लगाने के लिए आजादी के बाद दामोदर घाटी परियोजना (डीवीसी) शुरू हुई. बाढ़ पर तो खैर अंकुश लगा, पर असली नजर थी इसके बेसिन में मौजूद लोहे और कोयले पर. अनगिनत उद्योग लगे और आज की तारीख में दंतकथाओं में मौजूद दामोदर नदी देश की अधिक प्रदूषित नदियों की फेहरिस्त में शामिल है.
दामोदर नदी के किनारे 10 ताप बिजलीघर हैं जो सालाना कोई 24 लाख मीट्रिक टन राख पैदा करते हैं. इन बिजलीघरों में 65.7 लाख मीट्रिक टन कोयले की सालाना खपत होती है और इससे 8,768 मेगवॉट बिजली पैदा होती है.
दामोदर नदी को प्रदूषित करने का खेल रांची जिले के कोल बेल्ट खेलारी में शुरू होता है. फिर रामगढ़ जिले में घुसते ही पतरातू थर्मल पावर स्टेशन और सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की कोल वाशरी इस नदी को और भी प्रदूषित करते हैं. कोल वॉशरी से निकले मलबे की मात्रा 30 लाख टन सालाना होती है. बोकारो जिले में घुसते ही ये तीन बिजलीघर दामोदर में कोयले की राख सीधे बहा दिया करते थे.
धनबाद में इस नदी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उद्योग जगत के तमाम दवाबों के बावजूद पर्यावरण मंत्रालय ने धनबाद में नए उद्योगों को मंजूरी देने से मना कर दिया था.
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) की वेबसाइट में दामोदर में अपशिष्ट गिराने वाले 94 उद्योगों के नाम दर्ज हैं जिनमें अधिकतर तापबिजली घर और कोल वॉशरी ही हैं.
सन् 2004 में दामोदर बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले नेता और झारखंड सरकार में मंत्री सरयू राय का मानना है कि यह हालत तो तब है जब दामोदर के प्रदूषण स्तर में काफी सुधार हुआ है. लेकिन राज्य सरकार की एक इकाई तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट आज भी चोरी-छुपे कोयले की राख को सीधे नदी के किनारे डाल देता है क्योंकि इसका ऐश पॉन्ड अब किसी काम का नहीं. पिछले साल दिसंबर (2017) में सीपीसीबी ने तेनुघाट संयंत्र को बंद करने का निर्देश दिया था क्योंकि यह दामोदर नदी को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा था.
फिर भी स्थिति यह हो गई है कि बोकारो के आसपास के लोग दामोदर में छठ भी नहीं मनाने जाते. दामोदर का पत्थरों से अठखेलियां करता पानी काले और गंदले सड़न भरे बहाव में तब्दील हो गया है.
हालांकि जेएसपीसीबी के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी का दावा है कि पहले के मुकाबले प्रदूषण नियंत्रण के कानूनों को काफी कड़ाई के साथ लागू करवाया जाता है और इन उत्पादक इकाइयों की सतत मॉनीटरिंग चलती रहती है. पर इसका असर नदी की सेहत पर पड़ता दिखा नहीं है.
सन् 2011 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दामोदर नदी की सूरतेहाल पर एक सर्वे करवाया था जिसमें ताप बिजलीघरों की वजह से इस नदी के खराब हालात का ब्योरा मौजूद है. दामोदर घाटी के बिजलीघरों से हवा में गैस के रूप में जा रही गंधक बारिश के साथ तेजाब बन जाती है और नदी में मिल जाती है. सीएसएमई की करीब दो दशक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, इस गंधक की मात्रा करीब 65,000 टन सालाना से ज्यादा होती है.
दामोदर नदी घाटी के दायरे में आने वाले झारखण्ड के नौ जिले हैं और इसके किनारे कई शहर बसे हुए हैं. कई पर्यावरणविद तो दामोदर को जैविक रेगिस्तान और काला रेगिस्तान भी कहते हैं. कभी भारत सरकार ने बहुद्देश्यीय दामोदर परियोजना के ऐलान के साथ लोगों को विकास का सब्जबाग दिखाया था. फिलहाल स्थिति यह है कि दामोदर का पानी पीने लायक नहीं बचा है. पानी छोड़िए, यह इतना अधिक प्रदूषित है कि लोग नहाने से भी कतराते हैं.
हजारीबाग, बोकारो एवं धनबाद जिलों में इस नदी के दोनों किनारों पर बड़े कोल वाशरी हैं, जो रोजाना हजारों घनलीटर कोयले का धोवन नदी में बहाते हैं. इन कोलवाशरियों में गिद्दी, टंडवा, स्वांग, कथारा, दुगदा, बरोरा, मुनिडीह, लोदना, जामाडोबा, पाथरडीह, सुदामडीह और चासनाला शामिल हैं. इसके साथ ही इस इलाके में कोयला पकाने वाले बड़े-बड़े कोलभट्ठी हैं जो नदी को लगातार प्रदूषित करते रहते हैं.
चंद्रपुरा ताप बिजलीघर में रोजाना 12 हजार मीट्रिक टन कोयले की खपत होती है और उससे हर रोज निकलने वाला राख दामोदर में बहाया जाता है. नतीजतन, दामोदर नदी के पानी में ठोस पदार्थों का मान औसत से काफी अधिक है.
दामोदर नदी के पानी में भारी धातु, लोहा, मैगनीज, तांबा, लेड, निकल वगैरह मौजूद हैं, पहले यहां के लोगों में मान्यता थी कि दामोदर नदी में नहाने से त्वचा रोग दूर हो जाते हैं. पर आज स्थिति यह है कि आपने हिम्मत करके दामोदर में डुबकी लगाई तो त्वचा रोग होना तय है.
दामोदर नदी में प्रदूषण का असर यहां के लोगों की आजीविका पर भी पड़ा है. कुछ दशक पहले तक इस नदी में बहुत सारी नस्लों की मछलियां होती थीं. पर अब जहरीले पानी में मछली छोड़िए किसी भी किस्म का जलीय जीवन नामुमकिन है. दामोदर नदी के किनारे से सटे खेतों की मिट्टी जहरीली हो गई है और जानकार बताते हैं कि इस इलाके में खेतों में उपज पचास फीसदी कम हो गई है.
दामोदर नदी के दम पर इस नदीघाटी में मौजूद ताप बिजलीघर ही नहीं, कई सारे स्टील प्लांट भी चलते हैं. कई उद्योगों के इस्तेमाल का और शहरों के पीने का पानी दामोदर से मिलता है. जब दामोदर नदी ही मर जाएगी तो क्या इसके नाम पर चलने वाले बहुद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य आखिरकार सध जाएगा या फिर वह निरुद्देश्य रह जाएगा?
सवाल दुश्वार जरूर है पर जवाब जानना भी उतना ही जरूरी है. आखिर भविष्य से जो जुड़ा है.

Published on August 30, 2019 02:08
August 22, 2019
नदीसूत्रः दिल्ली के नाले यमुना में बाढ़ से कैसा डर
यमुना में बाढ़ का खतरा बताया जा रहा है. पर शुक्र मनाइए कि भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक यमुना में कुछ दिन तो इसी बहाने साफ पानी बहेगा. नदियों में बाढ़ एक कुदरती बात है. अतिक्रमण हमने किया है, नदी ने नहीं.
अगर आप टेलिविज़न पर खबरें देखते हैं तो हहाती हुई यमुना का दृश्य जरूर देख रहे होंगे. यमुना का यौवन देखने लायक है. पर खबरें दिल्ली को डराने की कोशिश कर रही है. बाढ़ का संकट बताया जा रहा है. नदियों में बाढ़ क्या कोई अघट जैसी घटना है? यह तो बहुत प्राकृतिक घटना है. हर नदी में बाढ़ आती है और आनी भी चाहिए. कई लोग ताज्जुब कर रहे हैं दिल्ली में बाढ़ क्यों, जबकि बारिश भी नहीं हुई.
ऐसा कहने वाले लोग न तो नदियों के स्वभाव को जानते हैं न नदी तंत्र को. कैचमेंट और बेसिन जैसे शब्दों से अनजान लोग यमुना पर बने लोहे को पुल को यमुना के पानी घटने-बढ़ने का आधार बताते हैं.
दिल्ली में रहने वाले या कभी यमुना को पार करने वाले लोग उसे रोज़ाना देखते होंगे, उसके काले गंधाते पानी पर हाय-हाय करते होंगे. पूरी दिल्ली में आपको यमुना में कभी भी साफ पानी नहीं दिखता होगा.
बस, दिल्ली से पहले वजीराबाद बराज ही वह जगह है जहां पर यमुना का पानी काला नहीं होता. लेकिन वहां तो हम यमुना का करीबन सारा पानी रोक लेते हैं और उसके आगे जो पानी हमें दिखता है वह दिल्ली का सीवर है. उद्योगों और घरों का गंदा प्रदूषित पानी जो बिना ट्रीटमेंट के सीधे उसमें गिराया जाता है.
यमुना नदी की बदहाली वजीराबाद से ही शुरू हो जाती है. दिल्ली में वजीराबाद से ओखला बैराज के बीच की यह दूरी, दुनिया में किसी भी नदी की तुलना में यमुना के लिये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. इसी हिस्से में यमुना सबसे अधिक प्रदूषित है.
आखिर यमुना को यूं ही वैज्ञानिक जैविक रेगिस्तान नहीं कहते. इसे भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी का शर्मनाक दर्जा मिला हुआ है. इसके पानी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और बायोमाइडस जैसे कृषि रसायन की मौजूदगी में पिछले 25 वर्षों में चार गुना वृद्धि हुई है. देहरादून, यमुना नगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा और आगरा घरेलू और औद्योगिक कचरा सीधे यमुना में गिराते हैं. अनुमान है कि हरियाणा के 22, दिल्ली की 42 और उत्तर प्रदेश की 17 फैक्टरियां यमुना में सीधे तरल कचरा बहाती हैं.
इसी हिस्से में आकर यमुना सिकुड़कर डेढ़ से तीन किलोमीटर चौड़ी रह जाती है. यमुना पर किए गए कई शोधों में से एक शोध कहता है कि गरमियों में इसकी गहराई भी करीबन एक मीटर और चौड़ाई महज 80 मीटर रह जाती है. अभी जिस धारा को देखकर आपको बाढ़ की धमकी दी जा रही है, गरमी में यमुना उसका महज 16 फीसद ही रह जाती है.
यमुना को दिल्ली ने मौत दी है और उसमें भी सबसे अधिक चुनौती सरकारी एजेंसियों से मिली है. 100 एकड़ पर शास्त्री पार्क मेट्रो, 100 एकड़ में यमुना खादर आइटीओ मेट्रो, 100 एकड़ में खेलगांव और उससे जुड़े दूसरे निर्माण, 61 एकड़ में इन्द्रपस्थ बस डिपो और 100 एकड़ में बनाया अक्षरधाम. नगर निगम के नालों ने यमुना का आंचल रोजाना मैला करने का ठेका लिया हुआ है सो अलग.
महरौली, वसन्त विहार से लेकर द्वारका तक की हरियाणा से सटी पट्टी साल भर त्राहि-त्राहि करती है.
यही वह हिस्सा है, जिसने 1947 से 2010 के बीच नौ बाढ़ देखे हैं. 1947, 1964, 1977, 1978, 1988, 1995, 1998, 2008 और 2010. यमुना के पेटे में धड़ाधड़ निर्माण किए जा रहे हैं. यह भूलकर कि यमुना भ्रंश रेखा में बहती है और कभी भी भूकंप के तगड़े झटके लगे तो यह सब ठाठ धरा रह जाएगा.
केन्द्रीय जल आयोग का प्रस्ताव कहता है कि यमुना धारा के मध्य बिन्दु और एकतरफ के पुश्ते के बीच की दूरी कम-से-कम पांच किमी रहनी चाहिए. लेकिन, हकीकत यह है कि मेट्रो, खेलगांव, अक्षरधाम जैसे सारे निर्माण सुरक्षा से समझौता कर बनाए गए हैं.
पर्यावरण संरक्षण कानून- 1986 की मंशा के मुताबिक, नदियों को ‘रिवर रेगुलेशन जोन’ के रूप में अधिसूचित कर सुरक्षित किया जाना चाहिए था. 2001-2002 में की गई पहल के बावजूद, पर्यावरण मंत्रालय आज तक ऐसा करने में अक्षम साबित हुआ है. बाढ़ क्षेत्र को ‘ग्राउंड वाटर सेंचुरी’ घोषित करने के केन्द्रीय भूजल आयोग के प्रस्ताव को हम कहां लागू कर सके?
यमुना जहां अभी बह रही है, यह उसी का रास्ता है. उफान मारते पानी को देखकर हम डर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने अवैध रूप से उसके पेटे में अपना घर बसा लिया है.
यमुना में बाढ़ से डरिए मत, इसी बहाने कुछ तो नदी में साफ पानी बहने दीजिए.
***
अगर आप टेलिविज़न पर खबरें देखते हैं तो हहाती हुई यमुना का दृश्य जरूर देख रहे होंगे. यमुना का यौवन देखने लायक है. पर खबरें दिल्ली को डराने की कोशिश कर रही है. बाढ़ का संकट बताया जा रहा है. नदियों में बाढ़ क्या कोई अघट जैसी घटना है? यह तो बहुत प्राकृतिक घटना है. हर नदी में बाढ़ आती है और आनी भी चाहिए. कई लोग ताज्जुब कर रहे हैं दिल्ली में बाढ़ क्यों, जबकि बारिश भी नहीं हुई.
ऐसा कहने वाले लोग न तो नदियों के स्वभाव को जानते हैं न नदी तंत्र को. कैचमेंट और बेसिन जैसे शब्दों से अनजान लोग यमुना पर बने लोहे को पुल को यमुना के पानी घटने-बढ़ने का आधार बताते हैं.
दिल्ली में रहने वाले या कभी यमुना को पार करने वाले लोग उसे रोज़ाना देखते होंगे, उसके काले गंधाते पानी पर हाय-हाय करते होंगे. पूरी दिल्ली में आपको यमुना में कभी भी साफ पानी नहीं दिखता होगा.
बस, दिल्ली से पहले वजीराबाद बराज ही वह जगह है जहां पर यमुना का पानी काला नहीं होता. लेकिन वहां तो हम यमुना का करीबन सारा पानी रोक लेते हैं और उसके आगे जो पानी हमें दिखता है वह दिल्ली का सीवर है. उद्योगों और घरों का गंदा प्रदूषित पानी जो बिना ट्रीटमेंट के सीधे उसमें गिराया जाता है.
यमुना नदी की बदहाली वजीराबाद से ही शुरू हो जाती है. दिल्ली में वजीराबाद से ओखला बैराज के बीच की यह दूरी, दुनिया में किसी भी नदी की तुलना में यमुना के लिये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. इसी हिस्से में यमुना सबसे अधिक प्रदूषित है.
आखिर यमुना को यूं ही वैज्ञानिक जैविक रेगिस्तान नहीं कहते. इसे भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी का शर्मनाक दर्जा मिला हुआ है. इसके पानी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और बायोमाइडस जैसे कृषि रसायन की मौजूदगी में पिछले 25 वर्षों में चार गुना वृद्धि हुई है. देहरादून, यमुना नगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा और आगरा घरेलू और औद्योगिक कचरा सीधे यमुना में गिराते हैं. अनुमान है कि हरियाणा के 22, दिल्ली की 42 और उत्तर प्रदेश की 17 फैक्टरियां यमुना में सीधे तरल कचरा बहाती हैं.
इसी हिस्से में आकर यमुना सिकुड़कर डेढ़ से तीन किलोमीटर चौड़ी रह जाती है. यमुना पर किए गए कई शोधों में से एक शोध कहता है कि गरमियों में इसकी गहराई भी करीबन एक मीटर और चौड़ाई महज 80 मीटर रह जाती है. अभी जिस धारा को देखकर आपको बाढ़ की धमकी दी जा रही है, गरमी में यमुना उसका महज 16 फीसद ही रह जाती है.
यमुना को दिल्ली ने मौत दी है और उसमें भी सबसे अधिक चुनौती सरकारी एजेंसियों से मिली है. 100 एकड़ पर शास्त्री पार्क मेट्रो, 100 एकड़ में यमुना खादर आइटीओ मेट्रो, 100 एकड़ में खेलगांव और उससे जुड़े दूसरे निर्माण, 61 एकड़ में इन्द्रपस्थ बस डिपो और 100 एकड़ में बनाया अक्षरधाम. नगर निगम के नालों ने यमुना का आंचल रोजाना मैला करने का ठेका लिया हुआ है सो अलग.
महरौली, वसन्त विहार से लेकर द्वारका तक की हरियाणा से सटी पट्टी साल भर त्राहि-त्राहि करती है.
यही वह हिस्सा है, जिसने 1947 से 2010 के बीच नौ बाढ़ देखे हैं. 1947, 1964, 1977, 1978, 1988, 1995, 1998, 2008 और 2010. यमुना के पेटे में धड़ाधड़ निर्माण किए जा रहे हैं. यह भूलकर कि यमुना भ्रंश रेखा में बहती है और कभी भी भूकंप के तगड़े झटके लगे तो यह सब ठाठ धरा रह जाएगा.
केन्द्रीय जल आयोग का प्रस्ताव कहता है कि यमुना धारा के मध्य बिन्दु और एकतरफ के पुश्ते के बीच की दूरी कम-से-कम पांच किमी रहनी चाहिए. लेकिन, हकीकत यह है कि मेट्रो, खेलगांव, अक्षरधाम जैसे सारे निर्माण सुरक्षा से समझौता कर बनाए गए हैं.
पर्यावरण संरक्षण कानून- 1986 की मंशा के मुताबिक, नदियों को ‘रिवर रेगुलेशन जोन’ के रूप में अधिसूचित कर सुरक्षित किया जाना चाहिए था. 2001-2002 में की गई पहल के बावजूद, पर्यावरण मंत्रालय आज तक ऐसा करने में अक्षम साबित हुआ है. बाढ़ क्षेत्र को ‘ग्राउंड वाटर सेंचुरी’ घोषित करने के केन्द्रीय भूजल आयोग के प्रस्ताव को हम कहां लागू कर सके?
यमुना जहां अभी बह रही है, यह उसी का रास्ता है. उफान मारते पानी को देखकर हम डर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने अवैध रूप से उसके पेटे में अपना घर बसा लिया है.
यमुना में बाढ़ से डरिए मत, इसी बहाने कुछ तो नदी में साफ पानी बहने दीजिए.
***

Published on August 22, 2019 03:08
August 19, 2019
नदीसूत्रः जहरीली हिंडन अब नदी नहीं एक त्रासदी है
एनजीटी की कमिटी की रिपोर्ट साफ तौर पर हिंडन को एक डेड रिवर यानी मृत नदी बताती है क्योंकि नदी के जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा तकरीबन शून्य तक पहुंच गई है.
दिल्ली में रहने वाले लोग हिंडन नदी से जरूर परिचित होंगे. इसका एक नाम हरनदी भी है और यह सहारनपुर के पास से निकलकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद होती हुई यमुना में जाकर मिल जाती है. खासकर जिन लोगों ने दिल्ली के पूरब की ओर होते विस्तार की तरफ अपना बसेरा बसाया होगा, वे लोग तो जरूर इस नदी के आसपास से गुजरते होंगे.
गाजियाबाद-दिल्ली में रहने वालों और हिंडन तट के आसपास के लोगों के लिए पिछले महीने खबर कुछ अच्छी नहीं है. यह हो सकता है कि नदियों की सेहत को लेकर आने वाली खबरों पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हमने अपनी चिंताओं में से नदियों की सेहत को बाहर कर दिया है, पर यह चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए.
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की एक कमिटी ने पिछले महीने रिपोर्ट दी है कि हिंडन नदी के आसपास रहने वाले लोगों में से करीब 40 फीसदी लोग जलजनित बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. इसकी वजह है कि इस इलाके में शहरीकरण काफी तेज गति से बढ़ा है और इसके साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों का अपशिष्ट बिना ट्रीटमेंट के ही हिंडन में बहाया जाता है.
इस बात के दस्तावेजी प्रमाण हैं कि पिछले डेढ़ दशक में प्रदूषित हिंडन के कारण सैकड़ों लोगों को कैंसर हुआ है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मेरठ के पास जयभीम नगर झुग्गियों में रहने वाले लोगों में से करीब 124 लोग काल के गाल में समाहित हो चुके हैं. इन गरीबों का कसूर यह है कि वे मिनरल वाटर नहीं पीते. जमीन से निकलने वाला पानी इतना जहरीला हो चुका है कि बचना मुमकिन नहीं.
हिमालय की तराई में सहारनपुर से अपनी 260 किलोमीटर की यात्रा में हिंडन इतनी जहरीली हो गई है कि अब यह एक नदी नहीं, बल्कि त्रासदी हो गयी है. हिंडन में किस उद्योग का अवशिष्ट नहीं जाता? नदी के गर्भ में चीनी मिल, पेपर मिल, स्टील के कारखाने, डेयरी उद्योग की गंदगी, बूचड़खानों का कचरा और बाकी के औद्योगिक अपशिष्ट, सब कुछ आकर समाहित हो जाते हैं.
सेंटर फॉर साईंस ऐंड एन्वायरमेन्ट और जनहित फाउण्डेशन ने 'हिंडन रिवरः गैस्पिगं फॉर ब्रीद' नाम से उन छह जिलों का एक अध्ययन किया था, जहां से हिंडन गुजरती है. इस अध्ययन के मुताबिक, न तो नदी सुरक्षित रही है और न ही नदी के किनारे रहनेवाले लोग. भूजल इस खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो गया है और नदी के पानी में भारी धातुओं और घातक रसायनों की मिलावट इतनी ज्यादा है कि पानी बहुत नीचे तक प्रदूषित हो गया है. इस प्रदूषण ने हिंडन की जैव विविधता पर बुरा असर डाला है.
हिडंन और उसकी सहायक नदी काली में धात्विक और जहरीले रसायनों का मिश्रण स्वीकृत मात्रा से 112 से 179 गुना अधिक है. इसीतरह क्रोमियम का स्तर स्वीकृत मात्रा से 46 से 123 गुना अधिक पाया गया है.
सिर्फ गाजियाबाद में ही हिंडन नदी में आठ बड़े नाले गिरते हैं. ज्वाला, अर्थला, कैला भट्टां, इंदिरापुरम, करहेडा, डासना, प्रताप विहार और हिंडन विहार ये सभी नाले आकर हिंडन में ही प्रवाहित होते हैं. और इन सबके जरिए बिना ट्रीट किया अपशिष्ट ही नदी में जाता है.
इस किसी भी सीवेज में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या ईटीपी नहीं है. एनजीटी की कमिटी की रिपोर्ट भी कहता है कि पूरा गाजियाबाद शहर ही हिंडन को प्रदूषित कर रहा है.
एनजीटी की कमिटी की रिपोर्ट साफ तौर पर हिंडन को एक डेड रिवर यानी मृत नदी बताती है क्योंकि नदी के जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा तकरीबन शून्य तक पहुंच गई है. इस टीम ने गाजियाबाद के 23 उद्योगों और सरकारी अस्पतालों का दौरा किया था और पाया कि होंडा को छोड़कर शायद ही कोई उद्योग पर्यावरणीय मानको का पालन करता है. जिन उद्योगों ने अपने परिसर में एसटीपी या ईटीपी भी लगा रखे हैं वे भी अपना अपशिष्ट सीधे-सीधे हिंडन में प्रवाहित कर रहे हैं.
इस कमिटी ने गाजियाबाद, बागपत, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और शामली में 168 स्थानों पर भूमिगत जल के भी नमूने लिए थे और उनमें से 93 नमूनों में पेयजल के बीआइएस मानकों से अधिक का एक या अधिक किस्म का प्रदूषण था. कमिटी ने फ्लोराइड, सल्फेट, ऑइल और ग्रीज जैसे प्रदूषकों की जांच की थी.
यह तय है कि मौत के मुंह में जाती हिंडन का असर हम सब पर पड़ेगा. खासकर इसके तट पर बसे इलाकों में खेती से लेकर पीने के पानी तक पर. थोड़ी देर के लिए शायद हिंडन में उड़लने से पहले घातक अपशिष्टों के उपचार में लागत अधिक लगती हो, लेकिन इसके दुष्परिणामों के बाद आने वाला खर्चा अधिक होगा. कई गुना अधिक. खेती से लेकर लाज तक, आप बस जोड़ते रह जाएंगे.
बरसात में उग्र नदी से ही मत डरिए, हमारी वजह से मरती हुई नदी भी बेहद नुक्सानदेह होगी.
दिल्ली में रहने वाले लोग हिंडन नदी से जरूर परिचित होंगे. इसका एक नाम हरनदी भी है और यह सहारनपुर के पास से निकलकर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद होती हुई यमुना में जाकर मिल जाती है. खासकर जिन लोगों ने दिल्ली के पूरब की ओर होते विस्तार की तरफ अपना बसेरा बसाया होगा, वे लोग तो जरूर इस नदी के आसपास से गुजरते होंगे.
गाजियाबाद-दिल्ली में रहने वालों और हिंडन तट के आसपास के लोगों के लिए पिछले महीने खबर कुछ अच्छी नहीं है. यह हो सकता है कि नदियों की सेहत को लेकर आने वाली खबरों पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हमने अपनी चिंताओं में से नदियों की सेहत को बाहर कर दिया है, पर यह चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए.
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की एक कमिटी ने पिछले महीने रिपोर्ट दी है कि हिंडन नदी के आसपास रहने वाले लोगों में से करीब 40 फीसदी लोग जलजनित बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. इसकी वजह है कि इस इलाके में शहरीकरण काफी तेज गति से बढ़ा है और इसके साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों का अपशिष्ट बिना ट्रीटमेंट के ही हिंडन में बहाया जाता है.
इस बात के दस्तावेजी प्रमाण हैं कि पिछले डेढ़ दशक में प्रदूषित हिंडन के कारण सैकड़ों लोगों को कैंसर हुआ है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मेरठ के पास जयभीम नगर झुग्गियों में रहने वाले लोगों में से करीब 124 लोग काल के गाल में समाहित हो चुके हैं. इन गरीबों का कसूर यह है कि वे मिनरल वाटर नहीं पीते. जमीन से निकलने वाला पानी इतना जहरीला हो चुका है कि बचना मुमकिन नहीं.
हिमालय की तराई में सहारनपुर से अपनी 260 किलोमीटर की यात्रा में हिंडन इतनी जहरीली हो गई है कि अब यह एक नदी नहीं, बल्कि त्रासदी हो गयी है. हिंडन में किस उद्योग का अवशिष्ट नहीं जाता? नदी के गर्भ में चीनी मिल, पेपर मिल, स्टील के कारखाने, डेयरी उद्योग की गंदगी, बूचड़खानों का कचरा और बाकी के औद्योगिक अपशिष्ट, सब कुछ आकर समाहित हो जाते हैं.
सेंटर फॉर साईंस ऐंड एन्वायरमेन्ट और जनहित फाउण्डेशन ने 'हिंडन रिवरः गैस्पिगं फॉर ब्रीद' नाम से उन छह जिलों का एक अध्ययन किया था, जहां से हिंडन गुजरती है. इस अध्ययन के मुताबिक, न तो नदी सुरक्षित रही है और न ही नदी के किनारे रहनेवाले लोग. भूजल इस खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो गया है और नदी के पानी में भारी धातुओं और घातक रसायनों की मिलावट इतनी ज्यादा है कि पानी बहुत नीचे तक प्रदूषित हो गया है. इस प्रदूषण ने हिंडन की जैव विविधता पर बुरा असर डाला है.
हिडंन और उसकी सहायक नदी काली में धात्विक और जहरीले रसायनों का मिश्रण स्वीकृत मात्रा से 112 से 179 गुना अधिक है. इसीतरह क्रोमियम का स्तर स्वीकृत मात्रा से 46 से 123 गुना अधिक पाया गया है.
सिर्फ गाजियाबाद में ही हिंडन नदी में आठ बड़े नाले गिरते हैं. ज्वाला, अर्थला, कैला भट्टां, इंदिरापुरम, करहेडा, डासना, प्रताप विहार और हिंडन विहार ये सभी नाले आकर हिंडन में ही प्रवाहित होते हैं. और इन सबके जरिए बिना ट्रीट किया अपशिष्ट ही नदी में जाता है.
इस किसी भी सीवेज में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या ईटीपी नहीं है. एनजीटी की कमिटी की रिपोर्ट भी कहता है कि पूरा गाजियाबाद शहर ही हिंडन को प्रदूषित कर रहा है.
एनजीटी की कमिटी की रिपोर्ट साफ तौर पर हिंडन को एक डेड रिवर यानी मृत नदी बताती है क्योंकि नदी के जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा तकरीबन शून्य तक पहुंच गई है. इस टीम ने गाजियाबाद के 23 उद्योगों और सरकारी अस्पतालों का दौरा किया था और पाया कि होंडा को छोड़कर शायद ही कोई उद्योग पर्यावरणीय मानको का पालन करता है. जिन उद्योगों ने अपने परिसर में एसटीपी या ईटीपी भी लगा रखे हैं वे भी अपना अपशिष्ट सीधे-सीधे हिंडन में प्रवाहित कर रहे हैं.
इस कमिटी ने गाजियाबाद, बागपत, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और शामली में 168 स्थानों पर भूमिगत जल के भी नमूने लिए थे और उनमें से 93 नमूनों में पेयजल के बीआइएस मानकों से अधिक का एक या अधिक किस्म का प्रदूषण था. कमिटी ने फ्लोराइड, सल्फेट, ऑइल और ग्रीज जैसे प्रदूषकों की जांच की थी.
यह तय है कि मौत के मुंह में जाती हिंडन का असर हम सब पर पड़ेगा. खासकर इसके तट पर बसे इलाकों में खेती से लेकर पीने के पानी तक पर. थोड़ी देर के लिए शायद हिंडन में उड़लने से पहले घातक अपशिष्टों के उपचार में लागत अधिक लगती हो, लेकिन इसके दुष्परिणामों के बाद आने वाला खर्चा अधिक होगा. कई गुना अधिक. खेती से लेकर लाज तक, आप बस जोड़ते रह जाएंगे.
बरसात में उग्र नदी से ही मत डरिए, हमारी वजह से मरती हुई नदी भी बेहद नुक्सानदेह होगी.

Published on August 19, 2019 06:59
August 9, 2019
नदीसूत्रः शिव के त्रिशूल पर बसी काशी में नदियों की दुर्गति
जिस देश में गंगा की ही फिक्र कम है उसमें बेचारी वरुणा और असि की क्या बिसात? जिन नदियों के नाम पर वाराणसी शहर बसा, उन नदियों के विलुप्त होने के बाद क्या शहर बचा रह जाएगा! कोई शहर लाख शिव के त्रिशूल पर बसा हो, पर बिना पानी के जड़े सूख ही जाएंगी.
बहुत समय से सुनते आए हैं कि नदियां किसी भी सभ्यता का आधार रही हैं और उसकी धमनियों की तरह होती हैं. दुनिया की तमाम महान सभ्यताएं नदी घाटियों में विकसित हुई हैं. आप चाहे सिंधु-गंगा घाटी की मिसाल लें या दजला-फरात की. एक नदी अपने इलाके की संस्कृति की वाहक होती है और अपने साथ एक इतिहास और सांस्कृतिक विरासत लेकर चलती है. किसी इलाके की खेती, वहां मछलीपालन और मछली समेत जलीय और तटीय जैव-विविधता नदी पर निर्भर होती है.
भारतीय साहित्य में नदियां मौजूद हैं. ऋग्वेद से ही हमारे साहित्य में नदियों का उल्लेख है. धार्मिक महत्व तो खैर है ही. आपको आज की परिस्थिति में संभवतया मजाक लगे लेकिन हाल तक देश के कई हिस्सों में सीधे नदियों का पानी पिया भी जाता था. मैं खुद ओडिशा के कालाहांडी इलाके में जब नियामगिरि पहाड़ियों पर जा रहा था, तो वहां स्थानीय लोगों को बमुश्किल छह सात फुट चौड़ी नदी का पानी पीते देखा था. मुझसे भी कहा गया कि यहां के नदियों का पानी अभी प्रदूषण से बचा है और इसमें पहाड़ियों की दुर्लभ जड़ी-बूटियों का मिश्रण हैं. वाकई पानी साफ था और सुस्वादु भी. (जी हां, आप माने न माने, पानी का भी स्वाद होता है)
लेकिन यकीन मानिए, जिस तरह से हम अपनी नदियों का नाश करते जा रहे हैं हम जल्दी ही दुनिया में जलसंकट का सामना करने वाले देशों में होंगे. हमारी आबादी भी अबाध गति से बढ़ती जा रही है और नदियां उतनी ही तेजी से लुप्त होती जा रही हैं.
वैसे हम जब भी नदी शब्द कहते हैं तो दिल्ली वालों को यमुना याद आती है (गाद से भरी, काली) और मैदानी लोगों को गंगा. लेकिन इसके साथ ही हम उन छोटी नदियों को भूल जाते हैं. पिछले हफ्ते मैंने कोलकाता की आदि गंगा का जिक्र किया था जो गंदे नाले में बदलकर रह गई है. लेकिन इन छोटी नदियों के योगदान से ही बड़ी नदियां वाकई बड़ी नदियां बन पाती हैं, यह भी हमें याद रखना चाहिए. इन छोटी नदियों मे से कई बड़े शहरों का शिकार बन गई हैं. इनमें से कुछ तो शहर के अपशिष्ट प्रवाह को बहाने के काम आने वाले नालों में बदल गई हैं. इन छोटी नदियों पर हमारा ध्यान तभी जाता है जब घटिया ड्रेनेज सिस्टम की वजह से बरसात के मौके पर इन नदियों का पानी सड़कों पर आकर जमा हो जाता है.
इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि एक सुचारू नदी तंत्र की भारत की बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव का एक रास्ता हो सकता है. इन दिनों बनारस बहुत चर्चा में है. प्रधानमंत्री जिस चुनाव क्षेत्र से मैदान में हो वह चर्चा में न आए तो क्या आए भला? हाल के हिंदी लेखकों की नौजवान पीढ़ी ने अस्सी घाट को भी बहुत तवज्जो दे दी है. पर इस बात का जिक्र लोग कम ही करते हैं कि वाराणसी का नाम जिन असि और वरुणा नदियों के नाम पर पड़ा और इन दोनों नदियों के भूखंड को ही वाराणसी कहा गया, उन नदियों का क्या हुआ? इस शहर को बनारस नाम तो मुगलों ने दिया था और बाद में अंग्रेजों ने भी इसी नाम को आगे बढ़ाया.
अस्सी नदी वाराणसी के घमहापुर गांव में स्थित कर्मदेश्वर महादेव कुंड से शुरू होकर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गंगा में मिलती है. इसका जल-ग्रहण क्षेत्र लगभग 14 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है.
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने शुम्भ-निशुम्भ नामक असुरों का वध करने के बाद जहां अपनी तलवार फेंकी थी, उस स्थान पर ही महादेव कुंड बना और इससे निकले पानी से ही असि (बाद में अस्सी) नदी का उद्गम हुआ. तलवार को संस्कृत में असि कहते हैं. यह अस्सी नदी पहले अस्सी घाट के पास गंगा में मिलती थी, पर गंगा कार्य योजना के बाद से इसे मोड़ कर लगभग दो किलोमीटर पहले ही गंगा में मिला दिया गया. यही नहीं, सरकारी फाइलों में भी इसे अस्सी नदी नहीं बल्कि अस्सी नाला का नाम दे दिया गया है.
आज की पीढ़ी को पता नहीं होगा कि अपनी विरासतों को सहेजने में जितनी उदासीन हमारी सरकार है उतने ही हम भी हैं. और जिस नाले में हम मूलमूत्र विसर्जित करके प्रकारांतर से गंगा में भेज रहे हैं वह नदी थी और वाराणसी के वातावरण के लिए आवश्यक थी.
पर जिस देश में गंगा की ही फिक्र कम है उसमें बेचारी वरुणा और असि की क्या बिसात. वरुणा भी साथ में ही काल का ग्रास बन रही है. पर क्या यह मुमकिन है कि जिन नदियों के नाम पर वाराणसी शहर बसा, उन नदियों के विलुप्त होने के बाद बचा रह जाएगा. कोई शहर लाख शिव के त्रिशूल पर बसा हो, पर बिना पानी के जड़े सूख ही जाएंगी.

Published on August 09, 2019 04:50
August 1, 2019
नदीसूत्रः बढ़ता कोलकाता लील गया आदि गंगा
कोलकाता में कालीघाट के पास एक नाला बहता है. यह नाला नहीं, स्थानीय लोगों के मुताबिक असली गंगा है. आदि गंगा नाम की इस नदी को शहर ने बिसरा दिया, पर परंपराओं में यह अब भी मौजूद
पिछले साल जब मैं कोलकाता में था तो मेरे मित्रों की जिद थी कि उन्हें कालीघाट में देवी के दर्शन करने हैं और कालीघाट में दर्शन के बाद अपनी सहज जिज्ञासा में हम नीचे उतर आए थे, जहां एक गंधाता हुआ नाला बह रहा था. लेकिन उस नाले को पार करने के लिए नावें मौजूद थीं और उस वक्त भी नाववाले ने हम चार लोगों से आठ आने (पचास पैसे) की दर से सिर्फ दो रूपए लिए थे. मल्लाह ने बताया था कि यह नाला नहीं, आदि गंगा है. उसने बताया कि नाकतल्ला से गरिया जाते समय रास्ते में अलीपुर ब्रिज के नीचे जिस नाले से भयानक बदबू आती है वह भी आदि गंगा ही है. जिसको स्थानीय लोग टॉली कैनाल कहते हैं.
असल में दो सौ साल पहले तक आदि गंगा हुगली की एक सहायक धारा थी. हालांकि इसका इतिहास थोड़ा और पुराना है. लेकिन अठारहवीं सदी में जब यह अपना स्वरूप खो रही थी तब 1772 से 1777 के बीच विलियम टॉली ने इसका पुनरोद्धार करवाकर इसको नहर और परिवहन की धारा के रूप में इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया था.
बहरहाल, गंगा की यह धारा कोलकाता में बढ़ती आबादी, बढ़ते लालच और बढ़ते शहरीकरण के स्वाभाविक नतीजों का शिकार हुई और अब यह घरों के सीवेज ढोती हुई नाले में बदल गई है. अंग्रेजों के जमाने में इस नहर को बाकायदे दुरुस्त रखा जाता था क्योंकि उस समय नदियों की परिवहन में खासी भूमिका होती थी, लेकिन आजादी के बाद इसको भी बाकी विरासतों की तरह बिसरा दिया गया. न तो इसमें पानी के बहाव की देखरेख की गई, न ही खत्म होते पानी के बहाव को बचाए रखने की कोई जरूरत महसूस की गई.
ज्वार के समय हुगली का पानी इसमें काफी मात्रा में आता था और अपने साथ काफी गाद भी लेकर आता था. नतीजतन, यह नदी गाद से भरती गई. इस नदी की तली ऊंची होती गई.
शहर बड़ा हुआ तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाले बेरोकटोक इसमें गिरते रहे. निगम के पास ज्वार और भाटे के वक्त इस नाले में आऩे वाले पानी को नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था.
कभी 75 किलोमीटर लंबी रही यह आदि गंगा आज की तारीख में कई जगहों से लुप्त हो चुकी है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसको पुनर्जीवित करने की भी कोशिशें हुईं और 1990 के बाद इसको फिर से जिलाने की गतिविधियों में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
आदि गंगा को लेकर हुआ एक एक शोध बताता है कि बंडेल के नजदीक, त्रिबेनी (त्रिवेणी) में गंगा तीन हिस्सों में बंट जाती है. एक धारा सरस्वती, दक्षिण-पश्चिम दिशा में सप्तग्राम की तरफ बहती है. दूसरी धारा जिसका नाम जमुना है, दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती है और तीसरी धारा हुगली बीच में बहती हुई आगे चलकर कोलकाता में प्रवेश करके आदि गंगा में मिलकर कालीघाट, बरुईपुर और मागरा होती हुई समुद्र में जा मिलती थी. कई प्राचीन लेख और नक्शों पर भरोसा करें तो आदि गंगा ही मुख्य धारा थी और उसकी वजह से कोलकाता ब्रिटिश काल में बड़ा बंदरगाह बन पाया था.
लेकिन लगभग 1750 में संकरैल के नजदीक हावड़ा में सरस्वती नदी के निचले हिस्से को हुगली नदी से जोड़ने के लिए आदि गंगा की धारा को काट दिया गया. और इसी कारण से ज्यादातर पानी का प्रवाह पश्चिमोत्तर हो गया और हुगली, गंगा की मुख्य धारा बन गई, जो आज भी है.
बहरहाल, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यूडब्ल्यू हंटर ने लिखा है कि इस (आदिगंगा) पुरानी नदी को ही हिंदू असली गंगा मानते हैं. जो इस नदी के किनारे बने पोखरों में अपने लोगों के मुर्दे जलाते हैं. जाहिर है, चिताएं जलाने को लेकर हंटर उस परंपरा की ओर इशारा कर रहे थे जिसके तहत गंगा के किनारे जलाए जाने से मोक्ष मिलने की मान्यता है.
1770 के दशक में आदि गंगा शहर से दूर जाने लगी थी, तब विलियम टॉली ने 15 किमी गरिया से समुक्पोता तक की धारा के बहाव को देखकर हैरान थे और उन्होने आदि गंगा को सुन्दरवन की ओर प्रवाहित होने वाली विद्याधरी नदी से जोड़ दिया. और आज इसी वजह से यह धारा टोलीनाला नाम से जाना जाता है.
पहले जो नदी सुन्दवन के किनारे बोराल, राजपुर, हरीनवी और बरूईपुर के माध्यम से प्रवाहित होती थी, उसका प्रवाह तेजी से अवरुद्ध हो रहा था. हालांकि यह 1940 के दशक तक नावों के जरिए माल ढुलाई का काफी बड़ा साधन था.
1970 के आसपास भी, सुंदरवन से शहद इकट्ठा करने वाले लोग नदी पारकर अपनी नावों को दक्षिण कोलकाला के व्यस्त उपनगर टॅालीगंज की ओर जाने वाले पुल के नीचे खड़ा करते थे.
बहरहाल, आज की तारीख में आदि गंगा लोगों के लालच की शिकार हो गई है. इसमें आपको प्लास्टिक की थैलियां, कूड़ा, कचरा, हेस्टिंग (हुगली के संगम) से गरिया (टूली के नाले) 15 किमी तक 7,851 अवैध निर्माण, 40,000 घर, 90 मंदिर, 69 गोदाम और 12 पशु शेड जैसे अतिक्रमण दिखेंगे (यह आंकड़ा 1998 का है, और हाइकोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने माना था). आपको अगर इसमें नहीं दिखेगा तो पानी.
फिलहाल, गरिया के आगे जाते ही नदी गायब हो जाती है. नरेन्द्रपुर और राजपुर-सोनापुर से लगभग तीन किमी आगे आदि गंगा दिखाई नहीं देती. और उसकी पाट की जगह पक्के मकान, सामुदायिक भवन और सड़कें नमूदार होती हैं. उसके पास कुछ बड़े तालाब दिखाई देते हैं जिनके करेर गंगा, घोसर गंगा जैसे नाम हैं. जाहिर है, ये भी आदि गंगा के पानी से बनने वाले तालाब थे और उनके नामों से यह साबित भी होता है.
इन दिनों आप देश में बाढ़ की खबरें देख रहे होंगे कि देश का पूर्वी इलाका कैसे इससे हलकान है. लेकिन आदि गंगा की मौत मिसाल है कि कैसे फैलते शहर ने नदी निगल ली है. कभी फुरसत हो तो सोचिएगा.
***
पिछले साल जब मैं कोलकाता में था तो मेरे मित्रों की जिद थी कि उन्हें कालीघाट में देवी के दर्शन करने हैं और कालीघाट में दर्शन के बाद अपनी सहज जिज्ञासा में हम नीचे उतर आए थे, जहां एक गंधाता हुआ नाला बह रहा था. लेकिन उस नाले को पार करने के लिए नावें मौजूद थीं और उस वक्त भी नाववाले ने हम चार लोगों से आठ आने (पचास पैसे) की दर से सिर्फ दो रूपए लिए थे. मल्लाह ने बताया था कि यह नाला नहीं, आदि गंगा है. उसने बताया कि नाकतल्ला से गरिया जाते समय रास्ते में अलीपुर ब्रिज के नीचे जिस नाले से भयानक बदबू आती है वह भी आदि गंगा ही है. जिसको स्थानीय लोग टॉली कैनाल कहते हैं.
असल में दो सौ साल पहले तक आदि गंगा हुगली की एक सहायक धारा थी. हालांकि इसका इतिहास थोड़ा और पुराना है. लेकिन अठारहवीं सदी में जब यह अपना स्वरूप खो रही थी तब 1772 से 1777 के बीच विलियम टॉली ने इसका पुनरोद्धार करवाकर इसको नहर और परिवहन की धारा के रूप में इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया था.
बहरहाल, गंगा की यह धारा कोलकाता में बढ़ती आबादी, बढ़ते लालच और बढ़ते शहरीकरण के स्वाभाविक नतीजों का शिकार हुई और अब यह घरों के सीवेज ढोती हुई नाले में बदल गई है. अंग्रेजों के जमाने में इस नहर को बाकायदे दुरुस्त रखा जाता था क्योंकि उस समय नदियों की परिवहन में खासी भूमिका होती थी, लेकिन आजादी के बाद इसको भी बाकी विरासतों की तरह बिसरा दिया गया. न तो इसमें पानी के बहाव की देखरेख की गई, न ही खत्म होते पानी के बहाव को बचाए रखने की कोई जरूरत महसूस की गई.
ज्वार के समय हुगली का पानी इसमें काफी मात्रा में आता था और अपने साथ काफी गाद भी लेकर आता था. नतीजतन, यह नदी गाद से भरती गई. इस नदी की तली ऊंची होती गई.
शहर बड़ा हुआ तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाले बेरोकटोक इसमें गिरते रहे. निगम के पास ज्वार और भाटे के वक्त इस नाले में आऩे वाले पानी को नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था.
कभी 75 किलोमीटर लंबी रही यह आदि गंगा आज की तारीख में कई जगहों से लुप्त हो चुकी है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसको पुनर्जीवित करने की भी कोशिशें हुईं और 1990 के बाद इसको फिर से जिलाने की गतिविधियों में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
आदि गंगा को लेकर हुआ एक एक शोध बताता है कि बंडेल के नजदीक, त्रिबेनी (त्रिवेणी) में गंगा तीन हिस्सों में बंट जाती है. एक धारा सरस्वती, दक्षिण-पश्चिम दिशा में सप्तग्राम की तरफ बहती है. दूसरी धारा जिसका नाम जमुना है, दक्षिण-पूर्व दिशा में बहती है और तीसरी धारा हुगली बीच में बहती हुई आगे चलकर कोलकाता में प्रवेश करके आदि गंगा में मिलकर कालीघाट, बरुईपुर और मागरा होती हुई समुद्र में जा मिलती थी. कई प्राचीन लेख और नक्शों पर भरोसा करें तो आदि गंगा ही मुख्य धारा थी और उसकी वजह से कोलकाता ब्रिटिश काल में बड़ा बंदरगाह बन पाया था.
लेकिन लगभग 1750 में संकरैल के नजदीक हावड़ा में सरस्वती नदी के निचले हिस्से को हुगली नदी से जोड़ने के लिए आदि गंगा की धारा को काट दिया गया. और इसी कारण से ज्यादातर पानी का प्रवाह पश्चिमोत्तर हो गया और हुगली, गंगा की मुख्य धारा बन गई, जो आज भी है.
बहरहाल, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यूडब्ल्यू हंटर ने लिखा है कि इस (आदिगंगा) पुरानी नदी को ही हिंदू असली गंगा मानते हैं. जो इस नदी के किनारे बने पोखरों में अपने लोगों के मुर्दे जलाते हैं. जाहिर है, चिताएं जलाने को लेकर हंटर उस परंपरा की ओर इशारा कर रहे थे जिसके तहत गंगा के किनारे जलाए जाने से मोक्ष मिलने की मान्यता है.
1770 के दशक में आदि गंगा शहर से दूर जाने लगी थी, तब विलियम टॉली ने 15 किमी गरिया से समुक्पोता तक की धारा के बहाव को देखकर हैरान थे और उन्होने आदि गंगा को सुन्दरवन की ओर प्रवाहित होने वाली विद्याधरी नदी से जोड़ दिया. और आज इसी वजह से यह धारा टोलीनाला नाम से जाना जाता है.
पहले जो नदी सुन्दवन के किनारे बोराल, राजपुर, हरीनवी और बरूईपुर के माध्यम से प्रवाहित होती थी, उसका प्रवाह तेजी से अवरुद्ध हो रहा था. हालांकि यह 1940 के दशक तक नावों के जरिए माल ढुलाई का काफी बड़ा साधन था.
1970 के आसपास भी, सुंदरवन से शहद इकट्ठा करने वाले लोग नदी पारकर अपनी नावों को दक्षिण कोलकाला के व्यस्त उपनगर टॅालीगंज की ओर जाने वाले पुल के नीचे खड़ा करते थे.
बहरहाल, आज की तारीख में आदि गंगा लोगों के लालच की शिकार हो गई है. इसमें आपको प्लास्टिक की थैलियां, कूड़ा, कचरा, हेस्टिंग (हुगली के संगम) से गरिया (टूली के नाले) 15 किमी तक 7,851 अवैध निर्माण, 40,000 घर, 90 मंदिर, 69 गोदाम और 12 पशु शेड जैसे अतिक्रमण दिखेंगे (यह आंकड़ा 1998 का है, और हाइकोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने माना था). आपको अगर इसमें नहीं दिखेगा तो पानी.
फिलहाल, गरिया के आगे जाते ही नदी गायब हो जाती है. नरेन्द्रपुर और राजपुर-सोनापुर से लगभग तीन किमी आगे आदि गंगा दिखाई नहीं देती. और उसकी पाट की जगह पक्के मकान, सामुदायिक भवन और सड़कें नमूदार होती हैं. उसके पास कुछ बड़े तालाब दिखाई देते हैं जिनके करेर गंगा, घोसर गंगा जैसे नाम हैं. जाहिर है, ये भी आदि गंगा के पानी से बनने वाले तालाब थे और उनके नामों से यह साबित भी होता है.
इन दिनों आप देश में बाढ़ की खबरें देख रहे होंगे कि देश का पूर्वी इलाका कैसे इससे हलकान है. लेकिन आदि गंगा की मौत मिसाल है कि कैसे फैलते शहर ने नदी निगल ली है. कभी फुरसत हो तो सोचिएगा.
***

Published on August 01, 2019 06:55



