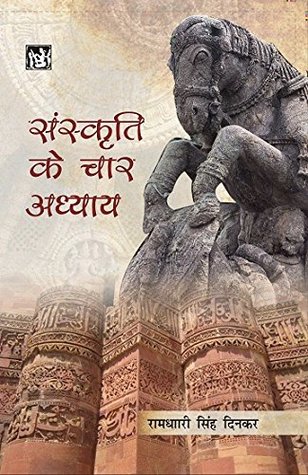Kindle Notes & Highlights
Read between
February 5 - February 26, 2023
प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था।
विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएँ दूर नहीं हुईं। वह आज भी दु:खी है।
व्यष्टि–समष्टि
संसार के सामने यह समस्या नहीं है कि धर्म और विज्ञान में से हम किसे लें और किसे छोड़ दें, प्रत्युत, उसकी समस्या का रूप यह है कि कौन वह उपाय है जिससे धर्म वैज्ञानिक तथा विज्ञान धार्मिक बनाया जा सके।
स्वर्ग का भूमीकरण
अतिमानस की अवतारणा और अतिमानव का विकास है।
बुद्धि से बुद्धि का सुधार करने में विश्वास नहीं करते।
अतिमानव का स्वप्न
अरविन्द से पूर्व, जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने अतिमानव की कल्पना की थी। किन्तु उसने यह सोचा था कि अतिमानव दबंग मानव ही होगा जो सबको मार–पीटकर आगे निकल जाएगा।
अतिमानस से संवलित सभी मनुष्य अतिमनुष्य हो जाएँगे। उनका यह भी कथन है कि अतिमानस, सम्भव है, पहले किसी समूह या व्यक्ति में उतरे। किन्तु, उसके बाद वह फैलता ही जाएगा एवं फैलते–फैलते, एक दिन वह अखिल मनुष्य–जाति को अतिमनुष्यों की जाति में बदल देगा।
संश्लिष्ट योग
परमात्मा की कृपा और मनुष्य के प्रयास, इन दोनों के योग के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता।
क्योंकि विश्व के सभी मनुष्यों को साधना और तपस्या में लगाना असम्भव है, इसलिए, अरविन्द ने अपने तथा अपने आश्रमवासी शिष्यों के ऊपर यह भार रखा कि वे साधनापूर्वक दिव्य जीवन को पृथ्वी पर अवतरित होने को बाध्य करें।
कर्म, ज्ञान और भक्ति के इस संश्लेषण से भी यही शिक्षा निकलती है कि अरविन्द भूत (द्रव्य), जीवन, और मस्तिष्क इन तीनों को दिव्य बनाकर इसी जीवन में दिव्य जीवन की अवतारणा करना चाहते थे।
भूमि का स्वर्गीकरण : महात्मा गांधी का प्रयोग
अहिंसा भारत में ही क्यों?
गांधीजी का मुख्य उद्देश्य अपने देशवासियों के कष्टों का निवारण नहीं, प्रत्युत, मनुष्य के पाशवीकरण का अवरोध था।
जैसा चिन्तन, वैसा कर्म
नय नहीं, आचार
मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं, करने में है।
धर्म सभी क्षेत्रों के लिए
अहिंसा
जहाँ प्रेम है, सत्य वहीं निवास करता है तथा जहाँ प्रेम और सत्य रहते हैं, वहाँ क्रिया, निश्चित रूप से, अहिंसामयी हो जाती है।
अनेकान्तवादी दृष्टिकोण
भारत में अहिंसा के सबसे बड़े प्रयोक्ता जैन मुनि हुए हैं, जिन्होंने मनुष्य को केवल वाणी और कार्य से ही नहीं, प्रत्युत, विचारों से भी अहिंसक बनाने का प्रयत्न किया था।
गांधी और अरविन्द
गांधीजी के नाम के साथ महात्मा की उपाधि पहले–पहल रवीन्द्रनाथ ने लगाई थी।
भारत की कृच्छ्र वैराग्य–साधना और यूरोप का उद्दाम भोगवाद, ये दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण हैं। उचित यह है कि हम दोनों के बीच कोई समन्वय स्थापित करें और मध्यम–मार्ग का सहारा लें।
आदर्श समाज वह होगा, जिसके संन्यासी भी गृहस्थ और गृहस्थ भी संन्यासी होंगे अथवा दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहेगा।
मध्यकालीन भारत में भी वीर–शैव–सम्प्रदाय इसी उद्देश्य को लेकर चला था, जिसका परिणाम यह हुआ कि संन्यास का आदर्श इस सम्प्रदाय के गृहस्थों का भी आदर्श हो गया।
नारी और वैराग्य
मनुष्य के सामने दो से अधिक विकल्प नहीं हैं। या तो वह इन्द्रियों की दासता स्वीकार कर ले और जिधर–जिधर इन्द्रियाँ जाने को कहें, उधर–उधर भागता फिरे। अथवा इन्द्रियों को वश में लाकर वह धर्म के पालन में तत्पर हो।
नारी गृहस्थ जीवन का प्रतीक है। इसलिए, जब–जब प्रवृत्ति का उत्थान हुआ, नारी और गृहस्थ, दोनों की पद–मर्यादा में वृद्धि हुई है। किन्तु, अपने देश में तो वैदिक काल को छोड़कर, प्राय:, सदैव निवृत्ति का ही बोलबाला रहा। अतएव, नारी की मर्यादा वहाँ सदैव दबी रही।
गांधीजी प्रत्येक कर्म का मूल्य इस कसौटी पर आँकते हैं कि उससे मुक्ति में सहायता मिलती है या नहीं।
बहुत प्राचीन काल से लोग जो यह कहते आए थे कि नर और नारी परस्पर एक–दूसरे के पूरक हैं, उस सिद्धान्त का गांधीजी और मार्क्स, दोनों ने, प्रयोगों द्वारा खंडन कर दिया है।
धर्म की अनुभूति
धर्म का वास्तविक निचोड़ नैतिकता के पालन में है। धर्म और नैतिकता परस्पर अविच्छिन्न हैं। फिर भी, बोए गए बीज के लिए जल जो महत्त्व रखता है, नैतिकता के लिए धर्म का वही महत्त्व है।
विश्वदर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन
श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्राचीन दर्शनाचार्यों के समान गीता और प्रमुख उपनिषदों की व्याख्या लिखी
श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन् 1888 ई. में हुआ था।
तुलनात्मक दर्शन का जन्म श्री राधाकृष्णन के ग्रन्थों में हुआ और उन्हीं के ग्रन्थों से प्रत्येक देश के विचारकों में यह भाव जाग्रत हुआ कि विश्व–दर्शन की रचना असम्भव नहीं, सम्भव कार्य है।2
मिशनरियों की आलोचनाओं से ठेस
राधाकृष्णन ने अपनी ‘खंडित आत्मकथा’ में स्वयं लिखा है कि ईसाई धर्म–प्रचारक संस्थाओं के शिक्षकों ने मुझे श्रद्धाहीन बनाकर जिज्ञासा की उस प्राथमिक अवस्था में डाल दिया जहाँ से सभी दर्शनों का जन्म होता
पूर्व और पश्चिम का मिलन
राधाकृष्णन का सन्देश है कि मनुष्य का भावी कल्याण इसमें है कि वह अतीत और वर्तमान तथा पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वय का पता लगाए तथा सामंजस्य स्थापित करे।
दर्शन की उत्पत्ति जीवन से
विज्ञान पर विचार
विज्ञान ने आधिभौतिक सुखों में तो काफी वृद्धि की, किन्तु, मनुष्य के मन को उसने विषण्ण बना डाला। आत्मा, परमात्मा एवं सृष्टि के ध्येय और उद्देश्य को अविचारणीय बताकर उसने मनुष्य को, मानो, यह शिक्षा दी है कि तुम्हारा काम जनमना, बढ़ना, कमाना और खर्च करना, सन्तान उत्पादन करके वृद्ध होना और फिर इस विश्वास को लेकर मर जाना है कि मनुष्य–शरीर भी प्रकृति-परिचालित यन्त्र है और इस यन्त्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त मानव–जीवन का और कोई ध्येय नहीं है।
आज की दुनिया में हम सबके सब नास्तिक हैं। हमारा ईश्वरीय सत्ता में विश्वास, हमारी पूजा और प्रार्थना, ये सब कृत्रिम आचार हैं। जब हम पूजा करते होते हैं, तब भी हमारा ध्यान पूजा में नहीं होकर कहीं और होता है। हमारा प्रत्येक कर्म इस बात की गवाही देता है कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते। हम परमात्मा के सामने नहीं झुककर संसार के सामने झुकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, जो ईश्वर की अपेक्षा हमें अधिक पसन्द न हो।
धर्म जीवन से एकाकार हो