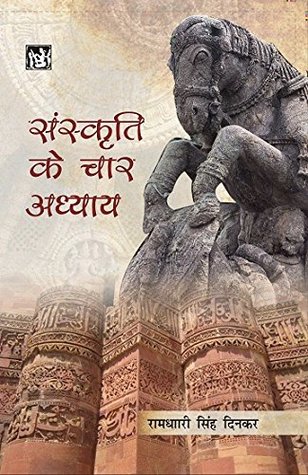Kindle Notes & Highlights
Read between
February 5 - February 26, 2023
क्षमा तभी करनी चाहिए, जब तुम्हारी भुजा में विजय की शक्ति वर्तमान हो।’’
जब पड़ोसी भूखा मरता हो, तब मन्दिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं, पाप है।
तुम साक्षात् नारायण हो। आज मुझे सन्तोष है कि भगवान् ने मेरे समक्ष भोजन किया।’’
मातृजाति के प्रति उदारता
ईसा अपूर्ण थे क्योंकि जिन बातों में उनका विश्वास था, उन्हें वे अपने जीवन में नहीं उतार सके। उनकी अपूर्णता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने नारियों को नरों के समकक्ष नहीं माना।
ब्राह्मण–रूपी सर्प
युगों से ‘ब्राह्मण’ भारतीय संस्कृति का थातीदार रहा है। अब उसेे इस संस्कृति को सबके पास विकीर्ण कर देना चाहिए। उसने इस संस्कृति को जनता में जाने से रोक रखा, इसीलिए, भारत पर मुसलमानों का आक्रमण सम्भाव्य हो सका।
एकता का मन्त्र
अगले पचास वर्षों तक भारतमाता को छोड़कर हमें और किसी का ध्यान नहीं करना है। भारतमाता को छोड़कर और सभी देवता झूठे हैं। उन्हें अपने मन से निकालकर फेंक दो। यही देवी, यही हमारी जाति वास्तविक देवी है।
यह अकरणीय है
पश्चिम से विनिमय
इस्लाम के प्रति दृष्टिकोण
हमारी जन्मभूमि का कल्याण तो इसमें है कि उसके दो धर्म, हिन्दुत्व और इस्लाम, मिलकर एक हो जाएँ। वेदान्ती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर के संयोग से जो धर्म खड़ा होगा, वही भारत की आशा है।’’
धार्मिक एकता पर विचार
भारत पर अशेष ऋण
नरेन्द्रनाथ के समक्ष प्रार्थना की मुद्रा में रामकृष्ण ने कहा था, ‘‘प्रभो! मुझे मालूम है कि तू पुरातन नारायण ॠषि है और जीवों की दुर्गति का निवारण करने के लिए पुन: शरीर धारण करके आया है।’’
प्रवृत्ति का उत्थान : लोकमान्य तिलक
प्रवृत्ति–निवृत्ति
प्रवृत्ति का अर्थ है, ‘संन्यास न लेकर मरण–पर्यन्त चातुर्वर्ण्य-विहित निष्काम कर्म’ करते जाना।
सच्चा योग वह है जो भोग के भीतर भी अक्षुण्ण रहता है, यह जनक के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी।
जीवन–जय का मार्ग
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया, जिनका गीता-विषयक ग्रन्थ कर्मयोगशास्त्र अभिनव हिन्दुत्व का सर्वश्रेष्ठ आचार–ग्रन्थ माना जाता
गीता पर निवृत्ति के बादल
गीता पर जो शांकर भाष्य है, वह भी यही शिक्षा देता है कि गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार–त्याग और कर्म–न्यास का मार्ग है।
गीता के प्रवृत्ति-विषयक रूप को निकाल बाहर करके उसे निवृत्ति–मार्ग का साम्प्रदायिक रूप शांकर भाष्य के द्वारा ही मिला है।’’
रामानुजाचार्य ने प्रस्थानत्रयी की टीका से यह तो सिद्ध किया कि शंकराचार्य का माया–मिथ्यावाद और अद्वैत-सिद्धान्त, दोनों झूठे हैं, किन्तु गीता में प्रवृत्ति की प्रेरणा अथवा कर्म के लिए स्थान है, इसे वे भी नहीं स्वीकार कर सके।
गीता की टीकाओं में महात्मा ज्ञानेश्वर–कृत भाष्य (ज्ञानेश्वरी) का भी बड़ा नाम है। किन्तु ज्ञानेश्वर महाराज का भी यही कहना है कि गीता में सांसारिक कर्मों का समर्थन नहीं है।
गार्हस्थ्य को लोग बहुत–कुछ अनिवार्य हीनता के रूप में देखते थे तथा प्रत्येक गृहस्थ के मन में यह भाव रहता था कि कब उसे सुयोग मिले कि वह संन्यासी हो जाए।
कोई भी पन्थ कर्मठ गृहस्थ को योगी, संन्यासी अथवा भक्त के समकक्ष मानने को तैयार नहीं था। यह अवस्था बहुत–कुछ उपनिषदों के समय से आ रही थी।
हमारा मत है कि गीता एक बार तो भगवान् कृष्ण के मुख से कही गई। किन्तु दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान लोकमान्य ने किया है।
कर्तव्याकर्तव्य
तिलकजी ने पहले–पहल उसके सामने धर्म का व्यावहारिक पक्ष उपस्थित किया और उसे यह बात समझाई कि धर्म वही नहीं है जो स्मृतियों में लिखा हुआ है, प्रत्युत, योग्य उपायों के द्वारा आत्म–रक्षा का प्रयास एवं अन्याय का विरोध भी धर्म का ही अंग है।
गुरुर्वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्। आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्।
‘‘न श्रेय: सततं तेजो, न नित्यं श्रेयसी क्षमा। तस्मान्नित्यं क्षमा तात पंडितैरपवादिता’’।
तिलक और गांधी
योग का अर्थ
स्वर्ग का भूमीकरण : महायोगी अरविन्द
वे तेजस्वी पत्रकार भी थे और एक समय उनके पत्र ‘वन्दे मातरम्’ ने देश के भीतर उग्र राष्ट्रीयता के उद्बोधन की दिशा में बड़ा ही अद्भुत काम किया था।
काल की पृष्ठभूमि
रामकृष्ण और अरविन्द
सारे जगत् की एक समस्या
बुद्धि की अराजकता
अतिमानस की कल्पना
जिस प्रकार जड़ से जीवन और जीवन से मानस की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार, मानस से अब अतिमानस का विकास होना चाहिए।
यह, कदाचित्, वह अवस्था है जब मनुष्य की जानकारी सूचना की स्थिति से ऊपर उठ जाएगी, जब मनुष्य तर्कों से किसी बात को समझने के बदले उसे प्रत्यक्ष रूप से जान लेगा, जैसे हम आँखों–देखी चीज को बुद्धि की प्रक्रिया से समझने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते हैं।
बुद्धि नहीं, सम्बुद्धि
बुद्धि विश्लेषण की पद्धति पर चलती है एवं वस्तुओं का संश्लिष्ट ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो पाता। वस्तुओं के विश्लिष्ट एवं विभक्त रूपों को अरविन्द सत्य नहीं मानते।
भोग और वैराग्य से परे
अरविन्द दोनों की सार्थकता मानते हुए भी मनुष्य को दोनों से आगे जाने का उपदेश देते हैं। सच्चिदानन्द सर्वत्र विद्यमान है। भेद केवल यह है कि निचले स्तर पर (जड़ तत्त्व में) वह सोया हुआ है, अचेतन अथवा अवचेतन का आवरण लिये हुए है। किन्तु उसकी अवज्ञा भी सच्चिदानन्द की ही अवज्ञा है।
विज्ञान की सीमा