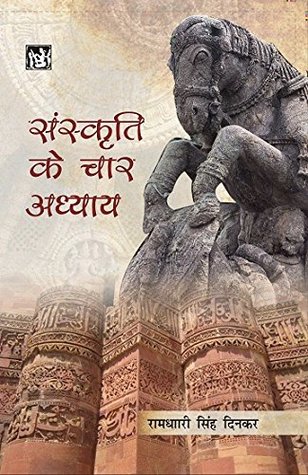Kindle Notes & Highlights
Read between
February 5 - February 26, 2023
ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ कार्य तो धर्म की उपस्थिति में करें और शेष कार्यों के समय उसे भुला दें। धर्म ज्ञान और विश्वास से अधिक कर्म और आचरण में बसता है। यदि हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, तो हमारे आचरण में इस विश्वास का प्रमाण मिलना ही चाहिए।
अरविन्द के प्रसंग में
आज तक हम व्यक्तियों को ईश्वर का अवतार मानते आए हैं। किन्तु ईश्वरावतार की अनुभूति जब व्यक्ति में नहीं होकर, सारे समूह में होने लगेगी, तभी नई मानवता का आविर्भाव होगा, तभी आज की मानवता किसी उज्ज्वलतर मानवता में रूपान्तरित होगी, तभी मनुष्य मात्र का पुनर्जन्म होगा और तभी संसार की नवीन रचना सम्भव होगी।
आज के बौद्धिक मनुष्य और आगामी आध्यात्मिक मनुष्य में वही भेद होगा, जो पशुओं और आज के मनुष्यों में है अथवा जो भेद पौधों और पशुओं के बीच देखा जा सकता है।
आत्मा का धर्म
थियोसोफ़ी जिन गुणों को ऊपर उठाकर सभी धर्मों को एक करना चाहती थी, वे गुण राधाकृष्णन द्वारा आख्यात धर्म में विद्यमान
प्रमाणवादी धर्म का है, जिसके उज्ज्वलतम उदाहरण ईसाई मत और इस्लाम हैं।
इनटुइशन या सम्बुद्धि
तर्कों का सहारा लिये बिना भी मनुष्य एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो सत्य है। पशु बिना सोचे–समझे आसन्न संकट को भाँप जाते हैं, यह उनकी सहज प्रवृत्ति या इंसटिंक्ट है।
‘सम्यक् ज्ञान’
हम आविष्कार तो सम्यक् ज्ञान के बल पर करते हैं, हाँ, उसे प्रमाणित करने के समय हमें तर्क से काम लेना पड़ता है।’’
निवृत्ति और हिन्दू–धर्म
व्यष्टि–समष्टि
धर्म प्राप्त करना नहीं, केवल होना है।
रहस्यवाद
रहस्यवादी अनुभूति का साधन ज्ञान नहीं, परम या सम्यक् ज्ञान है, इसलिए आज के बुद्धिवादी रहस्यवाद को शंका से देखते हैं।
रहस्यवाद मूढ़-धर्मों (डॉगमेटिक धर्म के अर्थ में) के विरुद्ध है, क्योंकि ये धर्म दावा करते हैं कि सृष्टि के सभी रहस्य उन्हें ज्ञात हैं।
प्रवृत्ति–निवृत्ति
बात यह है कि कार्यकारी मनुष्य (एक्ज़िक्यूटिव मैन) वैचारिक (रेफ्लेक्टिव) मनुष्य से बहुत आगे निकल गया है। आवश्यकता इस बात की है कि जीवन के आध्यात्मिक मूल्य और उसकी गहनता में वृद्धि लाई जाए।
धर्म का वास्तविक गुण यह है कि वह मनुष्य को सांसारिकता में विलीन होने से बचाता है। यदि धर्म अपने इस स्वभाव को छोड़ दे तो आधिभौतिक शक्तियाँ उसका गला घोंट डालेंगी।
इस युग में राजनीति धर्म की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन बन सकती है। वस्तुत:, राजनीति के भीतर जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, संसार को धार्मिक मूल्यों के लाभ दिखाई नहीं देंगे।’’
सभ्यता का शाप
हमें वस्तुओं पर नहीं, अपने–आप पर स्वामित्व पाना होगा।
मुस्लिम–नवोत्थान
इस्लाम का अन्तर्राष्ट्रीय रूप
अठारहवीं सदी के बाद से जैसे एशिया पर यूरोप का आतंक रहा है, कुछ वैसा ही आतंक मध्यकालीन यूरोप पर एशिया का था और यह आतंक हिन्दुओं, बौद्धों, कनफ्यूशियस धर्मावलम्बियों का नहीं, प्रत्युत, इस्लाम के धर्म–योद्धाओं का था।
विज्ञान ने यूरोप के भीतर ज्ञान के अद्भुत चक्षु खोल दिए एवं कोलम्बस तथा वास्को–डि–गामा के अनुसन्धानों ने उसे समुद्र का सम्राट् बना दिया।
इस्लाम के प्रति यूरोप का यह द्रोह–भाव प्रथम विश्व–युद्ध के अन्त में होनेवाली सन्धि–वार्ता में और भी प्रत्यक्ष हुआ जब सन्धि के शर्तनामे के अनुसार टर्की का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया और संसार में कोई भी ऐसा इस्लामी राज्य नहीं रह गया, जो अपने को स्वाधीन कह सके।
वहाबी आन्दोलन
वहाबी आन्दोलन के प्रवर्तक मुहम्मद इब्न–अब्दुल वहाब थे जिनका जन्म सन् 1700 ई. के करीब अरब–देश के नज्द प्रान्त में हुआ था।
तसव्वुफ और सूफी–मत की आलोचना वे इसलिए करने लगे कि सूफी इस्लाम के नियमों का उल्लंघन करते थे। फकीरों एवं साधुओं की पूजा को वे घृणित पाप बताने लगे।
बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने को बदलकर युगानुरूप बनाने के लिए इस्लाम ने जो भी प्रयास किए थे, उन्हें वहाब ने एकबारगी काट दिया और समाज को उन्होंने लौटाकर उस स्थान पर ले जाना चाहा, जो इस्लाम की आरम्भिक पवित्रता का स्थान था।’’
अब्दुल वहाब ने रोकों की जो धार्मिक सूची तैयार की, उसमें तम्बाकू और कॉफी ही नहीं, बल्कि संगीत, रेशम, सोना, चाँदी और हीरे भी आ गए क्योंकि ये सामग्रियाँ भी विलासिता की थीं। बुजुर्गों की क़ब्रों की कौन कहे, हज़रत मुहम्मद की क़ब्र पर जाकर पूजा करने को भी उन्होंने शिर्क करार दिया।
इस्लाम सुधारों का विरोधी है; यानी सुधरा हुआ इस्लाम, इस्लाम नहीं कोई और चीज है।’’
चौदहवीं सदी में अरब में इब्ने–तीमिया नाम के सुधारक हुए थे। उनका भी यही भाव था और सारी जिन्दगी वे लोगों को इस बात के लिए सजा दिलवाते रहे कि उन्होंने इस्लाम के परम्परागत नियमों का उल्लंघन किया था।
शेख अहमद सरहिन्द, इब्ने तीमिया, औरंगजेब, वहाब, हाली और इक़बाल ने इस्लाम के लिए जो कुछ किया, वह लगभग एक ही प्रकार का कार्य था।
अब्दुल वहाब की मृत्यु (सन् 1787 ई.) के बाद, सऊद वहाबी–सम्प्रदाय के नेता
भारत में वहाबी आन्दोलन
सन् 1804 ई. के लगभग हाजी शरीयतुल्लाह ने बहादुरपुर (जिला फरीदपुर, बंगाल) में किसान–आन्दोलन का आरम्भ किया। उनके अनुयायी फ़रायज़ी कहलाते थे।
यह देश दारुल–हरब (शत्रु-देश) हो गया है। इसलिए, मुसलमानों को चाहिए कि वे इस देश में जुमे की नमाज़ पढ़ना छोड़ दें।
भारत में वहाबी–आन्दोलन के सबसे प्रभावशाली नेता रायबरेली के सैयद अहमद हुए। सन् 1822 ई. में उन्होंने मक्का की तीर्थ–यात्रा की और वहीं वे वहाबी आन्दोलन के मूल–प्रवर्तकों के सम्पर्क में आए।
इस्लाम और अंग्रेजी राज
अंग्रेज और अंग्रेजियत से प्रेम
सर सैयद अहमद खाँ
इसी आन्दोलन के नेताओं ने मुल्लाओं से फतवा लेकर मुसलमानों में यह घोषणा करवाई कि भारत दारुल–हरब नहीं, दारुल–इस्लाम है और जो लोग जुमे के दिन सामूहिक नमाज नहीं पढ़ते, वे धर्म–विरुद्ध काम करते हैं, क्योंकि अंग्रेज बहादुर किसी के धर्म में कोई दखल देना नहीं चाहते।
एक दूसरी किताब लिखकर उन्होंने उन मुसलमानों की गिनती गौरव से करवाई जिन्होंने गदर के समय अंग्रेजों का साथ दिया था,10 यही नहीं, वहाबियों की ओर से भी उन्होंने यही दलील दी कि वे अंग्रेजों के विरोधी नहीं, सिर्फ सिक्खों के शत्रु थे।
कहा कि इस्लाम आजादी का तरफदार नहीं हो सकता।
अलीगढ़ में मोहमडन एंग्लो–ओरियंटल कॉलेज (जो सन् 1875 ई. में खुला और सन् 1920 ई. में मुस्लिम-यूनिवर्सिटी में परिणत हो गया) की स्थापना करते हुए उन्होंने उसके उद्देश्यों में जहाँ यह बात रखी कि ‘‘मुसलमान अपने धर्म की रक्षा करते हुए अंग्रेजी पढ़ सकें’’, वहाँ उसी घोषणा–पत्र में वे यह कहना नहीं भूले कि ‘‘इस संस्था का उद्देश्य मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार की सुयोग्य प्रजा बनने के योग्य बनाना है।’’
सर सैयद ने केवल अंग्रेजी शासन को ही स्वीकार नहीं किया, प्रत्युत, वे चाहते थे कि मुसलमान खुले दिल से अंग्रेजियत को भी कबूल कर लें। नई रोशनी के प्रति अपने इस रुजहान के कारण उन्हें प्राचीनता के पिष्ट-पेषकों की निन्दा भी सहनी पड़ी।12 उनके दल को लोग ‘नेचरी’ (अंग्रेजी के नेचर शब्द से) तथा उन्हें अंग्रेजों का भक्त कहा करते थे।
ईसाइयत के एकपत्नीव्रतवाले विश्वास को उन्होंने गलत कहा और यह दलील पेश की कि चूँकि मनुष्य का स्वभाव एकाधिक–त्रियागामी है इसलिए, इस्लाम यदि चार पत्नियाँ रखने की आज्ञा देता है, तो यह कोई अप्राकृतिक बात नहीं