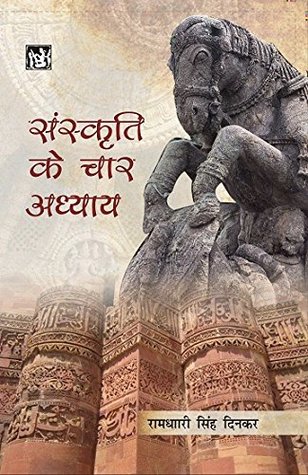Kindle Notes & Highlights
Read between
February 5 - February 26, 2023
नवोत्थान की रीढ़
जिस नवोत्थान का आरम्भ राममोहन राय, दयानन्द और विवेकानन्द ने किया था, और जिसकी धारा में हम आज भी तैरते हुए आगे जा रहे हैं, वेदान्त उस आन्दोलन की रीढ़ है।
निवृत्ति का त्याग
स्वामी विवेकानन्द और लोकमान्य तिलक ने वेदान्त और गीता की ही नई व्याख्या करके यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय वैदिक धर्म का मूल उपदेश निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति है।
उन्नीसवीं सदी का नवोत्थान, भारत में प्रवृत्तिवाद का ही अनुपम उत्थान था।
निवृत्ति की धारा में बहते–बहते हिन्दू एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे थे, जहाँ स्वाधीनता और पराधीनता में कोई भेद नहीं था, अन्याय और न्याय में कोई अन्तर नहीं था और न कोई अत्याचार ही ऐसा था, जिसका उत्तर देना आवश्यक हो।
उन्नीसवीं सदी के बाद से भारतीय साहित्य में क्रान्तिकारी और अन्य–विरोधी स्वर बड़े जोर से गूँजने लगे। यह, स्पष्ट ही, गीता और वेदान्त की प्रवृत्तिमार्गी टीका का परिणाम है।
ब्राह्म–समाज
राममोहन राय
वे जाति के ब्राह्मण थे।
1809 ई. में रंगपुर के कलक्टर के दीवान हो गए। बाद में, वे किसी नाबालिग जमींदार के मैनेजर नियुक्त किए गए और सन् 1815 ई. में उन्होंने नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया।
सुधार के कार्य
सन् 1829 ई. में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती–प्रथा को गैर–कानूनी घोषित करके इसके विरुद्ध कड़ा कानून बना दिया। यह राममोहन राय के ही प्रयत्नों का शुभ परिणाम था।
ईसाइयत पर विचार
ईसाई धर्म पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम ‘The precept of Jesus, the guide to peace and happiness’ था।
विश्ववादी और भारतीय
हिन्दुत्व की पवित्रता, इस्लाम की रुचि तथा ईसायत की सफाई उन्हें बेहद पसन्द थी।
सारे संसार में विश्ववाद के सबसे प्रथम व्याख्याता राममोहन राय हुए हैं।
विज्ञान और वेदान्त का मेल
राममोहन की विशेषता यह थी कि एक ओर तो वे वेदान्त के स्थान से हिलने को तैयार नहीं थे; दूसरी ओर, वे अपने देशवासियों को अंग्रेजी के द्वारा पाश्चात्य विद्याओं में निष्णात बनाना चाहते थे। भारतवासी संस्कृत, अरबी और फारसी पढ़कर बस मान लें अथवा वे अंग्रेजी पढ़कर क्रिस्तान हो जाएँ, इन दोनों खतरों से वे भारतवर्ष को बचाना चाहते
इतिहास में राममोहन का स्थान उस महासेतु के समान है जिस पर चढ़कर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत से अज्ञात भविष्य में प्रवेश करता है।
ब्राह्म–समाज के जन्म की वेदना
राममोहन राय ने सन् 1816 ई. में कलकत्ते में वेदान्त कॉलेज की स्थापना की।
ब्राह्म–समाज का जन्म
20 अगस्त, सन् 1828 ई. को उन्होंने ब्राह्म–समाज की स्थापना कलकत्ते में की। इस समाज का रूप, निर्विवाद रूप से, भारतीय था और भारतीय परम्परा में कहें तो कह सकते हैं कि यह अद्वैतवादी हिन्दुओं की संस्था थी।
ट्रस्ट के दस्तावेज में (सन् 1830 ई.) स्पष्ट प्रतिबन्ध रखा गया था कि इस समाज में होनेवाली पूजा में किसी भी ऐसी सजीव या निर्जीव वस्तु की निन्दा नहीं की जाएगी, जिसकी थोड़े से लोग भी पूजा या आराधना करते हों तथा इस समाज में केवल ऐसे ही उपदेश किए जाएँगे, जिनसे सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता, समीपता और सद्भाव की वृद्धि होती हो।
राममोहन की उदार दृष्टि
27 सितम्बर, 1833 ई. को ब्रिस्टल में उनका देहान्त हो गया।
महर्षि देवेन्द्रनाथ
ब्राह्म–समाज के नेतृत्व का भार महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के कन्धों पर पड़ा।
महर्षि देवेन्द्रनाथ के समय में आकर ब्राह्म–समाज अपनी जड़ (हिन्दुत्व) से दूर जाने लगा और केशवचन्द्र के समय में तो वह हिन्दुत्व से इतना अलग और ईसाइयत के इतना समीप जा पहुँचा
केशवचन्द्र सेन
केशवचन्द्र सेन ने ब्राह्म–समाज में प्रवेश सन् 1857 ई. में किया, जब उनकी उम्र केवल उन्नीस साल की थी।
1866 ई. में अपना समाज अलग कर लिया, जिसका नाम ब्राह्म–समाज ही बना रहा। देवेन्द्रनाथ ठाकुर के अधिकार में जो समाज रह गया, उसे वे आदि–ब्राह्म–समाज कहने लगे।
किन्तु, कूच–बिहार के राजकुमार से जब केशव बाबू की पुत्री के ब्याह का प्रस्ताव आया, तब चारों ओर कानाफूसी होने लगी कि देखें, अब केशवचन्द्र क्या करते हैं। कूच–बिहार के राजा हिन्दू थे।
जो समाजी केशवचन्द्र के विरोधी थे, उन्होंने अपने समाज को साधारण ब्राह्म–समाज कहना आरम्भ किया और केशवबाबू ने जो सभा अपने साथ रखी, उसका नाम उन्होंने नव–विधान–सभा कर दिया।
शरमाए हुए शूरमा
महाराष्ट्र में नवोत्थान
परमहंस–समाज और प्रार्थना–समाज
सन् 1849 ई. में बम्बई में परमहंस–समाज नामक एक संस्था बनी थी, जिसका उद्देश्य जाति–प्रथा का भंजन था।
प्रार्थना–समाज के नाम से खुली, जिसके मुख्य उद्देश्य चार थे–1. जाति–प्रथा का विरोध, 2. विधवा–विवाह का समर्थन, 3. स्त्री–शिक्षा का प्रचार और 4. बाल–विवाह का अवरोध।
प्रार्थना–समाज की भी प्रार्थनाओं में मन्त्र, वेद, उपनिषद्, कुरान, जेन्दावेस्ता और बाइबिल, सभी धर्म–ग्रन्थों से लिये जाते थे और समाज के सदस्य सभी धर्मों पर एक समान श्रद्धा रखते
महादेव गोविन्द रानाडे
गोपालकृष्ण गोखले रानाडे के शिष्य थे।
रानाडे चितपावन ब्राह्मण थे। उनका जन्म सन् 1842 ई. में नासिक जिले में हुआ
रानाडे की पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया और दूसरा विवाह उन्होंने विधवा से नहीं करके एक ग्यारह साल की कुमारी बालिका से किया। कहते हैं, यह विवाह उन्हें अपनी इच्छा और भावना के विरुद्ध, अपने पिता के दुराग्रह के कारण करना पड़ा था।
रानाडे, आगरकर और तिलक
सन् 1891 ई. में जब ‘एज अॉफ कान्सेंट बिल’ इम्पीरियल काउंसिल में पेश हुआ, तब उनका तीव्र विरोध तिलकजी ने किया
शारदा–सदन नामक संस्था को लेकर घटी। यह संस्था पंडिता रामा बाई की कायम की हुई थी।
श्रीयुत केलकर ने लिखा है कि उस समय सुधारकों का दल गणेश–पूजा पर जितनी ही बौखलाहट मचाए1 हुए था, मुसलमानों के अत्याचारों पर वह उतना ही मौन था। सरकार मुसलमानों के साथ थी।