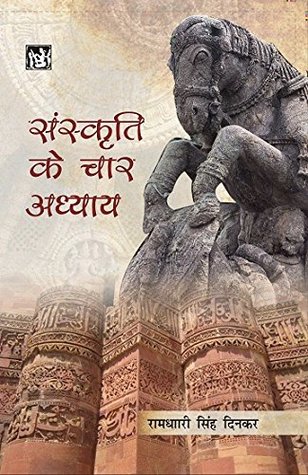Kindle Notes & Highlights
Read between
February 5 - February 26, 2023
इकबाल ने जिस पीर को अपना गुरु बनाया था, वह शेख अहमद सरहिन्दी की ही परम्परा में पड़ता था।
सिक्ख–धर्म
गुरु नानक
बगदाद में उनकी याद में एक मन्दिर भी है, जिस पर तुर्की भाषा में शिलालेख मौजूद हैं। गुरु नानक के सैयद–वंशी चेलों के उत्तराधिकारी अभी तक उस मन्दिर की रक्षा करते
गुरु नानक की उपासना के चारों अंग (सरन–खंड, ज्ञान–खंड, करम–खंड तथा सच–खंड) सूफियों के चार मुकामात (शरीअत, मारफत, उकबा और लाहूत) से निकले हैं, ऐसा विद्वानों का विचार है। गुरु नानक और शेख फरीद के बीच गाढ़ी मैत्री थी, इसके भी प्रमाण मिलते हैं।
सिक्ख–मत, हिन्दुत्व और इस्लाम
गुरु नानक का ईश्वर निराकार पुरुष है। ‘‘वह स्थान–विशेष में रहकर सिंहासनासीन होनेवाला नहीं है, बल्कि, सर्वात्म–भाव से अणु–अणु के भीतर ओत–प्रोत है और उसके सार्वभौमिक नियमों का पालन विश्व के प्रत्येक पदार्थ द्वारा, स्वभावत: होता जा रहा है।’’
वे कर्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, निर्वाण और माया को मानते हैं, एवं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिदेवत्व में विश्वास करते हैं।
सिक्ख–धर्म में ‘वाह गुरु’ का जो धार्मिक नारा प्रचलित है, उसकी एक व्याख्या कहीं से डोरोथी फील्ड ने उद्धृत की है,5 जिसके अनुसार ‘वा’ का संकेत वासुदेव, ‘ह’ का हरि, ‘गु’ का गोविन्द और ‘रु’ का राम की ओर है।
गुरु और ग्रन्थ
नानकदेव के वचनों को, पहले–पहल, गुरु अंगद ने ‘गुरुमुखी’ लिपि में लिखा। तभी से यह लिपि चालू हुई है।
‘ग्रन्थ साहिब’ का संकलन और सम्पादन सन् 1604 ई. में पाँचवें गुरु अर्जुनदेव ने किया।
‘दशम ग्रन्थ’
इस्लाम से टक्कर
‘उनके ऊपर जलती हुई रेत डाली गई, उन्हें जलती हुई लाल कड़ाही में बिठाया गया और उन्हें उबलते हुए गरम जल से नहलाया गया। गुरु ने सब–कुछ सहन कर लिया और उनके मुँह से आह तक नहीं निकली।’8 फिर रावी–स्नान के बहाने वे कैद से बाहर आए और रावी के तट पर जाकर उन्होंने जीवन–लीला समाप्त कर दी। सिक्खों के प्रसंग में सुविख्यात जहाँगीरी न्याय का यही उदाहरण संसार के सामने आया।
गुरु हरगोविन्द के समय सिक्खों से मुगल तीन लड़ाइयों में भिड़े। पहली लड़ाई सन् 1628 ई. में, दूसरी सन् 1630 ई. में और तीसरी सन् 1634 ई. में हुई। कहते हैं, सन् 1634 ई. वाली लड़ाई काफी भयानक थी।
यह परम्परा चल पड़ी कि हर हिन्दू–परिवार अपने ज्येष्ठ पुत्र को गुरु की शरण में उत्सर्ग कर दे।
गुरु गोविन्द का अवतार
‘पाँच प्यारे 9 धर्म के खालिस अर्थात् शुद्ध सेवक हैं और उन्हें लेकर मैं आज से खालसा–धर्म की नींव डालता हूँ।’
पंच ककार हैं—(1) कंघी (बाल सुलझाने के लिए); (2) कच्छा (फुर्ती के लिए); (3) कड़ा (यम, नियम और संयम का प्रतीक); (4) कृपाण (आत्मरक्षा के लिए) तथा (5) केश (जिसे, प्राय: सभी गुरु धारण करते आए थे)।
रहतनामे में केश–कर्तन को महान् अपराध माना गया है।
शासक वजीरखाँ के हाथों में सौंप दिया11 और उस दुष्ट ने इन दो बच्चों को सिर्फ इसलिए दीवारों में चुनवा दिया कि, पितृ–संस्कार के कारण, वे स्वेच्छा से मुसलमान होने को तैयार नहीं थे।
जिस परमात्मा को गुरुनानक ‘निरंकार पुरुख’ कहते थे, उसके नाम गुरु गोविन्द ने ‘असिध्वज’, ‘महाकाल’ और ‘महालौह’ रखे।
सेवक सिक्ख हमारे तारिय, चुनि–चुनि शत्रु हमारे मारिय। जो हो सदा हमारे पच्छा, श्री असिधुजजी करियहु रच्छा। मैं न गनेसहिं प्रथम मनाऊँ, किशन–विशन कबहूँ नहीं ध्याऊँ। महाकाल रखवार हमारे, महालोह मैं किंकर थारे। अपना जान मुझे प्रतिपारिय, चुनि–चुनि शत्रु हमारे मारिय। ×
सिक्खों ने शूकर को भक्ष्य मानकर एक प्रकार से गो–भक्षण की प्रवृत्ति का जवाब निकाला था।
सिक्ख–मत और हिन्दुत्व
जब अंग्रेजों ने पहले सिक्खों को हराकर पंजाब पर अधिकार किया, तो उन्हें सिक्ख–पन्थ तथा सिक्ख–मत को लोगों की दृष्टि में तुच्छ तथा हेय दिखलाने की आवश्यकता हुई, जिससे लोग उससे घृणा करने लगें।
कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव
कला की भारतीय परम्परा
बुद्ध के समय चित्र इतने मोहक बनते थे कि बुद्ध ने भिक्षुओं को चित्र देखने की मनाही कर दी थी।
भित्ति–चित्र का इस देश में इतना अधिक प्रचार था कि भत्ति शब्द ही यहाँ चित्रों के आधार के लिए रूढ़ हो गया, जैसे यूरोप में चित्र का आधार केनवास समझा जाता है।
अजन्ता के चित्रों के विषय, मुख्यत:, बौद्ध धर्म के विषय हैं।
अजन्ता की गुफाओं में जिस कला के उदाहरण हैं, उसी के उदाहरण सिगिरिया (श्रीलंका) और बाघ (ग्वालियर, मध्यभारत) की गुफाओं में भी मिलते हैं।
मुस्लिम–आगमन के बाद
इस्लाम में मूर्ति–पूजा सबसे भयानक शिर्क मानी जाती थी। इससे यह सिद्धान्त निकल आया कि मूर्ति और चित्र–रचना भी शिर्क हैं।
कुरान में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्राणियों के चित्र बनाता है, वह सृष्टि के रचयिता के काम में दखल देता है। कयामत के दिन भगवान् उससे कहेंगे कि तूने मेरी बराबरी करना चाहा था। अतएव, अपने चित्रों में जीवन डालकर, अपना काम पूरा कर। और जब चित्रकार यह काम नहीं कर पाएगा, तब भगवान् उसे नरक भेज देंगे।
मुगल–शैली
अकबर से पहले, मुगलों के समय में जो चित्र–शैली थी, वह ईरानी थी।
पंचतन्त्र का फारसी अनुवाद अयारे–दानिश के नाम से अबुल फजल ने तैयार किया था। पंचतन्त्र का एक दूसरा अनुवाद अनवार–सुहेली के नाम से भी प्रचलित था।
शाहजहाँ के बाद औरंगजेब का समय आया और मुगल–कला इसी काल में समाप्त हो गई।
जब अकबर ने ईरान से चित्रकार बुलवाए, तब आरम्भ में तो उनके चित्र भारतीय रहे, किन्तु, धीरे–धीरे ईरान की पुस्तकालेखन और लघुचित्रकारीवाली परम्परा का मेल यहाँ की भित्ति–चित्रवाली परम्परा से हो गया और इसी सामंजस्य से, मुगल–कलम का जन्म हुआ। यह मुगल–कलम जब राजपूत–कलम से मिलकर और अधिक भारतीय हो गई, तब पहाड़ी–कलम का विकास हुआ।
पहाड़ी चित्रों का सबसे मनोहर रूप कृष्णलीला के चित्रों में है।
हिन्दू और मुस्लिम कलाओं की विशेषताएँ
मूर्तियों और चित्रों में जब भी कोई देवता या मनुष्य किसी कार्य में रत दिखाया जाता है, तब उसकी आकृति पर अविचिलत शान्ति की आभा वर्तमान रहती है।
सुरम्य निर्वैयक्तिकता भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता है।
अच्छे चित्रकारों को दो वस्तुओं का चित्रण करना पड़ता है। एक वस्तु है मनुष्य की देह और दूसरी उसकी आत्मा की आकांक्षा। देह का चित्रण, फिर भी, अपेक्षाकृत सरल कार्य है, किन्तु आत्मा की आकांक्षा का चित्रण कठिन होता है, क्योंकि इस निराकार विषय को भी चित्रकार को अंगों के घुमाव एवं अवयवों की प्रवृत्ति के द्वारा ही चित्रित करना पड़ता है।’’
राजपूत और मुगल कलमों का भेद
मुगल–कला में व्यक्ति–चित्रों की प्रधानता है। राजपूत–कला में ऐसे चित्र बहुत कम हैं।
रीतिकाव्य और राजपूत–कलम
मुगल और राजपूत–कलमों के मेल से जो पहाड़ी–कलम निकली, वह खूब कामयाब रही और उसने भारतीय भावनाओं की अभिव्यक्ति भी सफलता से की।