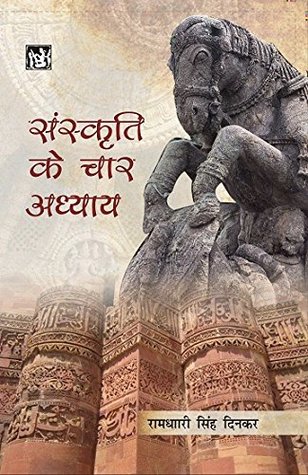Kindle Notes & Highlights
Read between
February 5 - February 26, 2023
वेद सारी मनुष्य जाति का प्राचीनतम ग्रन्थ है।
संसार भर की आर्य भाषाओं में जितने भी शब्द हैं, वे संस्कृत की सिर्फ पाँच सौ धातुओं से निकले हैं।
भारतवर्ष की जनता, मुख्यत: आर्य और द्राविड़ नस्लों की बनी हुई है और उसमें थोड़ी–सी छौंक शबर और किरात (मुंड और तिब्बत–बर्मी) की है।’’
धनुष चलाने की कला नीग्रो जाति की देन है। नीग्रो जाति असभ्य होती हुई भी बड़ी साहसी रही होगी,
आर्यों का संघर्ष दास और असुर जाति के लोगों से हुआ था
ईसा से लगभग 3500 वर्ष पूर्व ये लोग भूमध्यसागर से भारत की ओर चले। रास्ते में इनकी शाखाएँ इराक और ईरान में भी रह गईं, जिन्होंने, कदाचित्, सुमेर–सभ्यता की नींव डाली। जो लोग भारत पहुँचे, उन्होंने मोहनजोदड़ो आदि के पास सिन्धु-सभ्यता की स्थापना
यूरोपीय तर्क आधुनिक बुद्धि का सम्मोहनास्त्र
दूसरा अवन्ती की माहिष्मती नगरी होकर, जो नर्मदा पर अवस्थित थी।
शब्द के स्थान पर शब्द बैठाकर भी हम भारत की एक भाषा के साहित्य को भारत की दूसरी भाषा में ले जा सकते
आर्यों का मूल–स्थान
यह ठीक है कि वैदिक संहिताओं से यही विदित होता है कि आर्य जहाँ रहते थे, उस देश को वे सप्त–सैन्धव10 कहते
केवल भारत में संस्कृत ने नई भाषाओं को जन्म देकर भी अपने अस्तित्व को कायम रखा
आर्य शब्द की व्युत्पत्ति ऋ धातु से बताई जाती है जिसका अर्थ गति होता
भारत में इस प्लावन के नायक मनु हैं और सामी देशों में हजरत नूह।
जेन्दावेस्ता में इन्द्र का समावेश उन देवों में किया गया है, जो असुर नहीं हैं, जो असुर के विरोधी हैं और इस कारण घृणायोग्य हैं।’’
ऋग्वेद आर्यों का ही नहीं, समस्त विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ
ईसा से 3000 वर्ष पूर्व भारत में लेखन–कला का प्रचार था।
किरातों का मूल–अभिजन पूर्वी चीन में था।
किरात–समाज में नारियाँ उतनी पराधीन कभी नहीं थीं जितनी आर्यों के समाज में।
अवेस्ता इस जाति का प्राचीनतम ग्रन्थ
गाथा और ऋग्वेद के पारिभाषिक शब्दों में भी समानता
ईसाइयत और इस्लाम में भगवान् और शैतान की जो कल्पना उदित हुई, वह जरथुस्त्र–धर्म की देन थी।
यह अग्नि भी पारसी लोग अपने साथ भारत ले आए और उसे उन्होंने बम्बई के उत्तर उदवाद नामक स्थान में मन्दिर बनाकर स्थापित कर दिया। यह अग्नि आज भी जल रही है।
शीरीं और फरहाद, ये भी जरथुस्त्र–धर्मावलम्बी प्रेमी हुए हैं।
यह अनुमान अत्यधिक सुदृढ़ हो जाता है कि पुराणों की परम्परा वेदों की परम्परा से कम प्राचीन नहीं है।
निगम अपौरुषेय हैं; उन्हें किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, क्योंकि ईश्वर भी, आखिर को, पुरुष ही है। किन्तु, आगम शिव, शक्ति अथवा विष्णु के मुख से उद्गीर्ण माने जाते हैं। आगमों की पूर्ण परिणति भक्ति में हुई।
संसार को सत्य मानकर जीवन के सुखों में वृद्धि करने की प्रेरणा कर्मठता से आती है, प्रवृत्तिमार्गी विचारों से आती है। इसके विपरीत, मनुष्य जब मोक्ष को अधिक महत्त्व देने लगता है, तब कर्म के प्रति उसकी श्रद्धा शिथिल होने लगती
यह विलक्षण बात है कि वेदों में नरक और मोक्ष की कल्पना, प्राय:, नहीं के बराबर है।
मुनि गृहस्थ नहीं होते थे।
ऋषि और मुनि, दो भिन्न सम्प्रदायों के व्यक्ति समझे जाते थे।
शिल्प करनेवाले लोग त्रिवर्ण में नहीं गिने जाएँगे।
महर्षि व्यास का जन्म एक धीवर–कन्या की कुक्षि से हुआ था।
तमिल–परम्परा की कथा यह है
द्राविड़ भाषाओं की सभी लिपियाँ ब्राह्मी से निकली हैं।
यजुर्वेद-संहिता की दो शाखाएँ हैं जो, क्रमश:, शुक्ल-यजुर्वेद और कृष्ण-यजुर्वेद के नाम से विख्यात हैं।
भागवत पुराण की रचना दक्षिण में हुई थी।
हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो, सही माने में, किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा नहीं
तमिल जो भारत की अर्वाचीन भाषाओं में सबसे प्राचीन है, संस्कृत उससे भी, कम–से–कम दो हजार वर्ष अधिक पुरानी भाषा है।
हम सौ वर्षों तक जिएँ।
ऋग्वेद में तीन ही वर्ण हैं, शूद्र को चौथे वर्ण के रूप में वहाँ गिना नहीं गया है।
शूद्र भी, किसी–न–किसी प्रकार के, द्विज थे और उनका स्थान, घट–बढ़कर, क्षत्रियों के ही समान
जाबाला का पुत्र सत्यकाम ब्रह्मविद्या का अधिकारी ब्राह्मण समझा गया, यद्यपि, जाबाला इतना भी नहीं जानती थी कि सत्यकाम किस पुरुष के संसर्ग से जनमा
उच्च वर्ण के पुरुषों का हीन वर्ण की स्त्रियों से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। और हीन वर्ण के पुरुषों का उच्च वर्ण की स्त्रियों से विवाह प्रतिलोम विवाह।
जात–पाँत की ठीक जात–पाँत के रूप में स्थापना 10वीं शताब्दी ई. में आकर हुई है और, उसके बाद भी, मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया।
जो द्विज थे, उनके भीतर तो अन्तर्जातीय विवाह चलता ही था, द्विज और शूद्र के बीच भी विवाह पर रोक नहीं थी।
श्री सेनगुप्त ने 209 जातियों की गणना की है, जो आर्येतर जातियाँ थीं और जिनका आर्य–समाज में प्रवेश प्रतिलोम या अनुलोम विवाहों के द्वारा हुआ है।
वैदिक युग में नारियों का बड़ा ही पूजनीय स्थान था।
स्वयंवर–समारोह का आयोजन केवल कन्या-पक्षवाले ही नहीं, वर-पक्षवाले भी करते थे।
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा।
युधिष्ठिर–सर्प–संवाद में