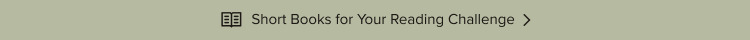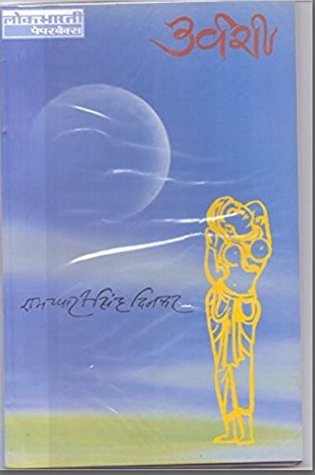More on this book
Kindle Notes & Highlights
नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती, न नर नारी के आलिंगन में सन्तोष मानता है। कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग रहने नहीं देती, और जब वे मिल जाते हैं, तब भी, उनके भीतर किसी ऐसी तृषा का संचार करती है, जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर अनुपलब्ध है।
इन्द्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है।
पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर नहीं रुकता, वह शरीर से जन्म लेकर मन और प्राण के गहन, गुह्य लोकों में प्रवेश करता है, रस के भौतिक आधार से उठकर रहस्य और आत्मा के अन्तरिक्ष में विचरण करता है।
कविता की भूमि केवल दर्द को जानती है, केवल बेचैनी को जानती है, केवल वासना की लहर और रुधिर के उत्ताप को पहचानती है।
जब देवी सुकन्या यह सोचती हैं कि नर-नारी के बीच सन्तुलन कैसे लाया जाए, तब उनके मुँह से यह बात निकल पड़ती है कि यह सृष्टि, वास्तव में, पुरुष की रचना है। इसीलिए, रचयिता ने पुरुषों के साथ पक्षपात किया, उन्हें स्वत्व-हरण की प्रवृत्तियों से पूर्ण कर दिया। किन्तु, पुरुषों की रचना यदि नारियाँ करने लगें, तो पुरुष की कठोरता जाती रहेगी और वह अधिक भावप्रवण एवं मृदुलता से युक्त हो जाएगा।
पुरुष की रचना पुरुष करे तो वह त्रासक होता है; और पुरुष की रचना नारी करे तो लड़ाई में वह हार जाता है।
दूर-दूर तक फैल रही दूबों की हरियाली है, बिछी हुई इस हरियाली पर शबनम की जाली है। जी करता है, इन शीतल बूँदों में खूब नहाएँ।
बिछा हुआ है जाल रश्मि का, मही मग्न सोती है, अभी मृत्ति को देख स्वर्ग को भी ईष्र्या होती है।
इन ज्वलन्त वेगों के आगे मलिन शान्ति सारी है, क्षण भर की उन्मद तरंग पर चिरता बलिहारी है।
इसमें क्या विस्मय है? कहते हैं, धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। लगता है यह जिसे, उसे फिर नींद नहीं आती है,
दिवस रुदन में, रात आह भरने में कट जाती है। मन खोया-खोया, आँखें कुछ भरी-भरी रहती है; भींगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है।
प्रेम मानवी की निधि है, अपनी तो वह क्रीड़ा है; प्रेम हमारा स्वाद, मानवी की आकुल पीड़ा है।
"स्वर्ग-स्वर्ग मत कहो, स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है, पर, इस महास्वर्ग में मेरे हित क्या आज धरा है? स्वर्ग स्वप्न का जाल, सत्य का स्पर्श खोजती हूँ मैं, नहीं कल्पना का सुख, जीवित हर्ष खोजती हूँ मैं। तृप्ति नहीं अब मुझे साँस भर-भर सौरभ पीने से, ऊब गई हूँ दबा कंठ, नीरव रहकर जीने से।
इसमें क्या आश्चर्य? प्रीति जब प्रथम-प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न-समान रम्य नारी नर को लगती है। कितनी गौरवमयी घड़ी वह भी नारी-जीवन की, जब अजेय केसरी भूल सुध-बुध समस्त तन-मन की पद पर रहता पड़ा, देखता अनिमिष नारी-मुख को, क्षण-क्षण रोमाकुलित, भोगता गूढ़ अनिर्वच सुख को!
किन्तु, बन्ध को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल, प्रशमित होने लगता है। पुरुष चूमता हमें अर्ध निद्रा में हम को पाकर, पर, हो जाता विमुख प्रेम के जग में हमें जगाकर।
कौन कहे? यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है। जो अलभ्य, जो दूर, उसी को अधिक चाहता मन है।
पुरुष सदा आक्रान्त विचरता मादक प्रणय-क्षुधा से, जय से उसको तृप्ति नहीं, सन्तोष न कीर्त्ति-सुधा से। असफलता में उसे जननि का वक्ष याद आता है, संकट में युवती का शय्या-कक्ष याद आता है।
अगम, अगाध, वीर नर जो अप्रतिम तेज-बल-धारी, बड़ी सहजता से जय करती उन्हें रूपसी नारी।
पति के सिवा योषिता का कोई आधार नहीं है। जब तक है यह दशा, नारियाँ व्यथा कहाँ खोएँगी? आँसू छिपा हँसेंगी, फिर हँसते-हँसते रोएँगी।
मन की व्यथा गाओ नहीं, नारी! उठे जो हूक मन में, जीभ पर लाओ नहीं।
तब भी मरुत अनुकूल हों, मुझको मिलें, जो शूल हों, प्रियतम जहाँ भी हों, बिछे सर्वत्र पथ में फूल हों।
दृष्टि का जो पेय है, वह रक्त का भोजन नहीं है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है।’’
फिर वही उद्विग्न चिन्तन, फिर वही पृच्छा चिरन्तन, “रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? स्नेह का सौन्दर्य को उपहार रस-चुम्बन नहीं तो और क्या है?’’
जब भी तन की परिधि पारकर मन के उच्च निलय में, नर-नारी मिलते समाधि-सुख के निश्चेत शिखर पर
तब प्रहर्ष की अति से यों ही प्रकृति काँप उठती है, और फूल यों ही प्रसन्न होकर हँसने लगते हैं।
उसे देखना हो तो आँखों को पहले समझा दे, श्वेत-श्याम एक ही रंग की युगपत् संज्ञाएँ हैं। और उसे छूना हो तो कह दे अपने हाथों से, भेद उठा दें शूल-फूल का, कमल और कर्दम का।
मांस-पेशियाँ नहीं जानतीं आनन्दों के रस को, उसे जानती स्नायु, भोगता उसे हमारा मन है;
दो हृदयों का वह मूक मिलन, तन शिथिल, स्रस्त अतिशय सुख से, अलसित आँखें देखतीं, न कोई शब्द निकलता है मुख से।
कितनी पावन वह रस-समाधि! जब सेज स्वर्ग बन जाती है, गोचर शरीर में विभा अगोचर सुख की झलक दिखाती है।
चिन्तन की लहरों के समान सौन्दर्य-लहर में भी है बल, सातों अम्बर तक उड़ता है रूपसी नारि का स्वर्णांचल। जिस मधुर भूमिका में जन को दर्शन-तरंग पहुँचाती है,
तुम पंथ जोहते रहो, अचानक किसी रात मैं आऊँगी। अधरों में अपने अधरों की मदिरा उँड़ेल, मैं तुम्हें वक्ष से लगा युगों की संचित तपन मिटाऊँगी।
सतत भोग-रत नर क्या जाने तीक्ष्ण स्वाद जीवन का? उसे जानता वह, जिसने कुछ दिन उपवास किया हो!
सदा छाँह में पली, प्रेम यह भोग-निरत प्रेमी का; पर, योगी का प्रेम धूप से छाया में आना है।
इसीलिए, कहती हूँ, जब तक हरा-भरा उपवन है, किसी एक के संग बाँध लो तार निखिल जीवन का; न तो एक दिन वह होगा जब गलित, म्लान अंगों पर क्षण भर को भी किसी पुरुष की दृष्टि नहीं विरमेगी; बाहर होगा विजन निकेतन, भीतर प्राण तजेंगे अन्तर के देवता तृषित भीषण हाहाकारों में।
अप्सरियाँ जो करें, किन्तु, हम मर्त्य योषिताओं के जीवन का आनन्द-कोष केवल मधुपूर्ण हृदय है। हृदय नहीं त्यागता हमें यौवन के तज देने पर, न तो जीर्णता के आने पर हृदय जीर्ण होता है।
दो प्रसून एक ही वृन्त पर जैसे खिले हुए हों। फिर रह जाता भेद कहाँ पर शिशिर, घाम, पावस का? एक संग हम युवा, संग ही संग वृद्ध होते हैं।
अप्सरियाँ उद्विग्न भोगतीं रस जिस चिर यौवन का, उससे कहीं महत् सुख है जो हमें प्राप्त होता है निश्छल, शान्त, विनम्र, प्रेमभर उर के उत्सर्जन से।
देखा उसे महर्षि च्यवन ने और सुप्त महिमा को जगा दिया आयास-मुक्त, निश्छल प्रशस्ति यह गाकर, ‘हरि प्रसन्न यदि नहीं, सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो?" लगा मुझे, सर्वत्र देह की पपरी टूट रही है,
"हरि प्रसन्न यदि नहीं, सिद्धि बन कर तुम क्यों आई हो?"
कहते हैं, "शिशु को मत देखो अगम्भीर भावों से; अभी नहीं ये दूर केन्द्र से परम गूढ़ सत्ता के; जानें, क्या कुछ देख स्वप्न में भी हँसते रहते हैं!
"जिसके भी भीतर पवित्रता जीवित है शिशुता की, उस अदोष नर के हाथों में कोई मैल नहीं है।"
"कितनी सह यातना पालती त्रिया भविष्य जगत् का?
"बाँध रहा जो तन्तु लोक को लोकोत्तर जगती से, उसका अन्तिम छोर, न जानें, कहाँ अदृश्य छिपा है। दृश्य छोर है, किन्तु, यहाँ प्रत्यक्ष त्रिया के उर में!
"नारी ही वह महासेतु, जिस पर अदृश्य से चल कर नए मनुज, नव प्राण दृश्य जग में आते रहते हैं। नारी ही वह कोष्ठ, देव, दानव, मनुष्य से छिपकर महा शून्य, चुपचाप, जहाँ आकार ग्रहण करता है। "सच पूछो तो, प्रजा-सृष्टि में क्या है भाग पुरुष का?
यह तो नारी ही है, जो सब यज्ञ पूर्ण करती है। सत्त्व-भार सहती असंग, सन्तति असंग जनती है; और वही शिशु को ले जाती मन के उच्च निलय में, जहाँ निरापद, सुखद कक्ष है शैशव के झूले का। "शुभे! सदा शिशु के स्वरूप में ईश्वर ही आते हैं। महापुरुष की...
This highlight has been truncated due to consecutive passage length restrictions.
कौन कहे, जो तेज दमकता है इसके आनन पर, प्राप्त हुआ हो इसे अंश वह जननी नहीं, जनक से?
अरी, जुड़ाना क्या इसको? ला, दे, इस हृदय-कुसुम को लगा वक्ष से स्वयं प्राण तक शीतल हो जाती हूँ।
माता वही, पालती है जो शिशु को हृदय लगा कर। सखी! दयामयि देवि! शरण्ये! शुभे! स्वसे! कल्याणी! मैं क्या कहूँ, वंश से बिछुड़ा कब तक आयु रहेगा यहाँ धर्म की शरण, तुम्हारे अंचल की
उठती है प्रणय-वह्नि, वैसे ही, शान्त हृदय
नर का भूषण विजय नहीं, केवल चरित्र उज्ज्वल है। कहती हैं नीतियाँ, जिसे भी विजयी समझ रहे हो, नापो उसे प्रथम उन सारे प्रकट, गुप्त यत्नों से, विजय-प्राप्ति-क्रम में उसने जिनका उपयोग किया है। डाल न दे शत्रुता सुरों से हमें दनुज-बाँहों में, महाराज!