दरबार : एक अत्यन्त रोचक पुस्तक
पत्रकार तवलीन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक ‘दरबार‘ पर मीडिया में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है। तहलका जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशित किया है कि यह पुस्तक गांधी परिवार के विरूध्द ”पुराने हिसाब किताब चुकाने” के उद्देश्य से लिखी गई एक गपशप है। जबकि दूसरी और दि एशियन एज ने पुस्तक की समीक्षा ‘दिल्ली दरबार के रहस्यपूर्ण वातावरण से पर्दा उठना‘ (Unraveling the mystique of Delhi’s Durbar) शीर्षक से प्रकाशित की है। हालांकि कोई भी इससे इंकार नहीं कर सकता कि तवलीन की नवीनतम पुस्तक अत्यन्त ही रोचक पठनीय है।
 ‘एशियन एज‘ में समीक्षक अशोक मलिक की यह टिप्पणी बिल्कुल सही है कि अपनी सारी पहुंच के बावजूद राजधानी में राजनीतिक पत्रकार अक्सर लुटियन्स दिल्ली के लिए अंतत: बाहरी ही रहते हैं। कम से कम 10 जनपथ के संदर्भ में यह शत-प्रतिशत सत्य है।
‘एशियन एज‘ में समीक्षक अशोक मलिक की यह टिप्पणी बिल्कुल सही है कि अपनी सारी पहुंच के बावजूद राजधानी में राजनीतिक पत्रकार अक्सर लुटियन्स दिल्ली के लिए अंतत: बाहरी ही रहते हैं। कम से कम 10 जनपथ के संदर्भ में यह शत-प्रतिशत सत्य है।
‘नीति सेंट्रल‘ के लिए की गई पुस्तक समीक्षा में अशोक मलिक तवलीन को ”अंदर की पूरी जानकारी रखने वाली एक अंतरंग” के रूप में निरूपित करते हुए पुस्तक पर अपनी टिप्पणी को अपने लेख के शुरूआत में इस तरह लिखते हैं:
”तवलीन सिंह की नई पुस्तक दरबार में कहानियां हैं, किस्से हैं और निपट गपशप भी है जो सिर्फ लुटियन्स जोन स्वाभाविक रूप से उपलब्ध कराती है। इसमें पैने अभिमत, राजनीतिक अंदरूनी चीजें, भारत की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं सम्बन्धी अनुमान और नीतियों की असफलताएं हैं, जो एक सतर्क पत्रकार ने प्रस्तुत किया है”।
अनगिनत समस्याओं वाला भारत एक विशाल देश है। संविधान और कानून सरकार को देश का शासन प्रभावी ढंग से चलाने की सभी जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। जैसाकि सभी लोकतंत्रों में लोकतांत्रिक तंत्र का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। लेकिन देश में सभी जानते हैं कि आज के भारत में मुखिया प्रधानमंत्री नहीं अपितु कांग्रेस अध्यक्ष हैं। यही वह स्थिति है जो इन दिनों देश की अनेक समस्याओं की मूल जड़ है।
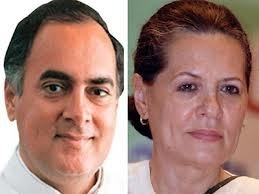 यह पुस्तक अपने पाठकों को बताती है कि एक समय था जब इसकी लेखक का न केवल राजीव गांधी के साथ अपितु श्रीमती सोनिया गांधी के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। तब अचानक यह निकटता समाप्त हो गई। अशोक मलिक लिखते हैं : तवलीन की पुस्तक हमें ”10 जनपथ की रहस्यात्मकता या गुप्तता” को समझने में सहायता करती है।
यह पुस्तक अपने पाठकों को बताती है कि एक समय था जब इसकी लेखक का न केवल राजीव गांधी के साथ अपितु श्रीमती सोनिया गांधी के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। तब अचानक यह निकटता समाप्त हो गई। अशोक मलिक लिखते हैं : तवलीन की पुस्तक हमें ”10 जनपथ की रहस्यात्मकता या गुप्तता” को समझने में सहायता करती है।
 मलिक द्वारा ”इंदिरा गांधी हत्याकाण्ड में राजीव के और सोनिया के सामाजिक मित्रों को फंसाने के विचित्र दुष्टताभरे अभियान” की ओर इंगित करने ने ‘मुझे पुस्तक के अध्याय 14 के उन सभी आठ पृष्ठों को पढ़ने को बाध्य किया‘ जिनपर मलिक की टिप्पणी आधारित है। तवलीन से भी इस सम्बन्ध में इंटेलीजेंस ब्यूरो (आई0बी0) ने पूछताछ की थी। इस प्रकरण के सम्बन्ध में तवलीन का अंतिम पैराग्राफ हमारी गुप्तचर एजेंसियों की काफी निंदा करता है:
मलिक द्वारा ”इंदिरा गांधी हत्याकाण्ड में राजीव के और सोनिया के सामाजिक मित्रों को फंसाने के विचित्र दुष्टताभरे अभियान” की ओर इंगित करने ने ‘मुझे पुस्तक के अध्याय 14 के उन सभी आठ पृष्ठों को पढ़ने को बाध्य किया‘ जिनपर मलिक की टिप्पणी आधारित है। तवलीन से भी इस सम्बन्ध में इंटेलीजेंस ब्यूरो (आई0बी0) ने पूछताछ की थी। इस प्रकरण के सम्बन्ध में तवलीन का अंतिम पैराग्राफ हमारी गुप्तचर एजेंसियों की काफी निंदा करता है:
”जांच के अंत में, हमारी गुप्तचर एजेंसियों के स्तर के बारे में मुझे गंभीर चिंता हुई। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब कुछ महीने बाद यह जांच कि भारत के प्रधानमंत्री की हत्या में कोई बड़ा षडयंत्र था, को चुपचाप समाप्त होने दिया गया।”
312 पृष्ठों वाले इस संस्मरण की शुरूआत में लेखक का चार पृष्ठीय ‘नोट‘ है। इस पुस्तक में तवलीन सिंह की टिप्पणियों से आप असहमत हो सकते हैं और उनके कुछ निष्कर्षों को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन मुझे उनके इस शुरूआती ‘नोट‘ में दम लगता है जिसे इस अंतिम पैराग्राफ में सारगर्भित ढंग से समाहित किया गया है:
”दरबार लिखना मुश्किल था। राजीव गांधी की मृत्यु के तुरंत बाद मैंने इसे लिखना शुरू किया। मैं उन्हें तब से जानती थी जब वह एक राजनीतिज्ञ नहीं थे और अपने को मैंने इस अनोखी स्थिति में पाया कि उन्हें यह बता सकूं कि कैसे भारतीय इतिहास में सर्वाधिक प्रचण्ड बहुमत वाला प्रधानमंत्री अंत में कैसे निराशाजनक स्थिति में पहुंचा। केवल इसलिए नहीं कि मैं भी उस छोटे से सामाजिक ग्रुप का हिस्सा थी जिसमें वह भी थे , लेकिन इसलिए कि एक पत्रकार के रूप में मेरा कैरियर इस तरह से बदला कि मैंने उस भारत को देखा जो राजीव के एक राजनीतिज्ञ के रूप में लगभग समानांतर चलता रहा था। तब मुझे लगा कि उन्होंने भारत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया लेकिन जब मैं इस पुस्तक को लिखने बैठी तो मुझे अहसास हुआ कि वही अकेले नहीं थे जिन्होंने भारत को शर्मिंदा किया। एक समूचे सत्तारूढ़ वर्ग ने ऐसा किया। वह सत्तारूढ़ वर्ग जिससे मैं भी सम्बन्धित हूं।
जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह मानों मेरे अपने जीवन का दर्पण है , राजनीतिज्ञ के रूप में राजीव के संक्षिप्त जीवन और कैसे वंशानुगत लोकतंत्र के बीज बोए गए-का ही यह एक संस्मरण नहीं है बल्कि एक पत्रकार के रूप में मेरा भी है। मैंने पाया कि पत्रकारिता की स्पष्ट दृष्टि ने उस देश को समझने के मेरे नजरिए को बदला जिसमें मैं अपने सारे जीवन भर रही हूं। और इसने मूलभूत रूप से उस नजरिए को बदला जिसमें मैं उन लोगों को देख सकी जिनके साथ मैं पली-बढ़ी। मैंने देखा कि कैसे वे भारत से अलिप्त हैं, उसकी संस्कृति और इतिहास उनके लिए कैसे विदेशी हैं, और इसी के चलते वे पुनर्जागरण और परिवर्तन लाने में असफल रहे। मैंने देखा कि एक पत्रकार के रूप में मेरे जीवन ने उन द्वारों को खोला जिनसे मुझे लगातार शर्म महसूस हुई कि कैसे मेरे जैसे लोगों ने भारत के साथ विश्वासघात किया है। मैं मानती हूं कि इसी के चलते भारत को उसके सत्तारूढ़ वर्ग ने शर्मिंदा किया है और वह वैसा देश नहीं बन पाया जैसा उसे बनना चाहिए था। यदि हम कम विदेशी होते और भारत की भाषाओं और साहित्य की महान संपदा, राजनीति और शासन सम्बन्धी उसके प्राचीन मूलग्रंथों और उसके ग्रंथों के बारे में और ज्यादा सचेत होते तो हम अनेक चीजों में परिवर्तन कर पाते लेकिन हम असफल रहे और अपने बच्चों कीे उनके ही देश में अपनी तरह, विदेशियों की तरह पाला। सभी विदेशी चीजों पर मंत्रमुग्ध और सभी भारतीय चीजों का तिरस्कार।
एक नया सत्तारूढ़ वर्ग धीरे से पुराने का स्थान ले रहा है। एक नयी , अभद्र राजनीतिज्ञों का वर्ग सत्ता पर नियंत्रण हेतु सामने आ रहा है। किसानों और चपरासियों के बच्चे और उन जातियों जो कभी अस्पृश्य माने जाते थे, की संतानें भारत के कुछ बड़े प्रदेशों पर शासन कर चुके हैं। लेकिन पुराने सत्तारूढ़ की बराबरी की चेष्टा में वे अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और उन्हें पश्चिम के विश्वविद्यालयों में भेजते हैं। इसमें भी कोई हर्जा नहीं है बशर्ते कि वे उन्हें अपनी भाषाओं और संस्कृति से विमुख नहीं करते हों।
एक भारतीय पुनर्जागरण की संभावना , जैसाकि पहली पीढ़ी के उन भारतीयों जो उपनिवेश के बाद के भारत में पली-बढ़ी है, हमारी हो सकती थी और सिमटती और दूर होती जा रही है। सत्तारूढ़ वर्ग के हाथों में एक राजनीतिक हथियार-वंशवाद, देश जिसकी आत्मा पहले से ही शताब्दियों से गहरे ढंग से दागदार है के नए उपनिवेश का मुख्य स्त्रोत बनता जा रहा है। यह वह मुख्य कारण है जिसके चलते तेजी से विस्तारित और फैलते शिक्षित मध्यम वर्ग का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं से मोहभंग होता जा रहा है।
तवलीन की इन पंक्तियों ने मुझे लार्ड मैकाले द्वारा फरवरी 1835 में ब्रिटिश संसद में की गई टिप्पणियों का स्मरण करा दिया:
 ”मैंने पूरे भारत की यात्रा की और ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कि भिखारी हो या चोर हो। इस तरह की संपत्ति मैंने इस देश में देखी है, इतने ऊंचे नैतिक मूल्य, लोगों की इतनी क्षमता, मुझे नहीं लगता कि कभी हम इस देश को जीत सकते हैं, जब तक कि हम इस देश की रीढ़ को नहीं तोड़ देते, जो कि उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमें इसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था, इसकी संस्कृति को बदलना होगा। इसके लिए यदि हम भारतीयों को यह सोचना सिखा दें कि जो भी विदेशी है और अंग्रेज है, वह उसके लिए अच्छा और बेहतर है, तो इस तरह से वे अपना आत्मसम्मान खो देंगे, अपनी संस्कृति खो देंगे और वे वही बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं-एक बिल्कुल गुलाम देश।”
”मैंने पूरे भारत की यात्रा की और ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो कि भिखारी हो या चोर हो। इस तरह की संपत्ति मैंने इस देश में देखी है, इतने ऊंचे नैतिक मूल्य, लोगों की इतनी क्षमता, मुझे नहीं लगता कि कभी हम इस देश को जीत सकते हैं, जब तक कि हम इस देश की रीढ़ को नहीं तोड़ देते, जो कि उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमें इसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था, इसकी संस्कृति को बदलना होगा। इसके लिए यदि हम भारतीयों को यह सोचना सिखा दें कि जो भी विदेशी है और अंग्रेज है, वह उसके लिए अच्छा और बेहतर है, तो इस तरह से वे अपना आत्मसम्मान खो देंगे, अपनी संस्कृति खो देंगे और वे वही बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं-एक बिल्कुल गुलाम देश।”
मैकाले द्वारा अपनाई गई उपनिवेशवादी नीति अंग्रेजों द्वारा भारत लागू शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान थी। इसका प्रभाव स्वतंत्रता के बाद भी बना हुआ है। वे लोग जो केवल हिंदी या कोई भारतीय भाषा बोलते हैं और अच्छी अंग्रेजी नही बोल पाते, उन्हें हमारे देश में निकृष्ट समझा जाता है। मैंने अक्सर इस तथ्य को समझने के लिए अपना उदाहरण दिया है। मैं अपने जीवन के आरंभिक बीस वर्षों में-जो मैंने सिंध में बिताए-बहुत कम हिंदी जानता था। राजस्थान आने के बाद मैंने परिश्रमपूर्वक इसका अध्ययन किया। लेकिन मुझे वर्ष 1957 में दिल्ली आने पर यह अनुभव हुआ कि अंग्रेजी भारत में उंचा स्थान कैसे रखती है।
उदाहरण के लिए, जब भी टेलीफोन की घंटी बजती थी और मैं इसे उठाता था, मेरा पहला वाक्य होता था आज भी है-‘हां, जी’ जिसके जवाब में अक्सर उधर से पूछा जाता था, ‘साहब घर में हैं?’ यह मान लिया जाता था कि घर से कोई नौकर बोल रहा है। और मैं उनसे कहता था, ‘आपको आडवाणी से बात करनी है तो मैं बोल रहा हूं।‘
टेलपीस (पश्च्यलेख)
मेरा मानना है कि तवलीन की पुस्तक के पाठक अध्याय पांच शीर्षक 1977 चुनाव को बड़े चाव से पढ़ेंगे-विशेषकर इस चुनावी भाषण के उदाहरण को, सर्वश्रेष्ठ वाजपेयी ( Vintage Vajpayee )।
जब दिल्ली की दीवारों पर पहला पोस्टर लगा कि रामलीला मैदान में एक रैली होगी जिसे प्रमुख विपक्षी नेता सम्बोधित करेंगे , तो हम सभी को लगा कि यह एक मजाक है।
स्टेट्समैन के रिपोरटर्स कक्ष में यह धारणा थी कि यदि पोस्टर सही भी हैं तो रैली फ्लॉप होगी क्योंकि लोग इसमें भाग लेने से डरेंगे। अभी भी आपातकाल प्रभावी था और पिछले अठारह महीनों से बना भय का वातावरण छंटा नहीं था।
चीफ रिपोर्टर राजू , सदैव की भांति निराशावादी था और उसने कहा कि श्रीमती गांधी को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। ‘यहां तक कि यह विपक्ष की रैली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उन्हें अपनी जीत के बारे में थोड़ा भी संदेह होता तो वह चुनाव नहीं कराती‘।
‘हां, लेकिन वह गलती तो कर सकती है,’ मैंने कहा। ‘मैंने सुना है कि उनका बेटा और उत्तराधिकारी इसके विरुध्द थे। उन्होंने बताया कि वह हार सकती हैं।‘ अनेक वर्ष बाद जब संजय गांधी के अच्छे दोस्त कमलनाथ दिल्ली में कांग्रेस सरकार में केबिनेट मंत्री थे, से मैंने पूछा कि क्या यह सही है कि संजय ने अपनी मां के चुनाव कराने सम्बन्धी निर्णय का विरोध किया था, कमलनाथ ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चुनावों के बारे में सुना तब संजय और वह श्रीनगर में एक साथ थे और इस पर संजय काफी खफा थे।
जब हम मैदान पर पहुंचे तो हमने दखा कि लोग सभी दिशाओं से उमड़ रहे हैं। मगर अंदर और ज्यादा भीड़ थी। इतनी भीड़ मैंने कभी किसी राजनीतिक रैली में नहीं देखी थी। भीड़ रामलीला मैदान के आखिर तक और उससे भी आगे तक भरी हुई थी।
लगभग शाम को 6 बजे विपक्षी नेता सफेद एम्बेसडर कारों के काफिले में पहुंचे। एक के बाद एक ने मंच पर उबाऊ, लम्बे भाषण दिए कि उन्होंने जेल में कितने कष्ट उठाए। हिन्दुस्तान टाइम्स के अपने एक सहयोगी को मैंने कहा यदि किसी ने कोई प्रेरणादायक भाषण देना शुरु नहीं किया तो लोग जाना शुरु कर देंगे। उस समय रात के 9 बज चुके थे और रात ठंडी होने लगी थी यद्यपि बारिश रुक गई थी। उसने मुस्कराहट के साथ उत्तर दिया ‘चिंता मत करो, जब तक अटलजी नहीं बोलेंगे, कोई उठकर नहीं जाएगा।‘ उसने एक छोटे से व्यक्ति की ओर ईशारा किया जिसके बाल सफेद थे और उस शाम के अंतिम वक्ता थे। ‘क्यों?’ ‘क्योंकि वह भारत के सर्वश्रेठ वक्ता हैं।‘
जब अटलजी की बारी आई उस समय तक रात के 9.30 बज चुके थे और जैसे ही वह बोलने के लिए खड़े हुए तो विशाल भीड़ खड़ी हो गई और तालियां बजानी शुरु कर दी: पहले थोड़ा हिचक कर, फिर और उत्साह से उन्होंने नारा लगाया, ‘इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, अटल बिहारी जिंदाबाद!‘ उन्होंने नारे का जवाब नमस्ते की मुद्रा और एक हल्की मुस्कान से दिया। तब उन्होंने भीड़ को शांत करने हेतु दोनों हाथ उठाए और एक मजे हुए कलाकार की भांति अपनी आंखे बंद कीं, और कहा बाद मुद्दत के मिले हैं दिवाने। उन्होंने चुप्पी साधी। भीड़ उतावली हो उठी। जब तालियां थमीं उन्होंने अपनी आंखें फिर खोलीं और फिर लम्बी चुप्पी के बाद बोले ‘कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने।‘ तालियों की गड़गडाहट लम्बी थी और इसकी अंतिम पंक्ति जो उन्होंने बाद में मुझे बताई थी , तभी रची: ‘खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने।‘ अब भीड़ उन्मत्त हो चुकी थी।
रात की ठंड बढ़ने और फिर से शुरु हुई हल्की बूंदाबांदी के बावजूद कोई भी अपने स्थान से नहीं हटा। उन्होंने अटलजी को पूरी शांति के साथ सुना।
सरल हिन्दी में , वाकपटुता से अटलजी ने उन्हें बताया कि क्यों उन्हें इंदिरा गांधी को वोट नहीं देना चाहिए। उस रात दिए गए भाषण की प्रति मेरे पास नहीं है और वैसे भी वह बिना तैयारी के बोले थे, लेकिन जो मुझे याद है उसे मैं यहां सविस्तार बता सकती हूं। उन्होंने शुरु किया आजादी, लोकतांत्रिक अधिकारों, सत्ता में बैठे लोगों से असहमत होने का मौलिक अधिकार, जब तक आपसे ले लिए नहीं जाते उनका कोई अर्थ नहीं होता। पिछले दो वर्षों में यह न केवल ले लिए गए बल्कि जिन्होंने विरोध करने का साहस किया उन्हें दण्डित किया गया। जिस भारत को उसके नागरिक प्यार करते थे, अब मौजूद नहीं था। उन्होंने यह कहते हुए जोड़ा कि यह विशाल बंदी कैम्प बन गया है, एक ऐसा बंदी कैंप जिसमें मनुष्य को मनुष्य नहीं माना जाता। उनके साथ इस तरह से बर्ताव किया गया कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुध्द काम करने को बाध्य किया गया जोकि एक मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के विरुध्द नहीं किया जाना चाहिए। विपक्षी नेता (उन्होंने कहा ‘हम‘) जानते हैं कि भारत की बढ़ती जनसंख्या के बारे में कुछ करने की जरुरत है; वे परिवार नियोजन का विरोध नहीं करते, लेकिन वे इसमें भी विश्वास नहीं करते कि मनुष्यों को जानवरों की तरह ट्रकों में डालकर उनकी इच्छा के विरुध्द उनकी नसबंदी कर दी जाए और वापस भेज दिया जाए। इस टिप्पणी पर तालियां बजीं और बजती रहीं, बजती रहीं तथा चुनाव वाले दिन ही मुझे समझ आया कि यह क्यों बज रहीं थीं।
अटलजी के भाषण समाप्ति के रुकी भीड़ ने और विपक्षी नेता अपनी सफेद एम्बेसेडर कारों में बैठे तथा भीड़ को छोड़ चले गए मानों तय किया था कि प्रेरणास्पद भाषण सुनने के बाद तालियों से भी ज्यादा कुछ और करना है। इसलिए जब पार्टी कार्यकर्ता चादर लेकर चंदा इक्ठ्ठा करते दिखाई दिए तो सभी ने कुछ न कुछ दिया। जनवरी की उस सर्द रात को मैंने देखा कि रिक्शा वाले और दिल्ली की सड़कों पर दयनीय हालत में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर भी जो दे सकते थे , दे रहे थे तो पहली बार मुझे लगा कि इंदिरा गांधी के चुनाव हारने की संभावना हो सकती है।
लालकृष्ण आडवाणी
नई दिल्ली
23 दिसम्बर, 2012

L.K. Advani's Blog
- L.K. Advani's profile
- 10 followers



