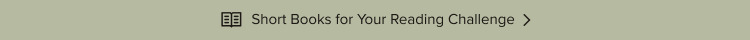More on this book
Kindle Notes & Highlights
'उर्दू साहित्य के भारतीय व्यक्तित्व' पर पी-एच.डी.
हम लोगों में और टोपी में केवल एक अन्तर है । हम लोग कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी अवसर पर 'कम्प्रोमाइज' कर लेते हैं
समय के सिवा कोई इस लायक़ नहीं होता कि उसे किसी कहानी का हीरो बनाया जाए
'आधा गाँव' में बेशुमार गालियाँ थीं । मौलाना 'टोपी शुक्ला' में एक भी गाली नहीं है ।–परन्तु शायद यह पूरा उपन्यास एक गन्दी गाली है । और मैं यह गाली डंके की चोट पर बक रहा हूँ । यह उपन्यास अश्लील है–जीवन की तरह
साधारण मनुष्य ग्रामर की समस्याओं पर विचार नहीं करता । वह तो अपनी भाषा के नाम पर शब्दों को काट-छाँट लेता है ।"
हर शरीफ़ के साथ एक दुमछल्ला लगा हुआ है । हिन्दू शरीफ़, मुसलमान शरीफ़, उर्दू शरीफ़, हिन्दी शरीफ़ : और बिहार शरीफ़ ! दूर-दूर तक शरीफों का एक जंगल फैला हुआ है । यह सोचकर इफ़्फ़न सदा उदास हो जाता । परन्तु मैं आपको इफ़्फ़न की उदासी की कहानी नहीं सुना रहा हूँ । बात हो, रही थी टोपी की । यह मैं बतला चुका कि उसका नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था । परन्तु लोग उसे टोपी शुक्ला ही कहा करते थे
बात यह है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जहाँ मट्टी, मक्खी, मटरी के बिस्कुट,मक्खन और मौलवी के लिए प्रसिद्ध है, वहीं भाँत-भाँत के नाम रखने के लिए भी प्रसिद्ध
इक़बाल ख़ाली । ख़ाली इसलिए कि बाक़ी तमाम इक़बालों के साथ कुछ-न-कुछ लगा हुआ था । अगर इनके नाम के साथ कुछ न जोड़ा जाता तो यह बुरा मानते
भूगोल के एक टीचर का नाम 'बहरुल काहिल' रख दिया गया । यह टीचर कोई काम तेज़ी से नहीं कर सकते थे । इसलिए इन्हें काहिली का सागर कहा गया (वैसे
अरबी भाषा में पैसिफ़िक सागर का नाम बहरुल काहिल ही है !)
टोपी शुक्ला बहुत ही यार टाइप के लोग थे । अपने उसूलों के भी बड़े पक्के थे । और उनका सबसे बड़ा उसूल यह था कि दोस्ती में उसूल नहीं देखे जाते ।
लगता ऐसा है कि ईमानदार लोगों को हिन्दू-मुसलमान बनाने में बेरोज़गारी का हाथ भी है
"धर्म सदा से पॉलिटिक्स ही का एक रूप रहा है । न सोमनाथ का मन्दिर तुम बनवा सकते हो और न दिल्ली की जामा मसजिद मैं । तो धर्म मेरा-तुम्हारा साथ क्यों देगा चौंघट !"
"अरे तो क्या यह लैला-मजनूँ और हीर-राँझा की कहानियाँ केवल प्रोपेगण्डा हैं । ?" "यह कहानियाँ मिडिल क्लास के पैदा होने से पहले की हैं
कहती हैं कि मैं मलेच्छ हो गया हूँ । परन्तु माँ है । कभी-कभी प्यार कर ही लेती है । तो प्यार करने के बाद सीधी गंगा नहाने जाती है । एक दिन मैंने कहा, माताजी मुसलमानों ने नहा-नहाकर गंगाजी को भ्रष्ट कर दिया है । जनाब वह खफ़ा हो गईं और छह महीने तक मुझसे नहीं बोलीं
"हाँ-हाँ–अरगती-परगती शील होगा कुछ । यह मुई भी कोई ज़बान है कि बोलो तो ज़बान छिनाल औरत की तरह सौ-सौ बल खाए ।"
यह है वह बलभद्र नारायण शुक्ला जो इस कहानी का हीरो है । जीवनी या कहानी सुनाने का एक तरीक़ा यह भी है कि कथाकार या जीवनीकार कहानी या जीवन को कहीं से शुरू कर दे । जीवन ही की तरह कहानी के आरम्भ का भी कोई महत्त्व नहीं होता । महत्त्व केवल अन्त का होता है । जीवन के अन्त का भी और कहानी के अन्त का भी । मैं यदि आपको यह दिखलाता कि बलभद्र नारायण शुक्ला एक पालने में स्याह गोश्त के एक लोथड़े की तरह पड़ा ट्याँव-ट्रयाँव कर रहा है और उसकी कमर में काले नाड़े की करधनी है और उसके काले माथे पर काजल का एक काला टीका है, तो सम्भव है कि आप मुँह फेर लेते कि इस बच्चे में क्या ख़ास बात है !–जबकि सच पूछिए तो हर कहानी और हर
...more
नाम की ज़रूरत तो मरनेवालों को होती है । गांधी भी बेनाम पैदा हुए थे और गोडसे भी । जन्म लेने के लिए आज तक किसी को नाम की ज़रूरत नहीं पड़ी है । पैदा तो केवल बच्चे होते हैं । मरते-मरते वह हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, नास्तिक, हिन्दुस्तानी, पाकिस्तानी, गोरे, काले और जाने क्या-क्या हो जाते हैं ।
जिस रात उसने जन्म लिया वह बरसात की एक सड़ी हुई काली रात थी । हवा बिलकुल बन्द थी । आकाश बादल से ठसा पड़ा था । एक तारे तक की जगह नहीं थी । इधर उसकी माँ के पेट में दर्द शुरू हुआ और उधर बिजली चमकी । बादल में दरार पड़ गई । पानी की चादर गिरने लगी । ऐसा लगता था जैसे बादल ओलती में फँस गए हों । आँगन में पानी चमकने लगा । फ़्यूज़ उड़ गया । अँधेरा सम्पूर्ण हो गया ।
परन्तु इतिहास और समय का पहिया उलटा नहीं चलता
गुलामी, धर्म और प्रकाश का पुराना बैर है । आदम को जब प्रकाश मिला तो अल्लाह मियाँ ने उन्हें तुरन्त जन्नत से निकाल दिया ।
वह पेट-पोंछना था, इसलिए माँ का चहीता था
सूरत तो होती है रण्डी की । बीवी की तो तबीअत देखी जाती है । लाजवन्ती सीरत और तबीअत दोनों ही की अच्छी थी–यानी वह पण्डित सुधाकर लाल की इकलौती बेटी थी
"दादीजी, आप उस काले-कलूटे कृष्न को पूजती हैं ना, तो एक-न-एक दिन आपकी पूजा जरूर काली हो जाएगी ।" उस दिन दादीजी को दो बातों पर गुस्सा आया । पहली बात तो यह थी कि उनका पोता 'ज़रूर' को 'जरूर' बोल रहा था । (टोपी उन्हें चिढ़ाने के लिए उनके जीवन-भर यही करता रहा ।) और दूसरी बात यह कि उसने प्रभु का मज़ाक उड़ाया था । उन्होंने ताने की कमान चढ़ाकर रामदुलारी का कलेजा छलनी कर दिया । उस दिन रामदुलारी ने टोपी को जी भरके ठोंका । टोपी घर से भाग गया
पशु-पक्षियों की रक्षा समितियाँ सैकड़े के हिसाब से बिक रही हैं और दूसरे बेटे मारे-मारे फिर रहे हैं ।
अवतारों में भी जिसे देखिए वही पहला बेटा है
बात कहानी और जीवनी दोनों ही के नियमों के विरुद्ध है कि पाठक को अँधेरे में रखा जाए । पाठक और गाहक में फ़र्क़ होता है । लेखक और दुकानदार में अन्तर होता है । दुकानदार को अपनी चीज़ बेचनी होती है, इसलिए वह जासूसी कथाकार की तरह कुछ छिपाता है और कुछ बताता है । परन्तु लेखक के पास बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं होती । कहानी का ताना-बाना गफ़ हो तो पाठकों से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है
मैं लेखक भी हूँ और पाठक भी । और मैं जो लेखक हूँ उस 'मैं' से इफ़्फ़न का परिचय कराने की आज्ञा माँग रहा हूँ जो पाठक है ।
नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मुहम्मद हो तो पैग़म्बर । नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देनेवाले जानवर चराया करते थे । दोनों ही पशुपति, गोबरधन और ब्रज-कुमार थे । इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़्फ़न और इफ़्फ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं, बल्कि बेमानी हैं
यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आँगन में कैसी हवाएँ चल रही हैं और परम्पराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं ।
बात यह है कि कोई कहानी कभी बिलकुल किसी एक की नहीं हो सकती । कथाकार जब यह बात भूल जाता है तो वह हीरो का क़द ऊँचा करने के लिए दूसरे चरित्रों को ऊपर या नीचे से काटना शुरू कर देता है ताकि हीरो दूर से दिखाई दे जाए
हिन्दू-मुसलमान अगर भाई-भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं । यदि नहीं हैं तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा । मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है । मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ ।
इफ़्फ़न की दादी भी नमाज़-रोज़े की पाबन्द थीं, परन्तु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टाँट पर खड़ी हुईं और बोलीं : "माता मोरे बच्चे को माफ करद्यो ।"
मरते वक़्त किसी को ऐसी छोटी-छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं । उस वक़्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है (यह कथाकार का ख़याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है
इफ़्फ़न की दादी बीबी कही जाती थीं ।
वह रात को उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलबकावली, हातिमताई, पंच फुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थीं ।
"सोता है संसार जागता है पाक परवरदिगार । आँखों की देखी नहीं कहती । कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुलुक में एक बादशा रहा..."
टोपी और दादी में एक ऐसा सम्बन्ध हो चुका था जो मुसलिम लीग, कांग्रेस और जनसंघ से बड़ा था । इफ़्फ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस सम्बन्ध को बिलकुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घरवाले न समझ पाए थे । दोनों अलग-अलग अधूरे थे । एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था । दोनों प्यासे थे । एक दूसरे की प्यास बुझा दी थी । दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे । दोनों ने एक-दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था । एक बहत्तर बरस की थी और दूसरा आठ साल का ।
इफ़्फ़न की ज़िन्दगी ने बिलकुल दूसरे रास्ते पर सफ़र किया
वह साहित्य का रसिया था । वामिक जौनपुरी, साहिर लुधियानवी, अली सरदार जाफ़री और दूसरे कवियों की कविताओं और कृश्नचन्दर, अब्बास और दूसरे कथाकारों की कहानियों ने उससे कहा कि इस आज़ादी में कोई घपला है ।
उस दिन पहली बार उसकी निगाहों में अल्लाह मियाँ की इज़्ज़त कुछ कम हुई । यह तो कोई बात न हुई कि गुनाह करें बड़े और उसे भुगतें बच्चे !
"कोई कहे कि कव्वा कान ले भागा तो तुम क्या करोगे ? कान देखोगे या कव्वे के पीछे भागोगे ? तुमने बनाया है पाकिस्तान
इसलिए वह हिन्दी की बुराई करने लगे : "लाहौलविला क़ुव्वत । क्या लग्व ज़बान है । दो लफ़्ज बोलो तो ज़बान बेचारी हाँफने लगती है
जब पण्डितजी तक ये बातें पहुँचीं तो उन्हें बहुत बुरा लगा । वह अच्छी उर्दू, फ़ारसी जानते थे । मगर मौलवी साहब की ज़िद में उन्होंने उर्दू बोलना छोड़ दिया । हिन्दी बोलने में उन्हें कठिनाई होती । परन्तु वह हिन्दी ही बोलने लगे । उर्दू-फ़ारसी के जो शब्द उनकी ज़बान पर चढ़े हुए थे उन्हें कोशिश करके उन्होंने भुला दिया ।
यह तनातनी इतनी बढ़ी कि स्कूल के सालाना मुशायरे की कमेटी में मौलवी साहब ने पण्डितजी का नाम नहीं रखा । मुशायरा हुआ । परन्तु लड़कों ने बहुत शोर किया । फिर पण्डितजी ने मुशायरे की चोट पर कवि-सम्मेलन किया । शहर का पहला कवि-सम्मेलन हुआ । परन्तु बाद में पण्डितजी ने अपने एक...
This highlight has been truncated due to consecutive passage length restrictions.
यह जो मैं बार-बार इफ़्फ़न की बात करने लगता हूँ तो इससे आप यह न समझिए कि यह कहानी टोपी और इफ़्फ़न दोनों की है ।
परन्तु बार-बार इफ़्फ़न की आत्मा में झाँकना ज़रूरी है, क्योंकि देश में जो परिवर्तन हो रहा है उसे केवल टोपी की खिड़की से नहीं देखा जा सकता । इफ़्फ़न भी टोपी ही का एक रूप है । इस टोपी के बेशुमार रूप हैं । बंगाल, पंजाब, यू.पी., आन्ध्र, असम...सारे देश में यह टोपी अपनी समस्याओं का कशकोल लिए विचारधाराओं, फ़लसफ़ों, राजनीतियों...के दरवाज़े खटखटा रहा है । परन्तु कोई इसे सहारा नहीं देता । मैं इस कहानी को इतना नहीं फैला सकता कि इसमें टोपी के तमाम रूप समा जाएँ । इसलिए मैंने केवल दो रूप चुन लिए हैं ।
परन्तु जब वह क्लास गया तो उसने देखा कि बुझी हुई आँखों वाले लड़के लाशों की तरह बैठे हुए हैं । किसी आँख की खिड़की से कोई आत्मा नहीं झाँक रही थी । आँखें झपक रही थीं । मालिक-मकान जैसे घबराहट में भागते समय खिड़कियाँ बन्द करना भूल गया था । और खिड़कियाँ हवा से खुल रही थीं और बन्द हो रही थीं । बन्द हो रही थीं और खुल रही थीं । शीशे टूट रहे थे । किवाड़ बरसात झेलते-झेलते अधमुए हो गए थे
इन लड़कों को क्या बतलाया जाए ? इनकी समझ में यह बात कैसे आएगी कि दो नदियाँ तीन नहीं हो जातीं–एक हो जाती हैं । इन लड़कों को यह कैसे बतलाया जाए कि इतिहास अलग-अलग बरसों या क्षणों का नाम नहीं है बल्कि इतिहास नाम है समय की आत्मकथा का । पानीपत की लड़ाइयाँ, या बक्सर की जंग या प्लासी का युद्ध तो इस नदी के बुलबुले हैं ।...
इफ़्फ़न का ख़याल यह था कि पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी जैसे लोग रिएक्शनरी थे क्योंकि वे हिन्दुस्तानी नेशनलिज़्म की धारा की राह में रुकावट डाल रहे थे ।