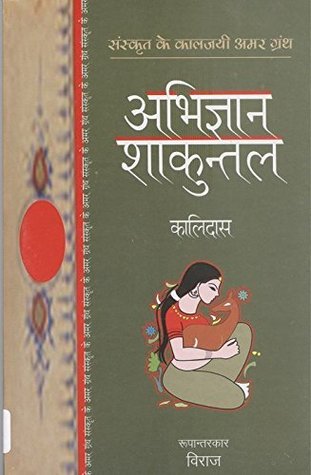More on this book
Kindle Notes & Highlights
उनके ये काव्य ‘रघुवंश’, ‘कुमार सम्भव’ और ‘मेघदूत’ हैं और नाटक ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’, ‘मालविकाग्निमित्र’ और ‘विक्रमोर्वशीय’ हैं।
विद्वानों में इस बात पर ही गहरा मतभेद है कि यह कालिदास कौन थे? कहाँ के रहने वाले थे? और कालिदास नाम का एक ही कवि था, अथवा इस नाम के कई कवि हो चुके हैं? कुछ विद्वानों ने कालिदास को उज्जयिनी-निवासी माना है, क्योंकि उनकी रचनाओं में उज्जयिनी, महाकाल, मालवदेश तथा क्षिप्रा आदि के वर्णन अनेक स्थानों पर और विस्तारपूर्वक हुए हैं। परन्तु दूसरी ओर हिमालय, गंगा और हिमालय की उपत्यकाओं का वर्णन भी कालिदास ने विस्तार से और रसमग्न होकर किया है। इससे कुछ विद्वानों का विचार है कि ये महाकवि हिमालय के आसपास के रहने वाले थे। बंगाल के विद्वानों ने कालिदास को बंगाली सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और कुछ लोगों ने
...more
फिर भी कालिदास का अनुराग दो स्थानों की ओर विशेष रूप से लक्षित होता है : एक उज्जयिनी और दूसरे हिमालय की उपत्यका।
यदि हम इस जनश्रुति में सत्य का कुछ भी अंश मानें कि कालिदास विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में से एक थे, तो हमारे लिए यह अनुमान करना और सुगम हो जाएगा कि उनका यौवनकाल उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्य की राजसभा में व्यतीत हुआ।
विक्रमादित्य उज्जयिनी के नरेश कहे जाते हैं। यद्यपि कालिदास की ही भाँति विद्वानों में महाराज विक्रमादित्य के विषय में भी उतना ही गहरा मतभेद है; किन्तु इस सम्बन्ध में अविच्छिन्न रूप से चली आ रही विक्रम संवत् की अखिल भारतीय परम्परा हमारा कुछ मार्गदर्शन कर सकती है। पक्के ऐतिहासिक विवादग्रस्त प्रमाणों की ओर न जाकर इन जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जा सकता है कि कालिदास अब से लगभग 2,000 वर्ष पूर्व उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में से एक थे।
यहाँ तक कि वहाँ की ओस से गीली झरबेरियों के बेर भी उनकी अमर रचना में स्थान पा गए हैं।
जनश्रुतियों से जिस प्रकार यह मालूम होता है कि कोई कालिदास विक्रमादित्य की सभा में थे, उसी प्रकार ‘भोज प्रबन्ध’ में भोज की सभा में भी एक कालिदास का उल्लेख है। कुछ विद्वानों ने तीन कालिदास माने हैं। रखर ने भी लिखा है कि ‘ललित शृंगार की रचनाओं में एक ही कालिदास को कोई नहीं जीत सकता, फिर तीन कालिदासों का तो कहना ही क्या!1
कालिदास की रचनाओं की प्रशंसा उनके परवर्ती कवियों ने मुक्तकंठ से की है। एक कवि ने कालिदास की सूक्तियों को मधुरस से भरी हुई आम्रमंजरियों के समान बताया है2 एक और कवि ने लिखा है कि ‘कवियों की गणना करते समय कालिदास का नाम जब कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया, तो अनामिका के लिए उनके समान किसी दूसरे कवि का नाम ही न सूझा; और इस प्रकार अनामिका अँगुली का अनामिका नाम सार्थक हो गया। आज तक भी कालिदास के समान और कोई कवि नहीं हुआ।’1 एक और आलोचक ने लिखा है कि ‘काव्यों में नाटक सुन्दर माने जाते हैं; नाटकों में ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ सबसे श्रेष्ठ है; शाकुन्तल में भी चौथा अंक; और उस अंक में भी चार श्लोक अनुपम हैं।2
जर्मन कवि गेटे ने ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ का अनुवाद जर्मन भाषा में पढ़ा था। शाकुन्तल
उसने लिखा, “यदि तुम तरुण वसन्त के फूलों की सुगन्ध और ग्रीष्मऋतु के मधुर फलों का परिपाक एकसाथ देखना चाहते हो; या उस वस्तु का दर्शन करना चाहते हो जिससे अन्तःकरण पुलकित, सम्मोहित, आनन्दित और तृप्त हो जाता है; अथवा तुम भूमि और स्वर्ग की झाँकी एक ही स्थान में देखना चाहते हो, तो ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ का रसपान करो।‘
आलोचना करते हुए लिखा है, “शाकुन्तल का आरम्भ सौन्दर्य से हुआ है और उस सौन्दर्य की परिणति मंगल में जाकर हुई है। इस प्रकार कवि ने मर्त्य को अमृत से सम्बद्ध कर दिया है।’
कालिदास ने ‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ की कथावस्तु मौलिक नहीं चुनी। यह कथा महाभारत के आदिपर्व से ली गई है। यों पद्मपुराण में भी शकुन्तला की कथा मिलती है और वह महाभारत की अपेक्षा शकुन्तला की कथा के अधिक निकट है। इस कारण विन्टरनिट्ज़ ने यह माना है कि शकुन्तला की कथा पद्मपुराण से ली गई
महाभारत का दुष्यन्त कालिदास के दुष्यन्त से यदि ठीक उलटा नहीं, तो भी बहुत अधिक भिन्न है। महाभारत की शकुन्तला भी कालिदास की शकुन्तला की भाँति सलज्ज नहीं है। वह दुष्यन्त को विश्वामित्र और मेनका के सम्बन्ध के फलस्वरूप हुए अपने जन्म की कथा अपने मुँह से ही सुनाती है। महाभारत में दुष्यन्त शकुन्तला के रूप पर मुग्ध होकर शकुन्तला से गान्धर्व विवाह की प्रार्थना करता है; जिस पर शकुन्तला कहती है कि मैं विवाह इस शर्त पर कर सकती हूँ कि राजसिंहासन मेरे पुत्र को ही मिले। दुष्यन्त उस समय तो स्वीकार कर लेता है और बाद में अपनी राजधानी में लौटकर जान-बूझकर लज्जावश शकुन्तला को ग्रहण नहीं करता। कालिदास ने इस प्रकार
...more
इसमें कवि को विलक्षण सफलता यह मिली है कि उसने कहीं भी कोई भी वस्तु निष्प्रयोजन नहीं कही। कोई
इसी प्रकार नाटक के प्रारम्भिक गीत में भ्रमरों द्वारा शिरीष के फूलों को ज़रा-ज़रा-सा चूमने से यह संकेत मिलता है कि दुष्यन्त और शकुन्तला का मिलन अल्पस्थायी होगा।
राजा धनुष पर बाण चढ़ाए हरिण के पीछे दौड़े जा रहे हैं, तभी कुछ तपस्वी आकर रोकते हैं। कहते हैं : “महाराज, यह आश्रम का हरिण है, इस पर तीर न चलाना।’ यहाँ हरिण से हरिण के अतिरिक्त शकुन्तला की ओर भी संकेत है, जो हरिण के समान ही भोली-भाली और असहाय है। ‘कहाँ तो हरिणों का अत्यन्त चंचल जीवन और कहाँ तुम्हारे वज्र के समान कठोर बाण!’ इससे भी शकुन्तला की असहायता और सरलता तथा राजा की निष्ठुरता का मर्मस्पर्शी संकेत किया गया
‘अभिज्ञान शाकुन्तल’ में नाटकीयता के साथ-साथ काव्य का अंश भी यथेष्ट मात्रा में है। इसमें शृंगार मुख्य रस है; और उसके संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों का परिपाक सुन्दर रूप में हुआ है।
शकुन्तला के विषय में एक जगह राजा दुष्यन्त कहते हैं कि ‘वह ऐसा फूल है, जिसे किसी ने सूँघा नहीं है; ऐसा नवपल्लव है, जिस पर किसी के नखों की खरोंच नहीं लगी; ऐसा रत्न है, जिसमें छेद नहीं किया गया और ऐसा मधु है, जिसका स्वाद किसी ने चखा नहीं है।’
इसी प्रकार पाँचवें अंक में दुष्यन्त शकुन्तला का परित्याग करते हुए कहते हैं कि ‘हे तपस्विनी, क्या तुम वैसे ही अपने कुल को कलंकित करना और मुझे पतित करना चाहती हो, जैसे तट को तोड़कर बहने वाली नदी तट के वृक्ष को तो गिराती ही है, अपने जल को भी मलिन कर लेती है।’
‘इन तपस्वियों के बीच में वह घूँघट वाली सुन्दरी कौन है, जो पीले पत्तों के बीच में नई कोंपल के समान दिखाई पड़ रही है।’
शब्दों का प्रसंगोचित चयन, अभीष्ट भाव के उपयुक्त छन्द का चुनाव और व्यंजना-शक्ति का प्रयोग करके कालिदास शकुन्तला के सौन्दर्य-वर्णन पर उतरे हैं, वहाँ उन्होंने केवल उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं द्वारा शकुन्तला का रूप चित्रण करके ही सन्तोष नहीं कर लिया है। पहले-पहल तो उन्होंने केवल इतना कहलवाया कि ‘यदि तपोवन के निवासियों में इतना रूप है, तो समझो कि वन-लताओं ने उद्यान की लताओं को मात कर दिया।’
के मुख से उन्होंने कहलवाया कि ‘इतनी सुन्दर कन्या को आश्रम के नियम-पालन में लगाना ऐसा ही है जैसे नील कमल की पंखुरी से बबूल का पेड़ काटना।’ उसके बाद कालि/दा/स कहते हैं कि ‘शकुन्तला का रूप ऐसा मनोहर है कि भले ही उसने मोटा वल्कल वस्त्र पहना हुआ है, फिर भी उससे उसका सौन्दर्य कुछ घटा नहीं, बल्कि बढ़ा ही है। क्योंकि सुन्दर व्यक्ति को जो भी कुछ पहना दिया जाए वही उसका आभूषण हो जाता है।’
कालिदास ने शरीर-सौन्दर्य को मानसिक सौन्दर्य के साथ मिलाकर अद्भुत लावण्य-सृष्टि की है। उनकी शकुन्तला तपोवन में रही है, इसलिए नगरों में होने वाले छल-प्रपंचों से वह अपरिचित है। स्नेह उसके मन में लबालब भरा है।
जब दुष्यन्त तपोवन से विदा लेकर अपनी राजधानी में लौट आए और उन्होंने शकुन्तला की कोई खबर नहीं ली, तो उस प्रसंग में विरह-व्यथा को प्रकट करने के लिए बहुत कुछ लिखा जा सकता था या शकुन्तला के मुख से कहलवाया जा सकता था परन्तु कालिदास ने इसके लिए कुछ भी उद्योग नहीं किया। केवल दुर्वासा के आगमन और शकुन्तला के दुष्यन्त के ध्यान में मग्न होने के कारण उनकी अवहेलना द्वारा ही शकुन्तला की करुणाजनक मनोदशा की झाँकी दे दी।
जब दुष्यन्त की राजसभा में राजा ने शकुन्तला को निरादरपूर्वक त्याग दिया, उस समय शकुन्तला के विभिन्न मनोभाव भय, लज्जा, अभिमान, अनुनय, भर्त्सना और विलाप सभी कुछ कवि ने चित्रित किए हैं। परन्तु उनके लिए शब्द बहुत ही परिमित व्यय किए गए हैं। जिस शकुन्तला ने विश्वास के साथ सरल भाव से अपने-आपको दुष्यन्त को समर्पित कर दिया था, वह ऐसे दारुण अपमान के समय अपनी सलज्ज मर्यादा की रक्षा कैसे करेगी, यह एकाएक पाठक के लिए कल्पना कर पाना सम्भव नहीं होता। परन्तु कालिदास ने इस परिस्थिति का निर्वाह महाकवि की कुशलता के साथ किया है। इस परित्याग के उपरान्त की नीरवता और भी अधिक व्यापक, गम्भीर और प्रभावशालिनी है।
शकुन्तला हमारे सम्मुख एक अभागी सुन्दरी के रूप में प्रकट होती है उसका जन्म महाप्रतापी ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका से हुआ है। उसका रूप विलक्षण है।
स्नेह, ममता और सेवा की भावना उसके रोम-रोम में समा गई। दुष्यन्त से गान्धर्व विवाह कर लेने के बाद भाग्य उस पर फिर रुष्ट होता है। दुष्यन्त शापवश उसे भूल जाते हैं और उसका त्याग कर देते हैं। इस अवसर पर उसका एक और रूप भी दिखाई पड़ता है, जिसमें वह राजा की विश्वासघातकता के लिए उनकी उग्र रूप में भर्त्सना करती है। किन्तु भारतीय परम्परा के अनुसार वह दुष्यन्त के लिए कोई अहितकामना नहीं करती और न इसका कुछ प्रतिशोध ही चाहती है। नाटक के अन्त में हमें उसकी क्षमाशीलता का एक और नया रूप दिखाई देता है। दुष्यन्त द्वारा किए गए सारे निरादर और तिरस्कार को वह खुले हृदय से क्षमा कर देती है; और जीवन में यह क्षमा ही समस्त
...more
कालिदास के वर्णन भौगोलिक दृष्टि से सत्य और स्वाभाविक होते हैं। जिस स्थान और जिस काल का यह वर्णन करते हैं, उसमें सत्यता और औचित्य रहता है। उन्होंने पूर्वी समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों में ताड़ के वनों, महेन्द्र पर्वत पर नागवल्ली के पत्तों और नारियल के आसव व केरल में मुरला नदी के निकट केतकी के फूलों का उल्लेख किया है।
सिरस के फूल बड़े सुकुमार! चाँदनी की किरणों से तन्तु, भरी है जिनमें सुरभि अपार! भ्रमर आते करने रसपान, जताते ज़रा चूमकर प्यार! उन्हीं से ललनाएँ अत्यन्त सदय अपना करतीं शृंगार!
के ढेर में कहीं इस प्रकार आग लगाई जाती है? कहाँ तो इन हरिणों का अत्यन्त चंचल जीवन और कहाँ आपके सनसनाते हुए वज्र के समान कठोर बाण! इसलिए महाराज, आप इस धनुष पर चढ़ाए हुए बाण को उतार लीजिए।
: महाराज, हम लोग समिधाएँ लाने के लिए निकले हैं। यह पास ही मालिनी नदी के तीर पर कुलपति कण्व का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। यदि आपके किसी अन्य कार्य में बाधा न हो तो, वहाँ पहुँचकर आतिथ्य स्वीकार कीजिए।
क्यों, देखते नहीं कि वृक्षों के नीचे तोतों के रहने के कोटरों के मुँह से नीचे गिरे हुए धान पड़े हैं। कहीं इंगुदी फलों को तोड़ने से चिकने हुए पत्थर बिखरे पड़े हैं। यहाँ के हरिण मनुष्यों के पास रहने के अभ्यस्त हैं, इसी से रथ के शब्द को सुनकर भी वे बिना चौंके पहले की ही भाँति निःशंक फिर रहे हैं। पानी लेकर आने के मार्ग पर वल्कल वस्त्रों के छोरों से चूने वाले जल-बिन्दुओं की रेखा बनी दिखाई पड़ रही है। छोटी-छोटी नालियों में पानी की धारा बह रही है, जिससे वृक्षों की जड़ें धुल गई हैं। घी के धुएँ के कारण तरुओं के नवपल्लवों का रंग बहुत बदल गया है। उस ओर उपवन की भूमि से दर्श के अंकुर निकालकर साफ कर दिए गए हैं।
...more
यदि आश्रम में रहने वाले लोगों का ऐसा रूप है, जो रनिवासों में भी दुर्लभ है, तो समझ लो कि वनलताओं ने उद्यान की लताओं को मात दे दी। कुछ देर इस छाया में खड़े होकर इनकी प्रतीक्षा करता हूँ। (देखता हुआ खड़ा रहता है।)
क्या यही कण्व की पुत्री है? महर्षि कण्व ने यह ठीक नहीं किया कि इसे भी आश्रम के कार्यों में लगा दिया है। इस निसर्ग सुन्दर शरीर को महर्षि कण्व तपस्या के योग्य बनाने की अभिलाषा करके मानो नीलकमल की पंखुरी से बबूल का पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पेड़ों की आड़ से ही कुछ देर इसे जी भर कर देख तो लूँ। (देखने लगता है।)
भले ही यह वल्कल वस्त्र इसके शरीर के अनुकूल नहीं है, फिर भी यह इसके सौन्दर्य को न बढ़ाता हो, यह बात नहीं। क्योंकि काई लगी होने पर भी कमल सुन्दर होता है। चन्द्रमा का मलिन कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाता है। यह छरहरी युवती वल्कल वस्त्रों से और अधिक सुन्दर लग रही है।
आकृति सुन्दर हो तो, जो कुछ पहना दिया जाए, वही आभूषण बन जाता है।
प्रियंवदा ने बात प्यारी होते हुए भी कही सच है। क्योंकि इस शकुन्तला के होंठ नवपल्लवों के समान लाल हैं। दोनों बाँहें कोमल टहनियों के समान हैं और फूलों की भाँति आकर्षक यौवन इसके अंग-अंग में समाया हुआ है।
सज्जनों को जहाँ किसी बात में सन्देह हो, वहाँ उनकी अन्तःकरण की बात ही अन्तिम प्रमाण होती है।
भ्रमर, तुम कभी उसकी बार-बार कांपती चंचल चितवन वाली दृष्टि का स्पर्श करते हो। और कभी उसके कान के पास फिरते हुए धीरे-धीरे कुछ रहस्यालाप-सा करते हुए गुनगुनाते हो। उसके हाथ झटकने पर भी तुम उसके सरस अधरों का पान करते हो। वस्तुतः तुम्हीं भाग्यवान् हो, हम तो वास्तविकता की खोज में ही मारे गए।
हृदय, अब तुम अभिलाषा कर सकते हो। अब सन्देह का निर्णय हो गया है। जिसे तुम आग समझकर डर रहे थे, वह तो रत्न निकला जिसे सरलता से स्पर्श किया जा सकता है।
भद्रे, मैं तो देखता हूँ कि ये वृक्षों को सींचने से पहले ही बहुत अधिक थक गई हैं; क्योंकि घड़े उठाने से इनकी बाँहें कन्धों पर से ढीली होकर झूल रही हैं और हथेलियाँ बहुत लाल हो गई हैं। मुँह पर पसीने की बूँदें झलक आई हैं, जिनसे कान में लटकाया हुआ शिरीष का फूल गालों पर चिपक गया है; और जूड़ा खुल जाने के कारण एक हाथ से संभाले हुए बाल इधर-उधर बिखर गए हैं। लीजिए, मैं इनका ऋण उतारे देता हूँ। (यह कहकर अंगूठी देना चाहता है।)
मुझे अब नगर जाने की उत्सुकता नहीं रही। फिर भी चलकर अपने अनुचरों को तपोवन से कुछ दूर टिका दूँ। इस शकुन्तला के काण्ड से मैं किसी प्रकार अपने-आपको वापस नहीं लौटा पा रहा। मेरा शरीर यद्यपि आगे की ओर जा रहा है, जैसे वायु के प्रवाह के विरुद्ध जाने वाले झण्डे का रेशमी वस्त्र पीछे की ओर ही लौटता है!
अभिलाषी व्यक्ति को सब जगह अपने मतलब की ही बात दिखाई पड़ती है।
क्यों मित्र, बेंत का पौधा पानी में खड़ा कुबड़े-सा खेल जो किया करता है, वह अपने-आप करता है या नदी के तेज़ बहाव के कारण?
क्योंकि अब उन हरिणों की ओर बाण साधकर मुझसे यह धनुष झुकाया नहीं जाता, जिन्होंने प्रियतमा शकुन्तला के पास रहकर उसे भोली चितवनों से देखना सिखलाया है।
इस मृगयानिन्दक माधव्य ने मेरे उत्साह पर पानी डाल दिया है।
है। पशु भयभीत और क्रुद्ध होने पर कैसा व्यवहार करते हैं, यह भी पता चल जाता है। चलायमान लक्ष्य पर भी यदि तीर जा लगे तो वह धनुर्धारियों की कुशलता का प्रमाण है। लोग शिकार को व्यर्थ ही व्यसन कहते हैं। ऐसा बढ़िया विनोद का साधन तो मिलना कठिन है।
देखो, इन शान्त तपस्वी महात्माओं के अन्दर जला डालने वाला तेज छिपा हुआ है। ये उन सूर्यकान्त मणियों की भाँति हैं, जो स्पर्श में तो शीतल होती हैं, किन्तु यदि किसी अन्य का तेज उनके ऊपर पड़ने लगे, तो वे आग उलगने लगती हैं।
ठीक ऐसे ही, जैसे नव-मल्लिका का फूल गिरकर आक के पौधे पर आ अटके।
जो इस मुनि-कन्या पर लट्टू हो रहे हैं, वह ऐसा ही है जैसे पिंडखजूर खा-खाकर जी भर जाने पर कोई आदमी इमली खाना चाहे।