Abir Anand's Blog, page 3
August 15, 2017
उम्र
साँसों की उम्र
अस्पताल में बिलबिलाते बच्चों से मत पूछो
सिलिंडर में कैद उस आॅक्सीजन से पूछो
जो अपराध बोध में तिल-तिल रिस रही है।
जबकि खाली हो चुका है आदमी।सङांध की उम्र
स्वच्छता अभियान के दावों से मत पूछो
पास खङे हुए आदमी की नीयत से पूछो
जो शहर के सीवर की तरह चोक हो चुका है।
जबकि गले तक भरा हुआ है आदमी।
अस्पताल में बिलबिलाते बच्चों से मत पूछो
सिलिंडर में कैद उस आॅक्सीजन से पूछो
जो अपराध बोध में तिल-तिल रिस रही है।
जबकि खाली हो चुका है आदमी।सङांध की उम्र
स्वच्छता अभियान के दावों से मत पूछो
पास खङे हुए आदमी की नीयत से पूछो
जो शहर के सीवर की तरह चोक हो चुका है।
जबकि गले तक भरा हुआ है आदमी।
Published on August 15, 2017 00:21
अनीता मंडा जी द्वारा #सिर्री की समीक्षापुस्तक क...
 अनीता मंडा जी द्वारा #सिर्री की समीक्षापुस्तक का नाम - सिर्री
अनीता मंडा जी द्वारा #सिर्री की समीक्षापुस्तक का नाम - सिर्रीविधा- कहानी
लेखक- अबीर आनन्द
प्रकाशन- Zorba books
Isbn -978-93-86407-22-1
सिर्री : नये जमाने की कहानियां : -
अनिता मण्डा
सिर्री पुस्तक का आवरण देखें तो पाते हैं कि एक चेहरा रस्सियों के जाल में लिपटा है और चेहरे से आँखें बाहर झाँक रही हैं। इन आँखों में एक ग़ज़ब की बैचेनी है। यही है आज के समय का मनुष्य। जो कि अन्तस् तक बुरी तरह से मजबूरी की रस्सियों से बंधा हुआ है और इन बन्धनों की कसक, पीड़ा दर्द उसकी आँखों में दिख रही है। ये बन्धन हमारे आस-पास रहने वालों के सबके जीवन को जकड़े हुए हैं। यह अलग बात है कि हम में से सबके पास वो दृष्टि नहीं है कि इन्हें देख पायें। सबके पास वो संवेदना भी नहीं है कि इस बैचेनी को महसूस कर पाएँ। लेकिन हम में से कुछ एक के पास वो दृष्टि भी है और वो हृदय भी है कि इनको देख महसूस कर पायें अबीर आनन्द के पास वो लेखनी भी है कि वो कहानियों में दर्ज़ कर पाये। इसलिए वो नए जमाने की कहानियां, नई शब्दावली में बुन पाये हैं।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अन्य प्राणियों से इस मामले में जरा भिन्न है कि वह अपनी बात कह सकता है संवाद कायम कर सकता है संवाद आएंगे तो कहानियां भी जन्म लेंगी और कहानियां होंगी तो उन पर बात भी होगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं युवा कहानीकार अबीर आनंद के कहानी संग्रह 'सिर्री' की। 'सिर्री' यूँ तो कहानीकार का पहला कहानी संग्रह है परंतु कहानियों पर दृष्टिपात करें तो यह बात हजम नहीं होती कि यह अबीर का पहला कहानी संग्रह ही है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है जो साहित्य समाज से सरोकार नहीं रखता वह मात्र व्यसन है। इस दृष्टि से हम पाते हैं कि सिर्री अपने समय का आईना है।
आज की व्यवस्था के प्रति अबीर आनन्द जी के मन में तीव्र आक्रोश है, भ्रष्टाचार की दलदल में धँसे सत्ता के पाँव, अपना ज़मीर बेच चूका मीडिया, बेरोजगारी की भट्टी में झोंकती शिक्षा-व्यवस्था और बाजारीकरण के चलते देश को लूट खसोटने वाली अनगिनत मल्टीनेशनल कम्पनियाँ। ये सब मिलकर जो माहौल बना रहे हैं उस माहौल में कोई भी सिर्री (पागल) हो जाये। 'सिर्री' में ये परिस्थितियाँ पृष्ठभूमि में काम कर रही हैं। यह सारा हलाहल पिया हुआ मन ही 'सिर्री' में अपनी दृष्टि रख रहा है।
इक्कीसवीं सदी में मल्टी नेशनल कम्पनियों में कार्यरत कर्मचारियों पर दबाव भरी परिस्थितियों में काम करने के दुष्परिणाम उभर कर देखने को मिल रहे हैं। 'रिंगटोन' मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हुए अपने से उच्च पदस्थ लोगों से कितना कुछ सहना पड़ता है इसको बहुत अच्छे से खोल कर रखती हैं छोटी-छोटी गलतफहमियों और गलतियों से तरक्की पर लगे ब्रेक के कारण एक भरे पूरे परिवार को परेशानियों के जंगल से गुजरना पड़ता है
'रिंगटोन' नायक मानस बेहरा की परेशानियों में इजाफा करने में उसके फोन की रिंगटोन "मैं परेशान परेशान परेशान" का अहम किरदार किस तरह है यह जानना रोचक है। 'रेसर टायर कंपनी' की फैक्ट्री में निम्नवर्गीय अधिकारी है मानस। कहानी में टायर बनाने के बारे में अच्छा विवरण भी लेखक के ज्ञान से परिचित कराता है। बड़े अधिकारियों द्वारा छोटे कर्मचारियों का लताड़ फटकार खाना उन्हें किस हद तक प्रभावित करता है सोचनीय है। जरा सी गलतफहमी से एक टायर का खराब होना भी बड़े प्रोजेक्ट हाथ से निकलने का सबब बन जाता है जिसकी बदौलत प्रमोशन भी रुक जाता है इन परेशानियों में फंसे मानस के चैन के दुश्मन है बैंक लोन वाले जो लोन देते वक्त तो जताते हैं कि उनके जैसा हितैेषी कोई नहीं और ज़रा देर होते ही जान के दुश्मन बन बैठते हैं।
बाजार केंद्रित मानसिकता के कारण बैंकों में होड़ लगी रहती है कि अधिक से अधिक ग्राहक बनायें व लोन देकर मुनाफा कमायें और जब कभी ग्राहक परिस्थितिवश समय पर लोन नहीं चुका पाते तो बैंक जिस अमानवीयता पर उतर आते हैं वह अकल्पनीय है उस से उपजे मानसिक संत्रास से जलते हुए युवाओं का जीवन कोल्हू के बैल के माफ़िक हो जाता है 'रिंगटोन' और 'सिर्री' दोनों में यह समस्या दिखाई है।
दिन-रात की पढ़ाई और उच्चांक प्राप्ति के बाद डिग्री लेने के बावजूद जब युवाओं को करने को अपने मनमुताबिक काम नहीं मिलता तो वह मानसिक अवसाद उठना स्वभाविक है और अवसाद से लड़ते हुए जिंदगी के बोझ को ढोते हुए पाँव घिसटना इस समय की तल्ख़ सच्चाई है। यह तल्ख़ सच्चाई बयान हुई है कहानी 'गुटखा तेंदुलकर' में। विज्ञापन जगत की बारीकियों पर लेखक का गहन अध्ययन 'गुटखा तेंदुलकर' को यथार्थ के करीब ले जाता है। किसी उत्पादन में अन्य उत्पादों से कोई श्रेष्ठता न होते हुए भी उसे बाज़ार में पैर जमाने हेतु किन तरीकों से लोगों के दिमाग तक पहुँचाया जाय, यही तो है विज्ञापन जगत। झूठ को सच का जामा पहनाना और लोगों के दिमाग में इस गहराई से उतार देना कि वही सच नज़र आये। यह सब करते हुए इन्हें जनता के स्वास्थ्य की परवाह करने की फुरसत नहीं, इन्हें बस अपना मुनाफ़ा दिखाई देता है। इसके लिए वे विज्ञापन को स्थापित नायकों पर फ़िल्माते हैं। इन नायकों को भी अपने कर्तव्यों से कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ़ पैसे मिलते रहें बस। तेंदुलकर को अपना आदर्श मानने वाले आशीष को मजबूरन यह काम करना पड़ता है लेकिन वो खुद अपनी ही नज़र में गिर जाता है। मानसिक अवसाद बढ़कर सिजोफ्रेनिया (लेखक ने इसे सिजोफ्रेनिया ही लिखा है) का रूप ले लेता है। और चिंता का विषय यह है कि यह कोई एक दो लोगों की परेशानी नहीं, बहुत लोग इसके शिकार हैं। समय पर न बीमारी पहचानी जाती है, न इलाज शुरू होता है।
'चिता' - रोजगार की समस्या, बुजुर्गों की समस्या उच्च पढ़ाई वह उसके बाद कंपनियों में नौकरी के चलते छोटे शहरों और गाँवों से नौजवानों के हुए पलायन विस्थापन के कारण पीछे रह गए बुजुर्गों की मानसिक पीड़ा व उनकी फ़िक्र में संतानों का चिंतित रहना माता-पिता को अपने साथ रहने के लिए चलने के लिए राजी करना बड़े शहरों में अपने गाँव, मित्रों परिचितों से दूर बुजुर्गों का समायोजित नहीं हो पाना यह भी आज के समय की एक महत्वपूर्ण समस्या है जो कि कहानी 'चिता' में उभरकर आई है। पिता पुत्र के बीच मन में बंधी गिरहें जब खुलती हैं, परेशानी दूर होती है, इस तरह कहानी सुझाव भी दिखाती है समस्या पर। दो पीढ़ियों के बीच आई संवादहीनता ने छोटी-छोटी समस्याओं को बढ़ा दिया है। जीवन शैली के बदलाव व साथ साथ लम्बे समय तक एक ही जगह काम करने से प्रेम विवाह जैसी घटनाएँ भी बढ़ गई। पिछली पीढ़ी इसे सहर्ष स्वीकार नहीं पाती, उन्हें यह अपने कहने की अवमानना दिखती है। यही छोटे-छोटे कारण समस्या को और बड़ी बनाते जाते हैं। आज हर गाँव में कई आशुतोष दिख जायेंगे जिनको प्रशांत से शिकायत, मनमुटाव है। बात स्वाभिमान तक पहुँच जाती है। रिश्तों की डोरियाँ खिचने लगती हैं।
कहानी 'हैंडओवर' का कथानक बुनने के लिए कहानीकार को विशेष बधाई। क्योंकि हम जैसे कितने ही लोग अखबारों में आए दिन इस तरह की घटनाएं व इन पर विवरण पढ़़ते हैं इन घटनाओं में आये पात्र जीवित हैं और समाज व राजनीति में हो रहे अत्याचार को झेल रहे हैं पर हम उस पर इतनी देर ठहर कर सोच भी नहीं सकते कि उन पात्रों का जीवन कैसा होगा इन घटनाओं का उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा एक सच्ची घटना को लेकर एक काल्पनिक संसार की रचना कर देना ही लेखक की कसौटी है झम्मन का किरदार किस कदर एक अभिनेता की ज़िंदगी में घटी घटना से प्रभावित होता है कैसे उसकी ज़िंदगी इंतजार और दर्द में झूल रही है यह तो कहानी पढ़कर ही देखा जा सकता है। बाजार नियंत्रित मानसिकता के कारण ही समर्थ वर्ग गुनाह करके भी आजाद घूमता है और पीड़ित वर्ग बेगुनाह होते हुए भी सजा जैसी जिंदगी जी रहा है। राजनीति में घोटाले अब प्रतिष्ठा पा चुके हैं कहीं विरोध की कोई आवाज नहीं जैसे अन्याय और अत्याचार को स्वीकृति मिल गई हो। यही लेखक का दर्द है। ऐसे समय में मौन का टूटना जरुरी है परंतु किसी भी बड़े घोटालेबाज को सजा मिलती नहीं दिखती। करोड़ों की फिल्में हीरो अभिनेता के कारण अटक जाती हैं। इसीलिए, इन अभिनेताओं को सजा न हो इसका बंदोबस्त कंपनियां जी जान से करती हैं। बेगुनाहों की मौत के बाद भी इन पर केस के फैसले सालों-साल नहीं आते। गुनहगार अपने मज़े से गुजर कर रहे हैं। झम्मन जैसे लोग बेगुनाह होते हुए भी इन लोगों के चक्कर में फँस जाते हैं। ओर अंत में मौत को गले लगा लेते हैं। भरपूर संवेदना है इस कहानी में।
एक कहानी 'फ़ेसबुक 2050' सोशल मीडिया को केंद्र में रखकर कथानक बुना गया है इस में बिछड़ा हुआ प्रेम फ़ेसबुक के माध्यम से मिलता है परंतु तब तक बहुत देर हो जाती है यह कहानी यथार्थ कम होकर भावुकता का कुछ अतिरेक कही जा सकती है। 2050 में आज के जैसे ही उद्धात्त प्रेम की परिकल्पना करना एक कल्पना ही लगती है परंतु जब देखते हैं आज "उसने कहा था" कहानी के 102 वर्ष बाद भी 'प्रेम' कहानी के तौर पर स्थापित कहानी है और समाज में भी उसका कुछ अंश ही सही प्रेम बचा हुआ है तो ईश्वर से कामना है कि लेखक की परिकल्पना में ही सही प्रेम को बचाए रखें स्वार्थी समय से।
एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह की है 'मैत्रेयी' जो पूर्णतः एक नारी पात्र पर केंद्रित है। मैत्रेयी कहानी की नायिका है या खलनायिका है यह तो आप पढ़ कर ही निर्धारित कीजिए। वह अपने प्यार हेमंत को कुंडली मिलाने जैसे दकियानुसी कारण से छोड़ने को तैयार नहीं उसकी ज़िद के आगे उस की इकलौती अभिभावक माँ व हेमंत के माता-पिता झुक जाते हैं। यहाँ तक कहानी बहुत ही सुखद है। हेमंत मैत्रेयी के प्रेम का पल्लवित होना बहुत सहजता से और ठहर कर लिखा गया है। यह तो अबीर की विशेषता ही है कि वह हर पहलू पर बहुत तन्मयता से लिखते हैं।
मैत्रेयी अपनी माँ को छोटी उम्र से ही संघर्षरत देखती है। वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो जाता है, अकेली माँ नौकरी करती है बेटी को पढ़ाती है। किसी का सहारा नहीं उसे बेटी के कारण वह दूसरा विवाह भी नहीं करती। मैत्रैयी के अचेतन में शायद कहीं न कहीं माँ का अकेलापन या समाज का यह रूप है कि विधवा विवाह को प्रतिष्ठा नहीं देता है। किसी कारण से उसकी यह सोच पक्की हो गई है कि वह अपने शहीद पति के अंश को भी जन्म नहीं देना चाहती। उसकी माँ उसे स्वार्थी तक कहती है। समझाती है। लेकिन इन सब भावनाओं को तिलांजलि दे कर वह अपनी कोख में पल रहे हेमंत के अंश को जन्म नहीं देकर कोख़ से हटा देती है। इस निर्मम स्तर तक नारी का चले जाना व्यथित करता है। हेमंत के माता-पिता जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है मैत्रियी के इस व्यवहार से आहत हैं। लेकिन इसके लिए उसकी मां को जिम्मेदार नहीं मानते। बाद में जब मैत्रयी को भूल का एहसास होता है वह पछतावा करती है। मैत्रयी के अंदर की स्त्री का व्यवहार पाठक को आंदोलित करता है पर वह इसे स्वार्थ कहे या परिस्थिति? इस तरह न मैत्रयी को थोथे आदर्शों की वाहक बनाया है न परिवार को बेवजह कोसने वाला।
कहानी 'मुक्ति' कर्मों के अकाउंट में अच्छे कर्म जमा करने व बुरे कर्मों को कम करते जाने की अवधारणा को लिए हुए है। कहानी नायक सुयोग को केंद्र में रख कर लिखी गई है जो पिता व ताऊ के जमीन के झगड़ों में पिता को खो चुका है। अपनी करनी को भुगत चुके ताऊ के अंतिम समय में सहारा देकर नफरतों से ऊपर उठता है और ताऊ के अच्छाई के अकाउंट को कम कर देता है और अपनी अच्छाइयों का अकाउंट बढा लेता है।
भाई-भाई के बीच बंटवारे को लेकर हुई वैमनस्यता के चलते एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर देता है यह बहुत घिनौना समय है, नैतिक मूल्यों का पतन पारिवारिक भावनाओं का, परिवार का खत्म होना, मानवता की समाप्ति व सम्वेदनाओं के क्षरण का प्रतीक है।
'प्रवासन' कहानी - कोई अधिकारी अपनी ईमानदारी पर अटल रहे तो महकमे के बड़े लोगों को परेशानी हो जाती है वह एक शरीफ इंसान को तालाब की गंदी मछली बनाने पर कैसे मजबूर करते हैं यह हम प्रवासन कहानी पढ़ कर समझ सकते हैं।
'वीडियो' कहानी में कस्बे के जीवन का सुंदर वर्णन है। दशहरे की धूम-धाम से शुरू हुई कहानी अजय और हरीश दो दोस्तों की कहानी भी है शिक्षक के गुरूतर कर्तव्यों से शिक्षक का कर्तव्यच्युत होना (अजय के पिता द्वारा हरीश के भाई को जान बूझकर फेल कर देना) भी इस कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। जिस तरह एक डॉक्टर का कर्तव्य मरीज को ठीक करना है। वैसे ही एक अध्यापक की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने शिष्यों के साथ न्याय करे, परन्तु यहाँ हम पाते हैं कि अजय के पिता ऐसा नहीं कर पाते। कारण कि हमारी सोच में वर्गभेद की जड़ें बुरी तरह पसरी हुई हैं। यह एक सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल है साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीरता से बात करने का भी मसअला देती है। समाज में वर्ग भेद के कारण ही हरीश का भाई नरेश आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ कहानी सवाल उठाती है, यही इस कहानी की सार्थकता है। यह वर्गभेद का बवंडर दो मित्रों के मन में उठता है, वापस भी बैठता है पर उससे उठी धूल मन पर भी जमती है। कहीं न कहीं सब कुछ वैसा ही नहीं रह जाता।
“झाड़ू लगाने के कारण, प्रांगण में उठा धूल का बवंडर एक बार फिर उठा और प्रांगण में लगे पौधों की स्वस्छ पत्तियों पर पसर गया।” (पृ.१५५ )
'नानी' ऐसा किरदार है जो वास्तविक जीवन में भी हम सब को बहुत प्रिय होता है बचपन की बहुत याद आने से जुड़ी रहती है नानी कहानी में नानी का जो रूप सामने आता है इसकी पुष्टि करता है। नानी बचपन का एक अभिन्न हिस्सा होती है। अभी तक शहरों की समस्याओं पर शहरी माहौल पर बात करते रहे हैं इस कहानी में हम पहली बार अबीर की लेखनी से गांव से परिचित होते हैं। वह भी आपसे कोई तीस साल पहले वाले गाँव क्योंकि 'नानी' कहानी का कथानक है लेखक ने 1987 के समय का बताया है 8 साल का संजू गाँव-ननिहाल को जिस दृष्टि से देखता है लगता है, संजू में लेखक खुद को ही देख रहे हों। अपना ही देखा हुआ अपना ही जिया हुआ प्रकट हो रहा है। संजू के माध्यम से यहां लेखक का मन गांव की प्रकृति के सानिध्य में खूब रमा है। सवारियाँ ढोते बैलों के गले की घंटियां हंसिया दरांत लिए खेतों में काम करते किसान, सुहानी भोर, तारों भरी रातें, बबूल आम के पेड़, गोबर लीपा आंगन, अमरुद ,अनार के पेड़। गांव की प्रकृति को दिखाने के बाद कहानी के माध्यम से लेखक ने गांव में प्रचलित जादू-टोना, भूत-प्रेत को मानने वाली घटनाओं की तरफ भी ध्यान खींचा है। संजू को ननिहाल में नानी नहीं मिलती। 8 साल का बालक कारण भी समझ नहीं पाता कि मामी और नानी में अनबन के कारण नानी कहीं चली गई है। नानी को याद करते हुए पहले की घटनाओं का अच्छा स्थान मिला है जैसे होली की घटना संजू का दीवार के ऊपर से एक चेहरा देखना और उसे नानी का चेहरा बताना नानी के प्रति संजू का असीम लगाव ही है।
सिर्री संग्रह के बाद भी कुछ कहानियाँ अबीर जी की पढ़ने को मिली हैं, निरन्तर प्रगति देख कहानी जगत का भविष्य समृद्ध दिख रहा है।
सिर्री में अबीर ने एक बहुत बड़ी दुनिया से मिलवाया। इसके कुछ पात्र हमारी सोच में जगह बना गये। सुनील (होम लोन से परेशान), मानस ( रिंगटोन बनी सांसत), आशीष ( गुटखे का विज्ञापन को लेकर असन्तुष्ट) ये किसी न किसी रूप में हमारे आसपास ही रहते हैं, बस नाम इनके बदलते रहते हैं। अभी भी अरमान भाई सरीखे कई पात्र गुनाह करके भी खुले घूम रहे हैं। कई अनोखेलाल पछतावे में जलते हुए मुक्ति का मार्ग जोह रहे हैं। कई आशुतोष, प्रशांत अंतर्द्वन्द से जूझ रहे हैं। अपनी अंतरात्मा को कुचल आशीष जैसे इंजीनियर गुटखे का विज्ञापन बना रहे हैं। एक हलचल सिर्री ने हमारे अंदर मचा रखी है। अबीर जी के इस मेहनतपूर्ण कार्य को पाठकों की सराहना का प्रतिसाद मिले इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पहले संग्रह की बहुत-बहुत बधाई।
Published on August 15, 2017 00:08
July 8, 2017
बर्फ़: गंभीर समाचार में छपी मेरी नई कहानी

बर्फ़
"ये जैसे शरीर में नाख़ून उगते हैं न...जिनकी किसी को ज़रुरत नहीं होती। सास, श्वसुर, चाचा, मामा...ये सब नाखून ही होते हैं....।"
वेटर ने पानी का जग मेज़ पर रखा और हड़बड़ी में वापस मुड़ गया। जग से रिसती हुई पानी की एक बूँद उसके सामने रखे व्हिस्की के गिलास के ऊपरी किनारे पर चिपक गईं। एक पैर में गोली खाए हुए सैनिक की तरह उस बूँद ने घिसटना शुरू किया। चिकनी सपाट सतह पर वह कुछ दूर घिसटती और सांसें भरने के उपक्रम में ठहर जाती। वातावरण में घुटन भरी ऊमस थी। सामने, लॉन में अम्बुज के बड़े बेटे आरव का जन्मदिन उत्सव समाप्त हो गया था। रेस्टोरेंट का स्टाफ खाने की प्लेटें, मेजें और इधर-उधर बिखरे गुब्बारों को एकत्रित करने में व्यस्त था। अम्बुज ने अपनी पत्नि अलका को दोनों बच्चों के साथ गाड़ी में बिठा दिया। मेहमान सहकर्मी और मित्र सब जा चुके थे। विनीत देर से आया था। लॉन से निकलकर वह रेस्टोरेंट में बैठ गया और व्हिस्की मंगा ली। अम्बुज भी उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके इशारे पर वेटर व्हिस्की का दूसरा गिलास ले आया।“बर्फ?” वेटर ने पूछा।“हाँ।“ अम्बुज ने इशारे से दोनों गिलासों में बर्फ डालने को स्वीकृति दी।गिलास में बर्फ के पड़ते ही आस-पास की ऊमस जैसे एक चुम्बकीय आकर्षण से गिलास की बाहरी सतह पर द्रवित हो गईं। जीवन की ऊमस में अदृश्य होकर तैरते हुए दुःख एक-एक कर उस बूँद की ओर बढ़ चले जो लँगङाते हुए अब तक अकेले गिलास से नीचे उतरने की लड़ाई लड़ रही थी। झरने की तरह गिरते हुए प्रवाह से सब दुःख एक धार में बह गए। बह जाने दो, मन कुछ तो हल्का होगा।“ज़िद छोड़, और ये रोज़-रोज़ गिलास हाथ में पकड़ने का सिलसिला ख़त्म कर।“ बात-चीत आगे बढ़ी तो अम्बुज ने विनीत को सलाह दी। विनीत लगभग उसकी उपेक्षा कर अपने पेग में व्यस्त था।“ये जैसे शरीर में नाख़ून उगते हैं न...जिनकी किसी को ज़रुरत नहीं होती। सास, श्वसुर, चाचा, मामा...ये सब नाखून ही होते हैं। बढ़ते रहते हैं उम्र के साथ। क्या करें? इनके लिए कोई दवाई नहीं करता..सरल सा उपाय है। सन्डे के सन्डे नेलकटर ले के कुतर दो... बस। अपना कद बढ़ने दो, समझ बढ़ने दो जिनसे प्यार है उनसे प्यार बढ़ने दो। और जो भी लगे कि नाख़ून हो गया है, कुतर दो। सन्डे के सन्डे।“वार्तालाप देर तक चला। कभी विनीत कुछ बोलता तो अम्बुज हावी हो जाता। तीन-तीन पेग पीने के बाद दोनों चल दिए।“तेरह साल हो गए। अपनी तरफ देख। अपनी ज़िन्दगी बना।“ टैक्सी में बैठे-बैठे विनीत के मन ने कई बार समझौता किया। वह जानता था कि सुरूर उतरा और समझौता खारिज़। ऐसा पहले कई बार हो चुका था। पर उस दिन पर वह कुछ ज्यादा आश्वस्त दिखा।कानपुर देहात के एक छोटे से गाँव से था विनीत। पिता रोज़गार के लिए पलायन कर गुजरात में बस गए थे। केमिकल फैक्टरी में कुछ साल काम किया। साँस की शिकायत उठी तो डॉक्टर ने सलाह दी कि कुछ और काम करें। संयोग से उसी समय कंपनी में स्वेच्छा-निवृत्ति की योजना आ गई तो नौकरी से पीछा छुड़ा वे अपने गाँव वापस आ गए और खेती-बाड़ी सँभालने लगे। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद विनीत अपने परिश्रम के सहारे आई आई टी पहुँच गया। पढ़ाई के तीसरे साल में ही उसकी शादी हो गई। पास ही के गाँव में रहने वाली सुनीता बारहवीं पास थी। अठारह साल की हुयी ही थी कि घर वालों ने लोक-लाज के डर से ब्याह कर दिया। गाँव वाले काना-फूसी करते रहे कि सुनीता का गाँव के ही किसी लड़के से चक्कर चल रहा है। पर न विनीत ने और न ही उसके माँ-बाप ने इस अफवाह पर ध्यान दिया। लड़की अगर देखने में थोड़ी भी सुन्दर हो तो ऐसी अफवाहें उठने ही लगती हैं। घर में इकलौता बेटा था, सो विनीत ने भी सोचा कि और कुछ नहीं तो बूढ़े-माँ बाप को सहारा ही हो जाएगा। विनीत की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई ही थी कि सुनीता के पिता ने विनीत के पिता पर दहेज़ उत्पीड़न का केस कर दिया। विनीत ने जिस चिंगारी को आरम्भ में सास-बहू की नोंक-झोंक समझकर नज़रंदाज़ किया वह अब कुटुंब अदालत में एक केस का रूप ले चुकी थी। विनीत जिस सम्बन्ध का कानूनी पंजीकरण भी न करा पाया था उस सम्बन्ध को अदालत ने एक नंबर दे दिया था, केस नंबर।उस दिन जब विनीत के पिता ने कचहरी का पहला चक्कर लगाया तो वह सुनीता और उसके पिता के प्रति घृणा से भर गया। पारिवारिक अवसाद जब कचहरी तक पहुँच जाए तो वह पारिवारिक नहीं रह जाता। वह समाज की ठिठोली का स्रोत बन जाता है। अदालत ने पड़ताल की तो केस में नए पहलू सामने आए। दरअसल दहेज़ की रकम का इस्तेमाल कर विनीत के पिता मगन राम ने अपना घर पक्का करा लिया था जिस पर सुनीता ने आपत्ति की। श्वसुर और बहू के बीच मामला एक बार उलझा तो उलझता ही चला गया। सुनीता के पिता जो पहले बीच-बचाव में सामने आए अब मुखर होकर मगन राम का विरोध कर रहे थे। सुनीता को उन्होंने अपने ही घर बुला लिया था। विनीत को नौकरी मिल गयी और वह बैंगलोर चला गया। कोर्ट कचहरी के चक्कर में कभी-कभार कानपुर जाता तो अपने माँ-बाप की दयनीय स्थिति देख सुनीता के प्रति ज़हर से भर जाता। कोर्ट की कार्यवाही के सिलसिले में उसके पिता परेशान रहने लगे थे। नौकरी में विनीत उन्नति करता रहा। कोर्ट ने बहुत जोर देकर दोनों परिवारों की सुलह करा दी और सुनीता विनीत के साथ रहने के लिए बैंगलोर आ गयी। विनीत आश्वस्त हो गया कि सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ भी ठीक न हुआ। बैंगलोर में भी खटास जस की तस बनी रही। मन का मैल साबुन घिसने से नहीं जाता। उसके लिए तो बस आँखों से आँखें मिलाकर सच बोलना होता है, धैर्य से, शालीनता से और पवित्रता से अपने मन के अंतर्कुंड में डुबकी लगानी पड़ती है। मन की ज़मीन बंजर हो तो तन के मिलन से भी फूल नहीं खिलते। दोनों के बीच सम्बन्ध बना फिर भी आँगन सूना ही रहा। एक दूसरे के पिता को कोसते हुए दोनों में झगड़ा होने लगा। एक दिन सुनीता सब कुछ छोड़-छाड़ कर वापस पिता के घर चली गयी। पिता आहत हुए तो उन्होंने फिर कचहरी का सहारा लिया और तलाक़ के लिए अर्जी डाल दी। विनीत को कंपनी ने दो साल के लिए अमेरिका भेज दिया। तलाक़ की अर्जी कचहरी में धूल छानती रही। विनीत, सुनीता और सुनीता के पिता, तीनों के अहम् विकराल रूप धर चुके थे। कचहरी के चक्करों में विनीत अपने पिता का बुढ़ापा उधड़ते हुए देख रहा था। वह खीझ उठता कि आखिर उसने विवाह किया ही क्यों? उसने सुनीता के पिता से सुलह करने का दोबारा प्रयास किया। पर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि तीनों एक दूसरे को शत्रु समझते लगे। सुनीता के पिता को मौका मिला तो उन्होंने दहेज़ में दिए गए 8 लाख रुपये वापस करने की माँग रख दी। फिर क्या था? विनीत को समझ आने लगा कि सारा खेल पैसे के लिए खेला जा रहा है। वह भी ज़िद थाम कर बैठ गया कि चाहे जो हो जाए वह किसी भी हाल में रुपया नहीं देगा।विवाह के पहले, गाँव के ही एक लड़के के साथ सुनीता के प्रेम वाली बात सच निकली। जाति बंधनों के चलते सुनीता के पिता ने लड़के को अस्वीकार कर दिया। एक फाँस रह गयी, जिसके चलते न उसके पिता उसे रास आते और न विनीत। यौवन की उमड़ती धधक में इतना विवेक कहाँ रहता है कि वह सही या गलत का तर्कसंगत निर्णय ले सके। पिता गेहूं बन पिसे तो विनीत घुन बन। उसी प्रेम प्रसंग को लेकर पिता को भी सुनीता से शिकायत थी। गाँव में उनकी अच्छी-खासी बदनामी हो चुकी थी। विनीत भी उन्हें दहेज़ का लालची बेटा जान पड़ा जो अपने बुद्धि-विवेक को ताक पर रखकर सिर्फ अपना करियर बनाने में व्यस्त था। विनीत को इस प्रेम-प्रसंग के बारे में भनक लगी तो वह भी शिकायत से भर उठा। श्वसुर के लिए नफरत तब जागी जब उन्होंने अपने दहेज़ की रकम वापस करने की माँग की। परिश्रम से कमाया हुआ रुपया एक लोभी पिता के हाथों सौंपकर अपना जीवन छुड़ाना उसे हरगिज़ मंजूर न हुआ। ज़िन्दगी खिसकती रही। विनीत अपने दोस्तों, सहकर्मियों के घर बसते हुए देखता रहा। उनके बच्चों के जन्मदिन या अन्य परिवारिक उत्सवों में मूक दर्शक बना भागीदारी करता रहा। कभी-कभी वह झुंझलाकर निर्णय भी ले लेता कि रुपए अपने श्वसुर के मुंह पर मारकर वह सुनीता को वापस ले आएगा, पर ऐसे विचार शराब गले के नीचे उतर जाने का बाद या फिर उसके आँसुओं के देर तक रिस जाने के बाद आते। शराब और आँसू सूख जाते तो ये विचार भी अपने आप सूख जाते। होश में आते ही अहम् धर दबोचता और विचारों को मिट्टी में मिला देता। वह हौसला जो पुरुष को भूल सुधार कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, विनीत कभी जुटा ही न सका।दोस्तों ने बहुत समझाया। नाख़ून समझकर अनचाहे रिश्तों को सन्डे के सन्डे कुतरते रहो। पर विनीत वह नेलकटर अपनी हथेली में उठा ही न सका। दोस्तों के जोर देने पर वह बहाना बना देता कि उसने पैसा पाने माँ-बाप की देखभाल के लिए जुटाया है। कल को हारी-बीमारी में एक वही तो है जो उनका खयाल रख सकता है। सुनीता ने अपने प्रेमी का विवाह होते देखा तो उसके विछोह का दर्द और बढ़ गया। वह उस मखमली स्वप्निल दुनिया में जीने लगी जहाँ वह असफल प्रेमिका थी, जिसने अपने प्रेमी को विछोह की आग में झोंक दिया था। वह कभी देख ही न सकी कि प्रेमी अपने दाम्पत्य में मग्न है। वह एक ऐसे अपराधबोध में सुलगती रही, जो संभवतः अपराध था ही नहीं।और कुछ साल गुजरे। बरसों तक खेत में हल नहीं चला। न कभी पानी दिया गया न गुड़ाई की गयी। धूप रोज़ आकर मिट्टी को कुछ और सुखा जाती। रिश्तों के बीच का पर्वत कुछ और कठोर हो जाता। रिश्तों की फसल यदि भाग्य के मानसून के सहारे छोड़ी जाए तो उतना ही राशन मिलता है जितना भाग्य में लिखा हो। भरपेट भोजन करना हो तो पसीने से सिंचाई करनी ही पड़ती है। कचहरी अपनी कार्यवाही करती रही। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को राजी न था। वकील और जज प्रसन्न थे कि उनका कारोबार चल रहा है। वैसे तो पिता ही कार्यवाही देखते रहते थे पर विनीत को कभी-कभी हाजिरी लगाने आना पड़ता था। फिर एक दिन पिता चल बसे। कचहरी में एक भीड़ भरी जगह पर साँस की दिक्कत बढ़ी और वहीं दम तोड़ दिया। जो साजोसामान विनीत ने उनका ‘खयाल’ रखने के लिए जुटा रखा था कुछ काम न आया। वह टूट गया। माँ से कुछ कहना चाहता था पर अनपढ़ माँ उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थी। सालों तक मूक बनी वह अपने पति और बेटे को जूझते हुए देखती रही। एक बार जब उसका स्त्री-विवेक हावी हुआ तो उसने सुलह के लिए पति और बेटे पर दवाब बनाया। वह सफल भी हुई। पर सुलह के बाद जब बात न बनी तो उसने भी अपनी समझ का प्रयोग कम कर दिया। विनीत के किसी भी प्रश्न का उत्तर माँ के पास न था।अम्बुज के बेटे की पार्टी के बाद वह घर पहुंचा और बिस्तर पर निढाल हो गिर पड़ा। शराब का असर कुछ कम हुआ तो उसे महसूस हुआ कि आँखों से नींद जा चुकी है। वह आँखें मींचे अपने मन के अँधेरे कोनों में नींद को तलाशने लगा। पिछले तेरह सालों की ज़िन्दगी का एक-एक कतरा उसकी आँखों में चुभ रहा था। ग़ालिब का वह शेर उसे अचानक याद हो आया ‘यूँ होता तो क्या होता’। सुनीता खूबसूरत है। यदि सब कुछ ठीक होता तो वह भी किसी का पिता होता। सुबह दफ्तर जाने से पहले कोई नाश्ता बना कर खिलाता। स्कूल से लौटे हुए बच्चे की शिकायतें होतीं, छुट्टियों में घूमने जाने की फ़रमाइशें होतीं। जिस पिता के ख्याल रखने की आस में वह रूपया जमा करता रहा, वह पिता तो अस्पताल जाए बिना ही चल बसा। बचपन की कितनी ही योजनाएँ धरी रह गईं। फिर ज़िन्दगी से ये ज़िद क्यों? जीवन उसी का है, परिवार उसका है, उम्मीदें भी उसी की हैं। फिर कोई और क्यों उसकी उम्मीदों को पार लगाने आएगा। उसे खुद ही पहल करनी होगी; और आधी-अधूरी पहल नहीं बल्कि उद्देश्य को एक सार्थक अंत तक पहुँचाने वाली पुरज़ोर पहल। वैसी पहल जैसी वह अपने दफ्तर के कामों में करता था। अगले सप्ताह कोर्ट की तारीख है। पिता तो रहे नहीं। अब उसे ही जाना होगा। उसने निश्चय किया कि वह सुनीता के पिता को 8 लाख रुपये दे देगा और सुनीता को वापस ले आएगा। रुपये लेकर उसके श्वसुर केस वापस ले लेंगे। वह सुनीता को मना लेगा। ज़िन्दगी फिर से पटरी पर आती दिख रही थी। नींद आये न आये। सुबह उसके होश में आते दुनिया यदि उधर की उधर होती हो तो हो जाए। वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। सुनीता को वापस लाकर ही दम लेगा। सुनीता के पिता से उसने फ़ोन पर बात की। उन्हें बता दिया कि वह सुलह करने को राज़ी है और उनकी शर्त के अनुसार रुपये भी देने को। सुनीता का एक छोटा भाई था जिसके विवाह की उम्र हो चली थी। पिता ने बेटे के विवाह में आने वाली अड़चनों के बारे में सोचा। सम्बन्धी प्रश्न तो ज़रूर उठाएंगे कि बेटी घर में क्यों बैठी है। सो तय कर लिया कि विनीत से पैसे लेकर केस वापस ले लेंगे। बेटी की राय लेना उन्होंने उचित न समझा।कोर्ट में तारीख के एक दिन पूर्व शाम को वह सुनीता के घर पहुंचा। श्वसुर ने आवभगत की और पिता की मृत्यु पर दुःख जताया। उसने रुपये दे दिए और आग्रह किया कि कल कोर्ट जाकर वह केस वापस ले लें। श्वसुर सहमत हो गए। नाश्ता कर के वह चला गया। सुनीता को पता चला तो उसने कोहराम मचा दिया। पिता को भला बुरा कहने लगी। पिता ने समझाने का प्रयास किया पर वह शांत न हुई। रात हुई तो खाने के बाद फिर पिता ने बेटी को समझाने का प्रयास किया। उसकी प्रतिक्रिया में उबाल कुछ शांत हो गया था। सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो विचलित हो उठी। वियोग की मारी प्रेमिका और पिता की ज़बरदस्ती से असंतुष्ट बेटी की जगह एक पत्नि ने ले ली। अदालत की कार्यवाही कुछ भी कहती हो पर आखिर वह विनीत की पत्नि थी। अपने पूर्व प्रेमी को पत्नि के साथ शहर जाते हुए देखती तो उसे खुद पर तरस आने लगता। प्रेमी तीन बच्चों का पिता बन चुका था।शाम के आठ नाजे समाचार फ़्लैश हुआ। विनीत के होश उड़ गए। पांच सौ और हज़ार रुपये के जो नोट वह अपने श्वसुर को थमा आया था वे अब मान्य नहीं रह गए थे। सरकार ने त्वरित प्रभाव से नोटबंदी का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया था। विनीत रात भर सो न सका। सुबह पौ फटने तक वह सुनीता के घर पहुँच गया। सूरज की लालिमा आकाश को दूषित करती नज़र आ रही थी। “रुपये तो तुम्हारे सब कागज़ हो गए।“ श्वसुर ने चाय तक को न पूछा।“हाँ, कागज़ तो हो गए पर आपके हाथों में आने के बाद। मेरे हाथों में वे आज भी मेरी पसीने की कमाई का हिस्सा हैं। किसी चीज़ का मूल्य वही समझ सकता है जिसे उसकी ज़रुरत हो।“ विनीत अधीर हो उठा।“अब जब नए नोट आ जाएँ तभी केस वापस होगा।“सुनीता भी बैठक में आ गई। वह देख रही थी विनीत के चेहरे पर लड़खड़ाते सूरज को। विवाह कर ले गया था उसे। अपनी बचाई हुई जमा-पूँजी उसने पिता के हाथ में रख दी थी, सिर्फ सुनीता को वापस ले जाने के लिए। विनीत अपनी ज़िद छोड़कर एक ऐसी शर्त मान ली थी जिसके लिए सुनीता स्वयं सहमत न थी। बर्फ़ गिलास में गिरकर पिघलने लगी थी। विनीत की ज़िद और पिता के विरोध के बहाने तले वह खुद को छलती आई थी। एक जीवन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और वह दूर भागती रही, शबनम की उन बूंदों की तलाश में जो सूरज की पहली किरण पाकर सूख चुकी थीं। पिता को उससे प्यार होता तो पिता की बर्फ पहले गलती। वह उठी और भीतर से अपना सामान बांधकर ले आई।“मुझे जाने दो, पिताजी।“ उसने कहा।पिता ने उसे डपट कर बिठा दिया। वह फिर खड़ी हो गई और विनीत को अपने साथ लेकर बाहर चली गई। सुनीता की माँ चुपचाप देखती रही। मन ही मन खुश होती रही। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के बोल भले दब जाते हों उनके अंतर्द्वन्द्व नहीं दबते; और न दबते हैं उनके आशीष। एक बर्फ और पिघली। बेटी को डपटता, प्रतिरोध करता पिता का स्वर अचानक कुंद हो गया।“रुको!” विनीत को संबोधित करते हुए पिता ने आवाज दी।“ये रुपये अपने पास रखो। तुम ठीक कहते हो...मेर हाथों में आने के बाद इनका मोल ख़त्म हुआ है।“ वातावरण से छँट-छँट कर सारे दुःख गिलास की सतह पर द्रवित हो गए और झरने के वेग से बह निकले। सुबह के सूरज की लालिमा अब सुहानी लग रही थी।
Published on July 08, 2017 22:11
'सिर्री': डॉ. लता अग्रवाल की समीक्षा
 कहानी संग्रह - सिर्री"न किसी प्रभावी व्यक्तित्व द्वारा भूमिका, न लेखक का लम्बा-चौड़ा परिचय, केवल विषय पर बात..."
कहानी संग्रह - सिर्री"न किसी प्रभावी व्यक्तित्व द्वारा भूमिका, न लेखक का लम्बा-चौड़ा परिचय, केवल विषय पर बात..."कहानी संग्रह: सिर्री
लेखक – अबीर आनन्दसमीक्षक – डॉ लता अग्रवाल
कथित सभ्यता के दौर में जीवन की परिभाषा भी बदल गई है। यही कारण है कि हम हर धडकते दिल को जिन्दा मान बैठे हैं। हमारी शिक्षा, सभ्यता कितनी भोथरी हो गई है कि हम चेहरों की इन लकीरों को पढने में असमर्थ हैं। हम ही क्यों? हमारा समाज, मीडिया, कानून-व्यवस्था, रिश्ते सभी तो उथले होकर रह गये हैं। अगर कोई इस आवरण के भीतर जाना भी चाहे तो लोग उसे ‘सिर्री’ (सनकी ) की संज्ञा देते हैं। किन्तु ये सिर्री एक समाज को बचाए रखने के लिए कितने उपयोगी हैं यह चिन्तन का विषय है।
अबीर आनन्द जी द्वारा रचित कहानी संग्रह ‘सिर्री’ ऐसी ही परतों को अनावृत कर समाज को हकीकत से रूबरू कराता है इससे पहले कि यह समाज पूर्णत: जड़ हो जाये। ग्यारह कहानियों का यह संग्रह मुझे अन्य कहानी संग्रहों से हटकर लगा। पहले, संग्रह को पढकर महसूस हुआ आज परिवार से लेकर कार्पोरेट जगत, समाज हर जगह परिस्थितियों से जूझते हुए व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है और यही अस्वस्थता उसके व्यवहार में परिलक्षित हो रही है। यही है सिर्री। दूसरे, यह संग्रह आम संग्रह से कुछ भिन्नता लिए है जैसे न किसी प्रभावी व्यक्तित्व द्वारा भूमिका, न लेखक का लम्बा चौड़ा परिचय, केवल विषय पर बात। हमारी जीवन शैली, रिश्ते, सुविधाएँ जुटाने की जद्दोजहद, जो मिला उसकी उपेक्षा कर जो नहीं मिला उसके पीछे भागम-भाग यह हमारा सिर्रीपन नहीं तो क्या है ?
कार्पोरेट जगत की दुनिया बहुत चुंधिया देने वाली है विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी आज पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में आ चुकी है , एक बार इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद यहाँ से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है और साँस लेना दूभर। परिणाम इस घुटन भरे वातावरण में रह कर वे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। 'रिंगटोन’ तो माध्यम है जीवन को प्रतिबिम्बित करने का, कहना न होगा जीवन और मोबाईल की रिंगटोन में सामंजस्य बना बात को खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। मैं परेशा ...परेशा ...यह मानस के मोबाईल की ही ट्यून नहीं है उसके जीवन की भी ट्यून बन गई है। मल्टी-कम्पनियों में जीवन कितना जटिल है, यहाँ केवल व्यवसाय की भाषा बोली और समझी जाती हैं इन्हें कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन से कोई सरोकार नहीं। उच्च अधिकारियों की तानाशाही अधीनस्थ कर्मचारियों के जीवन में खौफ पैदा करती है। इसका प्रतीक है, 'सावंत की चीखती आवाज के आभास भर से मानस के मस्तिष्क के बांध ढीले पड रहे थे।' अधिकारी अपनी असफलता का ठीकरा अधीनस्थों पर फोड़ता है, कौए कोयल पर राज कर रहे हैं। यही कलयुग की निशानी है और आज की ज्वलंत समस्या भी। चाटुकारों ने इमानदारों का जीवन दुश्वार कर रखा है। दूसरे शब्दों में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर रही है।
'बिना गलती डाँट खाना भी मानस जैसों की ड्यूटी का एक अंग बन चुका है।' इसका प्रभाव सीधे प्रमोशन पर ...प्रमोशन का न होना आत्मविश्वास का खंड-खंड होना, मानसिक कुंठा का उत्पन्न होना ...मल्टी-कम्पनियों की व्यवस्था एवं विसंगतियों को दर्शाती है। जहाँ कर्मचारी को भी मल्टीस्किल मान उसका चहुँ ओर शोषण होता है। उस पर बॉस का निरंकुश व्यवहार, 'सावंत की चीखती हुई आवाज के आभास भर से मानस के मस्तिष्क के बांध ढीले पड़ रहे थे।' 'भाप में वह तपिश कहाँ, जो सावंत के उबलते रुआब में थी?' इस तरह अधिकारी का खौंफ हावी होने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी प्रभावी होती है। अबीर जी ने कम्पनी की कार्य प्रणाली को जिस तरह प्रस्तुत किया है लगता है वे तकनीकी विशेषज्ञ हैं; यह विषय के प्रति उनकी समझ को प्रदर्शित करता है। 'यदि ब्लैडर जल्दी बदले, समय नष्ट होने का खतरा, समय पर नहीं बदला तो स्क्रेप होने का खतरा।'
ऐसी ही कार्पोरेट की आभासी दुनिया में उलझी कहानी ‘गुटखा तेंदुलकर’ के राहुल और आशीष की। शहरी परिवेश में अपनी चादर से अधिक पैर पसारने की लालसा मुंबई की ओर रुख कर देती है जहाँ मालिक और नौकर के बीच सिर्फ व्यापार का रिश्ता होता है, प्रतियोगिताओं वाली इन कम्पनियों में पिसता है बेचारा कर्मचारी। 'व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, सदाचार से कम्पनियों का मीलों तक कोई सम्बन्ध नहीं उन्हें बस अपने लाभार्जन से मतलब है लागत पूंजी का रिटर्न और लाभ यही उनकी शर्त है। जो कर्मचारी उन्हें लाभ देगा, बिजनेस देगा उसका ही जयकारा गूंजेगा; जो कर्मचारी दिन रात एक कर इस बिजनेस को कार्यान्वित करते हैं वे सदैव नेपथ्य में रहते हैं।' अपना माल बेचने के लिए वे जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से भी नहीं हिचकते, विज्ञापन का हकीकत से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं। चाहे मदिरा हो गुटखा या तम्बाखू। सरकार भी जानती है ये हानिकारक उत्पाद है मगर धडल्ले से व्यापार हो रहा है सुरक्षा के नाम पर कहीं कोने में बारीक़ अक्षरों में लिख दिया जायगा , 'दिखाया गया उत्पाद मात्र सृजनात्मक चित्रं है।' हकीकत में यहाँ तरक्की का एक ही सूत्र है, 'मिलाना, पिलाना, सुलाना' (पृ ३५),यही नैतिकता रह गई है। मीडिया भी हरे कागजों पर बिछी पड़ी है। ‘अपना काम बनता भाड़ में जाय जनता', युवाओं की कहीं मज़बूरी कह लीजिये कहीं लक्ज़री लाइफ स्टाइल की चाहत उन्हें इस और धकेल देती है। परिणाम सिजोफ्रेनिया का शिकार, कहानी में राहुल और आशीष दोनों ही सिजोफ्रेनिया के शिकार हैं, एक व्यवसाय से सामंजस्य न बैठा पाने के कारण इसका शिकार हुआ दूसरे ने मित्र की मुक्ति का हल उसके जीवन की मुक्ति से निकाला। लेखक ने मुंबई की भीड़ में सिमटी जिन्दगी का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। आज की मल्टी नेशनल कम्पनियों में मालिक- नौकर के तनावपूर्ण रिश्ते , परिणाम कई मानसिक बीमारियाँ। अतिश्योक्ति न होगी कहें तो कि ऊपर से महंगे सूट बूट से सजा तन, भीतर बीमार मन आज हर घर की कहानी है। यद्यपि आशीष का मारा जाना खलता है। संग्रह की शीर्ष कहानी है ‘सिर्री’,जिसमें पति- पत्नी के बीच के तालमेल और जीवन शैली को लेखक ने खूबसूरत अंदाज में व्यक्त किया है। 'उर्मिला के तवे के साथ पति के कमीज के बटनों की बरसों से चली आ रही बंदिश बटन का खुलना उधर तवे पर रोटियों का फुदकना।' इतनी प्यारी बंदिश के बाद आखिर इन्सान क्यों सिर्री हो जाता है? क्यों टूट जाती है यह बंदिश? कहानी का नायक सुनील समाज के ऐसे कई पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो परिवार के लिए सुविधा जुटाने हेतु प्रायोजित योजनाओं का आश्रय लेते हैं। सुनील ने भी अपनी छत का सपना देखा और बैंक की नीतियों के जाल में उलझ गया। बैंक या ऐसी योजना वाली कम्पनियां जो कि लोन लेते समय ग्राहक को सब्जबाग दिखा फ़ांस लेते हैं बाद में वसूली के नाम पर उनका जो व्यवहार होता है वह अच्छे भले इन्सान को मानसिक रूप से बीमार बना देता है। सुनील भी बैंक के इस रवैय्ये से भीतर ही भीतर टूट रहा था, टूट रहे थे पत्नी उर्मिला से उसके रिश्ते, बिखर रहा था उसका हँसते खेलते परिवार का सपना। ग्राहक, बिल्डर और बैंक के त्रिकोण को लेकर बुनी यह कहानी आम जीवन के बेहद निकट है। अपना टारगेट पूरा करने बैंक/ कम्पनियां ग्राहकों को बिल्डर के माध्यम से फंसाती है। 'कितने बैंक अधिकारियों ने रिश्वत लेकर कार्पोरेट जगत की बड़ी मछलियों के अवैध लोन पास किये फिर दोनों चैन की बंसी बजाते रहे और एक मध्यम वर्गीय ग्राहक को गिरवी लोन के लिए एक पूरी जिहाद लड़नी पड रही है...द भोकाल बैंकिंग'। (पृ .११५ ) सुनील जिस बीबी बच्चों के सुख के लिए यह सब कर रहा है तनाव उसे उन्हीं से दूर कर रहा है बेटे की मासूम गलती पर उसका क्रोध जब बच्चे पर फूट पड़ता है, 'जिन्दगी नर्क बनाकर रख दी है हरामखोर ने... कहीं मर खप क्यों नहीं जाता तू?' उसे भी एहसास है कि घर जिसका सपना हर इन्सान देखना चाहता है। मगर आज जिन्दगी की जद्दोजहद ने इस सपने को इतना दुरूह बना दिया है कि 'इस दुनिया में घर का सपना देखना गुनाह नहीं बल्कि ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं।” अपनी भावनाओं की कुर्बानी देकर सुनील यह जंग तो जीत जाता है मगर बिना भावनाओं, संवेदनाओं के स्वयं को मुर्दा महसूस करता है ठीक वैसे ही जैसे जठराग्नि के राख होने तक कोई भोजन का इंतजार करे और जब अग्नि राख बन जाय तब उसे भोजन मिले वही मनोदशा होती है सुनील की जब लोन का फीड बैक लेने कम्पनी फोन करती है तब प्रतिक्रिया ठीक ऐसी होती है, 'आप एक मुर्दे से बात कर रहे हैं और मुर्दे फीडबैक नहीं दिया करते' (पृ १२३)त्रासद है जिनसे हम जीवन को सुविधा सम्पन्न और सुखद बनाने की उम्मीद रखते हैं वही हमारे जीवन को नारकीय बना दे।कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ समाज के कई गंभीर प्रश्नों को उठाना है। जो लेखक जितने चुनौती भरे प्रश्न कहानी के माध्यम से उठायेगा कहानी उतनी ही कालजयी होगी। इस दृष्टि से मानवीयता, कानून और मीडिया को कटघरे में खड़ी करती कहानी'हेंडओव्हर' बहुत दमदार कहानी है। समाज के प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा किया गुनाह और चक्की में पिसते कई निरीह जन। आँखों में कई सपने लेकर गाँव से शहर आया झम्मन, मुंबई की भीड़ में खो गया। फुटपाथ पर पनाह मिलना भी बुरा संयोग हुआ कि एक अमीर के गुनाह का चश्मदीद गवाह बन गया। जिसने टूटे दिल के गम का कहर मासूमों पर ढाया और अपनी स्कार्पियो के पहिये तले निर्दोषों को कुचल दिया। कहानी समाज से कई अनुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मांगती है। क्या सत्य का साथ देना कितना मुश्किल है? कानून रसिकलाल के लिए इतना कठोर है तो भाई के लिए क्यों नहीं? रातों रात ख़बरों का बदलना, मीडिया को सवालों के घेरे में खड़ा करता है? बारह सालों में आधा दर्जन दरोगाओं का हेंड ओव्हर कर चले जाना? सुरक्षा विभाग से जवाब मांगता है। 'जो मुंबई ब्लास्ट में एक्यूज्ड हैं हम उनको परदे पर पुलिस इन्स्पेक्टर बना के सर पर ताज पहनाते हैं? सड़ा हुआ तंत्र है हमारा, दो लोगों का कत्ल करके चैन से बैठा है अपने घर में हमारे और तुम्हारे बच्चों के लिए हीरो है।' (पृ २१२) सीधे-सीधे जनता की राष्ट्र धर्मिता पर सवाल। '....फिर अमीर मुजरिम भले ही नागा कर ले, गरीब गवाह का नागा अदालत का समय व्यर्थ कर देता क्यों?' मुजरिम अदालत में पेश होने के बजाय शूटिंग में व्यस्त, हीरोइन से इश्क लडाता है? भय और तनाव में मुजरिम के चेहरे की रंगत उडनी चाहिए जबकि यहाँ भय और पुलिस के खौंफ से गवाहों की रंगत उडी हुई है? सबसे बड़ा सवाल 'बेबी डोल का फोटो रंगीन पेज में देश की सीमा पर शहीद जवानों की तस्वीर ब्लेक एंड व्हाइट में क्यों' ?(पृ २११) अपराधी खुले विचरण करते हैं और गवाहों को मिलती है पुलिस की प्रताड़ना। 'एक महिना तड़ीपार... फोन वोन कुछ नहीं ले जाना ...एक महिना पूरा होने के बाद पहले इधर थाने में सम्पर्क करना समझे ...!' (पृ २२४)आज देश में चाहे विजय माल्या हो या व्यापम जैसा कोई घोटाला सभी में मुजरिम अपने अनुसार शतरंज की बिछात बिछाकर कानून की गोटियों को अपने अनुसार फिट करते हैं। बालीवुड का बादशाह एक पात्र है ,जिसे भी लेखक ने निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत किया है | यही है लेखकीय दायित्व। 'पचास का होने को है , अभी तक शादी नहीं हुआ है , बाडी तो देखो अप्सरा पानी मांगे है।' (पृ २१२)अपराध में सारे गवाह, आर टी ओ का मुकर जाना, बोस्को द्वारा गाड़ी ड्राइव करना, स्वीकारना असहाय वर्ग पर दबाव नहीं तो क्या है? वहीँ न्याय व्यवस्था में राजनीति का दखल अपराध को बढ़ावा देता है, इसका प्रतीक है राजनेता की बेटी की शादी में मुजरिम की लोकप्रियता का लाभ उठाना। झम्मन प्रतीक है उन लोगों का जो बिना अपराध सजा पा जाते हैं , उनके समक्ष बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वे किस अदालत में जाएँ न्याय हेतु ..? अपराधी खुला घूम रहा है, वकीलों की चाँदी हो गई बस मुसीबत में हैं गवाह। बालीवुड का बादशाह तो फिर भी शादी कर देर सबेर घर बसा लेगा मगर झम्मन घर बसाने की आस लिए संसार से विदा हो गया। वैसे ही शिक्षा में भी सत्ता का हस्तक्षेप विद्यालय को रणस्थल बना रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के पक्षधर व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का उपकुलपति बनाया जाता है। (पृ २१५ ) 'पुलिस का शराबी दौर , गवाहों की फजीहत' ने आम आदमी की नजर में कानून के प्रति असम्मान पैदा कर दिया है।
संग्रह में दो प्रेमकथायें हैं, दोनों अलग-अलग कलेवर में नारी के दो रूपों से परिचय कराती है। एक और है ‘फेसबुक २०५०’ प्राचीन प्रेम को खोज निकालती तकनीकी पर आधारित खूबसूरत कथानक है, जहाँ फेसबुक के कई दोष गिनाये जाते हैं वहीँ फेसबुक ने पुराने बिछडे रिश्तों की डोर को पुन: जोड़ दिया। सुरेन्द्र और नेहा का प्रेम आया तो जवानी की दहलीज पर ही था किन्तु परिवार के बेरीकेड को पार नहीं कर सका, एक दूसरे को भुला भी न सका। वे उम्र के कई पडाव पार कर अचानक फेसबुक के जरिये बुढ़ापे में मिले। उम्र ने उनकी सोच में भी परिपक्वता ला दी तभी तो एक दूसरे को अफ़सोस न हो इसलिए दोनों ही उस आहत मन को झूठी ख़ुशी की चादर से ढकते रहे। आज तक अविवाहित रहकर भी झूठी कहानी रचते रहे। "मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे तुम्हें देखना चाहता हूँ।" बूढ़े ने कहा।'“मेरे पति को मेरा किसी गैर मर्द से मिलना अच्छा नहीं लगता।” (पृ.१७८)“तुम्हारी शादी कब हुई?”बुढिया ने उल्टा सवाल दागा ,”तुमसे टूटने के चार साल बाद ।”अबीर जी ने कहानी में कई स्थानों में कविता के माध्यम से भी अपनी भावनाओं को व्यकत किया है। “लफ्ज मिटटी के मचलते हैं बरसने को, तेरे पत्थर के आंगन में, कोई समझाये मेरे दिल को कि अफसाने कभी ऐसे नहीं बनते।” (पृ . १७९) मगर अफ़सोस यह प्रेम एक दर्द भरी दास्ता बनकर रह गया। जिसके तक़दीर में सिर्फ जुदाई ही लिखी थी। कहीं परिवार की खोखली मान्यता तो कहीं कुचक्र की भेंट आज भी कई प्रेम कहानियां चढ़ती हैं। ऐसे ही प्रेम के एक अलग अंदाज की कहानी है ‘मैत्रयी’। जब से माता पिता ने बच्चों को उनका सपनों का संसार उनकी शर्तों पर मुहय्या कराया है तब से उनके सदाचार की दीवार ढह गई है। बिन बाप की बेटी मैत्रयी को माँ के प्यार ने, जिद्दी और बदमिजाज बना दिया। हेमंत को हासिल करना उसका एक मात्र लक्ष्य बन गया। सितारों की चाल को चुनौती दे कर अपनी जिद पूरी कर लेती है। इतना ही नहीं इसके लिए वह हेमंत के माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करती है। “देखती हूँ किसकी दम है जो डोली लेकर आये यहाँ।”(पृ१९५) तसल्ली की बात यह है कि उसकी कुचालों में माँ उसके साथ नहीं है। लेखक ने माँ की गरिमा को बरकरार रखा। मैत्रयी की माता की समझाइश, “जीवन में सबकुछ अपनी शर्तों पर नहीं मिलता" इस बात को प्रमाणित करता है कि माँ तो सदैव बच्चों को अच्छे संस्कार हो देती है मगर बच्चों ने जो आभासी दुनिया अपने आस पास रची है उसके आगे उनके भी घुटने टिक जाते हैं।
कहानी एक ओर ज्योतिष को सच ठहराकर प्राचीन मान्यता या कुछ पाठक की दृष्टि में अन्धविश्वास को बढ़ावा देती है। किन्तु इसका दूसरा पक्ष है एक स्त्री की अतिशय स्वच्छंदता, हठ एक हँसते खेलते परिवार को कैसे मातम में बदल देती है, फिर वही लड़की जो ज्योतिष के सारे दावों को झुठलाकर अपने प्यार का दावा करती है वही हेमंत की मौत को कितनी आसानी से भुलाकर अपनी रह निकल जाती है इतना ही गर्भ में पल रही हेमंत की निशानी को उसके मारा पिता की अनुनय – विनय के बावजूद नष्ट कर कोई और जीवन साथी तलाश लेती है। “मैंने नहीं कराया कोई कारगिल युध्द, मैंने उसे नहीं कहा आर्मी में जाने के लिए, उसने अपना रास्ता खुद चुना, उसका अपना दुर्भाग्य था।” मुझे कहते कतई संकोच नहीं कि समाज में नारी का यह पक्ष भी प्रबल है। किन्तु कहते हैं न इन्सान जब कोई अपराध करता है तो देर सबेर मन की अदालत में वह स्वयं को मुजरिम करार पाता है।
आत्मीय रिश्तों में पगी मासूम सी किन्तु परिवार और समाज की कई स्याह परतों को खोलतो कहानी है ‘नानी’। नानी को हम बाल मनोविज्ञान से जुडी रिश्तों की अनूठी कहानी कह सकते हैं, (यद्यपि अब गाँव भी तकनीकी से काफी समृध्द हो चुके हैं, बैल गाड़ी के स्थान पर बसें, निजी वाहन, टूटी कच्ची सड़कों के स्थान पर पक्की तारकोल की सड़कें, खपरैल के मकान के स्थान पर पक्के मकान) फिर भी गाँव की प्राचीन झलक इस कहानी में देखने को मिलती है। ननिहाल बच्चे के जीवन का अहम हिस्सा होता है, वहां बिताये पलों की तुलना जीवन के किसी सुख से नहीं की जा सकती। ऐसे में गाँव में ननिहाल हो तो खेतों की मिटटी की सोंधी खुशबू, लहराती फसलें, मोबाईल और टेलिविजन की दुनिया से दूर उन्मुक्त वातावरण में विचरण करना, छप छप कर नहाना, पेड़ों पर चढ़कर आम अमरुद तोड़कर खाना, इतना ही नहीं घर के पालतू जानवरों से भी वहां आत्मीय सम्बन्ध होता था, शहरों में जहाँ इन्सान इन्सान की भाषा नहीं समझ पा रहा वहां जानवर इन्सान की और इन्सान जानवरों की भाषा बखूबी समझते हैं।खुले में चारपाई पर जो नींद आती है उसकी तुलना बंद ए.सी. के कमरों से भला कहाँ। किन्तु इसी गाँव में जब इंसानी स्वार्थ अपना डेरा डाल देता है तो परिवार का बिखराब बाल मन को बहुत सालता है। विधवा नानी-मामी का विवाद, परिवार की अंतर्कलह को उजागर करता है। नानी का घर से रूठकर अपने ही रिश्ते के देवर के यहाँ बैठ जाना (यद्यपि बच्चा नहीं जानता बैठ जाना से क्या आशय है) उसके लिए तो नानी का दूर जाना उनके प्यार से वंचित हो जाना है। यहाँ नानी का अपने देवर के साथ बैठ जाना एक ओर उस दौर की समाज व्यवस्था को दर्शाता है दूसरी और इस उम्र में नानी का दूसरे पुरुष के साथ रहना बताता है देह से उपर भी सम्बन्ध होते हैं, इन्सान को आत्मिक संबल की चाह सदैव बनी रहती है। स्त्री स्वतंत्रता का उस समय भी समाज विरोधी था आज भी है। नानी के प्रति देवरानी की प्रतिक्रिया, “कितनी उम्र रह गई अब ? इतना निकला तो कुछ साल और निभा लेती।”(पृ १३३) चाची का यह कथन, दर्शाता है नारी स्वयं अपने भीतर की नारी से मुक्त नहीं हो पाई। इन सबसे परे संजू अपनी परी लोक की सफेद फक्क पंखों वाली परी (नानी) को खोज रहा है। नानी-धेपते का परस्पर प्रेम ही है जो उसे घर में नानी की उपस्थिति का आभास करा रही है। इसे विज्ञान ने भी टेलीपेथी का नाम दे स्वीकार किया है।
पारिवारिक पृष्ठभूमि से उठाई एक और प्रासंगिक बल्कि कहूँगी जवलन्त विषयों पर आधारित कहानी है. ‘चिता’। दो पीढ़ियों के बीच कम होता कम्युनिकेशन, संबंधों के बीच तनाव की रस्सी तान देता है। आज यह कहना कि युवा वर्ग ही दोषी है एक तरफा आक्षेप होगा। अपनी निजी जीवन शैली के आदी बुजुर्ग वर्ग भी अपने जीवन में खलल पसंद नहीं करते। सबकी अपनी-अपनी अभिलाषा है जबकि एक छत में रहने के लिए आपसी तालमेल तो प्रथम शर्त है। चिंता एक बेटे की अपने पिता को लेकर है। आशुतोष जी स्वयं को बेटे के परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाते, कारण दो हैं एक तो वे सदैव अपने नियमों के अनुसार जिए हैं दूसरा बड़ा कारण है बेटे द्वारा अंतरजातीय विवाह, विधर्मी बहू की फांस उनके हृदय में अभी भी अटकी हुई है। उस पर अर्धांगिनी का बीच सफर में साथ छोड़ जाना उन्हें बेटे की शरण में जाने को विवश तो कर देता है मगर परिवार में रहकर भी स्वयं को तनहा, समेटे रखने वाले आशुतोष जी का व्यवहार बेटे के जीवन में व्यवधान उत्पन्न कर देता है। वह अव्यक्त कुंठा से घिरा रहता है। वह सफल उद्यमी आसानी से हो सकता है अपने कर्मचारियों के बीच तालमेल में कोई दिक्कत नहीं किन्तु घर और रिश्ते में ....वह भरसक प्रयास करता है, इस रिश्ते के तार आने वाली पीढ़ियों से जोड़े रखने किन्तु “जिन्दगी के सवालों के जवाब भौतिकी और गणित की तरह आसन क्यों नहीं होते?” (पृ १०३ )बड़ा सवाल लेखक ने इन पंक्तियों में उठाया है गणित और भौतिकी के तो पूर्व निर्धारित फार्मूले होते हैं जिनके माध्यम से उन्हें हल किया जा सकता है किन्तु जिन्दगी में हर पल नये सवाल उठते है जिनके फार्मूले हमें स्वयं निर्मित करने होते हैं यही कारण है जो इस फार्मूले को इजाद कर लेता है उसके लिए जिन्दगी जन्नत बन जाती है जो नहीं कर पाते उनके लिए जहन्नुम। अंततः बेटा इस फार्मूले को इजाद कर ही लेता है। मैं समझती हूँ इस सूत्र में लेखक ने जीवन का जो सन्देश दिया है उस पर यदि सच्चे मन से निबाह किया जाय तो कई परिवारों के बीच का बिखराव समाप्त हो सकता है। “बेटा बड़ा हो जाय जब, कमाने लगे और पिता रिटायर हो जाय तो भूमिकाएं बदल लेनी चाहिए। बूढ़े पिता को बेटा बन जाना चाहिए, बेटे को पिता, तब नेहा आपके लिए बहू नहीं रह जाएगी।”(पृ १०६) परिवार हो या समाज आज सारी जद्दोजहद अपनी भूमिकाओं पर अड़े रहने की है। लेखक को इस फार्मूले पर बहुत -बहुत साधुवाद देती हूँ। कम से कम मैं तो जीवन में इसे धारण कर चुकी हूँ।
‘प्रवासन’ व्यवस्था का भ्रष्टाचार से टकराव, केवल जनता या समाज ही इसके शिकार नहीं वरन सुरक्षा विभाग भी रसूखदारों के दबाव को सहते हैं। प्रतिबंधित स्थान पर एक उच्च अधिकारी की बेटी का पार्टी करना, वहीँ सुरक्षा विभाग द्वारा रोकने पर अभद्रता से पेश आना (यह विडम्बना है की कानून के रहनुमाओं की नाक के नीचे ही कानून की बखिया उधेडी जा रही है)सुरक्षा कर्मी को आहत कर जाता है। उसके अपने ईमानदार होने पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। भूखे पेट दिन रात खड़े रहकर वे अपना धर्म निभा रहे हैं किन्तु परिणाम में उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार। उसमें बदले की भावना जाग्रत होना स्वाभाविक है आखिर वह भी इन्सान है। “मैगी नहीं एक बटर चिकन, दो नान, एक फुल प्लेट ग्रीन सलाद, अंदर की व्ही.आई.पी. लाउंज में आर्डर कर दीजिये, आज के बाद हम खाना वहीँ खायेंगे भारत सरकार के खर्चे पर।” यह महज उस कर्मचारी की विडम्बना नहीं है देश के ऐसे कई नागरिक हैं जो स्वयं को संकट में डालकर राष्ट्र भक्ति में समर्पित हैं किन्तु जब देखते हैं उन्हें बदले में सिर्फ तिरस्कार ...और जो खुले आम देश को लूट रहे हैं घोटाले कर रहे हैं उन्हें पूजा जा रहा है तो आहत मन बगावत कर उठता है। कहानी प्रवासन एक कटाक्ष है ऐसे वर्ग पर अफ़सोस समाज में ऐसे वर्गों की बहुतायत है।
‘वीडियो‘ कहानी पढ़कर पंच परमेशवर याद आई। दो मित्रों के बीच जब हरीश के भाई के फेल होने पर आरोपी अजय के पिता साबित होते हैं। दोनों मित्रों की दोस्ती को ग्रहण लग जाता है। वहीँ अजय का वीडियो गायब होने पर हरीश की बस्ती वालों पर आरोप लगता देख हरीश स्वयं तफ्तीश में जुट जाता है और इल्जाम सही साबित होने पर अजय को उसका वीडियो दिलाने में मदद भी करता है। दो बच्चों द्वारा समाज के वर्गवाद का सन्देश देती सुंदर कहानी। वीडियो को केंद्र में रखकर बुनी कथा हरीश और अजय दो बच्चों के माध्यम से समाज के दो वर्गों के बीच की दीवार को अभिभावकों द्वारा बनने और बच्चों द्वारा ढहने की मर्मस्पर्शी कहानी है। निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे के जीवन में सदैव अभाव भी हैं, पिता का कठोर अनुशासन भी। दूसरी और सुविधाएँ, पिता का अपार स्नेह व लचीला अनुशासन भी। ऐसे में बाल बुध्दि वीडियो न देखने देने पर सुविधाओं के आधार पर पिता की तुलना कर बैठती है, वस्तुतः यह आज का यथार्थ है। “तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं अजय , काश! मेरे पापा भी ऐसे होते।”(पृ १४७) वहीँ बालमन की सहजता देखिये, ”एकदिन जब हम बड़े हो जायेंगे, इस टंकी पर बैठकर हमारे पैर लटका नहीं करेंगे...वे जमीन को छूकर ठहर जायेंगे।” काश! हमारी आज की वो समस्त पीढ़ी जो अपने अस्तित्व की तलाश में निकली और अपनी ही जमीं को भूलकर भटक गई है उनमें में यह जज्बात पैदा हो जाएँ। ”(पृ.१५५ ) समाज में जो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्गवाद की अमरबेल चली आ रही है उससे मुक्ति का दर्द है लेखक की इन पंक्तियों में। “झाड़ू लगाने के कारण, प्रांगण में उठा धूल का बवंडर एक बार फिर उठा और प्रांगण में लगे पौधों की स्वस्छ पत्तियों पर पसर गया।” (पृ.१५५ )
‘मुक्ति’ मर्म को भेदती गहन चिंतन को लेकर रची गई कहानी है, जो अलग दृष्टिकोणों से मुक्ति का प्रयास है। एक ओर परिवारों में विरासतों को लेकर हुए संघर्ष है, दूसरी और वृध्दों की उपेक्षा, देश में बढ़ते वृध्दाश्रम। किन्तु कहानी इन दोनों समस्याओं के लेकर चलने के बावजूद एक अलग कलेवर रचती है जिसमें एक इन्सान की अपने अतीत के कर्मों से मुक्ति की तडप है तो दूसरे इन्सान द्वारा उसे मुक्त न होने देने की जद्दोजहद। यह कहानी आदमी को उसके मन की अदालत के कटघरे में खड़े करती है। यही जीवन दर्शन है जिसे लेखक ने लोक – परलोक के कटघरे से निकल कर यथार्थ के धरातल पर ला रखा है। 'दरअसल गीता में कुछ लिखा ही नहीं है। बस एक बैंक का वर्णन है और मुझे उस बैंक में अगाध आस्था है।' (पृ ५९ ) यदि हर व्यक्ति इसमें आस्था रखे तो संसार में सर्वत्र शांति हो जाय। सम्पत्ति के लालच में ताऊ द्वारा अपने पिता को उपर से नीचे तक आरा मशीन में चीर देने की हृदय विदारक घटना के बाद सुयोग की आँखों में क्रोध की ज्वाला भडकना स्वाभाविक है। एक जख्म जो वह लम्बे समय से पाले था। सुयोग का वृध्दाश्रम के प्रति संवेदनशील होना अकारण नहीं। “मन पर एक बोझ है बहुत पुराना है और बहुत भारी भी।” (पृ ५८) वही ताऊ आज सम्पत्ति विहीन, देह से लाचार हो वृध्दाश्रम में अपने उस दुष्कृत्य से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है, सुयोग उनकी सेवा कर उनकी जिन्दगी के दिन बढ़ाने, उन्हें मुक्त न होने देने की। “सब करनी का गणित है जो किया है वह तो भरना ही पड़ेगा।” ( पृ ५६) वहीँ सुयोग का तर्क मानवता की कसौटी पर खरा है, ” इस दुनिया के परे कोई दुनिया नहीं है, बस यही है स्वर्ग नरक।” ( पृ ५६) जीवन में कर्मों के बल मुक्ति का सन्देश देती प्रभावपूर्ण कहानी है।
अबीर जी की सभी कहानियों को पढकर एक बात महसूस की या कि इसे मैं उनकी खूबी कहूँगी। प्रथमतः वे एक बड़ा परिदृश्य सामने रखते हैं उसमें अपने विषय को चिन्हित करते हैं। संग्रह की सभी कहानी मानवता एवं समाज पर प्रश्नचिन्ह उठाती है। भाषा के क्षेत्र में उनका कौशल बेजोड़ है, कथा तत्व के अनुरूप गढ़ी शब्दावली उनकी सिध्द्ता स्पष्ट करती है जो स्वयं में सूत्र वाक्य रच देती हैं। यथा "खुद से जूझना एक ज्वलनशील गैस के रिसाव की तरह था" (पृ १९४ ) “हर पेड़ को अपनी जड़ें खुद मजबूत करनी होती है, जीवन के तूफान से जूझने के लिए।” “गर्माहट रिश्तों में थी पुआल की आंच में नहीं।” “सेक्टर कोई भी हो तीन नुस्खे हर जगह काम आते हैं, मिलाना, पिलाना, सुलाना।”कहानी के समस्त कथानक जीवन से जुड़े तथा यथार्थ के बेहद करीब हैं जिससे हर इंसान गुजर रहा है। इससे कहानियां पाठक को बांधे रखने में सफल रही है। कथा आरम्भ होते ही पाठक उसमें खो जाता है उसे पात्र का दुःख अपना दुःख लगने लगता है उससे मुक्ति की छटपटाहट में वह लेखक की ऊँगली थामे शब्दों की वीथियों में यात्रा पर निकल पड़ता है। इसका प्रमुख कारण है लेखक ने समस्या हकीकत की दुनिया से उठाई है तो पात्र भी सजीव बन पड़े हैं। यह संग्रह मेरी दृष्टि में प्रेमचंद के समस्यामूलक संग्रह की तरह ही है जिसमें लेखक ने गहन विषयों पर अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है।लेखक समाज का वह संवेदनशील प्राणी है जो अव्यवस्था और विसंगतियों के बिरुध्द सदैव चिंतनशील रहता है। जब यह चिन्तन, तनाव मानस को उद्वेलित करने लगता है तो वह उसे कागज पर उतर हल्का हो लेता है। इसलिए लेखक सिर्री होने से बच जाता है। किन्तु आम इन्सान इस तनाव को कभी स्वयं पर, परिवार तो कभी समाज पर निकालता है। फिर चाहे वह आशीष, हरीश, सुयोग, अनोखे, मैत्रयी, संजू, मानस, आशुतोष जी, सुरेन्द्र, नेहा, झम्मन या फिर लौकिक समाज का कोई भी पात्र हो सिजोफ्रेनिया का शिकार होगा ही। अत: शीर्षक की कसौटी पर पूर्णत: खरा उतरता यह संग्रह जनमानस को चिन्तन हेतु बाध्य करेगा |ऐसे चिन्तन प्रधान कहानी संग्रह हेतु अबीर आनन्द जी को अनेकानेक शुभकामना प्रेषित करती हूँ तथा साहित्य में उनका लेखन उतरोत्तर समृध्दि प्राप्त करे एसी मंगलकामना करती हूँ।
Published on July 08, 2017 00:59
July 2, 2017
दुर्दिनों की बारिश में रंग: कविता संग्रह / मणि मोहन मेहता
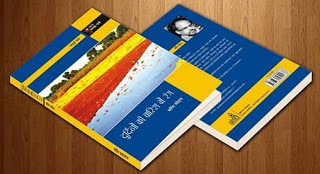 "अपने छोटे संसार में जहाँ यह सब पाषाणकालीन मौलिकता में जीवित है, वहाँ से इन कविताओं का फूटना..."
"अपने छोटे संसार में जहाँ यह सब पाषाणकालीन मौलिकता में जीवित है, वहाँ से इन कविताओं का फूटना..."
ज़िन्दगी को सजीव कर देती हैं कविताएँ। जिस ‘कम्फर्ट जोन’ में आदमी ने अपना नया जीवन तलाश लिया है और जिसे अपना पूरा संसार मान लिया है, उसे एक झटके में निरर्थक कर देती हैं। इस नए कम्फर्ट जोन पीले पत्ते गिरकर मिटटी के रंग के नहीं होते, किचन की स्लैब से बर्तन गिरने की आवाजें नहीं होतीं और होती भी हैं तो किताब में मग्न आदमी के ज़हन में बर्तन के नाम का अनुमान तो हरगिज़ नहीं होता; इस कम्फर्ट जोन में घरों की छतों पर अपने नीड़ों में वापसी करते परिंदों की परछाइयाँ नहीं गिरतीं। इस कम्फर्ट जोन के घरों पर तो छतें तक नहीं होतीं।
ये कविताएँ उस दिनचर्या से उपजी हैं जिसने हर पिघलते दिन के साथ इनके जीवंत एहसास को जिया है; घर लौटते हुए अपनी पत्नी के लिए वेणी और बेटी के लिए आइसक्रीम खरीदी है। अगर कवि उन तथाकथित ‘मशरूफ’ शहरों में रहता और यही विषय रहे होते तो अनुमान लगाना सहज है कि इन कविताओं का शून्य और गहरा होता, रंग और चटख होते, व्याकुलता और मार्मिक होती। इन ‘मशरूफ’ शहरों में रहने वाले लोग शाम को घरों की ओर चलते ज़रूर हैं पर कितने लौट पाते हैं पता नहीं।
अपने छोटे संसार में जहाँ यह सब पाषाणकालीन मौलिकता में जीवित है, वहाँ से इन कविताओं का फूटना कवि की मौलिकता और उसकी गहरी जड़ों का, उसके कुलबुलाते मन मस्तिष्क का, प्रश्न उठाने के साहस का, बूँद भर पानी से तृप्त हो जाने के संतोष का, लुप्तप्राय हो चले आम आदमी के खुद में मग्न रहने के पागलपन का, मिट्टी के आशीर्वाद का, परिवार को प्रसन्नता देने की उपलब्धियों का, चीटियों और गिलहरियों के साथ सुख-दुःख बाँटने के सौभाग्य का, किताबों की जिरह में हार जाने के मर्म का, शब्दों को कैद रखने के प्रायश्चित का और फिर उन्हें स्वतंत्र कर देने के उल्लास का.....गहन परिचायक है।
पन्ने करीब-करीब सब पलटे जा चुके हैं। शब्दों के मायने साथ-साथ ज़हन में तैरने लगे हैं, अंत में पाया कि एक भी शब्द कठिन नहीं था, न नया था कि गूगल से व्याख्या मांगने की ज़रुरत पड़े। इन साधारण से शब्दों के ज़रिये एक साधारण सी लगने वाली यात्रा में कुछ असाधारण पड़ाव हैं। एक कविता कभी अर्धविराम की तरह ख़त्म होती है और कहती है ‘तुम खुद सोचो’। कुछ पूर्ण विराम हैं जो कहते हैं ‘ये साधारण किन्तु स्थापित तर्क है, सोचना समय की बर्बादी है’। इन्हीं साधारण से शब्दों और उनमें बिंधी हुई भाषा को बचाने की और इस भाषा से उपजी कविता को अमृत्व देने की जिजीविषा एक सतत परछाईं की तरह हर पूर्णविराम में दिखाई देती है। वह फिर चाहे ‘डंपिंग ग्राउंड’ से ‘किसी तानाशाह की जी हुजूरी अभिनन्दन के बाद ज़हन में बची रह गयी भाषा’ हो, ‘इंतज़ार’ में ‘किसी दिन डाल दूँगा एक कटोरी आटे के साथ अपनी थोड़ी सी भाषा भी’, ‘कविता’ में बहते हुए पसीने और लुढ़कते हुए आंसुओं के साथ ‘कभी-कभी ऐसे ही आ जाती है कविता की भाषा भी होठों तक’, ‘अब और नहीं’ में ‘आपको पता नहीं इस वक़्त किस कदर बेचैन है कविता मेरे करीब आने के लिए’, ‘शरणार्थी शिविर’ में ‘अपने सिर पर बचे-खुचे अर्थ की गठरी उठाए कुछ शब्द आए’, ‘शायद’ के अलग मायने उभर कर आते हैं जब कवि कहता है ‘भाषा के आसमान का यह टूटा हुआ सितारा है....’ और ‘दुनिया की तमाम भाषाओं के अन्धकार में मौजूद है यह शब्द जुगनू की तरह बुझता-चमकता’, और अंत में ओ हेनरी की ‘लास्ट लीफ’ के गहरे हरे रंग के पत्ते में जड़ दिया भाषा का यह नगीना ‘यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फवारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है आइवि की लता से गहरे हरे रंग का पत्ता बनकर’, ‘घर’ में ‘अब बस घर चाहिए उन्हें, माँ चाहिए, हवा में उछलती गेंद की तरह, जानी पहचानी भाषा चाहिए’।
इन कविताओं में रिश्ते हैं... ‘एक दिन’ में ‘अपनी नम आँखों से मेरी तरफ देखते हुए तुम जिद करोगी वहाँ चलने की और मैं कहूँगा-उड़ सकोगी इतने प्रकाश वर्ष दूर’, ‘कन्फैशन’ में ‘छतरी की तरह बनी रही सिर पर दुर्दिनों की बारिश में बीसियों बार’, ‘पिता के लिए’ में ‘कहाँ दे पाया इतना प्यार बच्चों को जितना मिला मुझे अपने पिता से’, कई बार यह मन में गुजरा कि मैं पिता की तरह कैसा हूँ, कम से कम अपने पिता की तुलना में। ‘बाप बनकर तेरे करीने से लेटता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ, मैं बेटा बुरा था या बाप बुरा हूँ’। अच्छा है कि यह सवाल उठता है...उठता रहे। ‘बेटी’ में भी मुझे अपनी एक कविता का अक्स गहराई से नज़र आता है जब कवि कहता है ‘ज़रा सी आहट पर भागती है बेटी घर का दरवाजा खोलने के लिए’। एक निजी अनुभव से जन्मी उस कविता की अनुगूंज यहाँ भी सुनाई देती है ‘और यह कमबख्त दरवाजा भी अपने आप नहीं खुलेगा’। मेरी पत्नी की पहली प्रेगनेंसी थी जो हमें टर्मिनेट करानी पड़ी क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं थी। हम लोग बेटी की उम्मीद कर रहे थे। तब लिखी थी यह कविता ‘तू मेरे घर जरूर आई होगी, मैंने ही दरवाजा न खोला होगा। थक जाता हूँ, दफ्तर से आकर सो गया हूँगा और तेरी माँ भी दिन भर की थकी अलसाई होगी... तू मेरे घर जरूर आई होगी।’
प्रकृति है....‘रूपांतरण’ में ‘कितनी ख़ामोशी के साथ हो रहा है प्रकृति में रंगों का यह रूपांतरण’, ‘फूल’ में भी प्रकृति और दर्शन का प्रभावी संगम देखने को मिलता है ‘दिन निकलते ही आ बैठती है धूप, तितली, भंवरे, मधुमक्खी, दिन भर लगा रहता है किसी न किसी का आना-जाना..फूलों को पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है दिन और करीब आ जाती है शाम....जिसकी बाहों में उसे टूटकर बिखरना है’। पशु हैं... जो प्रकृति और कवि में एकाकार हो गए हैं। ‘अपना हिस्सा’ में ‘मुझे सिर्फ बादल के कुछ पहाड़, शेर, भालू, हाथी, बादल के कुछ टुकड़े दे दो’, ‘अफ़सोस’ में तोते, बिल्ली और कुत्ते के माध्यम से मनुष्य के दुर्व्यवहार को रेखांकित किया है जो सराहनीय है। ‘बिल्ली’ में मनुष्य की बुद्धिमत्ता को धराशाई कर देने वाला चित्रण है जो कवि की डिग्रियों के वर्णन से प्रभावी बन गया है. ‘और एक हम हैं ढपोर शंख, एम ए, एम फिल, पी एच डी’। करीब दस पंद्रह साल तो ज़रोर्र गुजर गए होंगे ‘ढपोर शंख’ को पढ़े या इस्तेमाल किए हुए। इस शब्द को पुनर्जीवित करने के लिए आभार।
दर्शन है...‘अलाव’ में ‘उसे रुकने के लिए पुकारती ही रह गई अलाव की आग’, ‘मिटटी’ में ‘मिटटी से ज्यादा अनमोल कुछ भी नहीं है इस संसार में’, ‘दुःख’ में फलसफा है ‘अब इतनी सी बात पर क्या उठा कर फेंक दें अन्न से भरी थाली, क्या इतनी सी बात पर देने लगें ज़िन्दगी को गाली’।
इन सब के अतिरिक्त ‘प्रेम गीत’ और ‘एकालाप’ में छोटी पर बेहद आकर्षक पंक्तियाँ हैं। संग्रह के अंत में ये वैसे ही पेश आती हैं जैसे छप्पन भोग खाने के बाद स्वादिष्ट मुखवास।
एक परिपूर्ण कविता संग्रह है जो न्यौता सा देता है कि यदि जीवन में सामंजस्य बनाए रखना है तो कौन से अवयवों की कितनी मात्र होनी चाहिए। जमीन से जुड़े हुए लोगों के जीवंत सन्देश हैं जो आशा है कि ‘मशरूफ’ लोगों के ज़हनों में पहुँचें। कुछ विचार फिसल गए हैं लिखते-लिखते। कभी याद आए तो मना कर भेज दूँगा। मणि भाई को हार्दिक बधाईयाँ। फेसबुक पर उनकी कविताओं और उनके अनुवादों से रू-ब-रू होते रहते हैं। बहुत कुछ सीखने और मनन करने को मिलता है। प्रार्थना है कि ये सफ़र इसी तन्मयता से जारी रहे। मधुमक्खियों, गिलहरियों, चींटियों और बेटियों को जीवन मिलता रहे, पुनर्चक्रण होता रहे। वरना आदमी को खुद कहाँ पता है कि वह क्या कमाने निकला था।
Published on July 02, 2017 01:20
July 1, 2017
बीज

धतूरे का बीज देखा है?
सफेद रेशमी पंखों पर सवार, धतूरे कीमासूम महत्त्वाकांक्षाओं का उड़नखटोला।दूसरे स्वादिष्ट फलों की तरह, धतूरे का बीज कोई नहीं रोपता। नीम हवाओं के इशारे तय करते हैं, कि बस्ती का अगला पड़ाव कहाँ होगा।
स्कूल के बाहर,उस अंग्रेजों के जमाने के अस्तबल के अवशेषों के पास, धतूरे की एक भरी पूरी बस्ती थी। और जब गर्मियों का मौसम आता था, तो सूखे फलों से फूटकर निकलते बीज, उक़ाबों की तरह मँडराते नज़र आते थे। कुछ के पंख उतर जाते थे बदन से, कभी थाने की दीवार से टकरा कर,तो कभी तेज हवा की शरारतों से।
खुशनसीब होते थे वह बीज, जिनके पंख जल्दी उतर जाते थे। उम्र भर उसी बस्ती में रहते थे,
अपनों के साथ।
Published on July 01, 2017 23:10



