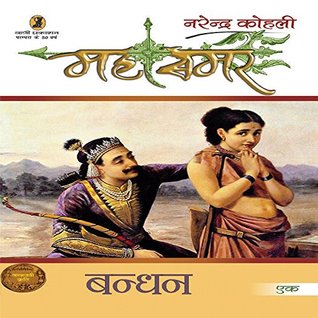More on this book
Kindle Notes & Highlights
और तभी से देवव्रत के मन में परिवार, समाज और संसार को ले कर अनेक प्रश्न उठते रहे हैं।...परिवार क्या है? पति-पत्नी का परस्पर आकर्षण एक-दूसरे को सम्मान और स्वतन्त्रता देने में है या अपने सुख के लिए अन्य प्राणी को अपनी इच्छाओं का दास बना लेने में? यदि दूसरे पक्ष के सुख के लिए स्वयं को खपा देना परिवार का आधार है तो दूसरे पक्ष की कामना ही क्यों होती है? स्त्री-पुरुष विवाह क्यों करते हैं–अपनी रिक्ति को भरने के लिए या दूसरे पक्ष के अभावों को दूर करने के लिए, या परस्पर एक-दूसरे का सहारा बन, अपनी-अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए?...वात्सल्य क्या है? व्यक्ति, सन्तान अपने सुख के लिए चाहता है?
...more
आज उन्हें अनुभव हो रहा था कि मनुष्य का सहज मन प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि त्रिकालसत्य आदर्शों पर स्वयं चलने का तो वह साहस ही नहीं करता, अपने प्रियजनों को उन आदर्शों की ओर बढ़ते देख कर भी कोई प्रसन्न नहीं होता...राम, राज्य को त्याग कर वनवास के लिए चले गये थे। तो दशरथ उनके त्याग से प्रफुल्लित नहीं हुए थे।
‘नियति चाहे डूबना हो, किन्तु नीति तो संघर्ष ही है।’
निराशा को जीवन से निकाला जायेगा, तो उससे जो शून्य बनेगा, वह रिक्त नहीं रहेगा–आशा आ कर उसमें डेरा डालेगी। आशा तभी टिकेगी, जब कुछ अर्जन होगा।…पर अर्जन तो कोई उपलब्धि नहीं है।
उसका मन जैसे ठिठक गया…उसके तर्क के पग किस ओर उठ रहे थे?...अर्जन की ओर? भोग की ओर?...पर तर्क रुका नहीं। वह जैसे आज बहुत ही संघर्षशील हो रहा था… अर्जन कोई उपलब्धि नहीं है, पर विसर्जन ही क्या उपलब्धि है? रिक्ति को भरना तो उपलब्धि हो सकती है; किन्तु पूर्ति को रिक्ति में परिवर्तित करना क्या उपलब्धि हुई…और रिक्ति से रिक्त तक जीना भी क्या जीवन हुआ…
राजमाता ने समझाया कि अम्बिका अभी युवती है, उसके सम्मुख एक लम्बा जीवन है, जीने के लिए। कोई तो व्याज उसे चाहिए जीने का–कोई कर्म, कोई गति-विधि, कोई आशा-अपेक्षा, कोई आस्था…कोई तो केन्द्र उसे चाहिए, जिसके चारों ओर वह कोल्हू के बैल के समान चक्कर लगा कर जीवन का समय पूरा कर सके; कुछ तो ऐसा हो, जिसके आस-पास, अपनी भीतरी ऊर्जा का जाला बुन कर, वह उसमें मकड़े के समान लटक सके।…
उसे लगता था कि उसके अपने भीतर एक बहुत बड़ी गुफा थी–काली और अँधेरी! उसका मन उसी गुफा में भटक रहा था।...उसका हरण... विचित्रवीर्य के साथ विवाह...अम्बा
“किसी को सन्तान की इच्छा होती ही क्यों है–मैं तो यह ही समझ नहीं पाती राजमाता।” अम्बिका धीरे-से बोली, “गर्भ में सन्तान का पोषण, प्रसव, फिर उसका पालन-पोषण, उसकी शिक्षा-दीक्षा...और फिर प्रत्येक क्षण उसके किसी अनिष्ट की आशंका...” उसने सत्यवती को देखा, “क्यों चाहते हैं लोग सन्तान? क्या सुख है उसका?”
“कोई बीज क्यों रोपता है? पौधा क्यों उगता है? हिम-आतप से उसकी रक्षा क्यों करता है? क्या सुख है पौधे से?” उसने अम्बिका को देखा, “उस पर अपना समय और श्रम ही नहीं; धन भी लगाना पड़ता है।
“मैं भी यही सोचती हूँ,” अम्बिका बोली, “क्यों रोपते हैं लोग पौधे? शायद उनका समय नहीं कटता।”
“मुझे विश्वास नहीं होता पुत्र!” सत्यवती बोली, “ऐसा त्याग क्या मानव के लिए संभव है।?” “विवेकी व्यक्तियों के लिए, अपने सुख के निमित्त कोई भी त्याग साधारण बात है।” “तुम अत्यन्त बुद्धिमान हो पुत्र! तुम्हारी बात में मुझे संदेह नहीं करना चाहिए।” सत्यवती बोली, “किन्तु मेरा मन आज भी यही कहता है कि ग्रहण का नाम सुख है; त्याग का दुख। अर्जन से लोग सुखी होते हैं, विसर्जन से दुखी।...राज्य-त्याग से भीष्म को दुखी होना ही चाहिए था।”
“तो लोग धन, सत्ता और शक्ति क्यों चाहते हैं पुत्र?”
“वह एक मद है, जो रक्त को उफ़नाता है। उससे उत्तेजना का अनुभव होता है। वह सुख नहीं है। सुख का भ्रम उससे अवश्य उत्पन्न होता है। उत्तेजना अपने-आप में कष्ट है। उसके अवसान की आशंका भय है।...और उसका अवसान पीड़ा है।”
“बद्धजीव कभी सुखी नहीं हो सकता माँ!” व्यास बोले, “जब तक तुम अपने बन्धनों को पहचानोगी नहीं, उन्हें अपने दुखों का कारण नहीं मानोगी, उन्हें तोड़ने का संकल्प नहीं करोगी...तब तक भीष्म तुम्हें अपने शत्रु दिखायी पड़ेंगे।...और तुम सुखी नहीं हो सकोगी माँ!”
अम्बालिका, राजमाता को देखती थी और चकित हो कर सोचती थी कि सत्यवती एक ही समय में इतनी समर्थ, अधिकारयुक्त, नियन्ता; और दूसरी ओर दीन, असहाय और आर्त्त कैसे हो जाती है। जो इस प्रकार क्रुद्ध हो कर सबसे लड़ सकती है, वह इस प्रकार अनाथ के समान रोती क्यों है।...और कितनी क्रूर है राजमाता: जैसे वाणी का कोई संयम ही नहीं है।
मनुष्य जब तक भ्रम में रहता है, सुखी रहता है। समझ कर तो फिर दुख-ही-दुख है।”
सुख’ और ‘भोग’ दो अलग स्थितियाँ हैं माँ!” द्वैपायन बोले, “‘सुख’ एक मानसिक स्थिति है, जो भोग के अभाव में भी सम्भव है। या शायद अधिक सत्य यही है कि सुख, भोग के अभाव में ही सम्भव है। और भोग तो दुख का प्रवेश-द्वार है माँ! भोग ने कभी किसी को सुखी नहीं किया।”
जो बहुत वेग से भागता है, वह बहुत शीघ्र थक जाता है माँ!”
द्वैपायन ने कहा था, उनकी दृष्टि में सारे जीव समान हैं। प्रकृति ने सबको समान अधिकार दिये हैं। सब अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करते हैं, और सब अपनी-अपनी क्षमताओं
“मुझे मालूम नहीं माँ!” विदुर बोला, “कि धृतराष्ट्र का हित किसमें है: उसे उसकी वीरता और शस्त्र-परिचालन की पारंगतता का झूठा विश्वास दिलाने में या स्पष्ट शुद्ध सत्य उसके सम्मुख रख देने में। दम्भ भरा असत्य जीवन जीने से अच्छा है कि व्यक्ति स्वच्छ और सत्य जीवन व्यतीत करे, चाहे वह असुविधापूर्ण ही क्यों न हो।”
तृष्णा, अधिकार-लालसा, प्रतिस्पर्धा–यह सब मानवता का शृंगार नहीं है माँ! इनसे किसी का न उद्धार होता है, न उत्थान! इनसे पतन ही होता है।”
“आदर न धन से मिलता है, न ज्ञान से, न यश से, न कुल से–आदर केवल आचरण से मिलता है देवि! इसलिए मेरा सबसे अधिक बल आचरण की शुद्धता पर है। आचरण शुद्ध रहे तो अनादर का कोई भय नहीं है।”
क्या पाण्डु के लिए यह सम्भव होगा? क्या वह कभी भूल पायेगा कि वह हस्तिनापुर का सम्राट है?...कुलपति ने कल उसे यही समझाया था कि जिसे वह त्याग समझ रहा था, वस्तुतः वह अधिक ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त करने की इच्छा मात्र थी।...वैसे भी जब वह साधारण बनने का प्रयत्न करता था, तो एक प्रकार का अहंकार उसके भीतर स्फीत होने लगता था कि देखो मैं कितना महान हूँ कि असाधारण हो कर भी साधारण बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वह अपने अहंकार को विगलित करने का प्रयत्न करता तो वह और भी स्फीत होता चला जाता।...और पाण्डु को लगता कि वह कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं हो पायेगा। कुन्ती ही थी, जो सहज भाव से सबकी सेवा कर लेती थी, सबको
...more
उसे इस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए, कि उसके लिए श्रेयस्कर क्या है! उसे तो अपना सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए।...और अपना सत्य स्वीकार करने का अर्थ अपनी सीमाओं को स्वीकार करना ही है।...उसकी सीमा है कि वह कामेच्छा को त्याग नहीं सकता। राज-वैभव को छोड़ना नहीं चाहता। लाख तपस्वी जीवन व्यतीत करे, किन्तु वह तपस्या, जीवन के भोग के लिए है, उसके त्याग के लिए नहीं...
“आकांक्षा ही सही! क्या दोष है आकांक्षाओं में? आकांक्षा, पाप है क्या?” “नहीं माँ! आकांक्षा पाप नहीं हैः आकांक्षा दुख और सुख का संगम है, अशान्ति का पर्याय है।” व्यास का स्वर गम्भीर था, “आकांक्षा और शान्ति” दोनों की कामना एक साथ नहीं की जा सकती। प्रकृति के नियम इसकी अनुमति नहीं देते।” “तो क्या व्यक्ति आकांक्षा न करे?” “करे। किन्तु तब न सुख से डरे, न दुख से। शान्ति की कामना न करे। शान्ति न सुख में है, न दुख में। शान्ति तो इन दोनों से निरपेक्ष होने में है।”