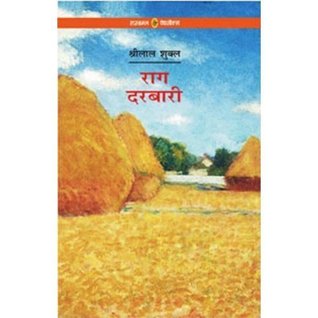More on this book
Community
Kindle Notes & Highlights
मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आरामकुर्सी बन गया था।
जिन रोमाण्टिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती है, उन्हें कुछ दिन रोके रखने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था।
वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की–सी थी, पर उनका रोब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते घोड़े का–सा जान पड़ता था।
इस देश में जाति–प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी–सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता। वह अपने–आप ख़त्म हो जाती है।
हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफ़रत करते थे और राजनीतिज्ञों का मज़ाक उड़ाते थे।
इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है और जाति–प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फ़रेब नहीं हैं तो रोमाण्टिक कार्रवाइयाँ हैं।
दरख़्वास्त बेचारी तो चींटी की जान–जैसी है। उसे लेने के लिए कोई बड़ी ताकत न चाहिए।
सज़ा भुगतकर आने के बाद उन्हें पता चला कि शहीद होने के लिए उन्हें अफ़ीम का क़ानून नहीं, नमक-क़ानून तोड़ना चाहिए था।
जिसे अपने को बम्बई में ‘सँडीलवी’ कहते हुए शरम नहीं आती, वही कुरता–पायजामा पहनकर और मुँह में चार पान और चार लिटर थूक भरकर न्यूयार्क के फुटपाथों पर अपने देश की सभ्यता का झण्डा खड़ा कर सकता है।
किसी भी सामान्य मूर्ख की तरह उसने एम.ए. करने के बाद तत्काल नौकरी न मिलने के कारण रिसर्च शुरू कर दी थी, पर किसी भी सामान्य बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना और नित्यप्रति पुस्तकालय में बैठना ज़रूरी नहीं है।
नयी पीढ़ी की यह आस्था थी कि पुरानी पीढ़ी जड़ थी, थोड़े से खुश हो जाती थी और अपने और समाज के प्रति ईमानदार न थी, जबकि हम चेतन हैं, किसी भी हालत में खुश नहीं होते हैं और अपने प्रति ईमानदार हैं और समाज के प्रति कुछ नहीं हैं, क्योंकि समाज कुछ नहीं है।
लेक्चर का मज़ा तो तब है जब सुननेवाले भी समझें कि यह बकवास कर रहा है और बोलनेवाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ।
घूम–फिरकर बात यही रहती थी कि भारत एक खेतिहर देश है, तुम खेतिहर हो, तुमको अच्छी खेती करनी चाहिए, अधिक अन्न उपजाना चाहिए। प्रत्येक वक्ता इसी सन्देह में गिरफ़्तार रहता था कि काश्तकार अधिक अन्न नहीं पैदा करना चाहते।
अपने मुहल्ले में देवदास पार्वती से शादी नहीं कर सका और एक समूची पीढ़ी को कई वर्षों तक रोने का मसाला दे गया था।
इसी को ‘ठाँय’ कहते हैं। इसी के साथ निशी और निक्कू फिलासफी की हज़ार मीटरवाली दौड़ पर निकल पड़ते हैं।
यानी इन्सानियत का प्रयोग शिवपालगंज में उसी तरह चुस्ती और चालाकी का लक्षण माना जाता था जिस तरह राजनीति में नैतिकता का।
उस गाँव में कुछ मास्टर भी रहते थे जिनमें एक खन्ना थे जो कि बेवकूफ़ थे; दूसरे मालवीय थे, वह भी बेवकूफ़ थे; तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें मास्टर का नाम गयादीन नहीं जानते थे, पर वे मास्टर भी बेवकूफ़ थे और गयादीन की निराशा इस समय कुछ और गाढ़ी हुई जा रही थी, क्योंकि सात मास्टर एक साथ उनके मकान की ओर आ रहे थे और निश्चय ही वे चोरी के बारे में सहानुभूति दिखाकर एकदम से कॉलिज के बारे में कोई बेवकूफ़ी की बात शुरू करनेवाले थे।
‘चमरही’ गाँव के एक मुहल्ले का नाम था जिसमें चमार रहते थे। चमार एक जाति का नाम है जिसे अछूत माना जाता है। अछूत एक प्रकार के दुपाये का नाम है जिसे लोग संविधान लागू होने से पहले छूते नहीं थे। संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं, बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है, इसलिए शिवपालगंज में भी दूसरे गाँवों की तरह अछूतों के अलग–अलग मुहल्ले थे और उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख मुहल्ला चमरही था जिसे ज़मींदारों ने किसी ज़माने में बड़ी ललक से बसाया था और उस ललक का कारण ज़मींदारों के मन में चर्म–उद्योग
...more
गाँधी, जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे और उनके अस्थि–कलश के साथ ही उनके सिद्धान्तों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया था कि गाँधी की याद में अब सिर्फ़ पक्की इमारतें बनायी जाएँगी
मेले का जोश बुलन्दी पर था और अॉल इण्डिया रेडियो अगर इस पर रनिंग कमेण्ट्री देता तो यह ज़रूर साबित कर देता कि पंचवर्षीय योजनाओं के कारण लोग बहुत खुशहाल हैं और गाते–बजाते, एक–दूसरे पर प्रेम और आनन्द की वर्षा करते वे मेला देखने जा रहे हैं।
फिर वह बौद्ध विहारों को गोपुरम् और गोपुरम् को स्तूप समझने की ग़लती भले ही कर बैठे, नारी-मूर्ति को पुरुष-मूर्ति मानने की भूल नहीं कर सकता।
अदालत के एक पंच उन राजनीतिज्ञों की तरह थे जो यू. एन. ओ. में समस्या से हटकर सिद्धान्त की बात करते हैं और इस तरह वे किसी का विरोध नहीं करते और बदले में कोई उनका विरोध नहीं करता। ‘जनता शान्ति चाहती है’, ‘हमारी सभ्यता की नींव विश्वबन्धुत्व और प्रेम पर पड़नी चाहिए’ आदि–आदि किताबी बातें सुनकर कमीना–से–कमीना देश भी सिर हिलाकर ‘हाँ’ करने से बाज़ नहीं आता और उस राजनीतिज्ञ का यह भ्रम और भी फूल जाता है कि उसने कितनी सच्ची बात कही है।
उनके पास दस गैसबत्तियाँ थीं जो शादियों के मौसम में किराए पर चलती थीं। साथ ही उनके पास दो बन्दूकें थीं, जो डकैतियों के मौसम में किराये पर चलती थीं।
चुनाव जीतने का यह तरीक़ा रामनगर के नाम से पेटेंट हुआ।
इसके बाद इस तरह की कई घटनाएँ हुईं और ब्राह्मण उम्मीदवार को मालूम हो गया कि पुरुष–ब्रह्म का मुख पुरुष–ब्रह्म के पैर से ज़्यादा दूर नहीं है और संक्षेप में जहाँ मुँह चलता हो और जवाब में लात चलती हो, वहाँ मुँह बहुत देर तक नहीं चल पाता।
शराबख़ाने से लगभग सौ गज़ आगे एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक भूत रहता था। भूत काफ़ी पुराना था और आज़ादी मिलने, जम़ींदारी टूटने, गाँव–सभा क़ायम होने, कॉलिज खुलने–जैसी सैकड़ों घटनाओं के बावजूद मरा न था।
इस तरह के मैत्रीपूर्ण समझौते को अंग्रेज़ी में ‘ आफ़िस-कम रेजीडेन्स’ कहा जाता है। हिन्दी में उसे ‘आफ़िस–कम–रेज़ीडेन्स–ज़्यादा’ कहते हैं।
राबिन्सन क्रूसो के बजाय कोई हिन्दुस्तानी किसी एकान्त द्वीप पर अटक गया होता तो फ्राइडे की जगह वह किसी पान बनानेवाले को ही ढूँढ़ निकालता।
पृथ्वी पर स्वर्ग का यह एक ऐसा कोना था जहाँ सारी सचाई निगाह के सामने थी।
गयादीन ने शर्मीले नौजवान से पूछा, ‘‘तुम कौन हो भैया ?’’ इस सवाल का प्रत्येक भारतीय के पास यही एक आसान जवाब है कि वह चट से अपनी जाति का नाम बता दे। उसने कहा, ‘‘मैं अगरवाल हूँ।’’
इस बार उस नौजवान ने, देश के औसत नौजवानों की तरह जो प्रेम अपने साथ पढ़नेवाली लड़कियों से और ब्याह अपने बाप के द्वारा दहेज की सीढ़ी से उतारकर लायी गई लड़की से करता है, कहा, ‘‘मैं कुछ नहीं जानता। पिताजी जैसा हुक्म देंगे, करूँगा।’’
सूअर का–सा लेंड़–न लीपने के काम आय, न जलाने के।
भाषण की असलियत दिए जाने में है, लिये जाने में नहीं।
उसने बेला के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया और कहा कि लड़की पढ़ी–लिखी है तो अच्छा है और नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे उससे मास्टरी नहीं करानी है; और लड़की सुन्दर है तो अच्छा है और नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे उसे कोठे पर नहीं बैठाना है।
भैंस ने इस बार खूँटे से कुछ दूर आकर एक ऐसा राक–एन–रोल दिखाया कि लगा अब भैंस की जगह यहाँ एल्विस प्रिस्ले को बुलाना पड़ेगा।
न ख़ून हो रहा था, न डाका पड़ रहा था, इसलिए पुलिस को जैसे ही याद किया गया, घटना समाप्त होने का इन्तज़ार किये बिना ही वह मौक़े पर आ गई।
वह जानता था कि जब वे बेवकूफ़ बनते हैं तो अपनी इच्छा से बनते हैं। बेवकूफ़ बनना उनके लिए मजबूरी नहीं, शौक की, लगभग ऐय्याशी की बात थी।