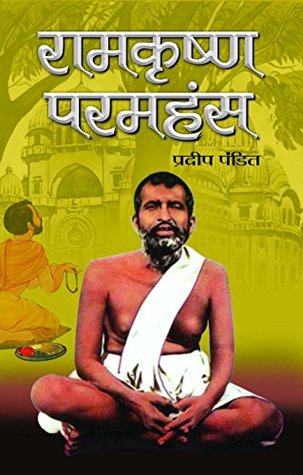More on this book
Kindle Notes & Highlights
‘डूबनेवाले को क्या मिला डूबनेवाले से पूछ! तैरनेवाले को तह की खबर कुछ भी नहीं।’
निग्रह एक के बाद एक होता है—इंद्रियों का भी, वस्तुओं का भी। एक साथ सबकुछ छूटता भी नहीं। छूट जाए तो जीवन चलता नहीं। जीवन आसक्ति के बीच ही साँस लेता है। आसक्ति डोर है। वह टूटी और जीवन खत्म। कम-से-कम तब जब जीवन को ध्यान के साथ जीना न आ जाए। उन्होंने आश्रम प्रबंधकों से कहकर एक कक्ष में ज्यादा-से-ज्यादा विभिन्न रुचियों का भोजन रखवा दिया। दो-तीन दिन रामकृष्ण उस कक्ष में ज्यादा-से-ज्यादा समय रहे, फिर सब कुछ सामान्य हो गया।
अगाध विश्वास, दैहिक प्रतीति, जैसा निश्चित भरोसा धरती के किसी पुजारी को आज तक नहीं हुआ, जैसा गदाधर को हुआ। इसी सबने उन्हें परमहंस बनाया। कोई और होता तो प्रश्न करता—आप कौन? मुझे पढ़ाने में आपकी रुचि क्यों? इत्यादि। कई सवाल हो सकते थे, जो पूछे जा सकते थे, मगर नहीं पूछे गए। कुछ विधायी उत्तर होते हैं, जिनके बाद आज्ञात्मक मुहर तो लगाई जा सकती है, लेकिन प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। रामकृष्ण ने भी यही किया।
मुद्दा यह कि रामकृष्ण को सबसे पहले भैरवी ने ही अवतार कहा; लेकिन वे सदैव इस बात से भिज्ञ नहीं रह पाती थीं कि रामकृष्ण अवतार ही हैं। वैसे भी इस तरह की बातें स्मरण रखना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य की स्मृति जितनी स्मरण के लिए जानी जाती है उतनी ही विस्मरण के लिए भी जानी जाती है। कृष्ण और अर्जुन के सख्य भाव और जबरदस्त मैत्री के बावजूद अर्जुन को सदैव यह बात ध्यान में नहीं रहती थी कि कृष्ण अवतार हैं। भगवद्गीता
मनुष्य के विचार में ईश्वर अत्यंत व्यापक संज्ञा है। इसीलिए ईश्वर को व्यक्त करता इतना ही व्यापक कोई शब्द चाहिए था, और व्यापक शब्द क्या हो सकता था? निश्चित ही वही ऐसा शब्द हो सकता था, जो उच्चारण में गले, मुँह और जिह्वा सभी का एक साथ इस्तेमाल करवा सके। यह ध्वनि आधारित शब्द है। भौतिक-शास्त्र में हुई नई खोजों ने साबित किया है कि ध्वनि का अपना प्रभाव है। संस्कृत में ध्वनि के ऐसे अनेक प्रयोग हैं, जिनसे शब्द का अर्थ के अनुवाद के अलावा भी इस्तेमाल है। इसमें ॐ भी एक है ‘अ’ ‘उ’ ‘म’ लगभग यह ध्वनि ‘ॐ’ के उच्चारण में प्रयुक्त होती है।
एक समय एक सूफी संत दक्षिणेश्वर आए। उनका नाम गोविंद राय था। उनकी सरलता, साधुता और सहिष्णु प्रवृत्ति ने रामकृष्ण को प्रभावित किया। वे उनसे दीक्षित भी हुए। बाजाप्ता उन्होंने उनसे भी साधना करना सीखा। इस बीच रामकृष्ण अल्लाह के मंत्र का जप करने लगे। इतना ही नहीं, दिन में पाँच बार नमाज भी अदा की। रामकृष्ण की इस साधना के समय उन्होंने मंदिरों में जाना बंद कर दिया था। इसलिए ऐसे में हिंदू पद्धति में साधना का तो सवाल ही नहीं उठता था। कहते हैं, तीन दिन तक लगातार उनकी साधना से प्रसन्न होकर उन्हें पैगंबर हजरत मोहम्मद के दर्शन हुए।
ऐसी ही एक घटना का जिक्र ईसा मसीह के दर्शन का भी आता है। सूफी
जैसे एक आदमी लैंप की रोशनी में भगवद्गीता पढ़ता है और दूसरा उसी रोशनी में चोरी करता है, लेकिन लैंप घटना से अप्रभावित रहता है। ऐसा ही ब्राह्मण होता है।
‘रामकृष्ण का धर्म क्या है? वैसे तो वह पारंपरिक हिंदूवाद है, मगर थोड़ा भिन्न तरह का हिंदूवाद। इसलिए भी कि रामकृष्ण किसी एक हिंदू देवता या देवी की उपासना नहीं करते। वे न तो शैव हैं, न शाक्त, न वैष्णव, न वेदांती—फिर भी वे सभी हैं, एक साथ। वे शिव की पूजा भी करते हैं और काली की भी, राम की भी और कृष्ण की भी, फिर भी वे वेदांत दर्शन के हक में रहते हैं। इस सबके बावजूद वे निराकार, अनंत और नित्य ईश्वर को मानते हैं, जिसे वे अखंड सच्चिदानंद कहते हैं।’
वर्ष १८७९ में ब्राह्मसमाज की पत्रिकाओं में रामकृष्ण पर कई लेख छपे। इससे उनके भविष्य के शिष्य तेजी से उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर खिंचने लगे। इतना ही नहीं, मध्यम वर्गीय बंगाली समाज भी रामकृष्ण की ओर मुड़ गया। इनमें सभी तरह के लोग थे।
रामकृष्ण वास्तव में धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाने की कोशिश में लगे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वधर्म समभाव का मंत्र भी हर धर्म से रखा। अंतरंग पार्षद तो बाद में जुड़े। इससे पहले ही शंभु मलिक, कृष्ण किशोर, गौरी पंडित, पद्म लोचन आदि ने रामकृष्ण के दर्शन कर उन्हें अवतार कहकर घोषणा की थी।
ही जन-सेवा करनी है। रामकृष्ण से भेंट ने उन्हें बुरी तरह हिला दिया था। वे बार-बार अपने को समझाते कि रामकृष्ण पागल हैं, झक्की हैं। फिर भी उनके मन के किसी कोने से पे्ररणा उठती कि उनका अनुगमन किया जाना चाहिए। तत्काल ही मन का कोई दूसरा कोना सजग हो उठता और कहता—यह कैसे संभव है? कैसे आप किसी पागल व्यक्ति का अनुगमन कर सकते हैं? फिर खुद ही उत्तर देने लगते—कौन पागल नहीं है! विचार अपने में ही बड़ी दीर्घ और गंतव्य-प्रेरित यात्रा है, फिर विचार पार की यात्रा तो निश्चित ही पागल कर सकता है। स्पेंसर हों या मिल, ये भी तो एक तरह के पागल ही हैं। नरेंद्र की दिक्कत यह थी कि वे आंशिक रूप से कुछ भी स्वीकार नहीं करते
...more
नरेंद्र से मिलने से पहले परमहंस माँ काली से कहा करते—माँ, किसी एक को तो भेज, जो मेरे प्रामाणिक अनुभवों की प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा कर सके। नरेंद्र ने हिंदू ईश्वरों को मानने से इनकार किया। आरंभ में उसकी अद्वैतवाद से भी पटरी नहीं बैठी। उसने परमहंस से कहा, ‘चाहे लाखों लोग आपको ईश्वर मानते हों, लेकिन मेरा मन जब तक इस बात के लिए राजी नहीं होता, क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह सकूँगा।’ रामकृष्ण ने मुसकराकर कहा, ‘हर वह बात, जो मैं कह रहा हूँ, उसे सिर्फ इसलिए मत मानना कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि तभी उन बातों को स्वीकार करना, जब तुम उन्हें जाँच-परख लो और इत्मीनान कर लो कि वे सही हैं।’ रामकृष्ण नरेंद्र के
...more
विवेकानंद ने स्वयं इस दशा का उल्लेख करते हुए बताया—‘‘नंगे पैर दफ्तर-दर-दफ्तर नौकरी के लिए भटका, लेकिन कोई ठोस बात हाथ नहीं लगी। यह जीवन के यथार्थ से मेरा पहला साक्षात्कार था। मुझे लगा कि जीवन में कमजोर और गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ समय पहले तक जो लोग मेरी मदद करके अपने आपको गौरवान्वित समझते थे, उन सभी ने अपने मुँह फेर लिये। मुझे सारी दुनिया शैतान का घर नजर आने लगी। एक
इसके बाद नरेंद्र सोचने लगा कि ईश्वर ने इतनी बार की उसकी प्रार्थना को अनसुना क्यों कर दिया? यदि वह है तो धरती पर इतनी तकलीफ क्यों है? इतना संत्रास और इतनी पीड़ा क्यों है? फिर उनके दिमाग में पं. ईश्वरचंद्र विद्यासागर (१८२०-९१) की बात कौंधी कि यदि ईश्वर इतना ही दयालु और अच्छा है तो लाखों लोगों को सिर्फ एक निवाले के लिए क्यों मरने देता है? नरेंद्र नास्तिक हो गए।
एक बार रामकृष्ण से किसी ने पूछा, ‘परमहंस, विवाह करना ठीक है या नहीं?’ उन्होंने बाइबल के हवाले से कहा था, ‘जहाँ तक संभव हो, विवाह नहीं करना चाहिए; लेकिन जलने से बेहतर है कि विवाह कर ही लिया जाए। यदि मन इस बात के लिए राजी न हो कि अकेले रहा जाए तो उसे दबाएँ नहीं, विवाह कर लें। विवाह करें, तभी उसकी निस्सारता का पता चलेगा।’ सिर्फ सुनकर पाया गया अनुभव रेडिमेड है।